The Hindi Editorial Analysis- 6th March 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download
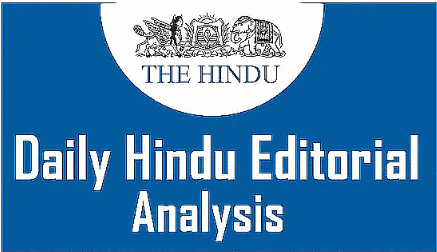
अति-केंद्रीकरण से संघीय स्वास्थ्य नीति को खतरा
चर्चा में क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश में निवास-आधारित आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है।
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या है?
डॉ. तन्वी बहल बनाम श्रेय गोयल (2025) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश के लिए निवास-आधारित आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने प्रवेश प्रक्रिया में राज्य-विशिष्ट कोटा पर योग्यता के महत्व पर जोर दिया।
इस फैसले के परिणामस्वरूप, राज्यों को अब स्नातकोत्तर चिकित्सा कार्यक्रमों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित करने की अनुमति नहीं है। यह निर्णय राज्यों की अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के भीतर चिकित्सा विशेषज्ञों को बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है।
यह फ़ैसला मेडिकल प्रवेश पर केंद्रीय प्राधिकरण को भी मजबूत करता है, लेकिन यह राज्यों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में निवेश करने से हतोत्साहित कर सकता है। इससे स्वास्थ्य सेवा की पहुँच और गुणवत्ता में क्षेत्रीय असमानताएँ बढ़ सकती हैं।
राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना में अधिवास कोटा की भूमिका
- राज्यों के लिए स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली से अच्छी तरह परिचित डॉक्टरों को बनाए रखने के लिए अधिवास-आधारित आरक्षण महत्वपूर्ण है, जिससे चिकित्सा विशेषज्ञों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती है।
- राज्य चिकित्सा शिक्षा में महत्वपूर्ण निवेश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि स्नातक स्थानीय आबादी की सेवा करेंगे, विशेष रूप से स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करते हैं।
- न्यायालय द्वारा पिछले कानूनी मामलों पर निर्भरता, स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की भूमिकाओं के बीच अंतर को स्वीकार करने में विफल रही है।
- अधिवास कोटा के बिना, राज्यों को डॉक्टरों की भर्ती में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्याशित और अकुशल कार्यबल पैदा हो सकता है।
चिकित्सा शिक्षा में राज्य के निवेश पर प्रभाव
- यदि राज्य यह गारंटी देने में असमर्थ हैं कि उनके प्रशिक्षित डॉक्टर वहीं रहेंगे और स्थानीय स्तर पर सेवाएं देंगे, तो वे मेडिकल कॉलेजों में अपने निवेश में कटौती कर सकते हैं।
- जबकि प्रतिस्पर्धी संघवाद राज्यों को अपने चिकित्सा संस्थानों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस प्रोत्साहन को कम कर सकता है।
- स्थानीय आधार पर आरक्षण न होने से मेडिकल कॉलेजों के लिए वित्त पोषण में कमी आ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप बुनियादी ढांचा खराब हो सकता है और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी असमानताएं बढ़ सकती हैं।
चिकित्सा शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंध
- अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के तहत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से जटिल रूप से जुड़ी हुई है।
- राज्य मेडिकल कॉलेज न केवल भावी स्वास्थ्य पेशेवरों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- राज्यों को चिकित्सा शिक्षा को स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के साथ प्रभावी ढंग से संरेखित करने के लिए अपनी प्रवेश नीतियों को निर्धारित करने की स्वायत्तता की आवश्यकता है।
- चिकित्सा शिक्षा पर अत्यधिक केन्द्रीय नियंत्रण राज्यों की अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
सख्त योग्यता-आधारित प्रणाली की समस्याएं
- इस फैसले में NEET-PG जैसी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा खामियों को दूर किए बिना सख्त योग्यता-आधारित प्रणाली की वकालत की गई है।
- एनईईटी-पीजी की अपनी संरचनात्मक समस्याएं हैं, जैसे कि ऐसे उदाहरण जहां नकारात्मक अंक वाले अभ्यर्थी प्रतिशत-आधारित कटऑफ के कारण उत्तीर्ण हो जाते हैं, जिससे योग्यता मूल्यांकन की वैधता के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती हैं।
- रिक्त सीटों को भरने के लिए 2023 में NEET-PG के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रतिशत को शून्य कर दिया जाना, योग्यता मूल्यांकन में विसंगतियों को उजागर करता है, तथा प्रणाली की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।
- पिछले कानूनी निर्णयों में यह माना गया है कि स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अधिक न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए योग्यता में सामाजिक और क्षेत्रीय विचारों को शामिल किया जाना चाहिए, न कि केवल परीक्षा के अंकों पर निर्भर होना चाहिए।
- निवास-आधारित आरक्षण, वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि विशेषज्ञ अपने गृह राज्यों में ही रहें, जिससे संतुलित स्वास्थ्य सेवा वितरण में योगदान मिलता है।
अधिक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता
- न्यायालय का निर्णय पुराने कानूनी उदाहरणों पर आधारित है, जो चिकित्सा विशेषज्ञों की वर्तमान तत्काल मांग को ध्यान में नहीं रखते, विशेष रूप से बढ़ती हुई बीमारी के प्रसार और पिछली स्वास्थ्य आपात स्थितियों के मद्देनजर।
- निवास कोटा को पूरी तरह से समाप्त करने के बजाय, अधिक प्रभावी तरीका यह होगा कि इन आरक्षणों को सेवा दायित्वों के साथ जोड़ दिया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मेडिकल स्नातक आरक्षित सीटों के बदले में निर्दिष्ट अवधि के लिए सार्वजनिक अस्पतालों में सेवा करें।
- कुछ राज्यों ने पहले ही ऐसी नीतियां अपना ली हैं, जहां मेडिकल कार्यक्रमों में आरक्षित सीटों की शर्तों के तहत मेडिकल स्नातकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सेवा करना अनिवार्य है।
- इस फैसले से मेडिकल प्रवेश पर केंद्रीय निगरानी बढ़ गई है, जिसके परिणामस्वरूप मेडिकल शिक्षा में राज्य का निवेश कम हो सकता है तथा स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और गुणवत्ता में व्यापक क्षेत्रीय असमानताएं पैदा हो सकती हैं।
- चिकित्सा शिक्षा नीतियों का अति-केंद्रीकरण स्वास्थ्य देखभाल प्रशासन के संघीय ढांचे को बाधित कर सकता है, तथा प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए आवश्यक सहयोगात्मक दृष्टिकोण को कमजोर कर सकता है।
- एक मजबूत और टिकाऊ स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए एक संतुलित नीति ढांचे की आवश्यकता होती है जो योग्यता-आधारित प्रवेश, राज्य स्वायत्तता और सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने की अनिवार्यता को सुसंगत बनाता हो।
'हिमालय' से कौन माफ़ी मांगेगा?
चर्चा में क्यों?
नॉर्वे ने हाल ही में सामी, केवेन और फ़ॉरेस्ट फ़िन लोगों जैसे स्वदेशी समूहों को आत्मसात करने के उद्देश्य से अपनी पिछली नीतियों के लिए औपचारिक माफ़ी जारी की है। ये नीतियाँ, जिन्हें नॉर्वेजियनाइज़ेशन के नाम से जाना जाता है, 1850 के दशक से 1960 के दशक तक लागू रहीं और इनमें मूल भाषाओं और संस्कृतियों का दमन शामिल था।
- नॉर्वे सरकार ने जारी भेदभाव से निपटने के लिए उपाय प्रस्तावित किए हैं , जिनमें स्वदेशी भाषाओं का संरक्षण और 2027 से शुरू होने वाले समावेशन प्रयासों की निगरानी शामिल है।
- हालाँकि, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें लुप्तप्राय सामी भाषाएँ और स्वास्थ्य देखभाल , शिक्षा और भूमि अधिकारों में असमानताएँ शामिल हैं ।
- इसी प्रकार, हिमालयी क्षेत्र में भी स्वदेशी समुदाय संसाधन दोहन और सांस्कृतिक क्षरण के मुद्दों से जूझ रहे हैं ।
- अफगानिस्तान से पूर्वोत्तर भारत तक 2,500 किलोमीटर तक फैला यह क्षेत्र विभिन्न जातीय समूहों के 52 मिलियन लोगों का घर है ।
- औपनिवेशिक शासन , स्वतंत्रता के बाद की नीतियां और आधुनिक आर्थिक परिवर्तन जैसे ऐतिहासिक कारकों ने इन समुदायों पर आत्मसात करने का दबाव डाला है।
औपनिवेशिक विघटन और स्वतंत्रता के बाद का शोषण
- औपनिवेशिक प्रभाव: ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने हिमालयी व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को काफी हद तक बाधित किया। पूर्वोत्तर में, व्यापार नाकाबंदी और जबरन समझौतों ने चाय, सोना, रेशम और अफीम जैसी वस्तुओं के व्यापार को प्रभावित किया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में, रेलवे निर्माण की सुविधा के लिए लकड़ी के लिए जंगलों का बड़े पैमाने पर दोहन किया गया, जिससे वनों की भारी कटाई हुई।
- स्वतंत्रता के बाद की नीतियाँ: शुरू में, स्वतंत्रता के बाद की नीतियों का उद्देश्य आदिवासी जीवन शैली का सम्मान और संरक्षण करना था। हालाँकि, 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजनाओं तक, संसाधनों के दोहन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और संस्कृतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
आर्थिक बदलाव और जलविद्युत परियोजनाएँ
- 1990 के दशक में आर्थिक परिवर्तन: 1990 के दशक में महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन हुए, जिससे हिमालयी राज्यों को नए राजस्व स्रोतों की तलाश करने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप पर्यटन और जल विद्युत पर निर्भरता बढ़ गई।
- जलविद्युत पहल: जलविद्युत परियोजनाओं को राज्य के राजस्व को बढ़ाने और वित्तीय निर्भरता को कम करने के साधन के रूप में बढ़ावा दिया गया। उदाहरण के लिए, अरुणाचल प्रदेश को इन परियोजनाओं के माध्यम से भारत की बिजली की मांग का एक बड़ा हिस्सा पूरा करने का अनुमान था।
- जलविद्युत परियोजनाओं की चुनौतियाँ: अपने संभावित लाभों के बावजूद, जलविद्युत परियोजनाओं में अक्सर स्थानीय कानूनों और प्रथागत भूमि स्वामित्व की अनदेखी की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप विस्थापन और सांस्कृतिक क्षरण होता है। बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण में नौकरशाहों, राजनेताओं और निगमों की भागीदारी के कारण पर्यावरण का क्षरण हुआ और पारंपरिक प्रथाओं का ह्रास हुआ।
मान्यता और सतत विकास
- मान्यता और न्याय की आवश्यकता: नॉर्वे की माफ़ी ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करने और सुलह के लिए प्रतिबद्ध होने के महत्व को रेखांकित करती है। इसके विपरीत, हिमालयी क्षेत्र को अभी तक संसाधन शोषण और सांस्कृतिक क्षरण के अपने अनुभवों के लिए औपचारिक मान्यता नहीं मिली है।
- सतत विकास: स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हिमालयी क्षेत्र में सतत और समावेशी विकास की सख्त जरूरत है। सवाल यह है कि क्या नॉर्वे द्वारा प्रदर्शित समान जवाबदेही और न्याय हिमालय में प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
|
4 videos|3448 docs|1079 tests
|
FAQs on The Hindi Editorial Analysis- 6th March 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC
| 1. अति-केंद्रीकरण का क्या अर्थ है और यह संघीय स्वास्थ्य नीति को कैसे प्रभावित कर सकता है? |  |
| 2. 'हिमालय' से कौन माफ़ी मांगेगा का संदर्भ क्या है? |  |
| 3. संघीय स्वास्थ्य नीति में अति-केंद्रीकरण के संभावित नुकसान क्या हैं? |  |
| 4. क्या संघीय स्वास्थ्य नीति में सुधार के लिए कोई उपाय प्रस्तावित किए गए हैं? |  |
| 5. अति-केंद्रीकरण के प्रभावों से निपटने के लिए नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है? |  |
















