The Hindi Editorial Analysis- 9th April 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download
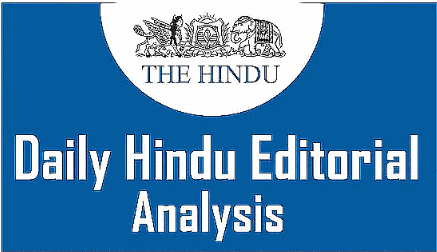
गृह मंत्रालय का क्रमिक परिवर्तन
यह समाचार क्यों है?
भारत में गृह मंत्रालय (एमएचए) एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है, जो एक प्रतिक्रियात्मक संकट प्रबंधन निकाय से एक सक्रिय, सुधार-संचालित संस्था में बदल गया है। इस बदलाव का उद्देश्य कानून प्रवर्तन और राष्ट्रीय स्थिरता के लिए भविष्य के लिए तैयार ढांचा तैयार करना है।
गृह मंत्रालय की बदलती भूमिका
- ऐतिहासिक रूप से, गृह मंत्रालय को "संकट मंत्रालय" के रूप में देखा जाता था, जो दंगों, विद्रोह और राज्यों में शासन की विफलता जैसी घटनाओं के दौरान हस्तक्षेप करता था। इसका मुख्य ध्यान अशांति को रोकने के बजाय उसे प्रबंधित करने पर था।
- वर्तमान बदलाव, अतीत के प्रतिक्रियात्मक रुख से हटकर, संस्थागत सुधारों के माध्यम से एक मजबूत आंतरिक सुरक्षा प्रणाली के निर्माण पर जोर देता है।
आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करें
- गृह मंत्रालय सुरक्षा कानूनों का आधुनिकीकरण कर रहा है, उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है, खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ा रहा है और संस्थानों का पुनर्गठन कर रहा है।
- इस सक्रिय दृष्टिकोण का उद्देश्य केवल मौजूदा खतरों का जवाब देने के बजाय भविष्य के खतरों के लिए तैयारी करना है।
- आंतरिक सुरक्षा और संघीय शासन दोनों के लिए गृह मंत्रालय महत्वपूर्ण है, जिसे अनुच्छेद 355, 256 और 356 जैसे संवैधानिक प्रावधानों का समर्थन प्राप्त है।
ऐतिहासिक चुनौतियाँ और विकास
- आतंकवाद और उग्रवाद जैसे उभरते खतरों से निपटने के लिए 1980 के दशक से आंतरिक सुरक्षा प्राथमिकताएं बदल गई हैं।
- माओवादी हिंसा से प्रभावित कश्मीर, पूर्वोत्तर और मध्य भारत जैसे क्षेत्र सुरक्षा प्रयासों के केन्द्र बिन्दु बने हुए हैं।
- इन मुद्दों के प्रबंधन में राज्य पुलिस बलों के सामने आने वाली चुनौतियों के कारण, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) पर निर्भरता बढ़ गई है।
- उदाहरण के लिए, सीआईएसएफ की स्थापना आंशिक रूप से 1970 और 1980 के दशक के दौरान औद्योगिक अशांति के जवाब में की गई थी।
अतीत में सीमित सुधार
- पहले विधायी कार्य अक्सर प्रतिक्रियात्मक होते थे, जो हमलों या विद्रोह जैसी विशिष्ट घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते थे। आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (टाडा), आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पोटा) और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) जैसे कानून और संस्थाएँ संकट के बाद स्थापित की गईं।
- नेतृत्व में बार-बार परिवर्तन से दीर्घकालिक योजना और सुधार प्रयासों में भी बाधा उत्पन्न हुई।
हालिया सुधार और नई दृष्टि
- 2019 से अब तक राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन को बढ़ाने के लिए 27 से ज़्यादा कानून बनाए गए हैं। इन सुधारों में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और एनआईए अधिनियम जैसे आतंकी कानूनों में संशोधन शामिल हैं, जिनका उद्देश्य आतंकी फंडिंग को रोकना और तकनीक और डेटाबेस का प्रभावी ढंग से उपयोग करना है।
- बहु-एजेंसी दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसे मजबूत कानूनी ढांचे, बेहतर वित्तपोषण और नियमित निष्पादन मूल्यांकन द्वारा समर्थन प्राप्त है।
आपराधिक न्याय का आधुनिकीकरण
- तीन नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं, साथ ही नए फोरेंसिक विज्ञान संस्थानों की स्थापना और बेहतर डिजिटल अपराध ट्रैकिंग प्रणाली भी लागू की गई है।
- न्याय प्रदान करने की दक्षता बढ़ाने के लिए राज्यों को पुलिस जांच को फोरेंसिक कार्य से अलग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
बढ़ी हुई फंडिंग
- गृह मंत्रालय के बजट में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो 2019 में ₹1 लाख करोड़ से बढ़कर 2025 में ₹2.33 लाख करोड़ हो गया है।
- अर्धसैनिक बलों पर खर्च भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जो 2013-14 में ₹38,000 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹97,000 करोड़ हो गया है।
ज़मीनी स्तर पर दिखाई देने वाला प्रभाव
- कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है, तथा कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में भी काफी कमी आई है।
- पूर्वोत्तर में चल रहे शांति प्रयासों और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में एकीकृत सुरक्षा-विकास रणनीतियों से सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं।
निष्कर्ष
गृह मंत्रालय एक प्रतिक्रियात्मक भूमिका से एक सक्रिय, सुधार-उन्मुख संस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसका ध्यान एक मजबूत आंतरिक सुरक्षा ढांचा बनाने पर है। संरचनात्मक सुधारों और रणनीतिक शासन के माध्यम से, गृह मंत्रालय का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत भविष्य की चुनौतियों के लिए अच्छी तरह से तैयार हो।
अभ्यास प्रश्न: चर्चा करें कि गृह मंत्रालय के एक संकट-प्रतिक्रिया निकाय से एक सुधार-उन्मुख संस्था में परिवर्तन ने भारत के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य को कैसे प्रभावित किया है। (150 शब्द / 10 अंक)
न्यायिक आदेशों के प्रवर्तन को सुदृढ़ बनाना
यह समाचार क्यों है?
- जयपुर में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा रात्रि में एयर हॉर्न के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद, इसका क्रियान्वयन कमजोर बना हुआ है, जिससे निवासियों को लगातार शोर से परेशानी हो रही है।
कार्यवाही योग्य न्यायिक आदेशों का महत्व
- न्यायिक आदेशों में ऐसी रणनीतियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करें, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो और जनता की संतुष्टि बढ़े।
- व्यावहारिक और परिणाम-उन्मुख आदेशों में सार्थक परिवर्तन लाने की क्षमता होती है।
- इसका एक सकारात्मक उदाहरण नेपाल के काठमांडू में देखने को मिलता है, जहां सख्त प्रवर्तन और जन जागरूकता पहलों के कारण ध्वनि प्रदूषण में काफी कमी आई है।
- प्रवर्तन न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू है, न कि केवल एक औपचारिकता।
- कमजोर प्रवर्तन से शासन व्यवस्था कमजोर होती है और न्यायपालिका में जनता का विश्वास कम होता है।
प्रवर्तन में चुनौतियाँ
- प्रवर्तन एजेंसियां अक्सर उन आदेशों को नजरअंदाज कर देती हैं जिन्हें वे "मामूली" मानती हैं, जिससे न्यायिक निर्णयों और वास्तविक दुनिया में कार्यान्वयन के बीच दूरी पैदा हो जाती है।
- न्यायालयों को आदेश जारी करते समय प्रवर्तन चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने तथा मजबूत एवं व्यावहारिक कार्यान्वयन ढांचे स्थापित करने की आवश्यकता है।
- विगत में प्रवर्तन विफलताएं खराब योजनाबद्ध आदेशों के कारण हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप देरी हुई और परिणाम अप्रभावी रहे।
कानूनी प्रावधान और उनकी सीमाएँ
- भारतीय कानून, सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 38 और आदेश 21 के माध्यम से, अदालती आदेशों के क्रियान्वयन के लिए तंत्र प्रदान करता है।
- इसके बावजूद, प्रवर्तन को डिक्री की वैधता पर संदेह और न्यायिक कदाचार के उदाहरणों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
सफल प्रवर्तन के उदाहरण
- स्पष्ट दिशा-निर्देशों, सख्त निगरानी और व्यवस्थित निरीक्षण के कारण कुछ अदालती आदेशों को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।
- उदाहरण के लिए, एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय के माध्यम से हरित पट्टी की स्थापना और नियमित वायु गुणवत्ता निगरानी को लागू किया गया।
- ये मामले प्रभावी प्रवर्तन के लिए विस्तृत निर्देशों और सतत निगरानी के महत्व को उजागर करते हैं।
सख्त प्रवर्तन के लिए सिफारिशें
- प्रत्येक सरकारी विभाग को न्यायालय के आदेशों को क्रियान्वित करने तथा नियमित अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करना चाहिए।
- प्रासंगिक एजेंसियों को विशिष्ट न्यायिक आदेशों से जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाना चाहिए, ताकि न्यायालय को समय पर रिपोर्ट करना सुनिश्चित हो सके।
- अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक प्रवर्तन उपकरण, पारदर्शिता और उचित सूचना साझाकरण महत्वपूर्ण हैं।
- न्यायालय के आदेशों को वास्तविक दुनिया में कार्रवाई में बदलने के लिए जवाबदेही तंत्र और जन भागीदारी महत्वपूर्ण है।
अभ्यास प्रश्न: कमजोर संस्थागत प्रवर्तन तंत्रों के मद्देनजर न्यायपालिका अपने पर्यावरण निर्देशों का बेहतर अनुपालन कैसे सुनिश्चित कर सकती है? (250 शब्द /15 अंक)
|
7 videos|3454 docs|1081 tests
|
FAQs on The Hindi Editorial Analysis- 9th April 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC
| 1. गृह मंत्रालय के क्रमिक परिवर्तन का क्या महत्व है? |  |
| 2. न्यायिक आदेशों के प्रवर्तन को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं? |  |
| 3. गृह मंत्रालय के कार्यों में न्यायिक आदेशों का प्रवर्तन कैसे शामिल होता है? |  |
| 4. क्या न्यायिक आदेशों के प्रवर्तन में तकनीकी नवाचारों का उपयोग किया जा सकता है? |  |
| 5. गृह मंत्रालय में सुधारों की प्रक्रिया कैसे संचालित होती है? |  |





















