The Hindi Editorial Analysis- 9th June 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download
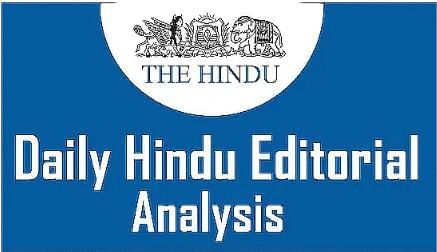
परामर्शी विनियमन-निर्माण को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए
चर्चा में क्यों?
आरबीआई और सेबी ने प्रारंभिक कदम उठाए हैं, लेकिन संसद के लिए यह आवश्यक है कि वह एक ऐसा कानून बनाने पर विचार करे जो विनियमन बनाने के लिए स्पष्ट और मानकीकृत प्रक्रियाएं स्थापित करे।
परिचय
मई 2023 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विनियमन, दिशा-निर्देश और अधिसूचनाएँ जारी करने के लिए एक स्पष्ट नीति की रूपरेखा तैयार की। इसके बाद फरवरी 2023 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने भी इसी तरह की पहल की, जहाँ उसने अपनी नियामक प्रक्रियाओं का विवरण देते हुए नियम प्रकाशित किए।
विनियमन निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना
संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित आरबीआई और सेबी जैसे विनियामकों के पास अर्ध-विधायी शक्तियां हैं। इसलिए, कानून के शासन को बनाए रखने के लिए मजबूत प्रक्रियात्मक सुरक्षा और जांच होना महत्वपूर्ण है। हाल ही में, आरबीआई और सेबी दोनों ने कानून बनाने के चरणों की रूपरेखा तैयार करने वाले ढांचे पेश किए, जो एक सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है।
- आरबीआई का नया दृष्टिकोण: आरबीआई अब नए नियमों या परिवर्तनों का प्रस्ताव करते समय प्रभाव विश्लेषण करेगा।
- सेबी की स्पष्टता: सेबी अपने प्रस्तावों के पीछे नियामक इरादे और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बताएगा।
- सार्वजनिक भागीदारी: दोनों नियामक अपने प्रस्तावों पर 21 दिनों तक सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित करेंगे।
- आवधिक समीक्षा: वे अपने मौजूदा विनियमों की भी आवधिक समीक्षा करेंगे।
- आगे बढ़ना: इन सकारात्मक बदलावों के बावजूद, सुधार की गुंजाइश है। विनियामकों को अपने निर्णयों के पीछे आर्थिक कारणों को स्पष्ट करने और नियमित समीक्षा और सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्रतिक्रियाओं के लिए जवाबदेही तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
बाजार की विफलता का मुद्दा
आरबीआई और सेबी को अपने नए नियमों को स्पष्ट आर्थिक तर्क पर आधारित करना चाहिए, जिसमें उस विशिष्ट समस्या या बाजार विफलता की पहचान की जानी चाहिए जिसे नियम संबोधित करना चाहते हैं। वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC) ने 2013 में इस बात पर जोर दिया था कि कानूनों को केवल प्रक्रियात्मक लक्ष्यों के बजाय उनके आर्थिक उद्देश्य से परिभाषित किया जाना चाहिए। कई अन्य देश मजबूत नियामक प्रथाओं का पालन करते हैं जिनसे भारत सीख सकता है।
- वर्तमान अंतराल: आरबीआई "आर्थिक वातावरण" के आधार पर "प्रभाव विश्लेषण" पर चर्चा करता है, और सेबी अपने उद्देश्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। हालांकि, किसी भी प्रस्तावित विनियमन के पीछे आर्थिक कारण या बाजार की विफलता को स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है।
- इसके विपरीत, आईएफएससीए ढांचे में संबोधित किए जा रहे मुद्दे का स्पष्ट विवरण अनिवार्य किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएँ बनाम भारतीय रूपरेखाएँ
देश / प्राधिकरण | विनियामक अभ्यास |
|---|---|
संयुक्त राज्य अमेरिका | लागत-लाभ विश्लेषण करना होगा, समाज पर न्यूनतम बोझ सुनिश्चित करना होगा तथा विकल्पों का आकलन करना होगा। |
यूरोपीय संघ | बेहतर विनियमन ढांचे के अंतर्गत: समस्या को परिभाषित करना होगा, समाधान सुझाना होगा, तथा मूल्यांकन विधियों की व्याख्या करनी होगी। |
आईएफएससीए (भारत) | उस मुद्दे का उल्लेख करना आवश्यक है जिसे विनियमन संबोधित करना चाहता है। |
आरबीआई (भारत) | इसमें प्रभाव विश्लेषण की आवश्यकता होती है, लेकिन आर्थिक औचित्य की व्याख्या अनिवार्य नहीं होती। |
सेबी (भारत) | उद्देश्यों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि अंतर्निहित बाजार विफलता का उल्लेख हो। |
भारत में वित्तीय नियामकों को क्या करना चाहिए?
- बाजार की विफलता की पहचान करें: उस मूल मुद्दे या बाजार की विफलता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें जिसके लिए विनियमन आवश्यक है।
- प्रस्तावित समाधान की व्याख्या करें: विस्तार से बताएं कि विनियमन का उद्देश्य पहचानी गई समस्या का समाधान कैसे करना है।
- लागत-लाभ विश्लेषण करें: विनियमन के संभावित लाभों और कमियों का आकलन करें।
- निगरानी योजना विकसित करें: कार्यान्वयन के बाद विनियमन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए तंत्र स्थापित करें।
परामर्शी विनियमन-निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार
वर्तमान चुनौतियाँ
- भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी जैसे भारतीय नियामकों का परामर्श आधारित नियम-निर्माण में खराब रिकॉर्ड है।
- जून 2014 से जुलाई 2015 तक के एक अध्ययन में पाया गया कि आरबीआई ने अपने केवल 2.4% परिपत्रों पर ही सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी थीं, तथा सेबी ने अपने आधे से भी कम विनियमों पर सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए थे।
- इससे पता चलता है कि हितधारकों को नये नियमों पर प्रतिक्रिया देने के लिए सीमित अवसर मिले हैं।
- यद्यपि सुधार की आशा है, फिर भी नियामकों को अपनी परामर्श प्रक्रियाओं के संबंध में पारदर्शिता बढ़ाने की आवश्यकता है।
सुझाए गए पारदर्शिता उपाय (वार्षिक रूप से रिपोर्ट किए गए)
- जवाबदेही में सुधार के लिए, नियामकों को निम्नलिखित प्रकाशित करना चाहिए:
- सार्वजनिक परामर्शों की कुल संख्या बनाम विनियमों या संशोधनों की कुल संख्या।
- प्राप्त प्रतिक्रियाओं की संख्या.
- स्वीकृत एवं अस्वीकृत सुझावों का विवरण।
- प्रत्येक सुझाव को स्वीकार या अस्वीकार करने के कारण।
- विनियमन के अंतिम संस्करण पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया का प्रभाव।
- सभी संबद्ध समयसीमाएं, जैसे कि परामर्श कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ।
- सेबी कभी-कभी बोर्ड मीटिंग के एजेंडे में ऐसे डेटा को शामिल करता है, लेकिन अक्सर गोपनीयता का हवाला देते हुए सार्वजनिक टिप्पणी सारांश को हटा देता है।
नियमित समीक्षा का महत्व
- आरबीआई और सेबी दोनों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे अपने नियमों की कितनी बार समीक्षा करेंगे।
- यह सरकार की विनियमन-मुक्ति के प्रति प्रतिबद्धता तथा नियमों के प्रासंगिक बने रहने की आवश्यकता को देखते हुए महत्वपूर्ण है।
- इसके विपरीत, आईएफएससीए प्रत्येक विनियमन की हर तीन साल में समीक्षा अनिवार्य करता है, जो एक मजबूत समीक्षा पद्धति को प्रदर्शित करता है।
भारतीय विनियामकों के लिए अनुशंसित समीक्षा अभ्यास
रेगुलेटर | वर्तमान अभ्यास | सुझाए गए सुधार |
|---|---|---|
भारतीय रिजर्व बैंक | कोई निश्चित समीक्षा अंतराल नहीं | नियमित समीक्षा के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करें |
अपने आप को | कोई नियमित कार्यक्रम नहीं | प्रत्येक विनियमन के लक्ष्यों से जुड़ी समीक्षा आवृत्ति निर्धारित करें |
आईएफएससीए | हर 3 साल में समीक्षा करें | पहले से ही सर्वोत्तम अभ्यास का पालन करता है |
सुझाव:
- पूर्व-निर्धारित और लगातार अंतराल पर, नियामकों को निम्नलिखित का मूल्यांकन करना होगा:
- क्या विनियम अपेक्षित रूप से काम कर रहे हैं, और क्या उनकी अभी भी आवश्यकता है या उन्हें अद्यतन करने की आवश्यकता है।
इससे भारतीय वित्तीय विनियमन की प्रतिक्रियाशीलता, साक्ष्य-आधारित प्रकृति और जन-मैत्री बढ़ेगी।
निष्कर्ष
अच्छे विनियामक अभ्यास के लिए किसी भी नए नियम के लिए स्पष्ट और मजबूत कारण की आवश्यकता होती है। आरबीआई और सेबी ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि, एक बड़ी चुनौती विनियामक प्रभाव आकलन करने और परामर्श आयोजित करने की सरकार की सीमित क्षमता है।
- इसके अलावा, अलग-अलग विनियामकों द्वारा किए गए छोटे-छोटे परिवर्तन हर जगह अच्छे विनियामक मानक बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते।
- संसद संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम जैसा कानून पारित करने के बारे में सोच सकती है, जो नियम बनाने के लिए मानक प्रक्रियाएं निर्धारित करता है।
- इस कानून में प्रभाव विश्लेषण, सार्वजनिक परामर्श और नियमित समीक्षा जैसे कदम शामिल होंगे।
- यूनाइटेड किंगडम और कनाडा जैसे देशों ने सरकारी एजेंसियों द्वारा नियम बनाने के लिए पहले ही ऐसे दिशानिर्देश बना लिए हैं।
- भारत में भी ऐसी ही प्रणाली अपनाने से सभी नियामक अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेंगे।
भावनाओं के प्रति न्यायिक संवेदनशीलता प्रतिगमन का संकेत है, चर्चा में क्यों?
भारत में न्यायपालिका लोगों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा रही है।
परिचय
आज, भारतीय न्यायालय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर रहे हैं - वे इसे नियंत्रित कर रहे हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) की वास्तविक भावना के विरुद्ध है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को - भले ही वह भड़काऊ या असुविधाजनक हो - सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ नागरिक की सुरक्षा के रूप में देखता है, न कि ऐसी चीज जिससे डरना या प्रतिबंधित होना चाहिए।
न्यायपालिका और स्वतंत्र अभिव्यक्ति: भूमिका में बदलाव
- न्यायपालिका, जिसे कभी बहुसंख्यकवादी सत्ता के विरुद्ध रक्षक के रूप में देखा जाता था, अब अक्सर विनम्रता के संरक्षक की तरह कार्य करती है, तथा शिष्टाचार, राष्ट्रीय गौरव या संवेदनशीलता के नाम पर क्षमा याचना करने को कहती है।
- जब अदालतें केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करती हैं कि क्या कहा गया, बजाय इसके कि कहने का अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, तो वे स्वतंत्र अभिव्यक्ति को कमजोर करती हैं और देश को भावनात्मक आक्रोश और सार्वजनिक दबाव के प्रति संवेदनशील बना देती हैं।
एक 24 वर्षीय व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ऑपरेशन सिंदूर के बाद मई 2025 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध विराम के बाद प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की।
- क्या यह पोस्ट खराब स्वाद वाली थी? हो सकता है। लेकिन "स्वाद" कोई संवैधानिक नियम नहीं है।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एफआईआर रद्द करने की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि "भावनाएं इस हद तक नहीं बह सकतीं कि राष्ट्रीय नेताओं की बदनामी हो।"
यह तर्क हमारे संविधान के मूल विचार को उलट देता है: नागरिक का उद्देश्य राज्य के प्रति जवाबदेह होना है, न कि एक बच्चे की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए जिसे बहुत अधिक बोलने के लिए दंडित किया जाता है।
अधिकारों की रक्षा से लेकर भावनाओं के प्रबंधन तक के बदलाव से मुक्त अभिव्यक्ति के अधिकार के बजाय विशेषाधिकार में बदलने का खतरा है।
अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मुक्त भाषण की व्याख्या में न्यायिक बदलाव
- पारंपरिक व्याख्या: अनुच्छेद 19(1)(ए) का उद्देश्य भाषण पर राज्य की शक्ति को सीमित करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना था।
- हालिया प्रवृत्ति: ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय अब इस अधिकार को सशर्त लाइसेंस के रूप में मानते हैं, जहां भाषण का मूल्यांकन व्यवहार मानकों के माध्यम से किया जाता है, जिन्हें अक्सर कानून में संहिताबद्ध नहीं किया जाता है।
- ये स्थितियाँ अब उकसावे या मानहानि जैसी कानूनी सीमाओं के बजाय कथित गरिमा, राष्ट्रीय भावना या सार्वजनिक आक्रोश द्वारा परिभाषित होती हैं।
इस बदलाव को दर्शाने वाले केस स्टडीज़
मामला | अभिव्यक्ति की प्रकृति | न्यायिक प्रतिक्रिया | मुख्य चिंता |
|---|---|---|---|
कमल हासन और "ठग लाइफ" टिप्पणी | कन्नड़ को "तमिल की बेटी" कहा गया | कर्नाटक हाईकोर्ट ने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माफी मांगने की सलाह दी | वैधानिकता के बारे में नहीं बल्कि कथित अपराध को शांत करने के बारे में |
रणवीर इलाहाबादिया पॉडकास्ट केस | स्पष्ट/अश्लील भाषा का प्रयोग | न्यायालय ने केंद्र से पूछा कि क्या इस तरह के भाषण को संरक्षण प्राप्त है? | स्वाद/विनम्रता पर ध्यान केन्द्रित करें, उकसावे पर नहीं |
प्रो. अली खान महमूदाबाद | भारत के युद्धकालीन मीडिया दृष्टिकोण की आलोचना | "भावनाओं को ठेस पहुँचाने" के आरोप में न्यायिक कार्यवाही शुरू की गई | अकादमिक आलोचना की डॉग व्हिसल जांच की गई |
खतरनाक मिसालें कायम की जा रही हैं
- वैध भाषण के लिए माफ़ी मांगने वाली अदालतें: भीड़ के आक्रोश या बहुसंख्यकवादी भावना को वैध कानूनी मानक के रूप में वैधता प्रदान करती हैं। लोकप्रिय अस्वीकृति से संवैधानिक संरक्षण के सिद्धांत को कमजोर करती हैं।
- अपराध, स्वाद या भावना जैसी व्यक्तिपरक सीमाएँ: स्पष्ट कानूनी मानकों को भावनात्मक मानदंडों से बदलें। अपराध का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को न्यायिक कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दें।
व्यापक निहितार्थ
- सांस्कृतिक पुलिसिंग का न्यायिक समर्थन: आत्म-सेंसरशिप को बढ़ावा देता है। न्यायालयों को स्वतंत्रता के रक्षक के बजाय सामाजिक शिष्टाचार के मध्यस्थ में बदल देता है।
- अभिव्यक्ति को वैधता के बजाय स्वीकार्यता के आधार पर आंका जाता है: यह उस मूल विचार का उल्लंघन करता है कि मुक्त भाषण केवल अलोकप्रिय विचारों की रक्षा के लिए मौजूद है। भावनाओं को ठेस पहुँचाना अब एक कानूनी सीमा है: न्यायालयों के ऐसे मंचों में बदलने का जोखिम है जो स्वतंत्रता को बनाए रखने के बजाय नाजुकता को मान्य करते हैं।
ग़लत व्याख्या
1. भावनात्मक प्रतिक्रिया ≠ कानूनी नुकसान
- उभरता पैटर्न: अदालतें भावनात्मक संकट या अपराध को कानूनी रूप से कार्रवाई योग्य नुकसान के बराबर मान रही हैं।
- संवैधानिक ग़लत व्याख्या: अनुच्छेद 19(2) केवल विशिष्ट आधारों पर प्रतिबंधों की अनुमति देता है: सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, मानहानि, अपराध के लिए उकसाना, आदि। केवल क्रोध या अपराध प्रतिबंध के लिए वैध आधार नहीं है।
- लोकतांत्रिक जोखिम: लोकतंत्र असहमति और असंतोष पर पनपता है। भावनात्मक कारणों पर न्यायिक निगरानी संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर करती है।
2. मुकदमेबाजी की रणनीति के रूप में आक्रोश
- क्षमा याचना के लिए न्यायिक प्रोत्साहन या नैतिक पुलिसिंग: एक खतरनाक प्रोत्साहन संरचना स्थापित करती है: अधिक आक्रोश → अधिक मुकदमेबाजी।
- प्रभाव: भीड़, ट्रोल और सिलसिलेवार मुकदमेबाज़ों को बढ़ावा देता है। भाषण पर नकारात्मक प्रभाव: कानूनी लड़ाई में घसीटे जाने के डर से आलोचनात्मक टिप्पणी करने से रोकता है।
उदाहरणात्मक केस उदाहरण
मामला | मुद्दा | न्यायिक प्रतिक्रिया | चिंता |
|---|---|---|---|
राहुल गांधी – सेना का अपमान | सेना के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी | इलाहाबाद हाईकोर्ट: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सेना को बदनाम करना शामिल नहीं है | सार्वजनिक संस्थाओं को लोकतांत्रिक आलोचना से बचाने का जोखिम |
प्रधानमंत्री पर 'कायरतापूर्ण' टिप्पणी | सैन्य गतिरोध के बाद व्यंग्यात्मक आलोचना | बीएनएस धारा 152 और 353(2) के तहत एफआईआर की अनुमति | व्यंग्य को राजद्रोह जैसा अपराध माना गया |
एफआईआर रद्द करने से इनकार करने का रुझान | शीघ्र बर्खास्तगी की मांग | न्यायालय ने पूर्ण पुलिस प्रक्रिया की अनुमति देते हुए इनकार कर दिया | दोषसिद्धि के बिना भी प्रक्रिया सज़ा बन जाती है |
मद्रास हाईकोर्ट के अपवाद | कभी-कभी अतिक्रमण का विरोध करता है | कथात्मक सुधार प्रदान करता है, संरचनात्मक सुरक्षा नहीं | सुसंगत भाषण-सुरक्षात्मक न्यायशास्त्र का अभाव |
न्यायिक अतिक्रमण और इसकी संरचनात्मक खामियां
- क्षमायाचना न्यायिक रूप से बाध्यकारी हो गई है: न्यायालय स्वीकारोक्ति कक्षों के समान हो गए हैं, जहां वाणी का मूल्यांकन पश्चाताप के आधार पर किया जाता है, तर्क के आधार पर नहीं।
- मनोवैज्ञानिक और कानूनी दबाव: सम्मन, एफआईआर और जांच, बिना दोषसिद्धि के भी असहमति पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
- सिद्धांत-केंद्रित मुक्त भाषण को सुदृढ़ करना: प्रतिबंध के लिए संवैधानिक सीमाओं की रक्षा के लिए वर्तमान प्रवृत्तियों में सुधार की आवश्यकता है (अनुच्छेद 19(2))।
नागरिकों के लिए संकेत
- राजद्रोह और सार्वजनिक व्यवस्था में परिवर्तन जैसे अस्पष्ट कानूनों की व्याख्या स्वतंत्रता के प्रति पूर्वाग्रह के साथ की जानी चाहिए।
- यद्यपि भारतीय न्यायालयों में ‘शीत प्रभाव’ सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है, लेकिन इसे संस्थागत साहस के साथ शायद ही कभी लागू किया जाता है।
- यह मुद्दा आम नागरिकों को प्रभावित करता है:
- यूट्यूबर्स को चुटकुले सुनाने के लिए कहा गया है।
- प्रोफेसरों को ट्वीट के लिए अदालत में घसीटा गया।
- फिल्म निर्माताओं को सांस्कृतिक या भाषाई गौरव के लिए माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
निष्कर्ष
- न्यायाधीश संविधान के संरक्षक हैं, सांस्कृतिक सुविधा के प्रवर्तक नहीं। उनकी भूमिका बोलने की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, श्रोताओं को शांत करना नहीं।
- जब न्यायालय भावनाओं के नाम पर बोलने पर रोक लगाते हैं, तो स्वतंत्रता चुपचाप खत्म हो जाती है। यह बढ़ती संवेदनशीलता सद्भाव को एकरूपता और सम्मान को संयम के साथ भ्रमित करती है।
- माफ़ी मांगना कभी भी कानूनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, न ही किसी भाषण को वैध होने के लिए मान्यता की ज़रूरत होनी चाहिए। भारत का गणतंत्र विरोध से पैदा हुआ है, विनम्रता से नहीं।
- जैसा कि डॉ. बीआर अंबेडकर ने कहा था, दुनिया उन लोगों की बहुत आभारी है जिन्होंने सत्ता को चुनौती देने का साहस किया। हमारी न्यायपालिका को बोलने के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए - खासकर तब जब यह अलोकप्रिय हो।
|
3421 docs|1074 tests
|
FAQs on The Hindi Editorial Analysis- 9th June 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC
| 1. परामर्शी विनियमन-निर्माण का क्या अर्थ है और यह क्यों महत्वपूर्ण है ? |  |
| 2. परामर्शी विनियमन-निर्माण में शामिल मुख्य हितधारक कौन हैं ? |  |
| 3. परामर्शी विनियमन-निर्माण की प्रक्रिया में आमतौर पर कौन से चरण शामिल होते हैं ? |  |
| 4. परामर्शी विनियमन-निर्माण के लाभ क्या हैं ? |  |
| 5. क्या परामर्शी विनियमन-निर्माण के लिए कोई विशेष कानूनी ढांचा आवश्यक है ? |  |





















