The Hindu Editorial Analysis- 7th February 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download
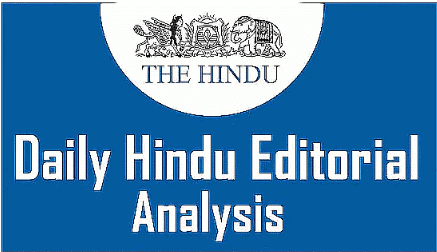
भारत के ताप विद्युत उत्सर्जन को विनियमित करने की गाथा
चर्चा में क्यों?
दिसंबर 2024 में, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने थर्मल पावर प्लांट्स को सख़्त सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने के लिए तीन साल का विस्तार देने की घोषणा की। यह निर्णय लगभग 20 गीगावाट (GW) थर्मल प्लांट्स को प्रभावित करता है, विशेष रूप से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित।
उत्सर्जन मानदंडों पर पृष्ठभूमि
- 2015 में, MoEFCC ने सार्वजनिक परामर्श के बाद थर्मल पावर प्लांट के लिए सख्त उत्सर्जन मानक पेश किए। इन मानकों का उद्देश्य पार्टिकुलेट मैटर को कम करना था और पहली बार SO2 उत्सर्जन पर सीमाएँ निर्धारित की गईं, जिससे भारत के नियम ऑस्ट्रेलिया, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के नियमों के अनुरूप हो गए।
- प्रारंभ में, सभी ताप विद्युत संयंत्रों से दिसंबर 2017 तक इन मानदंडों को पूरा करने की अपेक्षा की गई थी। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में इनके कार्यान्वयन में कई बार देरी हुई है।
विस्तार के कारण
- SO2 उत्सर्जन के लिए हाल ही में 31 दिसंबर, 2027 तक का विस्तार बिना किसी विशेष औचित्य के किया गया था, जिससे इन मानदंडों के कार्यान्वयन में देरी की प्रवृत्ति जारी रही। यह एक दशक से चल रही प्रक्रिया में एक और झटका है।
- अनुपालन के बारे में बहस समय के साथ बदल गई है। जबकि भारतीय कोयले में आमतौर पर सल्फर की मात्रा कम होती है, जिससे SO2 मानकों को पूरा करना आसान हो जाता है, चर्चाएँ फ़्लू गैस डिसल्फ़राइज़ेशन (FGD) तकनीक के इस्तेमाल की चुनौतियों पर केंद्रित रही हैं, जिसे उत्सर्जन से सल्फर को हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, विशेष रूप से उच्च-सल्फर कोयले से।
- एफजीडी को कभी भी अनिवार्य नहीं बनाया गया, लेकिन उनकी उच्च लागत, लंबी स्थापना अवधि और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी मुद्दों के बारे में चिंताएं चर्चाओं के केंद्र में रहीं।
बदलते परिप्रेक्ष्य और रिपोर्ट
- 2020 और 2021 के बीच, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने उत्सर्जन मानदंडों की एकरूपता पर सवाल उठाए और समय सीमा को 2035 तक बढ़ाने का सुझाव दिया।
- वर्ष 2022 में, आईआईटी दिल्ली द्वारा किए गए एक अध्ययन में एफजीडी के वायु गुणवत्ता संबंधी लाभों को स्वीकार किया गया, लेकिन उच्च लागत और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में संभावित वृद्धि के कारण उनके कार्यान्वयन में देरी की सिफारिश की गई।
- नीति आयोग और सीएसआईआर-नीरी द्वारा 2024 में किए गए एक अध्ययन में तर्क दिया गया है कि वायु गुणवत्ता के लिए SO2 मानदंड, पार्टिकुलेट मैटर मानदंडों की तुलना में कम महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय निहितार्थ
कई थर्मल प्लांट ने FGD के लिए अनुबंध शुरू कर दिए हैं, लेकिन संशोधित समयसीमा को पूरा करने के लिए पर्याप्त तेज़ी से प्रगति नहीं कर रहे हैं। बिजली नियामकों ने इन संयंत्रों को FGD की लागत उपभोक्ताओं पर डालने की अनुमति दी है, भले ही संयंत्र उत्सर्जन मानकों को पूरा करने में विफल रहे हों।
इस समय:
- 22 गीगावाट ताप विद्युत संयंत्रों में एफजीडी सफलतापूर्वक स्थापित कर दी गई है।
- 102 गीगावाट, जो भारत की ताप विद्युत क्षमता का लगभग 50% है, एफजीडी स्थापना के उन्नत चरणों में है।
हालांकि, विस्तारित समयसीमा के साथ, कई संयंत्र लागत बचाने के लिए FGD का उपयोग न करने का विकल्प चुन सकते हैं। इससे निम्न परिणाम हो सकते हैं:
- उपभोक्ता अप्रयुक्त FGD उपकरण के लिए भुगतान कर रहे हैं।
- आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में कम से कम अगले तीन वर्षों तक कोई सुधार नहीं होगा।
दीर्घकालिक परिणाम
SO₂ मानदंडों को लागू करने में देरी के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और वित्तीय निहितार्थ हैं। इस बारे में अनिश्चितता है कि क्या भारत इन देरी से सीख लेगा और भविष्य में अपनी प्रदूषण नियंत्रण नीतियों को बेहतर बनाएगा।
निष्कर्ष
SO2 उत्सर्जन मानदंडों का बार-बार विस्तार नियामक अक्षमताओं और उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ को उजागर करता है। ये देरी न केवल पर्यावरणीय जोखिम बढ़ाती है बल्कि प्रदूषण नियंत्रण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के बारे में भी चिंताएँ पैदा करती है।
क्या भारत को एक संप्रभु, आधारभूत एआई मॉडल का निर्माण करना चाहिए?
चर्चा में क्यों?
डीपसीक, एक नया कम लागत वाला आधारभूत एआई मॉडल, ने संप्रभुता, लागत और रणनीतिक उद्देश्यों जैसे कारकों पर विचार करते हुए भारत की अपनी स्वयं की एआई मॉडल बनाने की क्षमता के बारे में चर्चा को बढ़ावा दिया है।
भारत को एआई मॉडल क्यों बनाना चाहिए?
- भारत के लिए अपनी विशेषज्ञता और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आधारभूत एआई मॉडल विकसित करना महत्वपूर्ण है।
- ऐसे कुशल व्यक्तियों का होना आवश्यक है जो एआई मॉडल पर आधारित अनुप्रयोगों का निर्माण, सुधार और विकास कर सकें।
- चिप्स और सॉफ्टवेयर जैसी एआई-संबंधित प्रौद्योगिकियों पर प्रतिबंध भारत की एआई प्रगति में बाधा बन सकते हैं।
- ओपन-सोर्स एआई मॉडल उपलब्ध हैं, जिससे भारत को बिना शुरुआत किए उन्हें संशोधित करने और उपयोग करने में सुविधा होगी।
क्या संप्रभुता एक बड़ी चिंता है?
- जबकि कुछ लोग तर्क देते हैं कि संप्रभुता को एआई मॉडल के विकास को आगे बढ़ाना चाहिए, अन्य लोगों का मानना है कि भारत प्रभावी रूप से ओपन-सोर्स मॉडल को अपना सकता है।
- एआई की प्रगति परिष्कृत चिप्स पर निर्भर करती है, जिसका भारत वर्तमान में उत्पादन नहीं करता है।
- एआई प्रौद्योगिकी पर वैश्विक प्रतिबंध की स्थिति में, भारत अभी भी ओपन-सोर्स एआई मॉडल का लाभ उठा सकता है।
एआई मॉडल विकसित करने की वित्तीय चुनौतियाँ
- उच्च गुणवत्ता वाला एआई मॉडल बनाना अत्यधिक महंगा है, जिसके लिए अक्सर करोड़ों डॉलर की आवश्यकता होती है।
- यहां तक कि बजट-अनुकूल एआई मॉडल के लिए भी प्रशिक्षण और वेतन एवं बुनियादी ढांचे सहित चल रहे खर्चों के लिए लाखों की आवश्यकता होती है।
- भारत का एआई बाज़ार अन्य देशों की तुलना में छोटा है, जिससे निवेश की वसूली करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- भारतीय व्यवसाय केवल घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मुख्य रूप से वैश्विक बाजारों की सेवा करते हैं।
एआई विकास में सरकार की भूमिका
- सरकार ने GPU क्लस्टर जैसे AI संसाधनों को कम लागत पर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है।
- यह पहल एआई प्रशिक्षण को अधिक किफायती बनाकर स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को सहायता प्रदान कर सकती है।
- हालाँकि, प्रमुख प्रौद्योगिकी कम्पनियाँ एआई में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं, जबकि भारत के संसाधन अपेक्षाकृत सीमित हैं।
भारत को अपने एआई प्रयासों पर कहां ध्यान केंद्रित करना चाहिए?
- विश्व स्तर पर सबसे बड़े एआई मॉडलों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करने के बजाय, भारत को लक्षित एआई समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- एआई विकास को भारतीय भाषा प्रसंस्करण और वाक् पहचान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- एआई मॉडलों को स्थानीय उपयोग के मामलों के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए, जहां उनका महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।
- प्राथमिक चुनौती भारत के अनुसंधान वातावरण को बढ़ाना और निजी निवेश को आकर्षित करना है।
निष्कर्ष
- भारत को वैश्विक नेताओं के साथ होड़ करने के बजाय रणनीतिक रूप से अपने संसाधनों का आवंटन करना चाहिए और व्यावहारिक एआई अनुप्रयोगों पर जोर देना चाहिए।
- मजबूत अनुसंधान, निवेश और नवाचार द्वारा विशेषता वाले एक मजबूत एआई पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, केवल एक एआई मॉडल बनाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
|
1 videos|3438 docs|1076 tests
|





















