UPSC Daily Current Affairs (Hindi)- 2nd October 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download
GS2/राजनीति
अमेरिका में बंद होने की स्थिति: नई चुनौतियाँ सामने
 समाचार में क्यों है?
समाचार में क्यों है?
अमेरिकी सरकार 1 अक्टूबर 2025 को सुबह 12:01 बजे बंद हो गई—यह सात वर्षों में पहला ऐसा मामला है—क्योंकि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स संघीय धन के मुद्दे पर सहमति नहीं बना सके। इस गतिरोध के कारण हजारों संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा गया है और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में बाधा उत्पन्न हुई है।
मुख्य निष्कर्ष
- शटडाउन का कारण वार्षिक आवंटन विधेयकों को पारित करने में विफलता है।
- आर्थिक परिणामों में महत्वपूर्ण अमेरिकी डेटा रिलीज़ में देरी और बाजार的不确定ता का बढ़ना शामिल है।
- लगभग 750,000 कर्मचारियों के फर्लो पर जाने की उम्मीद है, जिससे दैनिक $400 मिलियन का वेतन नुकसान होगा।
- महत्वपूर्ण सेवाएँ, जैसे कि मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी, शटडाउन के बावजूद काम करना जारी रखेंगी।
अतिरिक्त विवरण
- यूएस सरकारी शटडाउन को क्या प्रेरित करता है: शटडाउन तब होता है जब कांग्रेस आवंटन विधेयकों को पारित करने में विफल रहती है, जो अक्सर एक "ओम्निबस" पैकेज में मिलाए जाते हैं। यदि फंडिंग समाप्त हो जाती है, तो विभिन्न एजेंसियों के लिए उपलब्ध फंडिंग के आधार पर सरकारी कार्य पूरी या आंशिक रूप से रुक सकते हैं।
- शटडाउन के पीछे के कारण: वर्तमान गतिरोध स्वास्थ्य देखभाल सब्सिडी और मेडिकेड में कटौती के लिए धन को लेकर असहमति से उत्पन्न हुआ है, जिसमें डेमोक्रेट पिछले कटौती को उलटने की कोशिश कर रहे हैं जबकि रिपब्लिकन एक साफ धन विस्तार का समर्थन कर रहे हैं।
- शटडाउन का प्रभाव: शटडाउन एंटीडेफिशिएंसी एक्ट के तहत गैर-आवश्यक संघीय कार्यों को सीमित करता है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव और प्रमुख आर्थिक डेटा के रिलीज़ में संभावित देरी हो सकती है।
- यह शटडाउन क्यों भिन्न हो सकता है: पिछले शटडाउन के विपरीत, यह स्थिति ट्रंप के सरकारी दक्षता विभाग की पहलों के कारण दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकती है, जो अस्थायी फर्लो के बजाय स्थायी कार्यबल में कटौती का सुझाव देती है, जिससे दीर्घकालिक कार्यक्रमों में कटौती हो सकती है।
वर्तमान सरकारी शटडाउन महत्वपूर्ण राजनीतिक विभाजन को उजागर करता है और संघीय कर्मचारियों और व्यापक अर्थव्यवस्था दोनों के लिए चुनौतियाँ पैदा करता है। इस शटडाउन के दीर्घकालिक प्रभाव संघीय संचालन और भविष्य की धन रणनीतियों को पुनः आकार देने में मदद कर सकते हैं।
भारत में स्मारक संरक्षण - नीति में बदलाव
 क्यों समाचार में?
क्यों समाचार में?
भारतीय सरकार ने अपने विरासत संरक्षण नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे निजी संस्थाओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के साथ मिलकर स्मारकों के संरक्षण में सहयोग करने की अनुमति मिली है, जो कि राष्ट्रीय संस्कृति निधि के माध्यम से होगा।
- भारत में 3,700 से अधिक संरक्षित स्मारक हैं, जिनका संरक्षण पहले केवल ASI की जिम्मेदारी थी।
- नई नीति स्मारक संरक्षण में निजी भागीदारी को बढ़ावा देती है, जिसका उद्देश्य संरक्षण क्षमता और दक्षता को बढ़ाना है।
- अब निजी खिलाड़ी सीधे संरक्षण परियोजनाओं को वित्तपोषित और प्रबंधित कर सकते हैं, ASI की निगरानी में।
- सार्वजनिक-निजी साझेदारी मॉडल: निजी कंपनियाँ और दाता राष्ट्रीय संस्कृति निधि (NCF) के माध्यम से संरक्षण परियोजनाओं को वित्तपोषित कर सकते हैं और 100% कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।
- पैनल में शामिल संरक्षण आर्किटेक्ट: संस्कृति मंत्रालय योग्य आर्किटेक्ट्स की एक सूची बनाएगा, जिससे दाताओं को अपने परियोजना के लिए आर्किटेक्ट चुनने का अवसर मिलेगा।
- चेक और बैलेंस: ASI निगरानी प्राधिकरण बनाए रखेगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs) को राष्ट्रीय संरक्षण नीति, 2014 के साथ संरेखित करना आवश्यक होगा।
- प्रारंभिक पायलट सूची: नीति कार्यान्वयन के पहले चरण में 250 स्मारकों को निजी भागीदारी के लिए खोला जाएगा।
यह ऐतिहासिक नीति बदलाव संरक्षण प्रयासों को तेज करने और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रबंधन में सुधार लाने का उद्देश्य रखता है। जबकि संभावित वाणिज्यीकरण के बारे में चिंताएँ हैं, निजी संस्थाओं की भागीदारी से समग्र संरक्षण परिदृश्य में सुधार की उम्मीद है, जिससे ऐतिहासिक स्थलों के पुनर्स्थापन और रखरखाव में अधिक दक्षता आएगी।
GS3/अर्थव्यवस्था
आरबीआई ने दरें बनाए रखीं, नियमों में ढील देकर विकास पर ध्यान केंद्रित किया
 समाचार में क्यों?
समाचार में क्यों?
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 1 अक्टूबर 2025 को अपनी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में 5.5% पर रेपो दर को स्थिर रखा। यह निर्णय वर्ष की शुरुआत में 100 बुनियादी अंकों की कमी के बाद आया है। खुदरा मुद्रास्फीति के 2025-26 के लिए औसतन 2.6% होने का अनुमान है, जो 4% के लक्ष्य से काफी नीचे है, जिससे आरबीआई के लिए भविष्य में दरों में कटौती करने की लचीलापन बनी हुई है, लेकिन इसने सतर्क रहने का विकल्प चुना। ब्याज दर समायोजन पर केवल निर्भर रहने के बजाय, आरबीआई ने विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 22 संरचनात्मक उपायों की घोषणा की, जो नियमों में ढील और सुधारों के माध्यम से हैं। अर्थशास्त्रियों ने इसे स्पष्ट संकेत के रूप में देखा कि आरबीआई दीर्घकालिक स्थिरता और लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो केवल ब्याज दर परिवर्तनों से परे विकास समर्थन का विस्तार करता है।
- रेपो दर 5.5% पर स्थिर रखी गई, मुद्रास्फीति नियंत्रण और विकास समर्थन के बीच संतुलन बनाते हुए।
- जीडीपी विकास अनुमान 6.8% के लिए FY 2025-26 में बढ़ाया गया, जो मजबूत खपत और निवेश से प्रेरित है।
- उपभोक्ता मुद्रास्फीति का अनुमान 2.6% है, जो भविष्य की मौद्रिक ढील के लिए स्थान बनाता है।
- वैश्विक एजेंसियों ने बाहरी अनिश्चितताओं के बीच सकारात्मक विकास दृष्टिकोण की पुष्टि की।
- मुद्रास्फीति की भविष्यवाणियाँ: सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान FY 2025-26 के लिए 2.6% में घटाया गया, जो 3.1% से नीचे है, जो खाद्य कीमतों में गिरावट और प्रभावी जीएसटी समायोजन से प्रभावित है।
- वैश्विक आर्थिक संदर्भ: चालू खाता घाटा Q1 FY 2025-26 में जीडीपी के 0.2% तक संकुचित हुआ, जिसे मजबूत सेवाओं के निर्यात और महत्वपूर्ण रेमिटेंस का समर्थन मिला।
- भविष्य के विकास के चालक: मजबूत घरेलू मांग, संरचनात्मक सुधार और एक सक्रिय सेवाओं के क्षेत्र द्वारा समर्थित विकास की अपेक्षा की जा रही है।
संक्षेप में, आरबीआई के हाल के नीतिगत निर्णय विकास को समर्थन देने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के बीच एक सावधानीपूर्वक संतुलन को दर्शाते हैं। केंद्रीय बैंक का दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए एक सक्रिय स्थिति को इंगित करता है, जबकि बाहरी जोखिमों के प्रति सतर्क रहता है।
आरबीआई के सुधार - रुपये को अंतरराष्ट्रीय बनाने और वित्तीय बाजारों को गहरा करने की दिशा में
 क्यों समाचार में?
क्यों समाचार में?
हाल के विकास भारत के अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार तनाव और डॉलर के विकल्पों पर वैश्विक संवाद को उजागर करते हैं। इसके जवाब में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय बाजारों को मजबूत करने, कॉर्पोरेट वित्तपोषण विकल्पों को बढ़ाने और रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार पेश किए हैं।
- आरबीआई ने रेपो दर को 5.5% पर बनाए रखा है, जिसमें एक तटस्थ मौद्रिक नीति का रुख है।
- भारतीय बैंकों को अब कॉर्पोरेट अधिग्रहण को वित्तपोषित करने की अनुमति है, जिससे कॉर्पोरेट क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
- पड़ोसी देशों के लिए रुपये में सीमा पार उधारी की अनुमति है, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी।
- आईपीओ वित्तपोषण और शेयरों के खिलाफ ऋण के लिए उधारी की सीमाएं बढ़ाई गई हैं, जिससे बाजार की तरलता में सुधार होगा।
- वित्तीय बाजार में दक्षता को बढ़ावा देने के लिए मानक मुद्राओं का विस्तार किया गया है।
- मौद्रिक नीति के निर्णय: आरबीआई का 5.5% पर रेपो दर बनाए रखने का निर्णय एक स्थिर आर्थिक वातावरण को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना है।
- अधिग्रहण वित्तपोषण: बैंकों को अब कॉर्पोरेट अधिग्रहणों को वित्तपोषित करने की अनुमति है, जो पहले जुड़े जोखिमों के कारण सीमित थे। यह विलय और अधिग्रहण के लिए एक संरचित और लागत प्रभावी चैनल खोलता है।
- रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण: रुपये में सीमा पार उधारी की अनुमति देकर, आरबीआई रुपये की स्थिरता को बढ़ाने और दक्षिण एशिया में डॉलर पर निर्भरता को कम करने का प्रयास कर रहा है।
- बाजार तरलता में वृद्धि: आरबीआई ने आईपीओ वित्तपोषण और शेयरों के खिलाफ ऋण के लिए उधारी की सीमाएं बढ़ाई हैं, जो बांड बाजार में विकास को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।
- उधारी ढांचे में छूट: 2016 की उधारी सीमाओं को समाप्त करने से बैंकों को बड़े कॉर्पोरेट्स को उधार देने में अधिक स्वतंत्रता मिली है, जबकि स्थापित ढांचों के माध्यम से प्रणालीगत जोखिमों का प्रबंधन किया जा सकेगा।
आरबीआई के हालिया सुधार एक अधिक खुले और वैश्विक वित्तीय प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि इन उपायों में अंतर्निहित जोखिम हैं, वे भारत के आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने और स्थानीय व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने में सक्षम बनाने की व्यापक महत्वाकांक्षा को भी दर्शाते हैं, जिससे एक बहु ध्रुवीय दुनिया में भारत की वित्तीय संप्रभुता मजबूत होगी।
GS2/ शासन
कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाना

अवधि श्रमिक बल सर्वेक्षण (PLFS) 2023-24 के अनुसार, कृषि में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, हालांकि, इनमें से लगभग आधी महिलाएँ बिना वेतन के काम कर रही हैं, जो कृषि रोजगार में गहरे जेंडर भेदभाव को दर्शाता है।
भारत में कृषि में महिलाओं की स्थिति क्या है?
- कृषि का स्त्रीकरण: महिलाएँ अब भारत की कृषि कार्यबल का 42% से अधिक हिस्सा बनाती हैं, जो पिछले एक दशक में 135% की वृद्धि है। तीन में से दो ग्रामीण महिलाएँ कृषि में काम कर रही हैं।
- बिना वेतन के काम की प्रचलन: कृषि में लगभग आधी महिलाएँ बिना वेतन की पारिवारिक श्रमिक हैं, जो कि आठ वर्षों (2017-18 से 2024-25) में 23.6 मिलियन से बढ़कर 59.1 मिलियन हो गई हैं।
- क्षेत्रीय संकेंद्रण: बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, 80% से अधिक महिला श्रमिक कृषि में हैं, हालाँकि, इनमें से आधे से अधिक बिना वेतन हैं।
- सरकारी समर्थन: महिला किसान सशक्तिकरण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और स्वयं सहायता समूह मिलकर महिलाओं किसानों को कौशल विकास, औपचारिक ऋण तक पहुँच, सतत कृषि और सामूहिक सौदेबाजी को मजबूत करने के माध्यम से सशक्त बनाते हैं।
भारत में कृषि का स्त्रीकरण करने वाले कारक क्या हैं?
- पुरुषों का पलायन: पुरुष बेहतर नौकरी के अवसरों के लिए शहरी क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं या अधिक लाभकारी ग्रामीण नौकरियों, जैसे निर्माण, सेवाएं, परिवहन और सरकारी काम के लिए छोड़ रहे हैं। यह परिवर्तन महिलाओं को पारिवारिक खेतों और कृषि जिम्मेदारियों को संभालने के लिए मजबूर कर रहा है।
- अनुबंध कृषि का विकास: फूलों की खेती, बागवानी, और चाय/कॉफी के बागानों जैसे क्षेत्रों में श्रम-गहन कार्यों के लिए महिलाओं पर बढ़ता निर्भरता है। महिलाओं को विश्वसनीय, कुशल, और कम वेतन स्वीकार करने के लिए तैयार माना जाता है, जिससे वे इन क्षेत्रों में पसंदीदा श्रमिक बन जाती हैं।
- पितृसत्तात्मक मानदंड: सामाजिक अपेक्षाएं निर्धारित करती हैं कि महिलाओं को घरेलू और हल्के कृषि कार्यों को संभालना चाहिए। महिलाओं की कृषि श्रम को अक्सर उनके घरेलू कर्तव्यों का विस्तार माना जाता है, जिससे यह धारणा बनती है कि वे पुरुषों की सहायता कर रही हैं, न कि मुख्य श्रमिक।
- सीमित वैकल्पिक अवसर: महिलाओं को कम साक्षरता स्तर, सीमित गतिशीलता, और सामाजिक मानदंडों जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें गैर-खेती में रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में बाधित करती हैं। इसके परिणामस्वरूप, कृषि उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एकमात्र व्यावहारिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य आजीविका बन जाती है।
कृषि में महिलाओं की प्रगति को सीमित करने वाली प्रणालीगत बाधाएँ क्या हैं?
स्मरणिका: WOMEN
- W - वेतन भेदभाव: भारत में महिलाएँ पुरुषों की तुलना में 20-30% कम कमाती हैं, जो लिंग वेतन अंतर और आर्थिक असमानता को दर्शाता है, जिससे आर्थिक सशक्तीकरण सीमित होता है।
- O - निर्णय लेने से वर्जित: कृषि विस्तार अधिकारी मुख्यतः पुरुष होते हैं, जो महिलाओं को बीज, कीटनाशकों और सतत प्रथाओं की जानकारी से बाहर रखते हैं, जबकि ग्राम पंचायतों और किसान सहकारी समितियों में उनके विचार अक्सर अनदेखे होते हैं।
- M - मशीनरी और उपकरणों में असंगति: फार्म मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेशर पुरुषों के शरीर के अनुसार डिजाइन की गई हैं, जबकि महिलाओं में अक्सर इसे संचालित करने या पहुँचने के लिए आवश्यक ताकत, प्रशिक्षण, या वित्तीय साधनों की कमी होती है।
- E - घरेलू डबल बोझ का मजबूती से कायम रहना: घरेलू कार्यों और बच्चों की देखभाल से सीमित गतिशीलता और समय की कमी, महिलाओं की बाजारों, कौशल विकास, और सामुदायिक भागीदारी तक पहुँच को सीमित करती है।
- N - भूमि और पहचान अधिकारों का नकार: महिलाएँ केवल 13-14% भूमि धारक होती हैं, और भूमि शीर्षकों के बिना उन्हें किसान के बजाय उत्पादक समझा जाता है, जो क्रेडिट, सरकारी योजनाओं और स्वतंत्र निर्णय लेने तक पहुँच को सीमित करता है।
भारत में महिला किसानों के सशक्तीकरण के लिए प्रभावी कदम क्या हो सकते हैं?
स्मरणिका: GROW
- G - बाजार पहुंच की गारंटी: यूके के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) जैसे, जो कृषि निर्यात को 20% बढ़ाने की उम्मीद करते हैं, को चाय, मसाले और डेयरी जैसे महिला-केंद्रित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और महिलाओं को जैविक खाद्य पदार्थों और जीआई-टैग किए गए सामानों जैसे प्रीमियम उत्पादों का निर्यात करने में मदद करनी चाहिए, उनकी पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके।
- R - संसाधन अधिकार और सुधार: महिलाओं के लिए संयुक्त या व्यक्तिगत भूमि मालिकाना हक को बढ़ावा देना चाहिए ताकि उन्हें ऋण, बीमा और सरकारी सहायता तक पहुंच में सुधार हो सके, और सिद्ध महिला-नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को व्यवस्थित रूप से बढ़ाना चाहिए ताकि पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को हासिल किया जा सके।
- O - डिजिटल द्वार खोलना: ई-नैम जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों को बढ़ाना चाहिए, आवाज-प्रथम एआई जैसे कि भाषिणी, जुगलबंदी, और डिजिटल साथी को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के लिए बढ़ावा देना चाहिए।
- W - कल्याण और सामाजिक समर्थन: खेतों के पास क्रेच सुविधाएं, जल आपूर्ति, और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करनी चाहिए ताकि महिलाओं के समय की कमी को कम किया जा सके, जबकि मीडिया अभियान और पुरस्कारों का उपयोग करके महिला किसानों को आदर्श के रूप में ब्रांड करना चाहिए।
निष्कर्ष
महिला-सशक्तिकरण के लिए कृषि में संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए, भारत को महिलाओं की श्रम शक्ति को पहचानने से उन्हें आर्थिक एजेंट के रूप में सशक्त बनाने की दिशा में बढ़ना होगा। इसके लिए भूमि अधिकारों के अस्वीकृति और वेतन अंतर जैसे प्रणालीगत बाधाओं को समाप्त करना आवश्यक है, जबकि तकनीक, बाजार, और निर्णय-निर्माण भूमिकाओं तक उनकी पहुँच को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना होगा ताकि समावेशी वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
GS2/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध
भारत-ईएफ़टीए मुक्त व्यापार समझौता
क्यों है यह समाचार?

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। यह भारत और ईएफ़टीए देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। यह FTA भारत की वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में बढ़ती भागीदारी और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बाजार पहुँच को व्यापक बनाने की रणनीति को रेखांकित करता है।
भारत-ईएफटीए एफटीए क्या है?
पृष्ठभूमि: भारत-ईएफटीए एफटीए, जिसे व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) के नाम से भी जाना जाता है, मार्च 2024 में अंतिम रूप दिया गया और यह 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ। इस समझौते का उद्देश्य भारत के व्यापार संबंधों को ईएफटीए ब्लॉक के साथ मजबूत करना है और यह भारत के हाल के एफटीए को यूएई, ऑस्ट्रेलिया, और यूके जैसे देशों के साथ पूरा करता है।
समझौते के उद्देश्य:
- बाजार पहुंच में वृद्धि: ईएफटीए देशों ने भारत के औद्योगिक और गैर-कृषि उत्पादों के लिए 100% बाजार पहुंच प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों पर शुल्क में राहत प्रदान की गई है।
- निवेश और रोजगार सृजन: ईएफटीए देशों ने 15 वर्षों में 100 बिलियन USD का बाध्यकारी निवेश करने का वचन दिया है, जिससे भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है।
- व्यापार सुगमता तंत्र: निवेश और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समर्पित ईएफटीए डेस्क स्थापित की गई है, जो भारत में निवेश करने, विस्तार करने और संचालन करने के इच्छुक ईएफटीए व्यवसायों को समर्थन प्रदान करती है।
मुक्त व्यापार समझौतों की समझ
मुक्त व्यापार समझौतें (FTAs) दो या दो से अधिक देशों के बीच समझौतें होते हैं, जिनका उद्देश्य व्यापार में बाधाओं को कम या समाप्त करना है, जैसे कि कस्टम शुल्क और कोटा, जो वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होते हैं। भारत के पास विभिन्न देशों और समूहों के साथ FTAs हैं, जिनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरिशस, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA), सिंगापुर, और श्रीलंका शामिल हैं। भारत-ईयू FTA के लिए बातचीत भी उन्नत चरणों में है।
भारत के लिए FTAs के लाभ
- बाजार पहुंच: FTAs भारत के निर्यात को बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि ये कस्टम शुल्क और गैर-कस्टम बाधाओं को कम करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) ने 90% निर्यात के लिए शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की, जिससे पहले वर्ष में निर्यात में 12% की वृद्धि हुई।
- निवेश में वृद्धि: FTAs स्थिर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को आकर्षित करते हैं। भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA) के परिणामस्वरूप FDI प्रवाह में 25% की वृद्धि हुई।
- कृषि लाभ: FTAs भारतीय किसानों के लिए नए निर्यात बाजार खोलते हैं। भारत-मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (CECPA) ने कृषि निर्यात जैसे कि चीनी और चाय में वृद्धि की।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: FTAs उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाते हैं। भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की ऊर्जा संक्रमण में सहायता कर रहा है।
- छोटी और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए समर्थन: FTAs SMEs को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल करने में मदद करते हैं। भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA) सूचना प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में SMEs को लाभ पहुंचा रहा है।
- नियामक समन्वय: FTAs मानकों के सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं, जिससे व्यवसायों के लिए अनुपालन लागत कम होती है। भारत-EFTA TEPA उत्पाद प्रमाणपत्रों को संरेखित करता है, जिससे भारतीय उत्पादों के EFTA बाजारों में प्रवेश करना आसान होता है।
भारत के एफटीए से संबंधित चिंताएँ
- व्यापार घाटे: बढ़ते व्यापार घाटे के बारे में चिंता है, जहाँ आयात निर्यात की तुलना में काफी बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत-ASEAN एफटीए के कारण आयात में काफी वृद्धि हुई है, जो वित्तीय वर्ष 23 में $44 बिलियन तक पहुंच गई है।
- विकसित बाजारों तक सीमित पहुंच: गैर- tarif बाधाएँ विकसित बाजारों तक पहुंच को प्रतिबंधित कर सकती हैं। यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में देरी आंशिक रूप से बौद्धिक संपदा अधिकारों और डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के कारण है।
- छोटे किसानों और MSMEs पर प्रभाव: छोटे किसानों और सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को सस्ते आयातों से तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, भारत में रबर के किसानों पर ASEAN एफटीए का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- श्रम और पर्यावरणीय धाराएँ: एफटीए में बंधनकारी धाराएँ, जैसे कि यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, भारतीय निर्यातों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं क्योंकि यह सख्त मानकों को लागू करता है।
- कमजोर विवाद समाधान तंत्र: कुछ एफटीए में विवाद समाधान प्रक्रियाएँ धीमी और असंतुलित मानी जाती हैं। भारत-ASEAN एफटीए में तेल पाम और मशीनरी टैरिफ के संबंध में विवाद समाधान के मुद्दे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ विवाद समाधान समस्याग्रस्त रहा है।
भारत द्वारा वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय
- निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना: भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उत्पादन और कृषि में गुणवत्ता, ब्रांडिंग और तकनीकी प्रगति में सुधार पर ध्यान केंद्रित करें।
- व्यापार साझेदारियों में विविधता लाना: व्यापार साझेदारों की संख्या को सीमित करने से बचने के लिए अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया-प्रशांत जैसे क्षेत्रों में उभरते बाजारों को शामिल करने के लिए एफटीए का विस्तार करें।
- MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए समर्थन: निर्यात के लिए उन्मुख छोटे और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप्स के लिए ऋण, लॉजिस्टिक्स, और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों तक पहुंच को सरल और बेहतर बनाएं। इससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिल सकती है।
- अवसंरचना विकास: बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स हब, माल परिवहन गलियारों और कोल्ड चेन सुविधाओं के विस्तार और उन्नयन में निवेश करें। इससे लेन-देन की लागत कम करने और माल के परिवहन की दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- अनुपालन और मानकों को बढ़ाना: निर्यातकों को गुणवत्ता, श्रम, और पर्यावरण मानकों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में मदद के लिए क्षमता निर्माण समर्थन प्रदान करें। इससे विदेशी बाजारों में प्रवेश को सुगम बनाने में सहायता मिलेगी।
- डिजिटल व्यापार प्लेटफार्मों का लाभ उठाना: व्यापार के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग बढ़ावा दें, जैसे कि वर्चुअल व्यापार मेले, ई-मार्केटप्लेस, और एफटीए का ऑनलाइन उपयोग, ताकि व्यापक दर्शकों तक पहुँच सकें और व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बना सकें।
भारत-ईएफटीए मुक्त व्यापार समझौता भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। हालांकि, इसके लिए घरेलू उद्योग की चुनौतियों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन और व्यापार में विविधता लाने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता भी है।
GS2/राजनीति और शासन
निवारक निरोध और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980
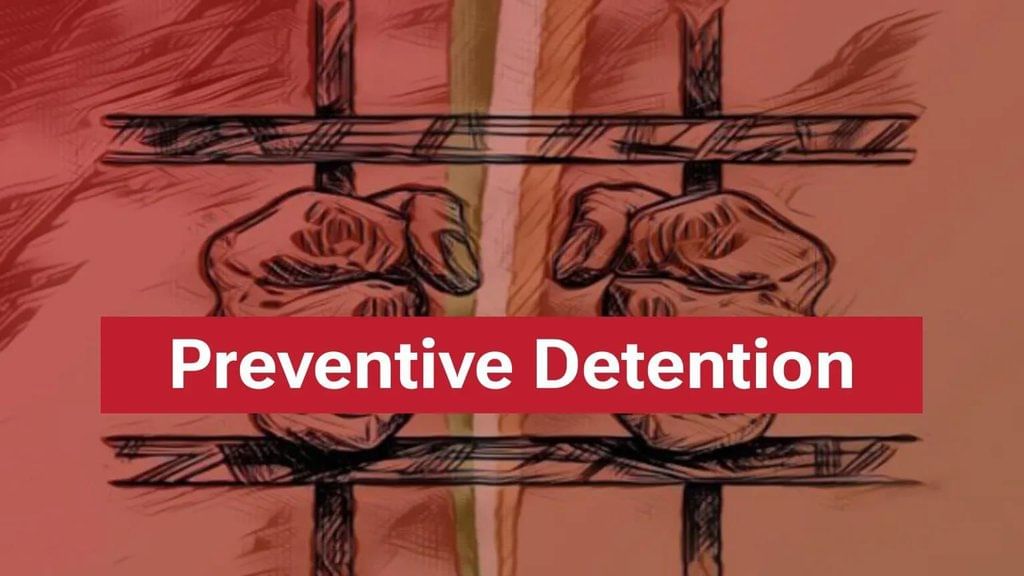
- जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980 के तहत गिरफ्तार किया गया। यह कानून सरकार को उन व्यक्तियों के खिलाफ निवारक कार्रवाई करने की अनुमति देता है जिन्हें सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है।
- वांगचुक लद्दाख के लिए राज्यhood और संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग करने वाले प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे हैं।
निवारक निरोध क्या है?
- निवारक निरोध उस प्रथा को संदर्भित करता है जिसमें किसी व्यक्ति को अपराध के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में संभावित खतरनाक क्रियाओं को रोकने के लिए रखा जाता है जो सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, या आवश्यक आपूर्ति को खतरा पहुंचा सकते हैं।
- दंडात्मक निरोध के विपरीत, जो कानूनी सजा के परिणामस्वरूप लगाया जाता है, निवारक निरोध भविष्य में हानिकारक क्रियाओं की संभावना के आधार पर पूर्वानुमानित होता है।
संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में स्पष्ट रूप से निवारक निरोध की अनुमति दी गई है।
- एक व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की अनुमति के बिना अधिकतम 3 महीने के लिए निरोध में रखा जा सकता है, जिसमें उच्च न्यायालयों में बैठने के योग्य न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- 3 महीने से अधिक के निरोध के लिए सलाहकार बोर्ड की अनुमति अनिवार्य है।
- संसद के पास 3 महीने से अधिक के निरोध के लिए शर्तें निर्धारित करने, अधिकतम निरोध अवधि तय करने और सलाहकार बोर्ड के लिए प्रक्रियाएँ स्थापित करने का अधिकार है।
- निरूद्ध व्यक्ति को उनके निरोध के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, हालाँकि कुछ तथ्यों को सार्वजनिक सुरक्षा के हित में छुपाया जा सकता है।
- निरूद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश को चुनौती देने का अवसर जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए।
महत्व: निवारक निरोध संविधान के अनुच्छेद 355 के साथ संरेखित है, जो संघ को बाहरी आक्रमण और आंतरिक विघटन के खिलाफ राज्यों की रक्षा करने और सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार कार्य करें।
भारत में निवारक निरोध से संबंधित प्रमुख कानून:
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980: राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लक्षित।
- अवैध गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 1967: आतंकवाद और अवैध गतिविधियों से निपटने पर केंद्रित।
- विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974: तस्करी और विदेशी मुद्रा उल्लंघनों पर अंकुश लगाने के लिए लक्षित।
- राज्य-विशिष्ट सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम: राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे से बचाने के लिए डिजाइन किए गए।
उच्चतम न्यायालय द्वारा निवारक निरोध:
- अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य (2023): उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निवारक निरोध एक असाधारण उपाय है जो आपातकालीन परिस्थितियों के लिए है और इसका नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य (2011): न्यायालय ने निर्धारित किया कि निवारक निरोध संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अपवाद है और इसका उपयोग सीमित रूप से और केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए।
- अनुकुल चंद्र प्रधान, अधिवक्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य (1997): न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि निवारक निरोध का उद्देश्य राज्य की सुरक्षा की रक्षा करना है, न कि दंडात्मक उपाय लागू करना।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 क्या है?
- पृष्ठभूमि: भारत में निवारक निरोध की प्रथा का आरंभ उपनिवेशी समय में हुआ, जब इसका उपयोग युद्ध के दौरान असहमति को दबाने के लिए किया जाता था। भारत की स्वतंत्रता के बाद, संसद ने 1950 में निवारक निरोध अधिनियम बनाया, इसके बाद 1971 में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के अधिनियम (MISA) को लागू किया गया। MISA का आपातकाल के दौरान व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया और 1978 में इसे निरस्त कर दिया गया।
- 1980 में, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) की स्थापना की गई। यह अधिनियम केंद्रीय और राज्य सरकारों, जिला मजिस्ट्रेटों और अधिकृत पुलिस कमिश्नरों को उन व्यक्तियों को निरोध करने का अधिकार प्रदान करता है, जिनकी गतिविधियाँ भारत की रक्षा, विदेशी संबंधों, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक आपूर्ति के लिए हानिकारक मानी जाती हैं।
- निरोध आदेश: NSA के तहत जारी किया गया निरोध आदेश गिरफ्तारी वारंट के समान कार्य करता है। एक बार निरोधित होने पर, व्यक्तियों को निर्धारित सुविधाओं में रखा जा सकता है, राज्यों में स्थानांतरित किया जा सकता है, और सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन रखा जा सकता है।
- प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ: निरोध के कारणों को निरोधित व्यक्ति को 5 से 15 दिनों के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। निरोधित व्यक्तियों को सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से बनी एक सलाहकार समिति को 3 सप्ताह के भीतर मामले की समीक्षा करनी होती है। यदि समिति निरोध का पर्याप्त कारण नहीं पाती है, तो व्यक्ति को रिहा किया जाना चाहिए। NSA के तहत निरोध की अधिकतम अवधि 12 महीने है, हालाँकि इसे पहले भी निरस्त किया जा सकता है।
- सुरक्षा उपायों की सीमाएँ: निरोधित व्यक्तियों को सलाहकार समिति के समक्ष कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं है। सरकार जनहित के आधार पर कुछ तथ्यों को रोकने का अधिकार रखती है। ये प्रावधान अधिकारियों को महत्वपूर्ण विवेकाधिकार प्रदान करते हैं, जिससे कानून के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
GS2/राजनीति और शासन
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की शताब्दी
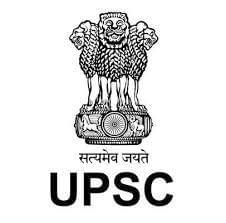
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 1 अक्टूबर, 2025 को अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई, जो 1926 में इसकी स्थापना के एक सदी का प्रतीक है।
- UPSC को योग्यता को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है और यह भारत की सिविल सेवाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- सिविल सेवाओं की देखरेख के लिए एक स्थायी निकाय की अवधारणा 1919 के संविधान सुधारों (Montagu-Chelmsford Reforms) में प्रस्तावित की गई थी।
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की सुविधा प्रदान की।
- ली आयोग की सिफारिशों के जवाब में, लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर, 1926 को की गई, जिसके पहले अध्यक्ष सर रॉस बार्कर थे।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अंतर्गत इसे संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में पुनः ब्रांड किया गया।
- 1950 में संविधान के कार्यान्वयन के बाद, FPSC का नाम संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) रखा गया, जो अनुच्छेद 378 के तहत आया।
यूपीएससी की भूमिका और कार्य
- UPSC भारत में एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है, जिसे संविधान के भाग XIV, अध्याय II के अनुच्छेद 315–323 के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
- इसकी मुख्य जिम्मेदारी अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों की भर्ती करना है।
- आयोग विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करता है, जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार होती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि विभिन्न समूह A और समूह B सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और अप्रभावित हो।
यूपीएससी द्वारा सुधार: प्रतिभा सेतु पहल
- प्रतिभा सेतु पहल एक केंद्रीयकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसमें उन उम्मीदवारों का सत्यापित बायोडाटा है जो यूपीएससी साक्षात्कार के लिए योग्य हुए लेकिन अंततः चयनित नहीं हुए।
- यह पहल इन उम्मीदवारों को वैकल्पिक रोजगार के अवसरों से जोड़ने का लक्ष्य रखती है, जिससे उनकी जानकारी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रुचि रखने वाले नियोक्ताओं के लिए सुलभ हो सके।
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO)
 यह समाचार क्यों महत्वपूर्ण है?
यह समाचार क्यों महत्वपूर्ण है?
- भारत को 2025-2028 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के परिषद के भाग II के लिए फिर से चुना गया है।
ICAO के बारे में:
- ICAO संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1944 में शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के सम्मेलन पर हस्ताक्षर करके की गई थी।
- यह सुरक्षित और शांतिपूर्ण हवाई नेविगेशन के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करता है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की सुव्यवस्थित वृद्धि को बढ़ावा देता है।
- यह कनाडा के मॉन्ट्रियल में मुख्यालय स्थित है, और इसके 193 सदस्य राज्य हैं, जिनमें भारत भी शामिल है।
ICAO सभा और परिषद:
- ICAO सभा, जो हर तीन साल में होती है, संगठन का संप्रभु निकाय है, जिसमें शिकागो सम्मेलन के सभी 193 हस्ताक्षरकर्ता राज्य शामिल हैं।
- 36-सदस्यीय ICAO परिषद, जिसे तीन भागों में विभाजित किया गया है, को सदस्य राज्यों द्वारा ICAO सभा के दौरान चुना जाता है और यह तीन साल के कार्यकाल के लिए शासन निकाय के रूप में कार्य करती है।
परिषद का गठन:
- भाग I: हवाई परिवहन में प्रमुख महत्व वाले राज्य, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, और जापान।
- भाग II: अंतर्राष्ट्रीय नागरिक हवाई नेविगेशन में सबसे बड़े योगदान देने वाले राज्य, जिनमें भारत, जर्मनी, और ब्राजील शामिल हैं।
- भाग III: भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने वाले राज्य, जैसे कि बोलिविया, मलेशिया, और इथियोपिया।
ICAO में भारत की भूमिका:
- ICAO के संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत ने सुरक्षित, सुरक्षित, टिकाऊ, और समावेशी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- 2025-2028 के कार्यकाल के लिए, भारत हवाई सुरक्षा और सुरक्षा को मजबूत करने, हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने, प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने, और ICAO की "कोई देश पीछे न छूटे" पहल का समर्थन करने का लक्ष्य रखता है।
|
7 videos|3454 docs|1081 tests
|
FAQs on UPSC Daily Current Affairs (Hindi)- 2nd October 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly
| 1. अमेरिका में बंद होने की स्थिति से क्या आशय है और इसके संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं? |  |
| 2. भारत में स्मारक संरक्षण के लिए हाल में किए गए नीति में बदलावों का क्या महत्व है? |  |
| 3. आरबीआई ने दरें बनाए रखने का निर्णय क्यों लिया और इसका विकास पर क्या असर पड़ेगा? |  |
| 4. कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत में कौन-कौन सी योजनाएँ लागू की गई हैं? |  |
| 5. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 का महत्व क्या है और यह कैसे कार्य करता है? |  |





















