UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 13th February 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download
जीएस1/इतिहास और संस्कृति
दयानंद सरस्वती: आधुनिक भारत के अग्रदूत
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
 चर्चा में क्यों?
चर्चा में क्यों?
12 फरवरी, 2025 को भारत ने भारतीय सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दयानंद सरस्वती की 201वीं जयंती मनाई। वर्ष 2023 में उनकी 200वीं जयंती को एक साल तक मनाया जाएगा, जिसमें आधुनिक भारतीय समाज में उनके योगदान पर जोर दिया जाएगा।
- 12 फरवरी 1824 को मोरबी, गुजरात में जन्मे।
- 1875 में सामाजिक सुधार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आर्य समाज की स्थापना की।
- उन्होंने वैदिक सिद्धांतों की ओर लौटने की वकालत करते हुए सत्यार्थ प्रकाश की रचना की।
- महिला शिक्षा का समर्थन किया और बाल विवाह और अस्पृश्यता जैसी प्रथाओं का विरोध किया।
अतिरिक्त विवरण
- आर्य समाज: इस संगठन का उद्देश्य हिंदू धर्म में कर्मकांड संबंधी प्रथाओं को अस्वीकार करके सामाजिक जागृति को बढ़ावा देना और वैदिक शिक्षाओं पर आधारित एकीकृत समाज को बढ़ावा देना था।
- दर्शन: दयानंद के दस संस्थापक सिद्धांतों ने व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा मानवता को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों पर जोर दिया, तथा वंशानुक्रम के बजाय योग्यता के आधार पर सुधारों की वकालत करके जाति व्यवस्था को चुनौती दी।
- गोरक्षा: वे गोरक्षा के शुरुआती पैरोकारों में से एक थे, उन्होंने 1881 में गोकरुणनिधि प्रकाशित की तथा 1882 में गौरक्षिणी सभा की स्थापना की।
- शिक्षा संबंधी पहल: 1883 में उनकी मृत्यु के बाद, उनके अनुयायियों ने आधुनिक शिक्षा को सांस्कृतिक और धार्मिक शिक्षा के साथ मिश्रित करने के लिए दयानंद एंग्लो वैदिक (डीएवी) स्कूल की स्थापना की।
दयानंद सरस्वती की विरासत सामाजिक न्याय, शैक्षिक सुधार और वैदिक सिद्धांतों के प्रचार के लिए उनके अथक प्रयासों से चिह्नित है, जो समकालीन समाज को प्रभावित करना जारी रखते हैं।
जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी
परमाणु ऊर्जा - दायित्व पर खतरनाक रियायतें
स्रोत: द हिंदू
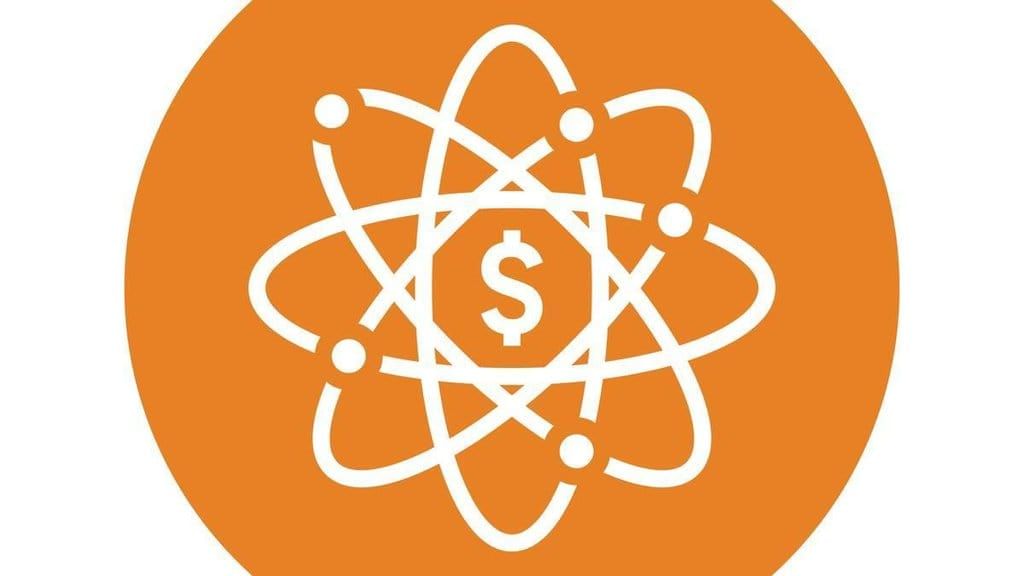 चर्चा में क्यों?
चर्चा में क्यों?
हाल ही में केंद्रीय बजट में परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व (सीएलएनडी) अधिनियम में संशोधन के बारे में की गई घोषणा ने भारत में परमाणु ऊर्जा सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएँ और चर्चाएँ पैदा की हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना है, लेकिन ये सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित जोखिम भी पैदा करते हैं।
- सीएलएनडी अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन भारत के परमाणु क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकते हैं।
- संचालक का दायित्व मुख्य रूप से परमाणु संयंत्र संचालकों पर डाला जाता है, जबकि आपूर्तिकर्ताओं की जवाबदेही सीमित होती है।
- भारत का परमाणु दायित्व ढांचा वैश्विक मानकों से भिन्न है, विशेष रूप से वित्तीय उत्तरदायित्व और क्षतिपूर्ति सीमा के संदर्भ में।
अतिरिक्त विवरण
- परमाणु ऊर्जा अधिनियम (1962): यह भारतीय कानून शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास और उपयोग को नियंत्रित करता है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है। यह सरकार को परमाणु सामग्री और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना पर विशेष नियंत्रण प्रदान करता है।
- परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व (सीएलएनडी) अधिनियम (2010): यह कानून दुर्घटना की स्थिति में परमाणु संयंत्र संचालकों के वित्तीय दायित्व को परिभाषित करता है, पीड़ितों के लिए मुआवजा सुनिश्चित करता है और संचालकों को जवाबदेह बनाता है।
- सीएलएनडी की मुख्य विशेषताएं:
- ऑपरेटर का दायित्व: दुर्घटनाओं के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी संयंत्र ऑपरेटर (एनपीसीआईएल) की है, आपूर्तिकर्ता की नहीं।
- सहारा का अधिकार: कई अन्य देशों के विपरीत, ऑपरेटर दोषपूर्ण उपकरणों के लिए आपूर्तिकर्ताओं से मुआवजे की मांग कर सकते हैं।
- देयता सीमा: ऑपरेटर की देयता ₹1,500 करोड़ (~$180 मिलियन) तक सीमित है, तथा सरकार किसी भी अतिरिक्त लागत को वहन करेगी।
- वैश्विक व्यवस्थाओं से बहिष्कार: भारत अंतरराष्ट्रीय परमाणु दायित्व समझौतों में शामिल नहीं हुआ है, तथा घरेलू वित्तीय उत्तरदायित्व को बरकरार रखा है।
- सुरक्षा संबंधी चिंताएं: भयावह दुर्घटनाओं का खतरा है, जैसा कि फुकुशिमा और चेर्नोबिल आपदाओं में देखा गया है, जो परमाणु ऊर्जा विफलताओं के संभावित दीर्घकालिक परिणामों को उजागर करते हैं।
- वैश्विक मानक बनाम भारत: अधिकांश देश आपूर्तिकर्ताओं को पूर्णतः क्षतिपूर्ति देते हैं, जबकि भारत ऑपरेटरों को जिम्मेदार मानता है, जिससे आपूर्तिकर्ताओं की जवाबदेही और सुरक्षा पर चिंता उत्पन्न होती है।
परमाणु ऊर्जा अधिनियम और सीएलएनडी अधिनियम में संशोधन करने की सरकार की योजना का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा में विदेशी निवेश के लिए अधिक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है, फिर भी इसमें परमाणु सुरक्षा और सार्वजनिक कल्याण पर पड़ने वाले प्रभावों पर सावधानीपूर्वक विचार करना भी आवश्यक है।
जीएस2/राजनीति
आप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025
स्रोत: द हिंदू
 चर्चा में क्यों?
चर्चा में क्यों?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद के मौजूदा बजट सत्र में अप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025 पेश कर सकते हैं। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य अप्रवासन और विदेशियों के पंजीकरण को नियंत्रित करने वाले कई पुराने कानूनों को बदलना है।
- यह विधेयक पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939, विदेशी अधिनियम, 1946 और आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 सहित मौजूदा कानूनों का स्थान लेगा।
- ये मौजूदा कानून संविधान-पूर्व युग के दौरान बनाए गए थे और विश्व युद्धों जैसी असाधारण परिस्थितियों के दौरान प्रासंगिक थे।
- विधेयक में विदेशियों के पंजीकरण के संबंध में शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और आवासीय परिसरों की जिम्मेदारियों को रेखांकित किया गया है।
- इसमें आव्रजन नियमों का पालन न करने वाले विमान सेवा प्रदाताओं के लिए दंड का प्रावधान किया गया है।
अतिरिक्त विवरण
- पंजीकरण दायित्व: विधेयक में यह अनिवार्य किया गया है कि विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को अपने यहां प्रवेश पाने वाले किसी भी विदेशी छात्र के बारे में पंजीकरण अधिकारी को जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
- स्वास्थ्य देखभाल जिम्मेदारियां: अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को इनडोर उपचार प्राप्त करने वाले किसी भी विदेशी मरीज और उनके परिचारकों के बारे में प्राधिकारियों को सूचित करना आवश्यक है।
- आवासीय रिपोर्टिंग: आवासीय परिसर को नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों को अपने परिसर में रहने वाले किसी भी विदेशी के बारे में पंजीकरण अधिकारी को सूचित करना होगा।
- वाहकों के कर्तव्य: एयरलाइनों और शिपिंग कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे आव्रजन अधिकारियों द्वारा प्रवेश से वंचित किए गए किसी भी यात्री को हटा दें और उन्हें यात्री और चालक दल का डेटा अग्रिम रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- दंड: विधेयक में निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर वाहकों पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
आव्रजन एवं विदेशी विधेयक, 2025 का उद्देश्य भारत में विदेशियों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना, समकालीन आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करते हुए बेहतर विनियमन और अनुपालन सुनिश्चित करना है।
जीएस3/रक्षा एवं सुरक्षा
पी-8आई विमान खरीद प्रस्ताव
स्रोत: द हिंदू
 चर्चा में क्यों?
चर्चा में क्यों?
भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका से छह अतिरिक्त पी-8आई लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान प्राप्त करने की अपनी योजना को पुनर्जीवित करने पर विचार कर रहा है।
चाबी छीनना
- पी-8आई नेप्च्यून भारतीय नौसेना के लिए डिज़ाइन किया गया एक परिष्कृत समुद्री गश्ती विमान है।
- यह विमान अमेरिकी नौसेना के पी-8ए पोसाइडन का एक संस्करण है और इसका उद्देश्य भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाना है।
अतिरिक्त विवरण
- पी-8आई नेप्च्यून: बोइंग पी-8आई नेप्च्यून एक बहु-मिशन समुद्री गश्ती विमान है, जिसने भारतीय नौसेना के पुराने टुपोलेव टीयू-142 बेड़े का स्थान लिया है।
- उन्नत क्षमताएं: उन्नत सेंसर और हथियार प्रणालियों से लैस, पी-8आई विभिन्न प्रकार के मिशनों को अंजाम दे सकता है, जिसमें पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW), सतह रोधी युद्ध (AsuW), खुफिया जानकारी एकत्र करना, समुद्री गश्त और निगरानी शामिल हैं।
- विशेष विवरण:
- लंबाई: 39.47 मीटर
- पंख फैलाव: 37.64 मीटर
- ऊंचाई: 12.83 मीटर
- अधिकतम टेक-ऑफ सकल वजन: 85,139 किलोग्राम
- अधिकतम गति: 789 किमी/घंटा
- अधिकतम ऊंचाई: 12,496 मीटर
- रेंज: 2,222 किमी से अधिक, स्टेशन समय चार घंटे।
इस प्रस्तावित खरीद का उद्देश्य तेजी से जटिल होते क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल में भारत की समुद्री सुरक्षा और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है।
जीएस1/इतिहास और संस्कृति
डोकरा कलाकृति
स्रोत: एनडीटीवी
 चर्चा में क्यों?
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को एक अत्यंत सावधानी से तैयार की गई डोकरा कलाकृति भेंट की, जिसमें इस पारंपरिक शिल्प के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
- डोकरा कला, जिसे बेल मेटल शिल्प के नाम से भी जाना जाता है, का इतिहास 4,000 वर्षों से भी अधिक पुराना है।
- यह लोक कला मुख्य रूप से ढोकरा दामर जनजातियों द्वारा प्रचलित है, जो कुशल धातुकार हैं।
- कारीगर मुख्यतः पूर्वी भारत में रहते हैं, विशेषकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में।
अतिरिक्त विवरण
- अद्वितीय विशेषताएं: प्रत्येक डोकरा टुकड़ा अद्वितीय है, हस्तनिर्मित है, और पौराणिक कथाओं, प्रकृति और रोजमर्रा की जिंदगी के विषयों से प्रेरित है।
- विनिर्माण प्रक्रिया: डोकरा कला के निर्माण में एक परिष्कृत खोई हुई मोम तकनीक शामिल है, जहाँ कारीगर एक बुनियादी मिट्टी के मॉडल को गढ़ते हैं, इसे मोम में लपेटते हैं, और जटिल विवरणों को उकेरते हैं। इसके बाद एक और मिट्टी की परत के साथ एक साँचा बनाया जाता है और उसमें पिघली हुई धातु - आमतौर पर पीतल या तांबा - डाली जाती है। गर्मी मोम को पिघला देती है, जिससे धातु मॉडल का आकार ले लेती है। ठंडा होने के बाद, बाहरी मिट्टी के साँचे को तोड़ दिया जाता है ताकि मूर्ति दिखाई दे।
कला का यह उत्कृष्ट रूप न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, बल्कि इसमें शामिल कारीगरों की शिल्पकला और रचनात्मकता को भी दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय नेताओं के सामने डोकरा कलाकृति की प्रस्तुति भारत की समृद्ध कलात्मक परंपराओं का प्रतीक है।
जीएस3/अर्थव्यवस्था
मित्रा प्लेटफॉर्म: सेबी की एक नई पहल
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हाल ही में MITRA नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसे निवेशकों को उनके म्यूचुअल फंड निवेश को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- MITRA का तात्पर्य म्यूचुअल फंड निवेश ट्रेसिंग और रिट्रीवल असिस्टेंट से है।
- इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य निवेशकों को निष्क्रिय या बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने और पुनः प्राप्त करने में मदद करना है।
- यह अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) मानदंडों के अनुपालन को प्रोत्साहित करता है।
अतिरिक्त विवरण
- MITRA का उद्देश्य: यह प्लेटफॉर्म निवेशकों की उस आम समस्या का समाधान करता है, जिसमें वे समय के साथ अपने म्यूचुअल फंड निवेशों पर नजर नहीं रख पाते, जिसके कारण संपर्क जानकारी अपडेट न होना या उनके नाम पर किए गए निवेशों के बारे में जानकारी न होना आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
- यह पहल रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स (आरटीए) द्वारा विकसित निष्क्रिय और दावा न किए गए म्यूचुअल फंड फोलियो का एक खोज योग्य डेटाबेस प्रदान करती है, जिससे निवेशकों को अपने अनदेखे निवेशों या दूसरों द्वारा किए गए निवेशों की पहचान करने में मदद मिलती है, जिनके वे सही दावेदार हो सकते हैं।
- निष्क्रिय फोलियो मानदंड: एक म्यूचुअल फंड फोलियो को निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि दस साल की अवधि के लिए निवेशक द्वारा शुरू किए गए कोई भी लेनदेन - वित्तीय या गैर-वित्तीय - नहीं हुआ है, भले ही यूनिट बैलेंस मौजूद हो।
- इसके अलावा, सेबी ने यूनिट धारक संरक्षण समिति (यूएचपीसी) के अधिदेश को अद्यतन किया है , जिसे अब दावा न किए गए लाभांश और मोचन के साथ-साथ निष्क्रिय फोलियो की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे मामलों को न्यूनतम करने के लिए सक्रिय उपाय किए जाएं।
सेबी की इस पहल का उद्देश्य निवेशकों की सहभागिता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति अपने सही निवेश को पुनः प्राप्त कर सकें, जिससे म्यूचुअल फंड प्रणाली में समग्र विश्वास में सुधार हो।
जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध
नॉर्डिक-बाल्टिक आठ (एनबी-8) देश
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
पेरिस में आयोजित एआई एक्शन समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एस्टोनियाई राष्ट्रपति अलार कारिस के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। चर्चा व्यापार, प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा को बढ़ाने और नॉर्डिक-बाल्टिक आठ (एनबी-8) ढांचे के भीतर मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के इर्द-गिर्द घूमती रही।
- पहली द्विपक्षीय बैठक व्यापार, डिजिटल संबंधों और साइबर सुरक्षा पर केंद्रित थी।
- प्रधानमंत्री मोदी ने एस्टोनियाई व्यवसायों को भारत के आईटी और साइबर सुरक्षा क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया।
- रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच डिजिटल शासन और साइबर सुरक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की गई।
- भारत-नॉर्डिक-बाल्टिक (एनबी-8) सहयोग और यूरोपीय संघ तथा संयुक्त राष्ट्र में भारत की कूटनीतिक भूमिका के महत्व पर बल दिया गया।
- योग में एस्टोनिया की रुचि पर प्रकाश डाला गया तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया गया।
अतिरिक्त विवरण
- नॉर्डिक-बाल्टिक आठ (एनबी-8) देशों के बारे में: इस क्षेत्रीय सहयोग मंच में शामिल हैं:
- नॉर्डिक देश: डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन
- बाल्टिक राज्य: एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया
- एनबी-8 सहयोग की शुरुआत 1990 के दशक में बाल्टिक राज्यों की सोवियत नियंत्रण से स्वतंत्रता के बाद हुई, तथा इसकी औपचारिक शुरुआत 1989 में हुई।
- क्षेत्रीय कूटनीतिक और आर्थिक पहल को बढ़ावा देने के लिए एनबी-8 की रूपरेखा आधिकारिक तौर पर 2000 में स्थापित की गई थी।
- संरचनात्मक अधिदेश:
- व्यापार एवं आर्थिक विकास: व्यवसाय एवं निवेश साझेदारी को मजबूत बनाना।
- प्रौद्योगिकी और नवाचार: डिजिटल शासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा पर सहयोग।
- सुरक्षा एवं रक्षा: नाटो और यूरोपीय संघ के ढांचे के भीतर सहयोग बढ़ाना।
- जलवायु एवं ऊर्जा नीति: स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा पहल को बढ़ावा देना।
- नेतृत्व प्रतिवर्ष एनबी-8 देशों के बीच घूमता है, जिसमें डेनमार्क 2025 में, स्वीडन 2024 में, तथा लातविया 2023 में अध्यक्षता करेगा।
इस सहयोग का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देते हुए व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा में आपसी हितों को आगे बढ़ाना है।
जीएस2/राजनीति
क्या दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए?
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में अश्विन उपाध्याय और अन्य की याचिकाओं की समीक्षा कर रहा है, जिसमें अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की वकालत की गई है।
- यह बहस राजनीतिक उम्मीदवारों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों और नैतिक मानकों के बीच संतुलन के इर्द-गिर्द केंद्रित है।
- वर्तमान कानून, अपराध की गंभीरता के आधार पर दोषी व्यक्तियों को विशिष्ट अवधि के लिए अयोग्य ठहराते हैं।
अतिरिक्त विवरण
- कानूनी ढांचा: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) उम्मीदवारों की पात्रता की रूपरेखा तैयार करता है। प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:
- धारा 8(1) और 8(2): आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों में दोषी पाए गए व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करता है।
- धारा 8(3): दो वर्ष या उससे अधिक की सजा पाने वाले व्यक्ति रिहाई के बाद छह वर्ष तक अयोग्य हो जाते हैं।
- ऐतिहासिक निर्णय:
- लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013): महत्वपूर्ण सजा वाले अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए विधायकों के लिए तत्काल अयोग्यता स्थापित की गई।
- पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2018): राजनीति के गैर-अपराधीकरण की वकालत की गई लेकिन विधायी कार्रवाई को संसद के लिए स्थगित कर दिया गया।
- चुनाव आयोग की सिफारिशें: गंभीर आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों को नामांकन के चरण में प्रतिबंधित करने का सुझाव दिया गया।
दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की अनुमति देने के पक्ष में तर्क
- निर्दोषता की धारणा: "दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष" के सिद्धांत को कायम रखा गया है, तथा अपील के बाद ही अयोग्यता की वकालत की गई है।
- राजनीतिक प्रतिशोध: राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के लिए कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग के बारे में चिंताएं।
- प्रतिनिधित्व का अधिकार: उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगाने से मतदाताओं की पसंद सीमित हो सकती है, विशेष रूप से लोकप्रिय हस्तियों के लिए।
- न्यायिक विलंब: लम्बी कानूनी प्रक्रिया के कारण बरी होने का इंतजार कर रहे व्यक्तियों को अनुचित रूप से दंडित किया जा सकता है।
दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की अनुमति देने के विरुद्ध तर्क
- नैतिक और आचारिक मानक: लोकतांत्रिक अखंडता बनाए रखने के लिए नेताओं को उच्च नैतिक मानकों का पालन करना चाहिए।
- राजनीति का अपराधीकरण समाप्त करना: आपराधिक रिकॉर्ड वाले राजनेताओं की संख्या कम करने से भ्रष्टाचार कम हो सकता है।
- सार्वजनिक विश्वास का क्षरण: मतदाताओं का विश्वास बनाए रखने के लिए पद पर गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- वैश्विक लोकतांत्रिक मानदंड: कई लोकतंत्रों में शासन की अखंडता को बनाए रखने के लिए उम्मीदवारों की पात्रता के नियम कड़े हैं।
कार्यान्वयन में चुनौतियाँ
- कानूनों का दुरुपयोग: न्यायिक प्रणाली में राजनीतिक हेरफेर से झूठे आरोपों के माध्यम से प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाया जा सकता है।
- चुनाव सुधारों में विलंब: प्रस्तावित सुधारों पर विधायी निष्क्रियता प्रगति में बाधा डालती है।
- फास्ट-ट्रैक अदालतों की आवश्यकता: गंभीर आरोपों का सामना कर रहे राजनेताओं के लिए शीघ्र सुनवाई से न्याय सुनिश्चित हो सकता है और चुनावी अधिकारों को बरकरार रखा जा सकता है।
इस बात पर बहस कि क्या दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ना चाहिए, भारत के लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें चुनाव लड़ने के संवैधानिक अधिकार के साथ-साथ राजनीति में अपराध के ज्वलंत मुद्दे को संबोधित करना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक तत्वों को राजनीति में प्रवेश करने से रोकने के लिए उपाय शुरू किए हैं, लेकिन संसद के लिए प्रभावी ढंग से कानून बनाना महत्वपूर्ण है, ताकि चुनावी अधिकारों और नैतिक शासन के बीच संतुलन सुनिश्चित हो सके।
जीएस2/राजनीति
लोक लेखा समिति (पीएसी)
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
संसद की लोक लेखा समिति ने हाल ही में सरकार से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स को नियंत्रित करने वाले वर्तमान नियमों का पुनर्मूल्यांकन करने का आग्रह किया है।
- पीएसी भारत की संसद द्वारा गठित एक समिति है जो सरकारी राजस्व और व्यय के लेखा-परीक्षण पर केंद्रित है।
- यह अनुमोदित बजट के अनुसार सरकार के व्यय के संबंध में जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अतिरिक्त विवरण
- पीएसी का उद्देश्य: यह समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा तैयार की गई ऑडिट रिपोर्ट की संसद में प्रस्तुत किए जाने के बाद जांच करती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सत्यापित करना है कि संसद द्वारा आवंटित धन का सरकार द्वारा विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जा रहा है।
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 1921 में स्थापित, PAC भारत की सबसे पुरानी संसदीय समितियों में से एक है। शुरुआत में, वित्त सदस्य 1950 में भारत के संविधान के लागू होने तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे, जिसके बाद यह अध्यक्ष के नियंत्रण में एक संसदीय समिति बन गई।
- सदस्यता: पीएसी में अधिकतम 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और अधिकतम 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर प्रतिवर्ष किया जाता है।
- कार्य: समिति की जिम्मेदारियों में सरकारी व्यय के लिए संसद द्वारा आवंटित धन के विनियोजन का विवरण देने वाले खातों की समीक्षा करना, साथ ही वार्षिक वित्त खातों और अन्य प्रासंगिक वित्तीय रिपोर्टों की जांच करना शामिल है।
निष्कर्षतः, पीएसी सरकार की वित्तीय गतिविधियों की संसदीय निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करती है, तथा सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है।
जीएस2/राजनीति
सार और तत्व का सिद्धांत
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुष्टि की है कि केंद्र लॉटरी वितरकों पर सेवा कर नहीं लगा सकता। यह निर्णय इस बात पर जोर देता है कि लॉटरी पर कर लगाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों के पास है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि लॉटरी को जुआ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, न कि सेवा के रूप में।
- राज्यों और लॉटरी वितरकों के बीच संबंध क्रेता-विक्रेता के रूप में होता है, जिससे सेवा कर लागू नहीं होता।
- संविधान राज्य विधानसभाओं को लॉटरी पर कर लगाने का विशेष अधिकार प्रदान करता है।
- लॉटरी गतिविधियों पर सेवा कर लगाने के खिलाफ सिक्किम उच्च न्यायालय के 2012 के फैसले को बरकरार रखा गया।
अतिरिक्त विवरण
- राज्यों की विशेष कर लगाने की शक्ति: संविधान राज्य विधानसभाओं को लॉटरी सहित सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों पर कर लगाने का अधिकार देता है, जो प्रविष्टि 62 - सूची II के अंतर्गत आते हैं। केंद्र अपनी अवशिष्ट शक्तियों से इसे रद्द नहीं कर सकता।
- सार और तत्व का सिद्धांत: यह सिद्धांत किसी कानून के प्रमुख उद्देश्य को निर्धारित करने में मदद करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि यह अधिनियम बनाने वाली सरकार की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है या नहीं। यह कानून की वास्तविक प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करता है और केंद्र और राज्य विधायी शक्तियों के बीच संघर्षों को हल करता है।
- सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख मामलों, जैसे कि बॉम्बे राज्य बनाम एफ.एन. बलसारा (1951) और प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स (1947), में इस सिद्धांत को लागू किया गया है, ताकि छोटे विधायी ओवरलैप की अनुमति दी जा सके, जब तक कि प्राथमिक ध्यान संबंधित प्राधिकरण के भीतर बना रहे।
सिक्किम उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट करने से यह बात पुष्ट होती है कि लॉटरी लेनदेन की प्राथमिक प्रकृति जुआ है, इस प्रकार इन गतिविधियों को विनियमित करने और उन पर कर लगाने के लिए राज्यों के विशेष अधिकार की पुष्टि होती है।
पिछले वर्ष का प्रश्न (PYQ): [2016] भारत की संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है यदि उस आशय का प्रस्ताव पारित किया जाता है:
- (क) लोक सभा द्वारा अपनी कुल सदस्यता के साधारण बहुमत से
- (ख) लोक सभा द्वारा अपनी कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से
- (ग) राज्य सभा द्वारा अपनी कुल सदस्यता के साधारण बहुमत से
- (घ) राज्य सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा
जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध
अरब लीग ने ट्रम्प की गाजा पुनर्वास योजना को अस्वीकार कर दिया
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
अरब लीग ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की गाजा पुनर्वास योजना को अस्वीकार कर दिया है, इसे अस्वीकार्य माना है। यह निर्णय चल रहे इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष पर लीग के रुख को दर्शाता है और मध्य पूर्वी भू-राजनीति में शामिल जटिलताओं को उजागर करता है।
- अरब लीग मुख्य रूप से अरबी भाषी देशों से बना संगठन है।
- इसका गठन 1945 में काहिरा में हुआ था, तथा मूलतः इसके सदस्य देश 6 थे।
- लीग के मुख्य उद्देश्यों में सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना और उनकी संप्रभुता की रक्षा करना शामिल है।
अतिरिक्त विवरण
- गठन: 1945 में काहिरा में स्थापित अरब लीग की शुरुआत छह संस्थापक सदस्यों से हुई: मिस्र, इराक, ट्रांसजॉर्डन (अब जॉर्डन), लेबनान, सऊदी अरब और सीरिया, बाद में यमन इसमें शामिल हुआ।
- वर्तमान सदस्यता: लीग में अब 22 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें अल्जीरिया, बहरीन, मिस्र, फिलिस्तीन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
- पर्यवेक्षक का दर्जा: चार देशों को लीग में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है: ब्राजील, इरीट्रिया, भारत और वेनेजुएला।
- संगठनात्मक संरचना: लीग का सर्वोच्च निकाय परिषद है, जिसमें प्रत्येक सदस्य राज्य के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रत्येक राज्य के पास एक वोट होता है, और निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं।
- महासचिव के नेतृत्व में महासचिवालय, लीग के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करता है।
अरब लीग द्वारा ट्रम्प की योजना को अस्वीकार करना, सामूहिक अरब हितों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता तथा क्षेत्र में शांति प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करता है।
|
7 videos|3454 docs|1081 tests
|
















