UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 16th December 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download
GS1/भारतीय समाज
असमानता की डिजिटल सीमाएँ
स्रोत: द हिंदू

खबर में क्यों?
भारत की डिजिटल क्रांति, जिसमें 1.18 अरब मोबाइल कनेक्शन और 700 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता शामिल हैं, महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही है, विशेष रूप से तकनीक-संवर्धित लिंग आधारित हिंसा के संदर्भ में। इसके जवाब में, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 'अब कोई बहाना नहीं' अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य भारत में लिंग आधारित हिंसा से निपटना है। यह अभियान 25 नवंबर, 2024 को प्रारंभ हुआ और यह वैश्विक 16 दिवसीय सक्रियता के साथ मेल खाता है।
- डिजिटल विभाजन भारत में सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को बढ़ाता है।
- शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बेहतर डिजिटल पहुंच है।
- महिलाओं को डिजिटल तकनीकों तक पहुँचने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो उनके अवसरों को प्रभावित करता है।
- सरकारी पहलों का उद्देश्य डिजिटल विभाजन को समाप्त करना और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है।
अतिरिक्त विवरण
- शहरी-ग्रामीण भेदभाव: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल पहुंच में महत्वपूर्ण अंतर है। शहरी क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी और उच्च इंटरनेट स्पीड का लाभ मिलता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कठिनाइयाँ हैं, जो उनके डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को सीमित करती हैं।
- लिंग असमानता: डिजिटल लिंग विभाजन स्पष्ट है, जहाँ महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है जो डिजिटल तकनीकों तक पहुंच रखते हैं, जो उनके आर्थिक और शैक्षिक अवसरों को सीमित करता है, इस प्रकार मौजूदा सामाजिक असमानताओं को और मजबूती प्रदान करता है।
- आर्थिक असमानता: तकनीक तक सीमित पहुंच निम्न-आय समूहों को असमान रूप से प्रभावित करती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार करने और बढ़ती ऑनलाइन नौकरी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता पर बाधाएं आती हैं।
डिजिटल असमानता के परिणाम गहरे हैं, विशेष रूप से शिक्षा और रोजगार के अवसरों में। उन क्षेत्रों में जहाँ डिजिटल बुनियादी ढाँचा सीमित है, छात्र शैक्षणिक संसाधनों तक पहुँचने में संघर्ष करते हैं, जो COVID-19 महामारी के दौरान स्पष्ट हुआ। इसके अतिरिक्त, नौकरी के आवेदकों के बीच डिजिटल कौशल की कमी उनकी तकनीक-आधारित नौकरी के बाजार में रोजगार क्षमता को सीमित करती है।
महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है
- अधिकारों और गरिमा की रक्षा: महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करना उनके मौलिक अधिकारों का समर्थन करता है, जिससे वे समाज में बिना उत्पीड़न के संपूर्ण रूप से भाग ले सकें।
- आर्थिक विकास: महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा में सुधार वैश्विक जीडीपी को 18 अरब डॉलर तक बढ़ा सकता है, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके।
- लिंग आधारित हिंसा (GBV) का समाधान: महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों में वृद्धि से ऑनलाइन लिंग आधारित हिंसा से लड़ने के लिए मजबूत कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता है।
- सामाजिक स्थिरता और एकता: सुरक्षा की संस्कृति सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देती है, हिंसा के चक्रों को तोड़ती है, जिसमें पुरुष और लड़के सहायक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए सरकारी पहलकदमियाँ
- भारतनेट परियोजना: 2011 में शुरू की गई, यह 250,000 पंचायतों को उच्च गति के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने के लिए है, जिससे ग्रामीण इंटरनेट पहुँच में सुधार हो सके।
- राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन: 2014 में स्थापित, इसका उद्देश्य हर घर में कम से कम एक डिजिटल रूप से साक्षर व्यक्ति होना है।
- पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान: 2017 में शुरू किया गया, यह लगभग 60 मिलियन ग्रामीण Haushalts में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए है।
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम: 2015 में शुरू किया गया, यह कार्यक्रम भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने का प्रयास कर रहा है, जिसमें सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- इंटरनेट साथी कार्यक्रम: 2015 में शुरू किया गया एक सहयोग, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल कौशल से सशक्त बनाना है।
- DIKSHA प्लेटफार्म: 2017 में शुरू किया गया, यह स्कूल शिक्षा के लिए डिजिटल संसाधन प्रदान करता है, जिससे शैक्षणिक सामग्री तक समान पहुँच को बढ़ावा मिलता है।
डिजिटल विभाजन को पाटने की रणनीतियाँ
- संरचना निवेश: ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड संरचना का विस्तार करना समान इंटरनेट पहुँच के लिए आवश्यक है।
- डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम: व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और हाशिए के समूहों को ऑनलाइन स्थानों में सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए कौशल प्रदान करने हेतु व्यापक पहलों की आवश्यकता है।
- शिक्षा में प्रौद्योगिकी का समावेश: स्कूलों को अपने पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण शामिल करना चाहिए, और सामुदायिक कार्यशालाएँ वयस्कों को शिक्षित कर सकती हैं।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी: तकनीकी कंपनियों के साथ सहयोग संसाधनों के आवंटन को बढ़ा सकता है ताकि डिजिटल विभाजन को पाटा जा सके।
- राष्ट्रीय जागरूकता अभियान: अभियानों का उद्देश्य समाज में प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रति दृष्टिकोण बदलना होना चाहिए, विशेष रूप से महिलाओं और हाशिए के समुदायों के लिए।
अंत में, डिजिटल असमानता को संबोधित करना समावेशी विकास को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि समाज के सभी सदस्य डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रभावी ढंग से भाग ले सकें।
GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी
खोज और बचाव सहायता उपकरण (SARAT)

खबर में क्यों?
भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवाएँ (INCOIS), जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) का हिस्सा है, ने अपने खोज और बचाव सहायता उपकरण (SARAT) का उन्नत संस्करण लॉन्च किया है, जिससे समुद्र में संकटग्रस्त व्यक्तियों और जहाजों की पहचान करने की क्षमताएँ बढ़ाई गई हैं।
मुख्य बातें
- SARAT को 2016 में खोज और बचाव अभियानों में सहायता के लिए शुरू किया गया था।
- यह उपकरण लापता वस्तुओं की पहचान में सटीकता बढ़ाने के लिए उन्नत मॉडल एन्सेम्बलिंग तकनीकों का उपयोग करता है।
- संस्करण 2 में बेहतर दृश्यांकन और खोज क्षेत्र की गणनाओं में सुधार शामिल है।
- मॉडल एन्सेम्बलिंग: यह दृष्टिकोण प्रारंभिक स्थान और वस्तु के आखिरी ज्ञात समय में अनिश्चितताओं पर विचार करता है, जिससे सटीक स्थान की संभावना बढ़ती है।
- पर्यावरणीय कारक: लापता वस्तुओं की गति मुख्यतः धाराओं और हवाओं से प्रभावित होती है, जिन्हें क्षेत्रीय महासागर मॉडलिंग प्रणाली के उच्च-रिज़ॉल्यूशन डेटा का उपयोग करके मॉडल किया जाता है।
- उपयोगकर्ता इंटरैक्शन: उपयोगकर्ता एक इंटरैक्टिव मानचित्र पर वस्तु के आखिरी देखे गए बिंदु को निर्दिष्ट कर सकते हैं या आखिरी ज्ञात स्थिति का अनुमान लगाने के लिए एक तटीय स्थान चुन सकते हैं।
- संवाद: परिणाम तटीय राज्यों की स्थानीय भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं, जिससे यह स्थानीय मछुआरों के लिए सुलभ होता है।
- उन्नत संस्करण खोज क्षेत्र के विस्तार को आखिरी ज्ञात स्थिति के चारों ओर केंद्रित करके सुधारता है, जिससे उपकरण की प्रभावशीलता बढ़ती है।
- नए दृश्यात्मक फीचर्स में खोज क्षेत्रों के लिए रंग कोडिंग और आखिरी ज्ञात स्थिति को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए मार्कर्स शामिल हैं।
SARAT में किए गए सुधारों का उद्देश्य खोज और बचाव अभियानों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है, यह सुनिश्चित करना कि संकटग्रस्त व्यक्तियों को यथाशीघ्र खोजा जा सके।
GS2/राजनीति
अखिल भारतीय नागरिक संहिता: अंबेडकर और के. एम. मुंशी के दृष्टिकोण
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
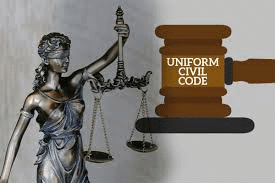
खबर में क्यों?
हाल ही में, प्रधानमंत्री ने एक अखिल भारतीय नागरिक संहिता (UCC) के लिए पुनः कॉल किया, जिसमें संविधान सभा की चर्चाओं से डॉ. बी. आर. अंबेडकर और के. एम. मुंशी के विचारों का उल्लेख किया गया।
- UCC का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक सामान्य सेट प्रदान करना है, जो उनके धर्म की परवाह किए बिना लागू होता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 UCC की स्थापना का आदेश देता है।
- भारत में विभिन्न व्यक्तिगत कानून मौजूद हैं, जिनमें हिंदुओं और मुसलमानों के लिए कानून शामिल हैं, जो वर्तमान में एकल कानूनी ढांचे के अंतर्गत नहीं आते।
- अखिल भारतीय नागरिक संहिता (UCC): संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत परिकल्पित, UCC का उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों पर समान धर्मनिरपेक्ष नागरिक कानून लागू करना है, जिसमें विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- हिंदू व्यक्तिगत कानून: 1956 में संहिताबद्ध, ये कानून हिंदुओं के लिए लागू होते हैं, जिसमें सिख, जैन और बौद्ध शामिल हैं। इनमें हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आदि शामिल हैं।
- मुस्लिम व्यक्तिगत कानून: 1937 के शरियत कानून द्वारा शासित, ये कानून धार्मिक अधिकारियों द्वारा राज्य हस्तक्षेप के बिना व्याख्यायित होते हैं।
- महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप: विशेष विवाह अधिनियम (1954) विभिन्न धर्मों में नागरिक विवाह की अनुमति देता है। शाह बानो (1985) और सारला मुदगल (1995) जैसे महत्वपूर्ण मामलों ने UCC की आवश्यकता को मजबूती से स्थापित किया है।
के. एम. मुंशी ने UCC पर क्या कहा
- UCC का समर्थन: 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा की बहस के दौरान, मुंशी ने UCC के पक्ष में तर्क किया, और इसे अल्पसंख्यकों के लिए दमनकारी मानने के डर को खारिज किया।
- महिलाओं के लिए समानता: मुंशी ने बताया कि UCC की कमी व्यक्तिगत मामलों में महिलाओं के लिए असमान अधिकारों को बढ़ावा देती है, विशेष रूप से हिंदू कानून में।
- राष्ट्रीय एकता: उन्होंने तर्क किया कि सामाजिक और नागरिक मामलों में समान नियम राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देंगे, यह सुझाव देते हुए कि धर्म केवल आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करना चाहिए।
अंबेडकर ने UCC के बारे में क्या कहा
- अनुच्छेद 44 का समर्थन: अंबेडकर ने बहस के दौरान अनुच्छेद 44 के महत्व पर जोर दिया, UCC के लिए समर्थन करते हुए इसके विशिष्ट विवरणों में गहराई से नहीं गए।
- धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों को चुनौती देना: उन्होंने इस दृष्टिकोण के खिलाफ तर्क किया कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून अपरिवर्तनीय हैं और विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तिगत कानूनों में ऐतिहासिक लचीलापन का उल्लेख किया।
- राज्य शक्ति और व्यक्तिगत कानून: अंबेडकर ने तर्क किया कि व्यक्तिगत कानूनों को राज्य सुधार के अधीन होना चाहिए ताकि भेदभाव और असमानताओं को कम किया जा सके।
बहस के अंत में क्या हुआ?
- अनुच्छेद 44 का पारित होना: विस्तृत चर्चाओं के बाद, अनुच्छेद 44 पारित हुआ, जो भारत में UCC के लिए निर्देश स्थापित करता है।
- पुनः क्रमांकन: प्रारंभ में अनुच्छेद 35 था, जिसे बाद में अनुच्छेद 44 में पुनः क्रमांकित किया गया, जो व्यक्तिगत मामलों पर कानूनों का मार्गदर्शक राज्य नीति का सिद्धांत बना हुआ है।
GS3/पर्यावरण
केर्च जलडमरूमध्य के बारे में मुख्य तथ्य
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
खबर में क्यों?
हाल ही में एक गंभीर तूफान के दौरान एक रूसी तेल टैंकर के टूटने से केर्च जलडमरूमध्य में एक बड़ा तेल रिसाव हुआ। यह घटना क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों से जुड़ी पर्यावरणीय खतरों को उजागर करती है।
- केर्च जलडमरूमध्य काला सागर को आज़ोव सागर से जोड़ता है।
- इसका ऐतिहासिक महत्व है, इसे पहले सिम्मेरियन बॉस्फोरस के नाम से जाना जाता था।
- केर्च जलडमरूमध्य एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है, जो वैश्विक व्यापार के लिए आवश्यक है।
- यह क्षेत्र 2014 से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष का केंद्र रहा है।
- केर्च जलडमरूमध्य पुल, जो 2018 में पूरा हुआ, क्रीमिया पर रूस के अधिग्रहण का प्रतीक है।
- भौगोलिक विशेषताएँ: केर्च जलडमरूमध्य लगभग 3 किमी लंबा, 15 किमी चौड़ा और 18 मीटर गहरा है। इसका सबसे संकीर्ण बिंदु, जो चूष्का भूमि की नोक पर स्थित है, केवल तीन से पांच किलोमीटर चौड़ा है।
- प्रमुख शहर: केर्च का शहर जलडमरूमध्य के केंद्र के पास क्रीमियाई पक्ष पर स्थित है, जो शिपिंग और व्यापार के लिए एक प्रमुख स्थान है।
- पर्यावरणीय प्रभाव: हालिया तेल रिसाव केर्च जलडमरूमध्य की पारिस्थितिकी स्वास्थ्य के लिए चिंताएँ उत्पन्न करता है, जो समुद्री जीवन और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है।
यह घटना केर्च जलडमरूमध्य के रणनीतिक महत्व को उजागर करती है, न केवल एक शिपिंग मार्ग के रूप में, बल्कि एक विवादास्पद भू-राजनीतिक क्षेत्र के रूप में भी। पर्यावरणीय घटनाओं की निरंतर निगरानी और प्रतिक्रिया क्षेत्र की पारिस्थितिकी की अखंडता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है।
फायरफ्लाई स्पार्कल गैलेक्सी
स्रोत: मनी कंट्रोल
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) ने हाल ही में फायरफ्लाई स्पार्कल नामक एक दुर्लभ गैलेक्सी की पहचान की है, जो प्रारंभिक गैलेक्सी गठन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। यह खोज खगोलीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड की स्थितियों पर प्रकाश डालती है।
- JWST द्वारा खोजी गई यह गैलेक्सी लगभग 600 मिलियन वर्ष बाद की है जब बिग बैंग हुआ था। इसे सबसे प्रारंभिक निम्न-मास गैलेक्सियों में से एक के रूप में पहचाना गया है, जो गैलेक्सियों के गठन के बारे में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
- गैलेक्सी के तारे समूह चमकीली रोशनी उत्सर्जित करते हैं, जो फायरफ्लाई की तरह लगते हैं, इसी कारण इसे यह नाम मिला।
- द्रव्यमान: फायरफ्लाई स्पार्कल गैलेक्सी का द्रव्यमान 10 मिलियन सूर्यों के बराबर है, जो इसे एक निम्न-मास गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत करता है।
- आकार: इसका दृश्य भाग केवल 1,000 प्रकाश वर्ष फैला है, जो मिल्की वे के 100,000 प्रकाश वर्ष से काफी छोटा है।
- तारे समूह: इसमें 10 विशिष्ट तारे समूह हैं, जो तारे निर्माण के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- यह फायरफ्लाई-बेहतर दोस्त और फायरफ्लाई-नए बेहतर दोस्त नामक दो छोटे गैलेक्सियों के साथ है, और इसका आकार एक लंबी बूंद जैसा है, जो निर्माण प्रक्रियाओं को दर्शाता है।
JWST द्वारा अवलोकन अध्ययन
- JWST ने गैलेक्सी की रोशनी को 16-26 गुना बढ़ाने के लिए गुरुत्वाकर्षण लेनसिंग का उपयोग किया, जिससे विस्तृत अवलोकन संभव हुआ।
- टेलीस्कोप ने तारे निर्माण के विभिन्न चरणों का अवलोकन किया, जिसमें युवा तारे नीले और पुराने तारे लाल दिखाई देते हैं।
- गैलेक्सी में प्रत्येक तारे समूह एक अलग निर्माण चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो गैलेक्सी विकास की हमारी समझ में योगदान करता है।
- यह खोजें गैलेक्सी गठन और प्रारंभिक ब्रह्मांड में तारे समूहों की गतिशीलता के संबंध में मौजूदा सिद्धांतों को परिष्कृत करने में मदद करती हैं।
यह खोज JWST की क्षमताओं को उजागर करती है, जो ब्रह्मांड के आरंभिक काल का अन्वेषण करता है और यह हमारी समझ को बढ़ाता है कि कैसे आकाशगंगाएँ, जिसमें हमारी खुद की मिल्की वे भी शामिल है, बन सकती हैं।
राजनीतिक दलों पर POSH अधिनियम का कार्यान्वयन
स्रोत: द हिंदू

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर विचार किया है, जो राजनीतिक दलों पर 2013 के महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, जिसे आमतौर पर POSH अधिनियम कहा जाता है, के लागू होने की मांग करती है। याचिकाकर्ता ने राजनीतिक दलों के भीतर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समितियों (ICCs) की उपस्थिति में असमानताएँ बताईं। इसके बाद, अदालत ने याचिकाकर्ता को भारत के चुनाव आयोग (ECI) से संपर्क करने के लिए कहा, जिसे उसने POSH अधिनियम के अनुपालन के लिए राजनीतिक दलों को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण माना। इस मामले ने POSH अधिनियम के राजनीतिक दलों पर लागू होने के बारे में बहस को जन्म दिया है, जो अक्सर पारंपरिक कार्यस्थल संरचनाओं से मेल नहीं खाते।
- सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दलों पर POSH अधिनियम के लागू होने की जांच कर रहा है।
- राजनीतिक संगठनों के भीतर आंतरिक शिकायत समितियों (ICCs) के बारे में असंगतताएँ हैं।
- ECI को राजनीतिक दलों के बीच POSH अधिनियम के अनुपालन को लागू करने के लिए एक प्रमुख प्राधिकरण के रूप में देखा जा रहा है।
- POSH अधिनियम 2013: यह कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और एक सुरक्षित कार्यस्थल वातावरण बनाने के लिए है। इसे 1997 के सुप्रीम कोर्ट के मामले, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में स्थापित विशाखा दिशानिर्देशों से प्रेरणा मिली।
- POSH अधिनियम का धारा 3(1): यह धारा कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें \"कार्यस्थल\" को सार्वजनिक और निजी संगठनों, अस्पतालों और घरों जैसे विभिन्न सेटिंग्स में व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, लेकिन राजनीतिक दलों पर इसका अनुप्रयोग अस्पष्ट है।
- कानूनी चुनौतियाँ: केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राजनीतिक दल \"कार्यस्थल\" की परिभाषा में नहीं आते, क्योंकि उनमें पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होता, इस प्रकार ICCs की आवश्यकता नहीं होती।
- अनुप्रयोग में चुनौतियाँ: राजनीतिक दलों की गैर-पारंपरिक संरचना ICCs स्थापित करने के लिए \"नियोक्ता\" की पहचान को जटिल बनाती है, और पार्टी कार्यकर्ताओं के पास अक्सर कोई निर्धारित कार्यस्थल नहीं होता।
- वर्तमान आंतरिक तंत्र: राजनीतिक दलों के पास आंतरिक अनुशासन समितियाँ हैं, लेकिन वे POSH अधिनियम द्वारा आवश्यक यौन उत्पीड़न को विशेष रूप से संबोधित नहीं करतीं।
अंत में, जबकि POSH अधिनियम का उद्देश्य विभिन्न कार्यस्थलों में महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाना है, इसका राजनीतिक दलों पर लागू होना महत्वपूर्ण कानूनी और संरचनात्मक चुनौतियों को प्रस्तुत करता है। यह राजनीतिक संगठनों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानूनों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता को उजागर करता है।
कार्बन बाजारों की समझ
स्रोत: भारतीय एक्सप्रेस
हाल ही में बाकू, अज़रबाइजान में आयोजित COP29 सम्मेलन ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन बाजारों का उपयोग करने के बारे में चर्चा को फिर से जीवित कर दिया है। सम्मेलन ने अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार स्थापित करने के लिए मानकों को मंजूरी दी है, जो अगले वर्ष के भीतर हो सकता है।
- कार्बन बाजार कार्बन उत्सर्जन अधिकारों की ख़रीद-फरोख्त की सुविधा प्रदान करते हैं।
- कार्बन क्रेडिट को 1,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की अनुमति देने वाले परमिट के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- ये बाजार आर्थिक प्रोत्साहनों के माध्यम से पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखते हैं।
- कार्बन बाजार: एक प्रणाली जो संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट व्यापार करने की अनुमति देती है, जहाँ सरकारें उन प्रमाणपत्रों को जारी करती हैं जो निश्चित मात्रा में कार्बन उत्सर्जन की अनुमति देते हैं। यह प्रणाली उपलब्ध क्रेडिट की संख्या को सीमित करके कुल कार्बन उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करती है।
- कार्बन ऑफसेट: इन्हें कंपनियाँ अपने उत्सर्जन के लिए मुआवजे के रूप में खरीदती हैं, अक्सर वृक्षारोपण जैसे परियोजनाओं को वित्तपोषित करके जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं।
- कार्बन बाजारों के लाभ:
- बाजार कीमतों में प्रदूषण की लागत को शामिल करके बाहरी प्रभावों को संबोधित करता है।
- कंपनियों को उत्सर्जन कम करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- बेहतर प्रौद्योगिकी और ढांचों के माध्यम से कार्बन लेखांकन को बढ़ाता है।
- व्यवसायों को व्यापार के माध्यम से अपने उत्सर्जन का प्रबंधन करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है।
- कार्बन बाजारों की चुनौतियाँ:
- सरकारी हस्तक्षेप बाजार की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकता है।
- अनुपालन की कमी और धोखाधड़ी हो सकती है, जिसके लिए सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता होती है।
- कुछ फर्में कार्बन ऑफसेट में सतही निवेश कर सकती हैं।
- छोटी कंपनियाँ उत्सर्जन की निगरानी में कठिनाई महसूस कर सकती हैं।
- विविध उत्पादन प्रक्रियाएँ समान कार्बन बजट स्थापित करने में जटिलता उत्पन्न करती हैं।
- बाह्यताओं को संबोधित करता है, जो बाजार की कीमतों में प्रदूषण की लागत को शामिल करता है।
- कंपनियों को उत्सर्जन में कमी लाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- बेहतर प्रौद्योगिकी और ढांचों के माध्यम से कार्बन लेखांकन को बढ़ाता है।
- व्यवसायों को व्यापार के माध्यम से अपने उत्सर्जन को प्रबंधित करने की लचीलापन प्रदान करता है।
- सरकारी हस्तक्षेप बाजार की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकता है।
- अनुपालन और धोखाधड़ी हो सकती है, जिसके लिए कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता होती है।
- कुछ कंपनियां कार्बन ऑफसेट्स में सतही निवेश कर सकती हैं।
- छोटी कंपनियां उत्सर्जन की निगरानी में संघर्ष कर सकती हैं।
- विविध उत्पादन प्रक्रियाएं समान कार्बन बजट स्थापित करने में जटिलता उत्पन्न करती हैं।
संक्षेप में, जबकि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में आशाजनक होते हैं क्योंकि यह उत्सर्जन में कमी के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, वे महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना भी करते हैं जिन्हें उनके प्रभावी होने को सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधित करना आवश्यक है।
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार
स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया
हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया, जो ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है।
- राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा मंत्रालय ऊर्जा के तहत आयोजित किया जाता है।
- यह पुरस्कार 1991 में स्थापित किया गया था और यह राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के साथ मेल खाता है, जिसे 14 दिसंबर को मनाया जाता है।
- इन पुरस्कारों का उद्देश्य उन संगठनों को मान्यता देना है जिन्होंने ऊर्जा खपत को सफलतापूर्वक कम किया है जबकि संचालन दक्षता में सुधार किया है।
- चयन प्रक्रिया: पुरस्कार समिति, जिसके अध्यक्ष सचिव (ऊर्जा) होते हैं, पुरस्कारों के लिए योग्य क्षेत्रों का आकलन करती है।
- आवेदन एक तकनीकी समिति द्वारा समीक्षा की जाती है, जिसमें रेलवे मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जैसे विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- मूल्यांकन के बाद, अंतिम स्वीकृति के लिए पुरस्कार समिति को सिफारिशें की जाती हैं।
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो: 1 मार्च 2002 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत स्थापित, BEE का मिशन आत्म-नियमन और बाजार के सिद्धांतों पर जोर देने वाली नीतियों का विकास करना है।
मुख्य लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करना है। BEE नामित उपभोक्ताओं और संगठनों के साथ संसाधनों का प्रभावी ढंग से अनुकूलन करने के लिए सहयोग करता है।
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों की ऊर्जा स्थिरता और संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
संगानेर ओपन एयर जेल
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त आयुक्त संगानेर ओपन जेल का दौरा करने वाले हैं, जो भारत की सबसे बड़ी जेलों में से एक है, यह विवाद के बाद है जिसमें राजस्थान सरकार की योजना एक अस्पताल बनाने की है जो वर्तमान में जेल द्वारा अधिग्रहित भूमि पर है। 25 नवंबर को हुई सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने आयुक्त को स्थल का निरीक्षण करने और चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया।
- संगानेर ओपन जेल भूमि उपयोग के विवाद का केंद्र है।
- सुप्रीम कोर्ट जेल के क्षेत्र के संरक्षण को सुनिश्चित करने में शामिल है, जबकि प्रस्तावित विकास हो रहे हैं।
- ओपन जेलें कैदियों की पुनर्वास में मदद के लिए कम सुरक्षा और बढ़ी हुई स्वतंत्रता प्रदान करती हैं।
- ओपन जेल: ओपन सुधार संस्थान पात्र कैदियों को पारंपरिक जेलों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जो उनके पुनर्वास में मदद करता है। राज्य सरकारें इन सुविधाओं के लिए नियम निर्धारित करती हैं, जो कैदी के व्यवहार और अपराध की प्रकृति जैसे कारकों पर आधारित होते हैं।
- भारत में ओपन जेलों का इतिहास: स्वतंत्र भारत में पहली ओपन जेल 1949 में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी। यह अवधारणा न्यायमूर्ति मुल्ला समिति की सिफारिशों के साथ लोकप्रिय हुई, जिसने बताया कि केवल कुछ राज्यों में ओपन जेलों के लिए कानूनी ढांचा था।
- वर्तमान स्थिति: 2022 तक, भारत के 17 राज्यों में 91 ओपन जेलें हैं, जिनमें राजस्थान में सबसे अधिक संख्या (41) है।
- संगानेर ओपन जेल की विशेषताएँ: यह सुविधा, जो 1963 में स्थापित हुई, कैदियों को अपने परिवार के साथ रहने और आत्मनिर्भर बनने की अनुमति देती है, जिससे वे सामुदायिक नौकरियों के माध्यम से अपने घरों और वित्त का प्रबंधन कर सकें।
- सुप्रीम कोर्ट का पूर्व निर्देश: मई 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ओपन जेलों के लिए निर्धारित क्षेत्रों को कम नहीं किया जाना चाहिए, उनके सुधारात्मक प्रणाली में महत्व को रेखांकित करते हुए।
संगानेर खुली जेल में चल रहे विकास यह दर्शाते हैं कि समुदाय स्वास्थ्य पहलों और कैदियों के पुनर्वास की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी का परिणाम इस अद्वितीय सुधारात्मक सुविधा के भविष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा।
जैतून रिडले कछुए
जैतून रिडले कछुओं के शवों को उनके प्रजनन मौसम के दौरान विशाखापत्तनम तट पर पाया गया है। पर्यावरण विशेषज्ञ इन मौतों के अधिकांश मामलों को समुद्री प्रदूषण और मछली पकड़ने के लिए ट्रॉव्लिंग गतिविधियों से जोड़ते हैं।
- जैतून रिडले कछुआ (वैज्ञानिक नाम: Lepidochelys olivacea) दुनिया में सबसे छोटा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला समुद्री कछुआ प्रजाति है।
- आकार: जैतून रिडले कछुए आमतौर पर लगभग 2 फीट लंबाई तक बढ़ते हैं और उनका वजन लगभग 50 किलोग्राम होता है।
- आवास: इन्हें प्रशांत, अटलांटिक और भारतीय महासागरों के गर्म और उष्णकटिबंधीय जल में पाया जाता है।
- आकृति: उनका नाम उनके जैतून के रंग के कवच से आता है, जो दिल के आकार का और गोल होता है।
- मांसाहारी आहार: उनका आहार मुख्य रूप से जेलीफिश, झींगे, घोंघे, केकड़े, मोलस्क, विभिन्न मछलियाँ और उनके अंडे शामिल हैं।
विशिष्ट व्यवहार
- अरिबादा: यह शब्द जैतून रिडले कछुओं के अद्वितीय सामूहिक घोंसला बनाने के व्यवहार को दर्शाता है, जहां हजारों मादाएँ एक ही समुद्र तट पर अपने अंडे देती हैं।
- घोंसला बनाने के स्थान: भारत में उड़ीसा का तट सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला बनाने का स्थान है, जबकि अन्य महत्वपूर्ण स्थल मेक्सिको और कोस्टा रिका में हैं।
- भारत में प्रमुख घोंसला बनाने के स्थानों में शामिल हैं:
- उड़ीसा: गहिरामथा समुद्र तट, रुशिकुल्या नदी का मुहाना, और देवी नदी का मुहाना।
- आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और अंडमान और निकोबार द्वीप।
- उड़ीसा: गहिरमथा समुद्र तट, रुशिकुल्या नदी का मुहाना, और देवी नदी का मुहाना।
- आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और अंडमान और निकोबार द्वीप।
जीवित चक्र
- अंडा देना: मादा ऑलिव रिडले कछुए अपने अंडों को مخروطीय घोंसले में देती हैं, जो लगभग 1.5 फीट गहरे होते हैं, जिन्हें वे अपनी पिछली पंखों से खोदती हैं।
- हैचिंग: अंडों से निकलने की अवधि लगभग 45-65 दिन होती है, जिसके बाद छोटे कछुए बाहर आते हैं और महासागर की ओर बढ़ते हैं।
- जीवित रहने की दर: केवल लगभग 1,000 में से 1 छोटे कछुए वयस्कता तक पहुंचते हैं।
संरक्षण स्थिति
- ऑलिव रिडले कछुआ वर्तमान में IUCN लाल सूची में कमजोर के रूप में वर्गीकृत है, विभिन्न खतरों के कारण, जिनमें निवास का नुकसान, प्रदूषण, और शिकार शामिल हैं।
संक्षेप में, ऑलिव रिडले कछुआ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यह ऐसे महत्वपूर्ण खतरों का सामना कर रहा है जो इसकी जीवित रहने की संभावनाओं को खतरे में डालते हैं। इस प्रजाति और उसके आवासों की सुरक्षा के लिए संरक्षण प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं।
|
7 videos|3454 docs|1081 tests
|
FAQs on UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 16th December 2024 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly
| 1. असमानता की डिजिटल सीमाएँ क्या हैं और यह समाज को कैसे प्रभावित करती हैं? |  |
| 2. खोज और बचाव सहायता उपकरण (SARAT) का क्या महत्व है? |  |
| 3. अखिल भारतीय नागरिक संहिता के तहत अंबेडकर और के. एम. मुंशी के दृष्टिकोण क्या हैं? |  |
| 4. केर्च जलडमरूमध्य के बारे में क्या जानना चाहिए? |  |
| 5. फायरफ्लाई स्पार्कल गैलेक्सी का क्या महत्व है? |  |















