UPSC Daily Current Affairs(Hindi)- 1st October 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download
GS3/अर्थव्यवस्था
भारत को रोजगार के जाल से बचने के लिए दुगना विकास चाहिए
 समाचार में क्यों?
समाचार में क्यों?
हाल ही में, मॉर्गन स्टेनली, एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी, ने भारत के लिए अपनी विकास दर को लगभग दोगुना करने की तात्कालिक आवश्यकता को उजागर किया है ताकि बढ़ती रोजगार मांगों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके और अधरोजगार (underemployment) को कम किया जा सके। विश्लेषण में बताया गया है कि एक स्थिर बेरोजगारी दर के लिए औसत GDP विकास दर 7.4% होनी चाहिए, यदि श्रम भागीदारी स्थिर रहती है। यदि श्रम भागीदारी 63% तक बढ़ती है, तो 9.3% की विकास दर आवश्यक है। बेरोजगारी को महत्वपूर्ण रूप से कम करने के लिए विकास दर को 12.2% तक पहुंचाना होगा। वर्तमान में, भारत की GDP विकास दर पिछले एक दशक में औसतन 6.1% है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 6.5% की विकास दर का अनुमान लगा रहा है, हालाँकि हालिया आंकड़े अप्रैल-जून 2025 की तिमाही के लिए 7.8% की मजबूत वृद्धि को दर्शाते हैं।
मुख्य निष्कर्ष
- भारत की युवा बेरोजगारी दर बेहद चिंताजनक रूप से उच्च है, जबकि यह सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
- भारतीय बेरोजगारी दर 5.1% है, लेकिन 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए यह दर 14.6% है, जो काफी अधिक है।
- शहरी क्षेत्रों में युवा महिलाओं की बेरोजगारी 25.7% तक पहुँच गई है, जो युवा शहरी पुरुषों की तुलना में अधिक है।
- 28.4 वर्ष की माध्य आयु के साथ जनसांख्यिकीय दबाव युवा जनसंख्या और नौकरी सृजन के बीच असंतुलन का कारण बन रहे हैं।
- भारत की श्रम शक्ति अगले दशक में 8.4 करोड़ बढ़ने की उम्मीद है, जिससे नौकरी सृजन की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है।
अतिरिक्त विवरण
- कमज़ोर रोजगार सृजन: हाल के वर्षों में रोजगार सृजन सुस्त रहा है, जिसमें मामूली सुधार देखे गए हैं। हालांकि, अगले दशक में औसत जीडीपी वृद्धि 6.5% रहने की उम्मीद है, यह आवश्यक रोजगार सृजन के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता।
- बेरोजगारी और अधेड़ रोजगार संकट: भारत उच्च बेरोजगारी और व्यापक अधेड़ रोजगार की दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है, जिसमें युवा बेरोजगारी 17.6% है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। कृषि में रोजगार वृद्धि कृषि की ओर लौटने का संकेत देती है, जो अक्सर अधेड़ रोजगार को दर्शाती है जहां कौशल का सही उपयोग नहीं हो रहा है।
- गरीबी और आर्थिक आपातकाल: लगभग 603 मिलियन भारतीय प्रतिदिन $3.65 की आय सीमा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो रोजगार सृजन और आर्थिक परिवर्तन की महत्वपूर्ण आवश्यकता को दर्शाता है ताकि सामाजिक अशांति को रोका जा सके।
- क्षेत्रीय संदर्भ: युवा बेरोजगारी केवल भारत में नहीं है; यह एशिया में एक व्यापक मुद्दा है, जहां युवा बेरोजगारी दर 16% है, जो अमेरिका में 10.5% से काफी अधिक है।
- भविष्य की चुनौतियाँ: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के संभावित अपनाने से नौकरियों में और कमी आ सकती है, जब तक कि निवेश और पुनः कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय सुधार लागू नहीं किए जाते।
- औद्योगिक और निर्यात वृद्धि: भारत का वैश्विक निर्यात में हिस्सा केवल 1.8% है, जो रोजगार सृजन के लिए पर्याप्त अनछुए संभावनाओं को दर्शाता है। आर्थिक वृद्धि के लिए औद्योगिक और निर्यात क्षेत्रों में तात्कालिक सुधार आवश्यक हैं।
संक्षेप में, जबकि भारत महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि के पथ पर है, यह रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए मजबूत उपाय लागू करना अत्यंत आवश्यक है, विशेष रूप से युवाओं के लिए। बिना इन परिवर्तनों के, देश बेरोजगारी और अधेड़ रोजगार के संकट को गहरा करने का जोखिम उठाता है, जिसका सामाजिक प्रभाव दूरगामी हो सकता है।
GS3/पर्यावरण
लेयते द्वीप और हालिया भूकंप
 क्यों समाचार में?
क्यों समाचार में?
हाल ही में फिलीपींस के लेयते द्वीप पर 6.7 की तीव्रता का भूकंप आया है, जिसने क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियों को उजागर किया और इसके स्थानीय जनसंख्या और अवसंरचना पर संभावित प्रभाव को रेखांकित किया।
- लेयते द्वीप विसायस द्वीप समूह का हिस्सा है और यह फिलीपींस का आठवां सबसे बड़ा द्वीप है।
- इस द्वीप में लेयते घाटी के रूप में जानी जाने वाली एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है।
- मुख्य शहरों में टैकलोबान और ओर्मोक शामिल हैं, जिसमें ओर्मोक में भू-तापीय विद्युत संयंत्र स्थित हैं।
- भूगोल: लेयते द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 7,056 वर्ग किलोमीटर है और इसकी तटरेखा 969 किलोमीटर है। यह सान जुआनिको जलडमरूमध्य द्वारा समर द्वीप से लगभग जुड़ा हुआ है, जो कुछ स्थानों पर केवल 2 किलोमीटर चौड़ा है। सान जुआनिको पुल, जिसकी लंबाई 2.16 किलोमीटर है, लेयते और समर के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
- इतिहास: 16वीं सदी के स्पेनिश खोजकर्ताओं द्वारा इसे टंडाया के रूप में जाना जाता था, लेयते की जनसंख्या 1900 के बाद तेजी से बढ़ी, विशेष रूप से लेयते और ओर्मोक घाटियों में। द्वीप द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 20 अक्टूबर 1944 को अमेरिकी बलों के द्वारा उतरे जाने के स्थान के रूप में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, जिसने लेयते की खाड़ी की लड़ाई के बाद जापानी बलों को बाहर निकाला।
- अर्थव्यवस्था: लेयते की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जिसमें किसान चावल, मक्का, नारियल और केले जैसी फसलें उगाते हैं। मछली पकड़ना भी स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द्वीप में मैंगनीज जैसे मूल्यवान खनिज हैं और यहाँ बालू और चूना पत्थर का सक्रिय खनन होता है।
लेयते द्वीप का हालिया भूकंप प्राकृतिक आपदाओं के प्रति तैयार रहने और सहनशीलता की आवश्यकता को रेखांकित करता है, विशेष रूप से इसके समृद्ध इतिहास और आर्थिक महत्व को देखते हुए।
GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध
वासेनार व्यवस्था
क्यों समाचार में?
वासेनार व्यवस्था वर्तमान में बादल प्रौद्योगिकी के विकसित परिदृश्य के लिए अपने निर्यात नियंत्रण उपायों के अनुकूलन से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रही है। इस स्थिति में इसके नियंत्रण सूचियों और प्रवर्तन तंत्रों में अद्यतन की आवश्यकता है।
- वासेनार व्यवस्था एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली है, जो पारंपरिक हथियारों और द्वि-उपयोग वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है।
- 1996 में स्थापित, यह व्यवस्था शीत युद्ध के दौरान की बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण समन्वय समिति का उत्तराधिकारी है।
- भारत ने 2017 में इस व्यवस्था में शामिल होकर अपनी सूचियों को अपने स्वयं के नियामक ढांचे के साथ समन्वित किया।
- उद्देश्य: यह व्यवस्था पारंपरिक हथियारों और द्वि-उपयोग वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है, ताकि अस्थिर करने वाली कार्रवाइयों को रोका जा सके।
- सदस्य देश: वर्तमान में वासेनार व्यवस्था में 42 सदस्य देश शामिल हैं।
- मुख्यालय: इस संगठन का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है।
- कार्यात्मक तंत्र: यह व्यवस्था नियमित रूप से प्रौद्योगिकी के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करती है, जो पारंपरिक और नाभिकीय-सक्षम दोनों होती है, सदस्य देशों के बाहर के देशों को बेची जाती है या इनसे मना की जाती है। इसमें सैन्य रूप से महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थों, प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं और उत्पादों की विस्तृत सूचियों को बनाए रखना शामिल है।
- यह सूचना का आदान-प्रदान प्रौद्योगिकी और सामग्री के उस आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर कर सकता है।
अंत में, वासेनार व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो हथियारों और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को नियंत्रित करती है, और इसे प्रभावी बने रहने के लिए आधुनिक तकनीकी प्रगति के अनुकूलित होना चाहिए।
GS2/शासन
NCRB डेटा बच्चों के खिलाफ अपराध पर
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने 2023 के लिए अपनी रिपोर्ट जारी की है, जो बच्चों के खिलाफ अपराधों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि को दर्शाती है, जो सुरक्षा उपायों और जागरूकता को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को प्रदर्शित करती है।
- 2023 में बच्चों के खिलाफ कुल 177,335 मामले दर्ज किए गए।
- यह 2022 की तुलना में 9.2% की वृद्धि दर्शाता है।
- अपराध दर एक लाख बच्चों की जनसंख्या पर 9 थी, जो 2022 में 36.6 थी।
- प्रमुख अपराध श्रेणियाँ:
- बच्चों का अपहरण और चोरी: 79,884 मामले (45%)
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम: 67,694 मामले (38.2%)
- बच्चों का अपहरण और चोरी: 79,884 मामले (45%)
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम: 67,694 मामले (38.2%)
- प्रवेशात्मक यौन उत्पीड़न:
- 40,434 मामलों में 40,846 पीड़ित प्रभावित हुए।
- इन मामलों में से 39,076 में अपराधी पीड़ितों के लिए जाने-पहचाने थे।
- 40,434 मामलों में 40,846 पीड़ित प्रभावित हुए।
- 39,076 में अपराधी पीड़ितों के लिए जाने-पहचाने थे।
- पीड़ितों की जनसांख्यिकी:
- 762 पीड़ित छह वर्ष से कम आयु के थे।
- 3,229 पीड़ित छह से 12 वर्ष की आयु के थे।
- 15,444 पीड़ित 12 से 16 वर्ष के बीच थे।
- 21,411 पीड़ित 16 से 18 वर्ष की आयु के थे।
- 762 पीड़ित छह वर्ष से कम आयु के थे।
- 3,229 पीड़ित छह से 12 वर्ष की आयु के थे।
- 15,444 पीड़ित 12 से 16 वर्ष के बीच थे।
- 21,411 पीड़ित 16 से 18 वर्ष की आयु के थे।
- अपहरण के आंकड़े:
- 79,884 IPC मामलों की रिपोर्ट, 82,106 बच्चों को प्रभावित किया।
- 58,927 से अधिक मामले सामान्य अपहरण के थे।
- 14,637 मामलों में विवाह के लिए नाबालिग लड़कियों का अपहरण शामिल था।
- 79,884 IPC मामलों की रिपोर्ट, 82,106 बच्चों को प्रभावित किया।
- 58,927 से अधिक मामले सामान्य अपहरण के थे।
- 14,637 मामलों में विवाह के लिए नाबालिग लड़कियों का अपहरण शामिल था।
- अन्य अपराध:
- बच्चों से जुड़े 1,219 हत्याएँ, जिनमें से 89 बलात्कार या POCSO उल्लंघनों से संबंधित थीं।
- 3,050 साधारण चोट के मामले और 373 आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले।
- बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत 6,038 मामले।
- बाल श्रम अधिनियम के तहत 1,390 मामले।
- 1,219 हत्याएँ बच्चों से जुड़ी, जिनमें से 89 बलात्कार या POCSO उल्लंघनों से संबंधित थीं।
- 3,050 साधारण चोट के मामले और 373 आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले।
- बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत 6,038 मामले।
- बाल श्रम अधिनियम के तहत 1,390 मामले।
- क्षेत्रीय अंतर्दृष्टियाँ:
- मध्य प्रदेश में कुल मामलों की संख्या 22,393 के साथ सबसे अधिक थी।
- असम (10,174 मामले) और बिहार (9,906 मामले) में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
- दिल्ली ने 7,769 मामले रिपोर्ट किए, जो इसकी जनसंख्या के सापेक्ष असमान दर को दर्शाता है।
- मध्य प्रदेश में कुल मामलों की संख्या 22,393 के साथ सबसे अधिक थी।
- असम (10,174 मामले) और बिहार (9,906 मामले) में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
- दिल्ली ने 7,769 मामले रिपोर्ट किए, जो इसकी जनसंख्या के सापेक्ष असमान दर को दर्शाता है।
- पुलिस जांच के परिणाम:
- चार्जशीटिंग दर 64.3% थी, लेकिन राज्यों के बीच में काफी भिन्नता थी।
- 2,57,756 की जांच की गई मामलों में से 1,12,290 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई।
- वर्ष के अंत में 80,198 मामले लंबित थे।
- चार्जशीटिंग दर 64.3% थी, लेकिन राज्यों के बीच में काफी भिन्नता थी।
- 2,57,756 की जांच की गई मामलों में से 1,12,290 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई।
- वर्ष के अंत में 80,198 मामले लंबित थे।
NCRB की रिपोर्ट भारत में बच्चों के खिलाफ अपराधों की गंभीर स्थिति को उजागर करती है, जो कमजोर जनसंख्या की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई और प्रणालीगत परिवर्तनों की आवश्यकता पर जोर देती है।
महिलाएँ श्रम बल में अधिक शामिल हो रही हैं, लेकिन क्या वे वास्तव में रोजगार में हैं?
महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी, जिसे महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) के रूप में संदर्भित किया जाता है, अक्सर लिंग समानता और आर्थिक सक्रियता का संकेतक माना जाता है। भारत में, FLFPR 2011-12 में 31.2% से घटकर 2017-18 में 23.3% हो गया था, लेकिन तब से 2023-24 में यह 41.7% तक बढ़ गया है। पहली नज़र में, यह वृद्धि आशाजनक लगती है; हालाँकि, गहरी विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि एक महत्वपूर्ण संख्या में महिलाएँ कृषि, अनपेक्षित घरेलू व्यवसायों, और कम वेतन वाली स्व-रोज़गार में प्रवेश कर रही हैं, बजाय इसके कि वे औपचारिक या स्थायी वेतन रोजगार प्राप्त कर सकें। इस प्रकार, जबकि अधिक महिलाएँ श्रम बाजार में मान्यता प्राप्त कर रही हैं, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और आय के स्तर या तो ठहरे हुए हैं या घट रहे हैं।
- FLFPR में तेज वृद्धि: 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गया।
- पहली बार उलटफेर: यह कई वर्षों की गिरावट के बाद FLFPR में पहली वृद्धि को चिह्नित करता है।
- निहित चिंता: भागीदारी में वृद्धि के बावजूद, आय में गिरावट आई है और सुरक्षित नौकरियाँ कम हैं।
- विरोधाभास: जबकि भागीदारी में वृद्धि हुई है, कृषि में वापसी हो रही है, सेवाओं या औद्योगिक क्षेत्रों में विविधीकरण के बजाय।
- ग्रामीण महिलाएँ प्रेरक: FLFPR में वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के कारण है।
- घरेलू कर्तव्यों से बदलाव: घरेलू कर्तव्यों का उल्लेख करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 2017-18 में 57.8% से घटकर 2023-24 में 35.7% हो गया।
- अनपेड सहायकों में वृद्धि: "घरेलू उद्यमों में सहायकों" के रूप में काम करने वाली महिलाओं का अनुपात 9.1% से बढ़कर 19.6% हो गया।
- स्व-रोज़गार में वृद्धि: "अपने खाता श्रमिक और नियोक्ता" की श्रेणी 4.5% से बढ़कर 14.6% हो गई।
- कृषि में प्रभुत्व: कृषि में काम करने वाली ग्रामीण महिलाओं का हिस्सा 2018-19 में 71.1% से बढ़कर 2023-24 में 76.9% हो गया।
- अन्य क्षेत्रों में गिरावट: औद्योगिक (द्वितीयक) और सेवा (तृतीयक) क्षेत्रों में महिलाओं की प्रतिनिधित्व में कमी आई है।
- सीमाओं का धुंधलापन: अनपेड घरेलू कार्य और घरेलू उद्यमों में सहायक भूमिकाओं के बीच ओवरलैप "रोजगार" की परिभाषा पर सवाल उठाता है।
- वास्तविक आय में गिरावट: विभिन्न नौकरी श्रेणियों में आय में गिरावट आई है, जिसमें स्व-रोज़गार, वेतनभोगी, और नियोक्ता शामिल हैं, केवल अस्थायी श्रमिकों को छोड़कर।
- स्व-रोज़गार की संवेदनशीलता: जबकि अधिक महिलाएँ स्व-रोज़गार में प्रवेश कर रही हैं, इससे आय में वृद्धि नहीं हुई है।
- वेतन में कोई विस्तार नहीं: FLFPR में वृद्धि ने सुरक्षित वेतन वाली नौकरियों में वृद्धि नहीं की है।
भारत में FLFPR में महत्वपूर्ण वृद्धि श्रम बाजार में गहरे मुद्दों को छुपाती है। महिलाएँ अक्सर अनपेक्षित या कम वेतन वाली भूमिकाओं में धकेल दी जाती हैं, विशेष रूप से कृषि और घरेलू उद्यमों में, जबकि उनकी वास्तविक आय लगातार घटती जा रही है। यह संकेत देता है कि भारत की आर्थिक वृद्धि महिलाओं के लिए सार्थक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित नहीं हो रही है। वास्तविक लिंग समानता के लिए, भागीदारी दर बढ़ाने के बजाय महिलाओं के काम की गुणवत्ता, सुरक्षा, और वेतन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। यह महिलाओं के लिए वास्तविक आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा।
PYQ प्रासंगिकता
[UPSC 2023] ‘देखभाल अर्थव्यवस्था’ और ‘मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था’ के बीच अंतर करें। देखभाल अर्थव्यवस्था को महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कैसे एकीकृत किया जा सकता है? लेख घरेलू भूमिकाओं से अनपेड सहायक पदों में महिलाओं के संक्रमण को उजागर करता है, जो सीधे देखभाल अर्थव्यवस्था को महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की चुनौती से जोड़ता है।
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन
भारत हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) की परिषद के भाग II के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है, जो इसके वैश्विक उड्डयन शासन में निरंतर संलग्नता को उजागर करता है।
- ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी।
- इस संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन को सुरक्षित और प्रभावी बनाना है।
- इसमें 193 सदस्य राज्य शामिल हैं, और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है।
- ICAO सभा: यह सभा हर तीन वर्ष में आयोजित होती है और ICAO का सर्वोच्च निकाय है, जिसमें शिकागो सम्मेलन के सभी 193 हस्ताक्षरकर्ता राज्य शामिल होते हैं।
- ICAO परिषद: यह 36 सदस्यों की होती है, जिन्हें सभा के दौरान 193 सदस्य राज्यों द्वारा चुना जाता है, और यह तीन वर्ष की अवधि के लिए शासन करती है।
- कार्य: ICAO नागरिक उड्डयन की सुरक्षा, सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए मानक और नियम निर्धारित करता है, जबकि नागरिक उड्डयन मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
- यह उड्डयन बाजारों को उदारीकरण करने और उड्डयन वृद्धि में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी मानकों की स्थापना के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रोत्साहित करता है।
अंत में, ICAO अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वायु परिवहन सभी सदस्य देशों के लिए सुरक्षित, प्रभावी और सतत बना रहे।
स्वावलंबी भारत में प्राकृतिक संसाधन - विकसित भारत 2047 के लिए एक स्तंभ
भारत का लक्ष्य 2047 तक एक विकसित भारत बनना है, जिसमें प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र पर स्वावलंबी भारत की प्राप्ति पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। वर्तमान में, यह क्षेत्र भारत के कुल आयात का 50% है, जो विदेशी संसाधनों पर एक महत्वपूर्ण निर्भरता को दर्शाता है।
- भारत की आयात निर्भरता महत्वपूर्ण है, विशेषकर तेल, तांबा और सोने जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए।
- भौगोलिक संसाधनों के बावजूद, भारत में आवश्यक खनिजों और हाइड्रोकार्बन्स के लिए आयात स्तर उच्च बना हुआ है।
- प्रभावी नीतिगत उपाय आयात को न्यूनतम करने और आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाने में मदद कर सकते हैं।
- भारत की आयात निर्भरता:
- तेल, सोना और तांबा भारत के कुल संसाधन आयात का 60% बनाते हैं।
- भारत लगभग 90% तेल, 95% तांबा और 99% से अधिक सोना आयात करता है।
- कोयला और बॉक्साइट का आयात शून्य तक कम किया जाना चाहिए, क्योंकि देश में महत्वपूर्ण भंडार उपलब्ध हैं।
- तेल, सोना और तांबा भारत के कुल संसाधन आयात का 60% बनाते हैं।
- भारत लगभग 90% तेल, 95% तांबा और 99% से अधिक सोना आयात करता है।
- कोयला और बॉक्साइट का आयात शून्य तक कम किया जाना चाहिए, क्योंकि देश में महत्वपूर्ण भंडार उपलब्ध हैं।
- प्राकृतिक संसाधनों की संभावनाएं: भारत भौगोलिक रूप से समृद्ध है और संसाधन समृद्ध क्षेत्रों जैसे ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के समान है। हालांकि, कई depósitos अभी भी कम खोजे गए हैं। सही नीतियों के साथ, भारत इन संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर सकता है ताकि आयात को कम किया जा सके।
- स्वावलंबन के लिए नीतिगत उपाय:
- बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) पर निर्भर रहने के बजाय छोटे अन्वेषण स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करना।
- खोज से खनन तक की प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए आत्म-प्रमाणन के माध्यम से कार्यान्वयन करना।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी और तकनीकी प्रवाह आमंत्रित करके निष्क्रिय खानों और कम प्रदर्शन करने वाली संपत्तियों को पुनर्जीवित करना।
- निजी क्षेत्रों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और निवेश को आकर्षित करने के लिए समान अवसरों का निर्माण करना।
- बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) पर निर्भर रहने के बजाय छोटे अन्वेषण स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करना।
- खोज से खनन तक की प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए आत्म-प्रमाणन के माध्यम से कार्यान्वयन करना।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी और तकनीकी प्रवाह आमंत्रित करके निष्क्रिय खानों और कम प्रदर्शन करने वाली संपत्तियों को पुनर्जीवित करना।
- निजी क्षेत्रों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और निवेश को आकर्षित करने के लिए समान अवसरों का निर्माण करना।
- सुझाए गए उपायों के लाभ:
- सामरिक संसाधनों के आयात पर निर्भरता को कम करना।
- संसाधन समृद्ध क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाना।
- बिना अतिरिक्त बजटीय समर्थन के सरकारी राजस्व में वृद्धि करना।
- खनन और संबंधित उद्योगों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
- प्राकृतिक संसाधन रणनीति को भारत के ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास के रोडमैप के साथ संरेखित करना, विकसित भारत 2047 की दिशा में।
- सामरिक संसाधनों के आयात पर निर्भरता को कम करना।
- संसाधन समृद्ध क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाना।
- बिना अतिरिक्त बजटीय समर्थन के सरकारी राजस्व में वृद्धि करना।
- खनन और संबंधित उद्योगों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
- प्राकृतिक संसाधन रणनीति को भारत के ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास के रोडमैप के साथ संरेखित करना, विकसित भारत 2047 की दिशा में।
अंत में, 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने और सच्चे स्वावलंबन को प्राप्त करने के लिए, भारत को प्राकृतिक संसाधनों के आयात पर अपनी निर्भरता को कम करना होगा। सक्रिय सुधारों को लागू करके और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र को मजबूत करके, भारत अपनी भौगोलिक संपत्ति को खोल सकता है, जो रणनीतिक आत्मनिर्भरता और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है, स्वावलंबी और विकसित भारत की दिशा में।
GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी
फॉल्स स्मट रोग क्या है?
 क्यों समाचार में?
क्यों समाचार में?
हालिया रिपोर्टों के अनुसार, पंजाब में धान की फसल, जो परिपक्वता और कटाई के चरण में है, फॉल्स स्मट रोग से गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, जिससे बड़े पैमाने पर कृषि क्षति हुई है।
- फॉल्स स्मट रोग का कारण कवक Ustilaginoidea virens है।
- इसे लक्ष्मी रोग या ऊथुपथि रोग के रूप में भी जाना जाता है।
- यह रोग मुख्य रूप से अनाज की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, न कि पौधे के अन्य भागों को।
- अनाज पर प्रभाव: फॉल्स स्मट से अनाज में चॉकनेस होती है, जिससे अनाज का वजन और बीज अंकुरण दोनों में कमी आती है।
- उत्पादकता हानि के कारक: संक्रमित पैनिकल्स का प्रतिशत और प्रत्येक पैनिकल में संक्रमण का स्तर उत्पादकता हानि में महत्वपूर्ण कारक हैं।
- अनुकूल परिस्थितियाँ:
- गर्म और आर्द्र मौसम: 25-30°C के बीच का आदर्श तापमान और 80% से अधिक की आर्द्रता कवक के विकास को बढ़ावा देती है।
- संक्रामक पौधों का मलबा: स्पोर पिछले फसल के बचे हुए ठूंठ और भूसे पर बने रह सकते हैं, जिससे संक्रमण का जोखिम बढ़ता है।
- नाइट्रोजन स्तर: मिट्टी में उच्च नाइट्रोजन मात्रा, अक्सर अत्यधिक उपयोग के कारण, फसलों को इस रोग के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है।
- नियंत्रण उपाय: जबकि कवकनाशी का उपयोग फॉल्स स्मट को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है, अधिक उपयोग ने फंगल एजेंटों में प्रतिरोध और पर्यावरणीय प्रदूषण को जन्म दिया है।
अंत में, फॉल्स स्मट रोग का प्रबंधन धान की फसल की उत्पादकता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जैसे पंजाब जहां इस रोग ने हाल ही में गंभीर नुकसान पहुँचाया है।
जिलों को लोकतांत्रिक कॉमन के रूप में पुनः प्राप्त करें
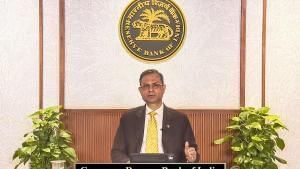 क्यों समाचार में?
क्यों समाचार में?
समाज में फूट और ध्रुवीकरण का संदर्भ तकनीकी, पारिस्थितिकीय, और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के साथ बढ़ता जा रहा है, जो वैश्विक स्तर पर मानव जीवन को पुनः आकार दे रहे हैं। भारत में, जहां युवा जनसंख्या महत्वपूर्ण है, चुनौतियाँ युवाओं को आर्थिक और लोकतांत्रिक ढांचों में एकीकृत करने में निहित हैं, जो देश की वृद्धि और लोकतांत्रिक जीवन शक्ति के लिए आवश्यक हैं।
- भारत की वृद्धि असमान है, शहरी क्षेत्रों का GDP में असमान रूप से अधिक हिस्सा है।
- शासन में केंद्रीकरण है जो स्थानीय राजनीतिक एजेंसी को कमजोर करता है।
- जिलों को लोकतांत्रिक कॉमन के रूप में पुनःकल्पना करने से जवाबदेही और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है।
- समावेशी वृद्धि के लिए कुलीनों के बीच साझा जिम्मेदारी आवश्यक है।
- वृद्धि की असमान भौगोलिकता: समतामूलक वृद्धि की आकांक्षाओं के बावजूद, 60% से अधिक GDP शहरों द्वारा उत्पन्न होता है, जो केवल भारत की 3% भूमि पर स्थित हैं। अधिकांश भारतीय अर्द्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिससे प्रतिभा का अंडरयूज और वेतन में ठहराव की दोहरी संकट उत्पन्न होती है।
- केंद्रीकरण और इसकी असंतोष: अत्यधिक केंद्रीकृत शासन मॉडल ने स्थानीय राजनीतिक एजेंसी को कम कर दिया है, जहां निर्वाचित प्रतिनिधि राज्य सेवाओं के मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, नेताओं के रूप में नहीं। इससे राजनीतिक थकान पैदा हुई है, विशेष रूप से युवाओं के बीच।
- लोकतांत्रिक परिवर्तन: जिलों के प्रशासनिक इकाइयों से नागरिक स्थानों के रूप में धारणा को बदलने से शासन में सुधार हो सकता है, जिससे यह अधिक जवाबदेह और स्थानीय रूप से प्रतिक्रियाशील बनता है। एक जिला-प्रथम ढांचा विषमताओं को उजागर कर सकता है और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा दे सकता है।
- साझा जिम्मेदारी: इस परिवर्तन की सफलता के लिए, भारत के शीर्ष 10% सामाजिक-आर्थिक नेताओं को स्थानीय शासन में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। यह दृष्टिकोण नीति और वास्तविक अनुभव के बीच की खाई को पाटता है, साझा राष्ट्रीय उद्देश्य को बढ़ावा देता है।
निष्कर्ष में, भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है जहां इसकी युवा शक्ति का प्रभावी ढंग से दोहन तभी संभव है जब शासन और अवसर शहरी केंद्रों से परे विस्तारित हों। जिलों को लोकतांत्रिक कॉमन के रूप में पुनःकल्पना करना केवल एक आवश्यक सुधार नहीं है, बल्कि विश्वास को पुनर्निर्माण और अवसरों का विस्तार करने के लिए एक नैतिक अनिवार्यता है, जिससे लोकतांत्रिक आधार का क्षय रोका जा सके।
आंतरिक्षीय मानचित्रण और त्वरण जांच
हाल ही में, NASA ने आंतरिक्षीय मानचित्रण और त्वरण जांच (IMAP) लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि सौर कण कैसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और वे पृथ्वी के लिए कैसे सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- IMAP का मुख्य लक्ष्य हेलीओस्फियर्स की सीमा का मानचित्रण करना है।
- यह ऊर्जावान कणों का पता लगाने और अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी को बेहतर बनाने का प्रयास करता है।
- IMAP पहले पृथ्वी-सूर्य लैग्रेंज बिंदु (L1) पर स्थित है, जो पृथ्वी से लगभग एक मिलियन मील दूर सूर्य की ओर है।
- हेलीओस्फियर: एक विशाल बुलबुला जो सौर वायु द्वारा निर्मित होता है और हमारे पूरे सौर प्रणाली को घेर लेता है।
- वास्तविक समय अवलोकन: IMAP लगभग वास्तविक समय में डेटा प्रदान करेगा, जिससे वैज्ञानिक अंतरिक्ष मौसम की स्थितियों की निगरानी कर सकेंगे, जो पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष वातावरण में खतरनाक स्थितियाँ उत्पन्न कर सकती हैं।
- वैज्ञानिक उपकरण: IMAP में 10 वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए हैं, जो विभिन्न प्रकार के कणों और घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिनमें ऊर्जावान न्यूट्रल-एटम डिटेक्टर्स (IMAP-Lo, IMAP-Hi, IMAP-Ultra) शामिल हैं।
- ये उपकरण मौलिक भौतिकी को उजागर करने, सौर वायु के व्यवधानों की भविष्यवाणी में सुधार करने और ब्रह्मांडीय सामग्री की हमारी समझ को बढ़ाने में मदद करेंगे।
- IMAP का मिशन यह स्पष्ट करने का भी प्रयास करता है कि हेलीओस्फियर पृथ्वी पर जीवन को ब्रह्मांडीय किरणों से कैसे सुरक्षा प्रदान करता है।
IMAP का लॉन्च हमारे अंतरिक्ष मौसम को समझने और उसके पृथ्वी पर प्रभावों को जानने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, जो हमारे गैलेक्सी के वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए भौगोलिक इंजीनियरिंग प्रस्तावों में खामियाँ पाई गईं
एक हालिया अध्ययन, जो एक्सेटर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया, ने ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित पांच प्रमुख भौगोलिक इंजीनियरिंग विधियों में महत्वपूर्ण खामियों की पहचान की है। इन विधियों को प्रभावहीन और संभावित रूप से जोखिम भरा माना गया है, जो जिम्मेदार जलवायु हस्तक्षेप के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में असफल रही हैं।
- पांच भौगोलिक इंजीनियरिंग विधियाँ ध्रुवीय जलवायु हस्तक्षेप के लिए प्रभावहीन पाई गईं।
- प्रत्येक विधि पर्यावरणीय सुरक्षा और प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण जोखिम और चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है।
ध्रुवीय क्षेत्रों में भू-इंजीनियरिंग: अध्ययन के निष्कर्ष
- स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन (SAI): इस विधि में सल्फरकणों जैसे एरोसोल को स्ट्रेटोस्फीयर में छोड़ना शामिल है ताकि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित किया जा सके।
- उपरी सतह के तापमान को कम करने के लिए सूर्य की विकिरण को अवरुद्ध करने का उद्देश्य।
- ध्रुवीय सर्दियों में अप्रभावी और गर्मियों में उच्च बर्फ की परावर्तकता के कारण सीमित पाया गया।
- यदि अचानक रोका गया तो "टर्मिनेशन शॉक" का जोखिम, जिससे वैश्विक तापमान तेजी से बढ़ सकता है।
- वैश्विक मौसम पैटर्न में संभावित व्यवधान, जो खाद्य और जल सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।
- यदि 30 देशों के बीच साझा किया जाए, तो अनुमानित लागत $55 मिलियन प्रति वर्ष प्रति देश।
- समुद्री परदे / समुद्री दीवारें:ये विशाल तैरते अवरोध हैं जो गर्म धाराओं को बर्फ की चादरों तक पहुँचने से रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- ग्लेशियरों के पिघलने को धीमा करने के लिए गर्म पानी से उन्हें इंसुलेट करने के लिए बनाया गया।
- अंटार्कटिका के अमुंडसेन समुद्र जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण।
- लागत $1 बिलियन प्रति किलोमीटर से अधिक हो सकती है; कठोर परिस्थितियों के कारण हर साल केवल कुछ महीने ही स्थापना संभव है।
- जोखिमों में समुद्री परिसंचरण में व्यवधान और समुद्र में विषैले पदार्थों के रिसाव की संभावना शामिल है।
- समुद्री बर्फ प्रबंधन (माइक्रोबीड्स):समुद्री बर्फ पर कांच के माइक्रोबीड्स फैलाने में शामिल है ताकि परावर्तकता को बढ़ाया जा सके और बर्फ की मोटाई बढ़ाई जा सके।
- गर्म होने को धीमा करने और गर्मियों की बर्फ को संरक्षित करने का लक्ष्य।
- अनिश्चित 360 मिलियन टन बीड्स की आवश्यकता, जो वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन के समान है।
- उत्पादन और तैनाती से संबंधित लॉजिस्टिकल चुनौतियाँ और महत्वपूर्ण उत्सर्जन।
- बीड्स जल्दी घुल जाते हैं, प्रभावशीलता कम करते हैं, और संभावित रूप से गर्म होने में योगदान कर सकते हैं।
- आर्कटिक तैनाती के लिए अनुमानित लागत $500 बिलियन प्रति वर्ष, जिसके लिए विशाल अवसंरचना की आवश्यकता है।
- बेसल जल निकासी:इस विधि में अंटार्कटिक ग्लेशियर्स के नीचे की पिघली हुई बर्फ के पानी को पंप करना शामिल है ताकि ग्लेशियर के फिसलने को कम किया जा सके।
- ग्लेशियर की गति को कम करके समुद्र स्तर में वृद्धि को धीमा करने का उद्देश्य।
- जियोथर्मल हीटिंग द्वारा अंतर्ग्रहणीय पानी के पुनःपूर्ति के कारण दोषपूर्ण तर्क के लिए आलोचना की गई।
- ऊर्जा और अवसंरचना के संदर्भ में उच्च उत्सर्जन-गहन और मांग वाला।
- इस विधि की दीर्घकालिक स्थिरता संदिग्ध है।
- महासागर उर्वरता: फाइटोप्लांकटन की वृद्धि को उत्तेजित करने के लिए आयरनजैसे पोषक तत्वों को जोड़ना ताकि कार्बन का अधिक अवशोषण किया जा सके।
- लक्ष्य महासागरों में अधिक कार्बन को सीक्वेस्टर करना है।
- फाइटोप्लांकटन प्रजातियों पर नियंत्रण की कमी, जो खाद्य श्रृंखलाओं को बाधित कर सकती है।
- समुद्री जैव विविधता को नुकसान और वैश्विक पोषक चक्रों को बदलने की संभावना।
- व्यावहारिक बड़े पैमाने पर तैनाती की आवश्यकता; जोखिम अनिश्चित फायदों से अधिक हैं।
संक्षेप में, जबकि भू-इंजीनियरिंग विधियाँ जलवायु परिवर्तन के समाधान पेश करती हैं, अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि इनका कार्यान्वयन ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक नुकसान कर सकता है। जिम्मेदार विचार और आगे अनुसंधान आवश्यक हैं इससे पहले कि कोई रणनीतियाँ अपनाई जाएँ।
निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करें:
- कृषि भूमि पर बारीक पिसे हुए बेसाल्ट चट्टान का व्यापक रूप से फैलाना
- चूना डालकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना
- विभिन्न उद्योगों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना और इसे abandoned subterranean mines (परित्यक्त भूमिगत खनियों) में कार्बोनेटेड पानी के रूप में पंप करना
उपरोक्त गतिविधियों में से कितनी को अक्सर कार्बन कैप्चर और सेक्वेस्ट्रेशन के लिए विचार किया जाता है और चर्चा की जाती है?
- विकल्प: (a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन* (d) कोई नहीं
|
7 videos|3454 docs|1081 tests
|
FAQs on UPSC Daily Current Affairs(Hindi)- 1st October 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly
| 1. भारत में दुगना विकास का क्या अर्थ है और यह रोजगार सृजन में कैसे मदद कर सकता है? |  |
| 2. NCRB डेटा में बच्चों के खिलाफ अपराधों की स्थिति क्या है? |  |
| 3. महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी में वृद्धि के बावजूद, क्या वे वास्तव में रोजगार में हैं? |  |
| 4. वासेनार व्यवस्था क्या है और इसका भारत पर क्या प्रभाव है? |  |
| 5. फॉल्स स्मट रोग क्या है और यह किस फसल को प्रभावित करता है? |  |





















