UPSC Daily Current Affairs(Hindi) - 4th April 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download
जीएस2/शासन
लोकपाल और लोकायुक्त
 चर्चा में क्यों?
चर्चा में क्यों?
अपने अधिनियमन के 12 वर्षों के बाद भी लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने सीमित प्रभावशीलता प्रदर्शित की है, तथा लोकपाल ने केवल 24 जांचें शुरू की हैं तथा 6 अभियोजन स्वीकृतियां दी हैं ।
चाबी छीनना
- भारत में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था।
- अपनी स्थापना के बावजूद, जांच और अभियोजन के संदर्भ में लोकपाल का कम उपयोग किया गया है।
अतिरिक्त विवरण
- लोकपाल का इतिहास: 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC-I) ने भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल बनाने की सिफारिश की थी। 1971 से 2008 तक कई लोकपाल विधेयक प्रस्तावित किए गए , लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ।
- 2011 में , कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में जन लोकपाल आंदोलन ने एक प्रभावी भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे के लिए सार्वजनिक मांग को तेज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित हुआ।
- लोकपाल केन्द्रीय स्तर पर लोक सेवकों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों को देखता है और इसमें कुछ विशेष अपवादों को छोड़कर प्रधानमंत्री जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी भी शामिल होते हैं।
- नियुक्ति: लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं।
- राज्य स्तरीय लोकायुक्त: लोकपाल के राज्य स्तरीय समकक्ष के रूप में स्थापित, यह मुख्यमंत्रियों और विधायकों जैसे राज्य के लोक सेवकों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों को संभालता है।
- लोकायुक्त की शक्तियां और संरचना राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है, जो अक्सर लोकपाल मॉडल को प्रतिबिंबित करती है।
लोकपाल और लोकायुक्त भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में काम करते हैं, भले ही उन्हें अपनी संचालन प्रभावशीलता में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो। उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए निरंतर सार्वजनिक भागीदारी और विधायी समर्थन महत्वपूर्ण है।
जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी
Third Launchpad at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota
 चर्चा में क्यों?
चर्चा में क्यों?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्चपैड के निर्माण को मंज़ूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह प्रक्षेपण में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना है।
चाबी छीनना
- नया लॉन्चपैड अगली पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल (एनजीएलवी) मिशनों का समर्थन करेगा।
- यह उन्नत उपग्रहों और अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने की इसरो की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- इसरो का दूसरा रॉकेट प्रक्षेपण पोर्ट तमिलनाडु के कुलसेकरपट्टिनम में विकसित किया जा रहा है।
सतीश धवन के बारे में
- पृष्ठभूमि: सतीश धवन का जन्म श्रीनगर में हुआ था और उन्हें भारत में 'प्रायोगिक द्रव गतिविज्ञान अनुसंधान के जनक' के रूप में जाना जाता है।
- कैरियर की उपलब्धियां: उन्होंने 1972 में विक्रम साराभाई के बाद इसरो के अध्यक्ष का पद संभाला और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक परिवर्तनकारी युग का नेतृत्व किया, जिसमें निम्नलिखित का विकास शामिल है:
- इन्सैट: भारत की दूरसंचार उपग्रह प्रणाली।
- आईआरएस: भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह कार्यक्रम।
- पीएसएलवी: ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसने भारत को एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष यात्रा करने वाले राष्ट्र के रूप में स्थापित किया।
- विरासत: सतीश धवन का 2002 में निधन हो गया और श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र का नाम उनके सम्मान में रखा गया।
नए लॉन्चपैड के बारे में
- यह लॉन्चपैड अंतरिक्ष मिशनों में भारत की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएगा।
- महत्व: यह भारत का एकमात्र परिचालन अंतरिक्ष बंदरगाह है, जो अपनी स्थापना के बाद से अंतरिक्ष यान और उपग्रह प्रक्षेपण की सुविधा प्रदान कर रहा है।
प्रक्षेपण स्थल के रूप में श्रीहरिकोटा का चयन
- 1960 के दशक की खोज: स्वदेशी उपग्रह विकास की आवश्यकता के कारण आदर्श प्रक्षेपण स्थल की खोज 1960 के दशक में शुरू हुई।
- सर्वेक्षण और अधिग्रहण: अक्टूबर 1968 तक श्रीहरिकोटा में लगभग 40,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया।
- श्रीहरिकोटा को चुनने के कारण:
- पूर्वी तट स्थान: रॉकेट को पूर्व की ओर प्रक्षेपित करने से पृथ्वी की घूर्णन गति का उपयोग होता है, जिससे 450 मीटर/सेकेंड की गति बढ़ जाती है, जो भूस्थिर उपग्रहों के लिए लाभप्रद है।
- भूमध्य रेखा से निकटता: भूमध्य रेखा के निकट स्थित स्थानों पर रॉकेटों को भूस्थिर कक्षाओं तक पहुंचने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- निर्जन क्षेत्र: विरल जनसंख्या प्रक्षेपण के दौरान जोखिम को न्यूनतम कर देती है।
- समुद्र तक पहुंच: बंगाल की खाड़ी की निकटता के कारण रॉकेट का मलबा समुद्र में गिर सकता है, जिससे भूमि पर खतरा कम हो जाता है।
- सामरिक पहुंच: संसाधनों और बुनियादी ढांचे तक पर्याप्त पहुंच ने प्रक्षेपण सुविधा के विकास में सहायता की।
पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQ)
[2018] भारत के उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- पीएसएलवी पृथ्वी संसाधनों की निगरानी के लिए उपयोगी उपग्रहों को प्रक्षेपित करते हैं, जबकि जीएसएलवी मुख्य रूप से संचार उपग्रहों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह पृथ्वी पर एक विशिष्ट स्थान से आकाश में एक ही स्थिति में स्थिर प्रतीत होते हैं।
- जीएसएलवी एमके III एक चार-चरणीय प्रक्षेपण यान है, जिसके पहले और तीसरे चरण में ठोस रॉकेट मोटर्स का उपयोग किया जाता है, तथा दूसरे और चौथे चरण में द्रव रॉकेट इंजन का उपयोग किया जाता है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
- (ए) केवल 1
- (बी) 2 और 3
- (सी) 1 और 2
- (d) केवल 3
यह नया विकास न केवल वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि उपग्रह और रॉकेट प्रक्षेपण में अपनी तकनीकी क्षमताओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
जीएस3/पर्यावरण
याला ग्लेशियर
 चर्चा में क्यों?
चर्चा में क्यों?
नेपाल में स्थित याला ग्लेशियर पर तेजी से पीछे हटने और द्रव्यमान में कमी के कारण 2040 के दशक तक विलुप्त होने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। यह हिमालय का एकमात्र ग्लेशियर है जिसे ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअल्टी लिस्ट में शामिल किया गया है, जो 2024 में शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में लुप्तप्राय या लुप्त हो चुके ग्लेशियरों का दस्तावेजीकरण करना है।
चाबी छीनना
- संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया है, तथा 2025 से 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
- याला ग्लेशियर क्रायोस्फीयर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हिमालयी क्षेत्र के लगभग 240 मिलियन लोगों को जीवन प्रदान करता है।
- 1974 से 2021 तक ग्लेशियर में 680 मीटर की उल्लेखनीय कमी आई है, इसी अवधि के दौरान इसके क्षेत्र में 36% की कमी आई है।
अतिरिक्त विवरण
- स्थान: याला ग्लेशियर मध्य नेपाल की लांगटांग घाटी में स्थित है और इस पर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
- निगरानी: ग्लेशियर पर एक दशक से अधिक समय से निगरानी की जा रही है, जिसमें खूंटियों, बर्फ के गड्ढों और उपग्रह चित्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे हिमालयी ग्लेशियरों की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध हुआ है।
- वैश्विक ग्लेशियर दुर्घटना सूची: राइस विश्वविद्यालय, डब्ल्यूजीएमएस, डब्ल्यूएमओ और यूनेस्को के एक संघ द्वारा शुरू की गई यह सूची उन ग्लेशियरों का दस्तावेजीकरण करती है जो लुप्त हो गए हैं या गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं।
- सूचीबद्ध महत्वपूर्ण ग्लेशियरों में पिको हम्बोल्ट ग्लेशियर (वेनेजुएला) शामिल है, जो 2024 में लुप्त हो जाएगा, तथा डागू ग्लेशियर (चीन) भी शामिल है, जिसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, तथा जिसके 2030 तक लुप्त हो जाने की आशंका है।
ग्लेशियरों के पिघलने की खतरनाक दर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है, क्योंकि ग्लेशियरों में दुनिया का लगभग 70% ताजा पानी मौजूद है, जिससे अरबों लोगों की जल सुरक्षा प्रभावित होती है।
पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQ):
निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:
- ग्लेशियर: नदी
- बंदरपूँछ : यमुना
- Bara Shigri : Chenab
- Milam : Mandakini
- सियाचिन : नुबरा
- निम्न: मेरा
उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं?
- (ए) 1, 2 और 4
- (बी) 1, 3 और 4
- (सी) 2 और 5
- (घ) 3 और 5
जीएस3/पर्यावरण
सर्वेक्षण से मुन्नार के जीव-जंतुओं में 24 नई प्रजातियां जुड़ीं
 चर्चा में क्यों?
चर्चा में क्यों?
मुन्नार वन्यजीव प्रभाग में हाल ही में किए गए एक जीव सर्वेक्षण ने पक्षियों, तितलियों और ओडोनेट्स की नई प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करके क्षेत्र की जैव विविधता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का खुलासा किया है। यह सर्वेक्षण मुन्नार की मौजूदा जैव विविधता चेकलिस्ट को बढ़ाता है, जो पारिस्थितिक संरक्षण और अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है।
चाबी छीनना
- 24 नई प्रजातियां जोड़ी गईं, जिनमें 11 पक्षी, 8 तितलियाँ और 5 ओडोनेट्स शामिल हैं।
- कुल दस्तावेज़ीकरण में 217 पक्षी प्रजातियाँ, 166 तितली प्रजातियाँ और 5 नए ओडोनेट रिकॉर्ड शामिल हैं।
सर्वेक्षण की गई साइटें
- मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान (एमएसएनपी): पश्चिमी घाट के भीतर एक जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट।
- पंबादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान (पीएसएनपी): केरल का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, जो अपनी अनूठी वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है।
- अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान (एएनपी): इसका नाम दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी के नाम पर रखा गया है।
- कुरिन्जिमाला वन्यजीव अभयारण्य (KWLS): नीलकुरिन्जी के निवास स्थान की रक्षा करता है, एक फूल जो हर 12 साल में एक बार खिलता है।
- एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान (ईएनपी): नीलगिरि तहर के लिए प्रसिद्ध।
- चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य (सीडब्ल्यूएलएस): यह अभयारण्य केरल-तमिलनाडु सीमा के निकट पश्चिमी घाट के वर्षा-छाया क्षेत्र में स्थित है।
अतिरिक्त विवरण
- नई प्रजातियां जोड़ी गईं: इसमें ब्राउन हॉक उल्लू, बैरर्ड बटनक्वेल, स्पॉटेड उल्लू, मोटल्ड वुड उल्लू आदि शामिल हैं।
- उल्लेखनीय वन्यजीवन: इसमें नीलगिरि तहर, बाघ, तेंदुए और हाथी जैसे स्तनधारी, साथ ही सरीसृप और उभयचरों की 12 प्रजातियां शामिल थीं।
- अनोखे दृश्य: ग्रास ज्वेल (केरल की सबसे छोटी तितली) और साउदर्न बर्डविंग (भारत की सबसे बड़ी तितली) देखी गईं।
- नए ओडोनेट रिकॉर्ड: प्रलेखित प्रजातियों में क्रैटिला लिनेटा कैल्वेर्टी और मैक्रोडिप्लाक्स कोरा शामिल हैं।
यह सर्वेक्षण न केवल मुन्नार की जैव विविधता को समृद्ध करता है, बल्कि विभिन्न प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए निरंतर पारिस्थितिक सर्वेक्षण के महत्व पर भी जोर देता है।
जीएस2/राजनीति
चुनावी बॉन्ड प्रतिबंध के बाद ट्रस्ट रूट में उछाल
चर्चा में क्यों?
भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा हाल ही में जारी चुनावी ट्रस्ट योगदान रिपोर्ट में फरवरी 2024 में चुनावी बांड को समाप्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक दलों को मिलने वाले दान में पर्याप्त वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है।
चाबी छीनना
- चुनावी बांड प्रतिबंध के बाद चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से राजनीतिक दान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- चुनावी ट्रस्ट गैर-लाभकारी संस्थाएं हैं जो राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता बढ़ाती हैं।
- चुनावी ट्रस्ट प्रणाली में बड़े कॉर्पोरेट दाताओं के प्रभाव पर चिंता।
अतिरिक्त विवरण
- चुनावी ट्रस्ट: ये गैर-लाभकारी संगठन हैं जो पारदर्शी राजनीतिक फंडिंग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए हैं। वे मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं जो व्यक्तियों और निगमों से स्वैच्छिक योगदान एकत्र करते हैं, उन्हें पंजीकृत राजनीतिक दलों में पुनर्वितरित करते हैं।
- पात्र कंपनियाँ: कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी कंपनी चुनावी ट्रस्ट स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकती है।
- निर्माण और विनियमन: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13बी के तहत शुरू किए गए चुनावी ट्रस्टों को कर प्रोत्साहन का लाभ मिलता है। इनका संचालन चुनावी ट्रस्ट योजना, 2013 द्वारा नियंत्रित होता है, जिसकी देखरेख ईसीआई करता है।
- दानकर्ता पात्रता: भारतीय नागरिक और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत घरेलू कंपनियां योगदान दे सकती हैं, लेकिन उन्हें अपनी पहचान और दान की राशि का खुलासा करना होगा।
- दान पर प्रतिबंध: विदेशी संस्थाओं, सरकारी कंपनियों और कुछ ट्रस्टों को दान देने पर प्रतिबंध है।
- पारदर्शिता के मुद्दे: चुनावी ट्रस्ट दानदाताओं के नाम का खुलासा तो करते हैं, लेकिन प्रत्येक राजनीतिक दल को आवंटित की गई विशिष्ट राशि का खुलासा नहीं किया जाता, जिससे पारदर्शिता संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती हैं।
- राजनीतिक दलों की जवाबदेही: चुनावी ट्रस्टों के लिए राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान का सार्वजनिक खुलासा करना आवश्यक होता है, जबकि चुनावी बांडों के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती।
- विदेशी प्रभाव की रोकथाम: चुनावी ट्रस्ट विदेशी दान पर रोक लगाते हैं, जिससे भारतीय राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप का जोखिम कम हो जाता है, जबकि चुनावी बांड में विदेशी नियंत्रित संस्थाओं पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं होता है।
15 फरवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने के फैसले ने कॉरपोरेट राजनीतिक दान के परिदृश्य को काफी हद तक बदल दिया है, जिससे चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से योगदान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह प्रवृत्ति चुनावी बॉन्ड प्रणाली से चुनावी ट्रस्टों को धन के उल्लेखनीय मोड़ को रेखांकित करती है, जिन्हें पारदर्शिता का एक ऐसा स्तर बनाए रखने की आवश्यकता होती है जो चुनावी बॉन्ड नहीं रखते हैं।
जीएस1/इतिहास और संस्कृति
नामधारी कौन हैं?
 चर्चा में क्यों?
चर्चा में क्यों?
हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने मलेरकोटला में नामधारी शहीद स्मारक पर आयोजित एक समारोह में कूका शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यह कार्यक्रम 17 और 18 जनवरी, 1872 को ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा 66 नामधारी सिखों (कूका) को फांसी दिए जाने की याद में मनाया जाता है।
चाबी छीनना
- नामधारी संप्रदाय की स्थापना सतगुरु राम सिंह ने 12 अप्रैल, 1857 को लुधियाना, पंजाब में की थी।
- शब्द "नामधारी" उनकी विशिष्ट ऊंची आवाज में गुरबानी के पाठ से लिया गया है, जहां पंजाबी में "कूक" का अर्थ "रोना" या "चीखना" होता है।
अतिरिक्त विवरण
- सामाजिक सुधार: नामधारी लोगों ने शराब और मांसाहार जैसी हानिकारक प्रथाओं के खिलाफ़ वकालत की। उन्होंने स्वदेशी सिद्धांतों को बढ़ावा दिया और विदेशी वस्तुओं, ब्रिटिश सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों के बहिष्कार को प्रोत्साहित किया।
- यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन का अग्रदूत था, जिसमें आत्मनिर्भरता और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध पर जोर दिया गया था।
कूका विद्रोह
- कूका विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक स्थानीय विद्रोह था जो 1857 के विद्रोह के बाद हुआ था।
- नामधारी लोगों ने ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया, विशेषकर गौहत्या से संबंधित नीतियों का, जो उनके प्रतिरोध का प्रमुख मुद्दा बन गया।
विद्रोह की ओर ले जाने वाली प्रमुख घटनाएँ
- जनवरी 1872 में, हीरा सिंह और लहना सिंह के नेतृत्व में नामधारियों की मलेरकोटला में गौहत्या की घटना के बाद ब्रिटिश अधिकारियों के साथ झड़प हुई।
- उन्होंने लुधियाना में मलौद किले पर हमला किया, जो अंग्रेजों के प्रति वफादार था, लेकिन अंततः उनके विद्रोह को दबा दिया गया।
ब्रिटिश जवाबी कार्रवाई
- अंग्रेजों ने 17 जनवरी 1872 को 49 नामधारियों को तथा 18 जनवरी 1872 को 17 अन्य नामधारियों को फांसी पर चढ़ा दिया।
- दूसरों को डराने के उद्देश्य से किए गए क्रूर प्रदर्शन में, कुछ कूकाओं को तोपों के सामने खड़ा कर दिया गया और सार्वजनिक रूप से उनकी हत्या कर दी गई।
कूका शहीद दिवस
- यह दिवस उन 66 नामधारियों के सम्मान में प्रतिवर्ष मनाया जाता है जिन्हें 1872 में फांसी दी गई थी।
बहादुरी की महत्वपूर्ण कहानियाँ
- मात्र 12 वर्ष की आयु में बिशन सिंह ने अपना संप्रदाय त्यागने से इनकार कर दिया और एक ब्रिटिश अधिकारी की दाढ़ी खींचने के साहसी कार्य के कारण उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया।
- वरयाम सिंह ने पत्थरों का उपयोग करके तोप के मुँह तक पहुंचकर अविश्वसनीय साहस का परिचय दिया तथा अपने उद्देश्य के प्रति अटूट समर्पण का परिचय दिया।
परंपरा
- विद्रोह के बाद कई नामधारी नेताओं को रंगून निर्वासित कर दिया गया।
- नामधारी मानते हैं कि राम सिंह की आत्मा अभी भी जीवित है और वे सफेद वस्त्र पहनकर उनकी अनुपस्थिति पर शोक मनाते हैं।
पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQ)
2016 में, 'स्वदेशी' और 'बहिष्कार' को पहली बार संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया:
- (क) बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन
- (बी) होम रूल आंदोलन
- (ग) असहयोग आंदोलन
- (घ) साइमन कमीशन का भारत दौरा
यह संरचित सामग्री नामधारियों, उनके ऐतिहासिक महत्व और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान का स्पष्ट और व्यापक अवलोकन प्रदान करती है।
जीएस3/अर्थव्यवस्था
दिवालियापन समाधान का पुनर्गठन
 चर्चा में क्यों?
चर्चा में क्यों?
दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) ने आर्थिक दक्षता बढ़ाने और कॉर्पोरेट चूक को दूर करने के उद्देश्य से दिवाला समाधान के लिए भारत के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण सुधार किया है। हालाँकि, इसके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ सामने आई हैं, जिसके कारण मौजूदा ढाँचे का गहन मूल्यांकन आवश्यक हो गया है।
चाबी छीनना
- आईबीसी का उद्देश्य दिवालियापन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और भारत में कारोबारी माहौल में सुधार करना है।
- कार्यान्वयन से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के भीतर संरचनात्मक अकुशलताएं उजागर हुई हैं।
- दिवालियापन समाधान प्रक्रिया की प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने के लिए सुधारों की आवश्यकता है।
अतिरिक्त विवरण
- दोहरी जिम्मेदारी: एनसीएलटी और एनसीएलएटी का ध्यान शुरू में कॉर्पोरेट दिवालियापन पर केंद्रित था, लेकिन अब इनका विस्तार कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विभिन्न मामलों के प्रबंधन के लिए हो गया है, जिसके कारण प्रणाली पर अत्यधिक भार पड़ गया है।
- अस्थायी विच्छेदन: 1999 में स्थापित एनसीएलटी आज के गतिशील आर्थिक परिदृश्य की मांगों को पूरा करने के लिए विकसित नहीं हुआ है, जिससे यह मामलों की मात्रा के लिए अपर्याप्त है।
- विशेषज्ञता में कमी: दिवालियापन के मामलों में अक्सर विशेषज्ञ ज्ञान की कमी होती है, जिससे समाधान प्रक्रिया प्रभावित होती है। नौकरशाही की अक्षमता भी काफी देरी का कारण बनती है।
- लंबित मामलों की संख्या: लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप समाधान समय में वृद्धि हुई है, तथा वित्त वर्ष 2023-24 में दिवालियापन मामलों का औसत समय बढ़कर 716 दिन हो गया है।
- निहितार्थ: दिवालियापन प्रक्रिया में देरी से ऋणदाताओं और निवेशकों के लिए अनिश्चितता पैदा होती है, जिससे कारोबारी माहौल में विश्वास कम होता है।
- सुधारों की आवश्यकता: कार्यकुशलता में सुधार के लिए न्यायिक अनुभव को डोमेन विशेषज्ञता के साथ संयोजित करने वाला एक संकर मॉडल, साथ ही विभिन्न प्रकार के मामलों के लिए विशेष पीठों की आवश्यकता है।
आईबीसी की क्षमता का एहसास करने के लिए, भारत को अपने संस्थागत ढांचे और प्रक्रियात्मक प्रथाओं के व्यापक पुनर्मूल्यांकन को प्राथमिकता देनी चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह वैश्विक आर्थिक मानकों के अनुरूप हो और समय पर समाधान की सुविधा प्रदान करे।
जीएस2/शासन
ट्राई और सरकार स्पैम से कैसे निपट रहे हैं?
 चर्चा में क्यों?
चर्चा में क्यों?
अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी), जिसे आम तौर पर स्पैम कहा जाता है, भारत में एक बड़ी चुनौती बन गया है। परेशान करने वाले मार्केटिंग संदेशों और धोखाधड़ी वाली योजनाओं के प्रचलन ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) और दूरसंचार विभाग (डीओटी) को इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न उपायों को लागू करने के लिए प्रेरित किया है।
चाबी छीनना
- ट्राई की पहलों में डू-नॉट-डिस्टर्ब (डीएनडी) रजिस्ट्री और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है।
- संचार साथी पोर्टल और एआई-संचालित पहचान प्रणालियों जैसे तकनीकी हस्तक्षेपों का उपयोग किया जा रहा है।
- वर्तमान चुनौतियों में स्पैम की गतिशील प्रकृति और डिस्पोजेबल वीओआईपी नंबरों से होने वाली धोखाधड़ी का बढ़ना शामिल है।
अतिरिक्त विवरण
- स्पैम से निपटने में ट्राई की भूमिका: ट्राई ने स्पैम को नियंत्रित करने के लिए कई पहलों को लागू किया है, जिसमें डीएनडी रजिस्ट्री भी शामिल है, जो उपयोगकर्ताओं को अवांछित कॉल और संदेशों को ब्लॉक करने की अनुमति देती है।
- ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी: दूरसंचार कंपनियों द्वारा अनुमोदित एसएमएस प्रेषकों की अद्यतन सूची बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे डेटा अपरिवर्तनीयता और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित होती है।
- संचार साथी पोर्टल: दूरसंचार विभाग द्वारा नागरिकों के लिए धोखाधड़ी वाले संचार की रिपोर्ट करने हेतु विकसित एक मंच, जिसके कारण हजारों अनधिकृत टेलीमार्केटर्स निष्क्रिय हो गए हैं।
- एआई-संचालित जांच: दूरसंचार प्रदाता संदिग्ध कॉलों की पहचान करने और उन्हें चिह्नित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को संभावित धोखाधड़ी से बचने में मदद मिलती है।
- उपायों की प्रभावशीलता: यद्यपि अनुपालन करने वाले व्यवसायों से स्पैम संचार में कमी आई है, फिर भी घोटालेबाजों की विकसित होती रणनीति के कारण चुनौतियां बनी हुई हैं।
स्पैम से प्रभावी रूप से निपटने के लिए, ट्राई और सरकार ने अन्य उपायों का प्रस्ताव रखा है, जैसे वीओआईपी निगरानी को मजबूत करना, सार्वजनिक रिपोर्टिंग प्रणालियों को बढ़ाना, एआई एकीकरण का विस्तार करना और स्पैम नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर दंड लगाना।
जीएस2/राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में संवेदनशीलता पर जोर दिया

चर्चा में क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 306 के तहत आने वाले मामलों के बारे में जांच एजेंसियों और अदालतों को संवेदनशील बनाने के महत्व को रेखांकित किया है , जो आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है। जस्टिस अभय एस. ओका और केवी विश्वनाथन की अगुवाई वाली बेंच ने इस प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, साथ ही यह सुनिश्चित किया कि वैध मामलों में मुकदमा चलाया जाए। कोर्ट ने ये टिप्पणियां एक बैंक मैनेजर को ऋण चुकौती के मुद्दों के कारण एक उधारकर्ता को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से बरी करते हुए कीं, साथ ही बेबुनियाद मुकदमों के खिलाफ चेतावनी दी जो कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर सकते हैं।
चाबी छीनना
- सर्वोच्च न्यायालय ने दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के सावधानीपूर्वक प्रयोग की वकालत की है।
- कानूनी मानदंडों को पूरा करने वाले वास्तविक मामलों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जबकि आधारहीन अभियोजन से बचना चाहिए।
- हाल के निर्णयों में कार्यस्थल से संबंधित आत्महत्या के मामलों में सबूत पेश करने की अधिक आवश्यकता पर बल दिया गया है।
अतिरिक्त विवरण
- उकसावे की परिभाषा: आईपीसी की धारा 107 के अनुसार , उकसावे में निम्नलिखित शामिल हैं:
- किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए उकसाना।
- किसी कार्य को करने के लिए दूसरों के साथ षडयंत्र करना।
- किसी कार्य को जानबूझकर किसी कार्य या अवैध चूक के माध्यम से सहायता प्रदान करना।
- आत्महत्या के लिए उकसाने की सजा: इस अपराध की सुनवाई सत्र न्यायालय में की जाती है और यह:
- संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय।
- दंड में 10 वर्ष तक का कारावास और संभव जुर्माना शामिल है।
- दोषसिद्धि दरें: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 2022 के आंकड़ों के अनुसार :
- धारा 306 आईपीसी के लिए दोषसिद्धि दर 17.5% है ।
- सभी आईपीसी अपराधों के लिए समग्र सजा दर 69.8% है ।
- संज्ञेय अपराधों के लिए दोषसिद्धि दर 54.2% है ।
- सर्वोच्च न्यायालय का अक्टूबर 2024 का निर्णय: न्यायालय ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न से जुड़े आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले को खारिज कर दिया, तथा इस बात पर बल दिया कि जहां पक्षों के बीच संबंध पेशेवर हों, वहां साक्ष्यों की उच्च सीमा की आवश्यकता है।
आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित कानूनों के जिम्मेदाराना आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान व्यक्तियों को गलत आरोपों से बचाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने में भी मदद करता है कि वास्तविक मामलों को उचित तरीके से संबोधित किया जाए। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य मृतक के परिवारों के लिए न्याय और आरोपी के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना है।
जीएस1/भारतीय समाज
भारत में घटती प्रजनन दर
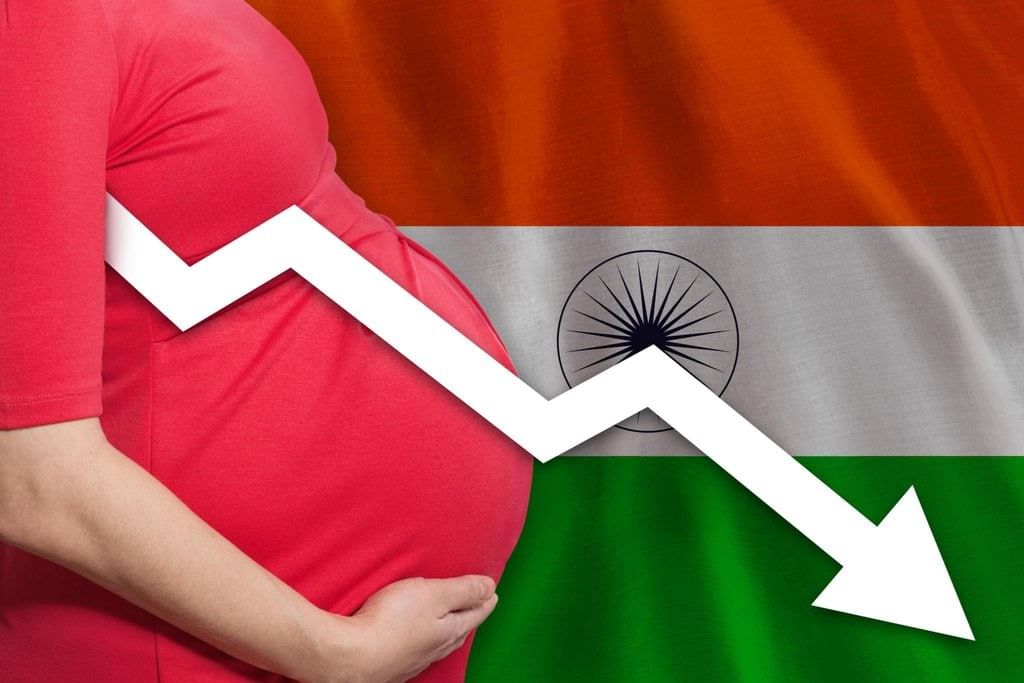 चर्चा में क्यों?
चर्चा में क्यों?
ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी (जीबीडी) 2021 में भारत की प्रजनन दर में उल्लेखनीय गिरावट पर प्रकाश डाला गया है, जो 1950 के दशक में प्रति महिला 6.18 बच्चों से घटकर 2021 में प्रति महिला 1.9 बच्चे रह गई है।
चाबी छीनना
- भारत की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) जनसंख्या स्थिरता के लिए आवश्यक प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर गई है।
- भविष्य के अनुमानों के अनुसार 2100 तक यह और घटकर 1.04 हो जाएगी, जो प्रति महिला एक से भी कम बच्चे की संभावित औसत को इंगित करता है।
- यह गिरावट सामाजिक-आर्थिक चिंताएं उत्पन्न करती है, विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और जनसांख्यिकीय बदलाव के संबंध में।
अतिरिक्त विवरण
- परिवार नियोजन नीतियों को जल्दी अपनाना: तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों ने 1950 के दशक में परिवार नियोजन नीतियों को अपनाया, जिससे प्रजनन दर में उल्लेखनीय कमी आई। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश का टीएफआर वर्तमान में 1.5 है, जो नॉर्डिक देशों के समान है।
- उच्चतर महिला साक्षरता और कार्यबल भागीदारी: शिक्षा प्राप्ति में वृद्धि ने महिलाओं को विवाह और बच्चे को जन्म देने में देरी करने का अधिकार दिया है, जैसा कि केरल में देखा गया है, जिसने 1988 तक प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता हासिल कर ली थी।
- बदलते सामाजिक मानदंड: सांस्कृतिक बदलाव पारंपरिक भूमिकाओं की तुलना में करियर को प्राथमिकता देते हैं, जिससे परिवार का आकार छोटा होता जा रहा है।
- शहरीकरण और आर्थिक दबाव: बढ़ती जीवन लागत और शहरी जीवनशैली बड़े परिवारों को हतोत्साहित करती है, जो तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में स्पष्ट है।
दक्षिणी राज्यों की चिंताएँ
- वृद्ध होती जनसंख्या: केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में वृद्धों की जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके काफी बढ़ने का अनुमान है, जिससे आर्थिक उत्पादकता पर दबाव पड़ सकता है।
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व: 2031 की जनगणना के आधार पर आगामी परिसीमन के कारण धीमी जनसंख्या वृद्धि के कारण दक्षिणी राज्यों में संसदीय सीटें कम हो सकती हैं।
- आर्थिक तनाव: घटती हुई कार्यबल आर्थिक स्थिरता के लिए चुनौती बन सकती है, ठीक उसी तरह जैसे वृद्ध होती आबादी वाले देशों को सामना करना पड़ता है।
- प्रवासन संबंधी मुद्दे: उत्तरी राज्यों से आंतरिक प्रवास पर निर्भरता सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को बढ़ा सकती है।
आगे बढ़ने का रास्ता
- न्यायसंगत संसाधन वितरण: नीतियों को क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए परिसीमन के बाद संसदीय सीटों में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व और संसाधन आवंटन सुनिश्चित करना चाहिए।
- वृद्ध होती आबादी के लिए समर्थन: प्रवास-अनुकूल नीतियों के साथ-साथ मजबूत सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों का विकास करने से कार्यबल की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है।
संक्षेप में, प्रजनन दर में गिरावट भारत के लिए, विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों के लिए, महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करती है, जिसके कारण सामाजिक-आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
जीएस2/शासन
2047 तक स्वस्थ राष्ट्र के लिए भारत का रोडमैप
 चर्चा में क्यों?
चर्चा में क्यों?
भारत का लक्ष्य 2047 तक एक विकसित राष्ट्र (विकसित भारत) में तब्दील होना है, इस बात पर जोर देते हुए कि इस आकांक्षा के लिए इसकी आबादी का स्वास्थ्य और उत्पादकता महत्वपूर्ण है। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए, भारत को 2025 तक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करनी होगी, जिसमें रोकथाम, समान उपचार और डिजिटल समाधानों के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
चाबी छीनना
- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) की स्थापना।
- स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ाने के लिए डेटा-संचालित निर्णय-निर्माण का कार्यान्वयन।
- पहुंच और दक्षता में सुधार के लिए डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों का एकीकरण।
अतिरिक्त विवरण
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी): यूएचसी का उद्देश्य सभी नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा और व्यापक सेवा कवरेज प्रदान करना है। इसके लिए निम्न की आवश्यकता होती है:
- सार्वजनिक वित्तपोषण में वृद्धि, केन्द्रीय और राज्य बजट को प्राथमिकता देना।
- अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर कुशल स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी को दूर करना।
- आयुष्मान भारत: यह पहल स्वास्थ्य प्रणालियों में परिवर्तन के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती है, जिसमें शामिल हैं:
- प्राथमिक देखभाल वास्तुकला में सुधार।
- कमजोर आबादी को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
- स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना।
- डिजिटल स्वास्थ्य मिशन: महामारी संबंधी डेटा एकत्र करने, कार्यक्रमों की निगरानी करने और स्वास्थ्य प्रणालियों को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए आवश्यक।
- डेटा-संचालित निर्णय लेना: स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए सटीक और पृथक डेटा महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से:
- गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) और मानसिक स्वास्थ्य विकारों पर नज़र रखना।
- स्वास्थ्य संबंधी खतरों पर समय पर प्रतिक्रिया के लिए उन्नत निगरानी प्रणालियों को लागू करना।
- डिजिटल रूप से एकीकृत स्वास्थ्य सेवा: इसकी आवश्यकता पर बल देता है:
- स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में नैदानिक और उपचार डेटा की अंतरसंचालनीयता।
- देखभाल और डेटा एकीकरण की निरंतरता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी।
- बेहतर निदान और नैदानिक प्रबंधन के लिए एआई का उपयोग करना।
- बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए डिजिटल उपकरणों के माध्यम से समुदायों को शामिल करना।
2047 तक भारत में स्वस्थ और उत्पादक आबादी की ओर बढ़ने के लिए तत्काल और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। 2025 तक, देश को उसके स्वास्थ्य लक्ष्यों की ओर ले जाने के लिए डिजिटल रूप से एकीकृत, डेटा-संचालित और सार्वभौमिक रूप से सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है।
जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों पर ILO की रिपोर्ट
 चर्चा में क्यों?
चर्चा में क्यों?
जिनेवा में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों पर वैश्विक अनुमान के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की वैश्विक जनसंख्या 2022 में 284.5 मिलियन तक पहुंच गई, जिनमें से 255.7 मिलियन कार्यशील आयु (15 वर्ष और उससे अधिक) के हैं।
चाबी छीनना
- वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी जनसंख्या 284.5 मिलियन तक पहुंच गई है।
- पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्रवासन और रोजगार में काफी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- उच्च आय वाले देश अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों को अपने यहां काम पर रखते हैं।
- प्रवासी श्रमिक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में केंद्रित हैं।
अतिरिक्त विवरण
- लिंग भूमिकाएं और मानदंड: पारंपरिक सामाजिक अपेक्षाएं अक्सर महिलाओं की स्वायत्त रूप से प्रवास करने की क्षमता को प्रतिबंधित करती हैं, तथा श्रम बाजार में भागीदारी की तुलना में पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देती हैं।
- श्रम बाजार विभाजन: महिलाएं बड़े पैमाने पर कम कुशल, कम मूल्यांकित क्षेत्रों जैसे घरेलू कार्य और देखभाल में पाई जाती हैं, जबकि पुरुष निर्माण और कृषि जैसे उच्च वेतन वाले क्षेत्रों पर हावी हैं।
- रोजगार में बाधाएं: भाषा संबंधी बाधाओं, गैर-मान्यता प्राप्त योग्यताओं, सीमित बाल देखभाल विकल्पों और मेजबान देशों में लिंग आधारित भेदभाव के कारण प्रवासी महिलाओं को पुरुषों (6.2%) की तुलना में उच्च बेरोजगारी दर (8.7%) का सामना करना पड़ता है।
- प्रमुख मेजबान देश: लगभग 68.4% अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उच्च आय वाले देशों में रहते हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख गंतव्य हैं।
- क्षेत्र संकेन्द्रण: अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों को आकर्षित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में निर्माण, कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें प्रवासी महिलाओं के बीच देखभाल संबंधी भूमिकाओं पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है।
- क्षेत्रीय वितरण: अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का बहुमत यूरोप और मध्य एशिया (34.5%) में केंद्रित है, इसके बाद अमेरिका (27.3%) और एशिया और प्रशांत (16.2%) का स्थान है।
निष्कर्ष रूप में, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए यह आवश्यक है कि वे लिंग-संवेदनशील प्रवासन नीतियों को लागू करें, जो महिलाओं के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करें, जिसमें बाल देखभाल के लिए सहायता प्रणालियां, विदेशी योग्यताओं की मान्यता, और मेजबान देशों में कानूनी रोजगार के अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है।
|
7 videos|3454 docs|1081 tests
|
FAQs on UPSC Daily Current Affairs(Hindi) - 4th April 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly
| 1. लोकपाल और लोकायुक्त क्या हैं और इनकी भूमिका क्या है? |  |
| 2. दिवालियापन समाधान का पुनर्गठन क्या है और इसका महत्व क्या है? |  |
| 3. ट्राई और सरकार स्पैम से कैसे निपट रहे हैं? |  |
| 4. सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में संवेदनशीलता पर क्यों जोर दिया? |  |
| 5. भारत में घटती प्रजनन दर के क्या कारण हैं? |  |
















