Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): (29th September 2025 to 5th October 2025) - 1 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download
GS3/अर्थव्यवस्था
भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025
समाचार में क्यों?
भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025, अगस्त 2025 में लागू किया गया, जो 1908 के पुराने भारतीय बंदरगाह अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है। यह नया कानून भारत के बंदरगाह क्षेत्र के लिए एक आधुनिक कानूनी और संस्थागत ढांचा बनाने का लक्ष्य रखता है, जिससे दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सके।
मुख्य बिंदु
- यह अधिनियम बंदरगाह कानून, टैरिफ नियमन, सुरक्षा, पर्यावरण मानक, और केंद्र-राज्य सहयोग को एक समग्र कानूनी ढांचे में एकीकृत करता है।
- यह मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 2025 और कार्गो ऑफ गुड्स बाय सी अधिनियम, 2025 के साथ व्यापक समुद्री सुधारों के साथ मेल खाता है।
- यह अधिनियम भारत के बंदरगाह क्षेत्र को पारदर्शिता, स्थिरता, और कुशल नियमन के माध्यम से वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए तैयार करता है।
अतिरिक्त विवरण
- समुद्री राज्य विकास परिषद (MSDC): एक वैधानिक परामर्शी निकाय जो केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय करता है, जो राष्ट्रीय पोर्ट रणनीति, टैरिफ पारदर्शिता, डेटा मानक और कनेक्टिविटी योजना पर सलाह देता है।
- राज्य समुद्री बोर्ड: प्रत्येक तटीय राज्य को 6 महीने के भीतर एक बोर्ड स्थापित या मान्यता प्राप्त करनी होगी ताकि गैर-महान बंदरगाहों का प्रबंधन, लाइसेंसिंग, टैरिफ, विकास, सुरक्षा और पर्यावरण अनुपालन की देखरेख की जा सके।
- टैरिफ सेटिंग: प्रमुख बंदरगाहों के टैरिफ पोर्ट अथॉरिटी बोर्ड द्वारा तय किए जाते हैं, जबकि गैर-महान बंदरगाहों के टैरिफ राज्य समुद्री बोर्ड या संविदाकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें पारदर्शिता के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित करना आवश्यक है।
- विवाद समाधान: राज्यों को विवाद समाधान समितियाँ स्थापित करनी चाहिए, जहां अपील उच्च न्यायालयों में की जाएगी; मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) की अनुमति है।
- पर्यावरण मानदंड: यह अधिनियम अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, आपदा तैयारी, बैलास्ट जल प्रतिबंध और उल्लंघनों के लिए दंड का प्रावधान करता है।
- लागू होने की स्थिति: यह अधिनियम सभी मौजूदा और भविष्य के बंदरगाहों, नौगम्य चैनलों और बंदरगाह सीमाओं के भीतर के जहाजों को कवर करता है, जिसमें सशस्त्र बलों, तटरक्षक बल या कस्टम के लिए सेवा देने वाले अपवाद हैं।
संक्षेप में, भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025, भारत के बंदरगाह प्रशासन को आधुनिक बनाने, दक्षता बढ़ाने और वैश्विक मानकों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
UPSC 2023 प्रश्न
भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें:
- बंदरगाह : प्रसिद्ध के रूप में
- 1. कमराजर बंदरगाह : भारत में कंपनी के रूप में पंजीकृत पहला बड़ा बंदरगाह
- 2. मुंद्रा बंदरगाह : भारत में सबसे बड़ा निजी स्वामित्व वाला बंदरगाह
- 3. विशाखापत्तनम बंदरगाह : भारत में सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह
- 1. कमराजर बंदरगाह : भारत में कंपनी के रूप में पंजीकृत पहला बड़ा बंदरगाह
- 2. मुंद्रा बंदरगाह : भारत में सबसे बड़ा निजी स्वामित्व वाला बंदरगाह
- 3. विशाखापत्तनम बंदरगाह : भारत में सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह
उपर्युक्त में से कितने जोड़ ठीक से मिलाए गए हैं?
- (a) केवल एक जोड़ा
- (b) केवल दो जोड़े*
- (c) सभी तीन जोड़े
- (d) कोई भी जोड़ा नहीं
जीएस3/अर्थव्यवस्था
आरबीआई ने दरें बरकरार रखीं, नियामक आसानियों के साथ विकास पर ध्यान केंद्रित किया
 क्यों समाचार में?
क्यों समाचार में?
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 1 अक्टूबर 2025 को अपनी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के दौरान रेपो दर को 5.5% पर स्थिर रखा। यह निर्णय वर्ष की शुरुआत में 100 आधार अंकों की कटौती के बाद लिया गया। खुदरा महंगाई 2025-26 के लिए 2.6% रहने का अनुमान है, जो 4% के लक्ष्य से काफी कम है, जिससे आरबीआई के पास भविष्य में दर कटौती के लिए लचीलापन है, लेकिन उसने सावधानी बरतने का निर्णय लिया। केवल ब्याज दर समायोजनों पर निर्भर रहने के बजाय, आरबीआई ने विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नियामक आसानियों और सुधारों के तहत 22 संरचनात्मक उपाय पेश किए। अर्थशास्त्रियों ने इसे स्पष्ट संकेत के रूप में व्याख्यायित किया कि आरबीआई दीर्घकालिक स्थिरता और सहनशीलता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो केवल ब्याज दर परिवर्तनों से परे विकास समर्थन का विस्तार कर रहा है।
- रेपो दर 5.5% पर बरकरार, महंगाई नियंत्रण और विकास समर्थन के बीच संतुलन बनाए रखा।
- जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.8% बढ़ाया गया, जो मजबूत खपत और निवेश द्वारा प्रेरित है।
- उपभोक्ता महंगाई 2.6% होने की उम्मीद, जिससे भविष्य की मौद्रिक आसानियों के लिए जगह बनती है।
- वैश्विक एजेंसियों ने बाहरी अनिश्चितताओं के बीच सकारात्मक विकास दृष्टिकोण की पुष्टि की।
- महंगाई अनुमान: सीपीआई महंगाई का अनुमान 2.6% (जिसे 3.1% से घटाया गया) खाद्य कीमतों में गिरावट और प्रभावी जीएसटी प्रावधानों से प्रभावित।
- वैश्विक आर्थिक संदर्भ: चालू खाता घाटा Q1 FY 2025-26 में जीडीपी का 0.2% तक घटा, जो मजबूत सेवा निर्यात और महत्वपूर्ण प्रेषणों द्वारा समर्थित है।
- भविष्य के विकास के कारक: मजबूत घरेलू मांग, संरचनात्मक सुधार और जीवंत सेवा क्षेत्र द्वारा समर्थित विकास की अपेक्षा।
संक्षेप में, आरबीआई के हाल के नीति निर्णय विकास का समर्थन करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन को दर्शाते हैं। केंद्रीय बैंक की दृष्टिकोण दीर्घकालिक सहनशीलता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय है, जबकि बाहरी जोखिमों के प्रति सतर्क भी है।
जीएस2/राजनीति
भारत में स्मारक संरक्षण - नीति में बदलाव
 क्यों समाचार में?
क्यों समाचार में?
भारतीय सरकार ने अपनी विरासत संरक्षण नीति में महत्वपूर्ण बदलाव शुरू किया है, जिससे निजी संस्थाओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के साथ मिलकर स्मारकों के संरक्षण में सहयोग करने की अनुमति दी गई है, जो कि राष्ट्रीय संस्कृति कोष के माध्यम से किया जाएगा।
- भारत में 3,700 से अधिक संरक्षित स्मारक हैं, जिनका पूर्व में संरक्षण का अनन्य उत्तरदायित्व ASI के पास था।
- नई नीति स्मारक संरक्षण में निजी भागीदारी को पेश करती है, जिसका उद्देश्य संरक्षण क्षमता और दक्षता को बढ़ाना है।
- अब निजी खिलाड़ी सीधे संरक्षण परियोजनाओं को वित्तपोषित और प्रबंधित कर सकते हैं, ASI की निगरानी में।
- जन-निजी भागीदारी मॉडल: निजी कंपनियां और दानदाता राष्ट्रीय संस्कृति कोष (NCF) के माध्यम से संरक्षण परियोजनाओं को वित्तपोषित कर सकते हैं और 100% कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।
- पैनल में शामिल संरक्षण आर्किटेक्ट: संस्कृति मंत्रालय योग्य आर्किटेक्ट्स की एक सूची बनाएगा, जिससे दानदाता अपने परियोजना के लिए आर्किटेक्ट का चयन कर सकें।
- जांच और संतुलन: ASI निगरानी प्राधिकरण बनाए रखेगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs) को 2014 की राष्ट्रीय संरक्षण नीति के अनुरूप होना चाहिए।
- प्रारंभिक पायलट सूची: नीति कार्यान्वयन के पहले चरण में 250 स्मारकों को निजी भागीदारी के लिए खोला जाएगा।
यह ऐतिहासिक नीति में बदलाव संरक्षण प्रयासों को तेज करने और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रबंधन में सुधार करने का लक्ष्य रखता है। हालांकि संभावित वाणिज्यीकरण पर चिंताएं हैं, निजी संस्थाओं की भागीदारी से समग्र संरक्षण परिदृश्य में सुधार की उम्मीद है, जिससे ऐतिहासिक स्थलों के पुनर्स्थापन और रखरखाव में अधिक दक्षता आएगी।
जीएस3/अर्थव्यवस्था
चीन में दुनिया का सबसे ऊँचा पुल यातायात के लिए खोला गया
 क्यों समाचार में?
क्यों समाचार में?
चीन के गुइझौ प्रांत में स्थित हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन पुल आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे ऊँचा पुल बन गया है, जो बेइपान नदी से 625 मीटर ऊँचा है। यह ऐतिहासिक संरचना चीन में इंजीनियरिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।
- यह पुल पिछले रिकॉर्ड धारक, बेइपानजियांग पुल, को पीछे छोड़ता है, जो 565 मीटर ऊँचा है।
- यह लियुज़ी विशेष जिला और अनलोंग विशेष जिला को जोड़ता है, यात्रा समय को 2 घंटे से केवल 2 मिनट तक कम कर देता है।
- यह पुल गुइझौ S57 एक्सप्रेसवे और 190 किमी लंबी शांटियन-पूसी एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, जो क्षेत्र में परिवहन, आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देता है।
- गुइझौ को \"दुनिया का पुल संग्रहालय\" का खिताब मिला है, जिसमें दुनिया के 100 सबसे ऊँचे पुलों में से लगभग आधे हैं, जो चीन की ऊँचाई पर नागरिक इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता को दर्शाते हैं।
- ऊँचाई रिकॉर्ड: पुल की डेक-से-पानी की ऊँचाई अधिकांश गगनचुंबी इमारतों से अधिक है, जो पुल निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- स्पैन और लंबाई: इसकी कुल लंबाई 2,890 मीटर है, जिसमें 1,420 मीटर का निलंबन स्पैन है, जो किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में सबसे लंबा है।
- निर्माण समयरेखा: पुल का निर्माण जनवरी 2022 में शुरू हुआ और इसे तीन वर्षों से थोड़ा अधिक समय में पूरा किया गया, जिसमें अंतिम ट्रस जनवरी 2025 में स्थापित किया गया। संरचना को सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 96 ट्रकों के साथ लोड-टेस्ट किया गया।
हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन पुल न केवल एक नया रिकॉर्ड स्थापित करता है बल्कि क्षेत्र में संयोग और आर्थिक संभावनाओं को भी बढ़ाता है, जो चीन की इंजीनियरिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रगति को दर्शाता है।
GS2/शासन
जिले को लोकतांत्रिक साझा क्षेत्र के रूप में पुनः प्राप्त करें
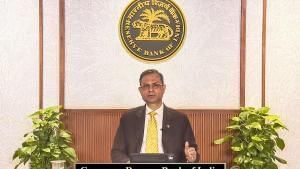 क्यों समाचार में?
क्यों समाचार में?
समाजिक विखंडन और ध्रुवीकरण का संदर्भ तेजी से प्रासंगिक होता जा रहा है क्योंकि तकनीकी, पारिस्थितिकी, और जनसांख्यिकीय परिवर्तन वैश्विक स्तर पर मानव जीवन को पुनः आकार दे रहे हैं। भारत में, एक महत्वपूर्ण युवा जनसंख्या के साथ, चुनौती यह है कि युवाओं को आर्थिक और लोकतांत्रिक ढांचों में शामिल किया जाए, जो देश की वृद्धि और लोकतांत्रिक जीवंतता के लिए महत्वपूर्ण है।
- भारत की वृद्धि असमान है, जहाँ शहरी क्षेत्रों का GDP में असमान रूप से बड़ा योगदान है।
- शासन में केंद्रीकरण है जो स्थानीय राजनीतिक एजेंसी को कमजोर करता है।
- जिलों को लोकतांत्रिक साझा क्षेत्रों के रूप में पुनः कल्पना करने से जवाबदेही और नागरिक भागीदारी बढ़ सकती है।
- समावेशी विकास के लिए अभिजात वर्ग के बीच साझा जिम्मेदारी आवश्यक है।
- विकास की असमान भौगोलिकता: न्यायसंगत विकास की आकांक्षाओं के बावजूद, 60% से अधिक GDP शहरों द्वारा उत्पन्न होता है, जो केवल भारत की भूमि का 3%占 करते हैं। अधिकांश भारतीय अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिससे उपयोग न किए गए प्रतिभा और स्थिर वेतन का द्वंद्व उत्पन्न होता है।
- केंद्रीकरण और इसके असंतोष: अत्यधिक केंद्रीकृत शासन मॉडल ने स्थानीय राजनीतिक एजेंसी को कम कर दिया है, जहाँ निर्वाचित प्रतिनिधि राज्य सेवाओं के मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, न कि नेताओं के रूप में। इससे राजनीतिक थकान का परिणाम हुआ है, विशेषकर युवाओं के बीच।
- लोकतांत्रिक परिवर्तन: जिलों की धारणा को प्रशासनिक इकाइयों से नागरिक स्थानों में बदलने से शासन में सुधार हो सकता है, जिससे यह अधिक जवाबदेह और स्थानीय रूप से प्रतिक्रियाशील बन सके। एक जिला-प्रथम ढांचा विषमताओं को उजागर कर सकता है और नागरिक भागीदारी को बढ़ा सकता है।
- साझा जिम्मेदारी: इस परिवर्तन की सफलता के लिए, भारत के शीर्ष 10% सामाजिक-आर्थिक नेताओं को स्थानीय शासन में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। यह दृष्टिकोण नीतियों और जीवन के अनुभवों के बीच की खाई को पाटता है, और एक साझा राष्ट्रीय उद्देश्य को बढ़ावा देता है।
अंत में, भारत एक महत्वपूर्ण क्षण में है जहाँ इसकी युवा शक्ति का कुशलता से उपयोग तभी किया जा सकता है जब शासन और अवसरों का विस्तार शहरी केंद्रों से परे किया जाए। जिलों को लोकतांत्रिक साझा क्षेत्रों के रूप में पुनः कल्पना करना न केवल एक आवश्यक सुधार है, बल्कि यह विश्वास को पुनर्बनाने और अवसरों का विस्तार करने के लिए एक नैतिक अनिवार्यता भी है, जिससे लोकतांत्रिक नींव के क्षय को रोका जा सके।
GS3/रक्षा और सुरक्षा
BRO प्रोजेक्ट स्वस्तिक ने 65 वर्षों की सेवा का जश्न मनाया
 क्यों समाचार में है?
क्यों समाचार में है?
सीमा सड़क संगठन (BRO) प्रोजेक्ट स्वस्तिक ने 1 अक्टूबर 2025 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया, जो रणनीतिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति इसकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को उजागर करता है।
- 1960 में स्थापित, मूल रूप से इसे प्रोजेक्ट ड्रैगन कहा गया था और 1 अक्टूबर 1963 को इसका नाम बदला गया।
- यह रक्षा मंत्रालय का हिस्सा है, जो रणनीतिक सड़कों, पुलों और सुरंगों के निर्माण और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करता है।
- यह उत्तर और पूर्व सिक्किम और उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, जहां की भौगोलिक और जलवायु स्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हैं।
- जिम्मेदारी का क्षेत्र: प्रोजेक्ट स्वस्तिक उन क्षेत्रों में काम करता है जो भूस्खलनों और चरम मौसम के लिए प्रवृत्त हैं, जिससे सशस्त्र बलों और स्थानीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी सुनिश्चित होती है।
- रणनीतिक भूमिका: यह सशस्त्र बलों की गतिशीलता, आपदा राहत संचालन और दूरदराज के क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक हालात में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- मुख्य उपलब्धियाँ: इसकी स्थापना के बाद से 1,412 किमी से अधिक सड़कें और 80 प्रमुख पुल बनाए गए हैं, जिसमें पिछले दशक में 350 किमी नई सड़कें, 26 पुल और 1 सुरंग शामिल हैं।
- महत्वपूर्ण सड़क लिंक: गंगटोक–चुंगथांग और गंगटोक–नाथुला जैसी महत्वपूर्ण मार्गें रक्षा लॉजिस्टिक्स और नागरिकों की आवाजाही के लिए आवश्यक हैं।
- आपदा प्रतिक्रिया: 2023 के सिक्किम में आई बाढ़ के बाद कनेक्टिविटी बहाल करने में प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया।
संक्षेप में, BRO प्रोजेक्ट स्वस्तिक की 65 वर्षों की समर्पित सेवा राष्ट्रीय सुरक्षा और समुदाय समर्थन में इसके महत्व को मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से उजागर करती है।
GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी
सरकार ने धार्मिक और आहार संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए 11 बायोस्टिमुलेंट्स की मंजूरी वापस ली
 क्यों समाचार में?
क्यों समाचार में?
केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने चिकन के पंखों, सुअर के ऊतकों, गाय की खाल, और कॉड की तराजू से बने 11 बायोस्टिमुलेंट्स की मंजूरी वापस ले ली है। ये उत्पाद पहले धान, टमाटर, आलू, खीरा, और मिर्च जैसी फसलों में उपयोग के लिए स्वीकृत थे, लेकिन "धार्मिक और आहार संबंधी प्रतिबंधों" के संबंध में शिकायतों के बाद इन्हें वापस लिया गया है।
- यह वापसी विभिन्न फसलों के लिए बनाए गए बायोस्टिमुलेंट्स को प्रभावित करती है।
- मुख्य चिंताएँ नैतिक, धार्मिक, और आहार संबंधी थीं।
- भारत में बायोस्टिमुलेंट क्षेत्र में नियामक परिवर्तन जारी हैं।
- बायोस्टिमुलेंट्स: ये प्राकृतिक या सिंथेटिक पदार्थ हैं जो पौधों की वृद्धि, पोषक तत्वों का अवशोषण, और तनाव सहिष्णुता को बढ़ाते हैं, बिना पारंपरिक उर्वरकों या कीटनाशकों के रूप में कार्य किए।
- बायोस्टिमुलेंट्स विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनमें पौधों के अर्क, सूक्ष्मजीव, और पशु उपोत्पाद शामिल हैं।
- बायोस्टिमुलेंट्स के उदाहरण:
- समुद्री शैवाल के अर्क: जड़ विकास में सुधार करते हैं, फूलने को बढ़ावा देते हैं, और सूखा और लवणता के प्रति प्रतिरोध बढ़ाते हैं।
- ह्यूमिक और फुल्विक एसिड: पोषक तत्वों के अवशोषण और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं।
- प्रोटीन हाइड्रोलिसेट्स और अमीनो एसिड: प्रारंभिक पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, उपज बढ़ाते हैं, और फलों की गुणवत्ता में सुधार करते हैं।
- सूक्ष्मजीव इन्क्यूलेंट्स (जैसे, Azotobacter, Mycorrhizae): नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फोरस घुलनशीलता, और मिट्टी के स्वास्थ्य में मदद करते हैं।
- काइटोसान (कर्कट के कवच से): कीटों और रोगों के खिलाफ पौधों के रक्षा तंत्र को बढ़ाता है।
- भारत में बायोस्टिमुलेंट्स का नियमन: इन उत्पादों को उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO), 1985 के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है, जिसमें 2021 के संशोधन के माध्यम से औपचारिक समावेशन की आवश्यकता है जिसमें निर्माताओं को सुरक्षा और प्रभावशीलता पर विस्तृत डेटा प्रदान करना आवश्यक है।
- बाजार अवलोकन: भारत का बायोस्टिमुलेंट्स बाजार 2024 में 355.53 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था और 2032 तक 1,135.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, जिसमें प्रमुख उत्पादक Coromandel International, Syngenta, और Godrej Agrovet शामिल हैं।
इन अनुमतियों की हालिया वापसी बायोस्टिमुलेंट बाजार में नियामक निगरानी की आवश्यकता को उजागर करती है, विशेष रूप से नैतिक, धार्मिक, और आहार संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए। जैसे-जैसे बाजार विकसित हो रहा है, यह आवश्यक है कि हितधारक सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए नियमों के साथ संरेखित हों।
GS2/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध
भारत-ईएफटीए मुक्त व्यापार समझौता
यह समाचार क्यों है?

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA), जिसमें स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, और लिकटेंस्टाइन शामिल हैं, आधिकारिक रूप से प्रभाव में आ गया है। यह भारत और EFTA देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। FTA भारत की वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में बढ़ती भागीदारी और विदेशी निवेशों को आकर्षित करने की रणनीति को उजागर करता है।
भारत-ईएफटीए एफटीए क्या है?
पृष्ठभूमि: भारत-ईएफटीए एफटीए, जिसे व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) के नाम से भी जाना जाता है, मार्च 2024 में अंतिम रूप दिया गया और 1 अक्टूबर 2025 को प्रभावी हुआ। यह समझौता भारत के व्यापार संबंधों को ईएफटीए ब्लॉक के साथ मजबूत करने का लक्ष्य रखता है और भारत के हालिया एफटीए को यूएई, ऑस्ट्रेलिया, और यूके जैसे देशों के साथ complement करता है।
समझौते के उद्देश्य:
- बाजार पहुंच में सुधार: ईएफटीए देशों ने भारत के औद्योगिक और गैर-कृषि उत्पादों के लिए 100% बाजार पहुंच प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों पर शुल्क छूट भी दी गई है।
- निवेश और नौकरी निर्माण: ईएफटीए राष्ट्रों ने 15 वर्षों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बंधनकारी निवेश करने का वादा किया है, जिससे भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है।
- व्यापार सुविधा तंत्र: निवेश और व्यापार को आसान बनाने के लिए एक समर्पित ईएफटीए डेस्क स्थापित किया गया है, जो ईएफटीए व्यवसायों को भारत में निवेश, विस्तार, और संचालन करने में सहायता प्रदान करता है।
मुक्त व्यापार समझौतों की समझ
मुक्त व्यापार समझौतें (FTAs) दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसे समझौते होते हैं, जिनका उद्देश्य व्यापार में बाधाओं को कम करना या समाप्त करना है, जैसे कि सामान और सेवाओं पर टैरिफ और कोटा। भारत के पास जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरिशस, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA), सिंगापुर और श्रीलंका जैसे विभिन्न देशों और समूहों के साथ FTAs हैं। भारत-ईयू FTA की वार्ता भी उन्नत चरणों में है।
भारत के लिए FTAs के लाभ
- बाजार पहुंच: FTAs भारत के निर्यात को बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि ये टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) ने 90% निर्यात को शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप पहले वर्ष में निर्यात में 12% की वृद्धि हुई।
- निवेश में वृद्धि: FTAs स्थिर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को आकर्षित करते हैं। भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA) के परिणामस्वरूप FDI प्रवाह में 25% की वृद्धि हुई।
- कृषि लाभ: FTAs भारतीय किसानों के लिए नए निर्यात बाजार खोलते हैं। भारत-मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (CECPA) ने चीनी और चाय जैसे कृषि निर्यात में वृद्धि की।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: FTAs उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को सरल बनाते हैं। भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भारत के ऊर्जा संक्रमण में सहायता कर रहा है।
- छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए समर्थन: FTAs SMEs को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने में मदद करते हैं। भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA) सूचना प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में SMEs को लाभ पहुंचा रहा है।
- नियामक समरूपता: FTAs मानकों के समरूपता को बढ़ावा देते हैं, जिससे व्यवसायों के लिए अनुपालन लागत कम होती है। भारत-EFTA TEPA उत्पाद प्रमाणपत्रों को संरेखित करता है, जिससे भारतीय उत्पादों के लिए EFTA बाजारों में प्रवेश करना आसान होता है।
भारत के एफटीए के साथ चिंताएँ
- व्यापार घाटे: व्यापार घाटे में वृद्धि की चिंता है, जहाँ आयात निर्यात की तुलना में काफी बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत-ASEAN एफटीए ने आयात में एक महत्वपूर्ण वृद्धि की है, जो FY23 में $44 बिलियन तक पहुँच गई है।
- विकसित बाजारों तक सीमित पहुँच: गैर-शुल्क बाधाएँ विकसित बाजारों तक पहुँच को सीमित कर सकती हैं। यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में देरी आंशिक रूप से बौद्धिक संपदा अधिकार और डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के कारण है।
- छोटे किसानों और MSMEs पर प्रभाव: छोटे किसानों और सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को सस्ते आयातों से तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, भारत में रबर के किसानों पर ASEAN एफटीए का प्रभाव पड़ा है।
- श्रम और पर्यावरण संबंधी धाराएँ: एफटीए में बाध्यकारी धाराएँ, जैसे कि यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, भारतीय निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं, क्योंकि यह कड़े मानकों को लागू करता है।
- कमजोर विवाद समाधान तंत्र: कुछ एफटीए में विवाद समाधान प्रक्रियाएँ धीमी और असंतुलित मानी जाती हैं। भारत-ASEAN एफटीए में ताड़ के तेल और मशीनरी शुल्क से संबंधित मुद्दे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ विवाद समाधान समस्या बन गया है।
भारत द्वारा वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय
- निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाना: भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उत्पादन और कृषि में गुणवत्ता, ब्रांडिंग और तकनीकी उन्नति पर ध्यान केंद्रित करें।
- व्यापार साझेदारियों का विविधीकरण: व्यापार भागीदारों की सीमित संख्या पर निर्भरता को कम करने के लिए अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया-प्रशांत जैसे क्षेत्रों में उभरते बाजारों को शामिल करने के लिए एफटीए का विस्तार करें।
- MSMEs और स्टार्टअप्स का समर्थन: छोटे और मध्यम उद्यमों तथा निर्यात उन्मुख स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों तक पहुँच को आसान और बेहतर बनाएं। यह उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने और विकसित करने में मदद कर सकता है।
- अवसंरचना विकास: बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स हब, माल परिवहन गलियारों और कोल्ड चेन सुविधाओं के विस्तार और उन्नयन में निवेश करें। इससे लेन-देन की लागत को कम करने और सामान के परिवहन की दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- अनुपालन और मानकों को बढ़ाना: निर्यातकों को गुणवत्ता, श्रम और पर्यावरण मानकों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में मदद करने के लिए क्षमता निर्माण का समर्थन प्रदान करें। यह विदेशी बाजारों में सुगम प्रवेश में सुविधा प्रदान कर सकता है।
- डिजिटल व्यापार प्लेटफार्मों का लाभ उठाना: व्यापार के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग बढ़ावा दें, जैसे कि वर्चुअल ट्रेड शो, ई-मार्केटप्लेस, और एफटीए का ऑनलाइन उपयोग, ताकि व्यापक दर्शकों तक पहुँच सके और व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके।
निष्कर्ष
भारत-ईएफटीए मुक्त व्यापार समझौता भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। हालांकि, इसके लिए घरेलू उद्योग की चुनौतियों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन और व्यापार के विविधीकरण के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
GS2/ शासन
कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाना

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2023-24 के अनुसार, कृषि में महिलाओं की भागीदारी में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, हालांकि, उनमें से लगभग आधी महिलाएँ बिना वेतन के बनी हुई हैं, जो कृषि रोजगार में गहरे जड़ित लिंग असमानताओं को दर्शाता है।
भारत में कृषि में महिलाओं की स्थिति क्या है?
- कृषि का नारीकरण: महिलाएँ अब भारत के कृषि कार्यबल का 42% से अधिक हिस्सा बनाती हैं, जो पिछले दशक में 135% की वृद्धि है। तीन में से दो ग्रामीण महिलाएँ कृषि में काम करती हैं।
- बिना वेतन का काम: कृषि में लगभग आधी महिलाएँ बिना वेतन के पारिवारिक श्रमिक हैं, जो आठ वर्षों में 23.6 मिलियन से बढ़कर 59.1 मिलियन हो गई हैं (2017-18 से 2024-25)।
- क्षेत्रीय संकेंद्रण: बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, 80% से अधिक महिला श्रमिक कृषि में हैं, हालाँकि, इनमें से आधे से अधिक बिना वेतन के हैं।
- सरकारी समर्थन: महिला किसान सशक्तिकरण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और स्वयं सहायता समूह मिलकर महिलाओं किसानों को कौशल विकास, औपचारिक ऋण तक पहुँच, सतत कृषि, और सामूहिक सौदेबाजी को मजबूत करने के माध्यम से सशक्त बनाते हैं।
भारत में कृषि के स्त्रीकरण के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं?
- पुरुषों का पलायन: पुरुष ग्रामीण क्षेत्रों से बेहतर नौकरी के अवसरों के लिए शहरों या अधिक लाभकारी ग्रामीण नौकरियों, जैसे निर्माण, सेवाएँ, परिवहन, और सरकारी कामों के लिए जा रहे हैं। यह बदलाव महिलाओं को पारिवारिक खेतों और कृषि जिम्मेदारियों को संभालने के लिए मजबूर कर रहा है।
- अनुबंध खेती का विकास: फूलों की खेती, बागवानी, और चाय/कॉफी के बागानों जैसे क्षेत्रों में श्रम-गहन कार्यों के लिए महिलाओं पर अधिक निर्भरता बढ़ रही है। महिलाओं को विश्वसनीय, कुशल, और कम वेतन स्वीकार करने वाली श्रमिकों के रूप में देखा जाता है, जिससे ये क्षेत्र उनके लिए प्राथमिक श्रमिक बन जाते हैं।
- पितृसत्तात्मक मानदंड: सामाजिक अपेक्षाएँ यह निर्धारित करती हैं कि महिलाओं को घरेलू और हल्के कृषि कार्यों को संभालना चाहिए। महिलाओं का कृषि श्रम अक्सर उनके घरेलू कर्तव्यों के विस्तार के रूप में देखा जाता है, जो इस विचार को मजबूत करता है कि वे पुरुषों की सहायता कर रही हैं, न कि मुख्य श्रमिक हैं।
- सीमित वैकल्पिक अवसर: महिलाओं को निम्न साक्षरता स्तर, सीमित गतिशीलता, और सामाजिक मानदंडों जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें गैर-खेती के रोजगार तक पहुँचने से रोकती हैं। इसके परिणामस्वरूप, कृषि उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एकमात्र व्यवहार्य और सामाजिक रूप से स्वीकार्य आजीविका बन जाती है।
महिलाओं की कृषि में प्रगति को सीमित करने वाली प्रणालीगत बाधाएँ क्या हैं?
स्मरणिका: WOMEN
- W - वेतन भेदभाव: भारत में महिलाएँ पुरुषों की तुलना में 20-30% कम कमाती हैं, जो लिंग वेतन अंतर और आर्थिक असमानता को दर्शाता है, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण सीमित होता है।
- O - निर्णय लेने से वंचित: कृषि विस्तार अधिकारी मुख्यतः पुरुष होते हैं, जिससे महिलाएँ बीज, कीटनाशकों और सतत प्रथाओं की जानकारी से वंचित रहती हैं, जबकि ग्राम पंचायतों और किसान सहकारी समितियों में उनके विचार अक्सर अनदेखे रहते हैं।
- M - मशीनरी और उपकरणों की असंगति: कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेशर पुरुषों के शारीरिक आकार के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जबकि महिलाओं के पास इसे संचालित करने या पहुँचने के लिए आवश्यक ताकत, प्रशिक्षण या वित्तीय साधनों की कमी होती है।
- E - घरेलू दोहरी जिम्मेदारी: घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल से सीमित गतिशीलता और समय की कमी महिलाएँ के लिए बाजारों, कौशल विकास, और सामुदायिक भागीदारी तक पहुँच को सीमित करती है।
- N - भूमि और पहचान अधिकारों का नकारना: महिलाएँ केवल 13-14% भूमि धारिता की मालिक होती हैं, और भूमि शीर्षक के बिना उन्हें कृषक के बजाय उपजकर्ता के रूप में देखा जाता है, जिससे उन्हें ऋण, सरकारी योजनाओं, और स्वतंत्र निर्णय लेने में सीमाएँ आती हैं।
भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए प्रभावी उपाय क्या हो सकते हैं?
स्मरणिका: GROW
- G - बाजार पहुंच की गारंटी: यूनाइटेड किंगडम के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) की तरह, जो कृषि निर्यात को 20% बढ़ाने की उम्मीद है, को चाय, मसाले और डेयरी जैसे महिला-गहन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और महिलाओं को जैविक खाद्य पदार्थों और जीआई-टैग वाले उत्पादों जैसे प्रीमियम उत्पादों के निर्यात में समर्थन देना चाहिए, जिससे वे अपनी पारंपरिक ज्ञान का उपयोग कर सकें।
- R - संसाधन अधिकार और सुधार: महिलाओं के लिए संयुक्त या व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व को बढ़ावा देना चाहिए ताकि उन्हें क्रेडिट, बीमा और सरकारी समर्थन तक पहुंच मिले, और सिद्ध महिला-नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को व्यवस्थित रूप से बढ़ाना चाहिए ताकि वे पैमाने की अर्थव्यवस्था को प्राप्त कर सकें।
- O - डिजिटल द्वार खोलना: डिजिटल प्लेटफार्मों जैसे e-NAM को बढ़ाना, आवाज-प्रथम एआई जैसे BHASHINI, जुगलबंदी और डिजिटल सखी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि डिजिटल और वित्तीय साक्षरता बढ़ सके।
- W - कल्याण और सामाजिक समर्थन: खेतों के पास क्रेच सुविधाएं, जल आपूर्ति और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना चाहिए ताकि महिलाओं का समय गरीबता कम हो सके, जबकि मीडिया अभियानों और पुरस्कारों का उपयोग करके महिला किसानों को आदर्श के रूप में ब्रांड किया जा सके।
कृषि के feminising की क्षमता को harness करने के लिए, भारत को महिलाओं की श्रम शक्ति को पहचानने से उन्हें आर्थिक एजेंटों के रूप में सशक्त बनाने की ओर बढ़ना चाहिए। इसके लिए भूमि अधिकारों की अस्वीकृति और वेतन अंतर जैसे प्रणालीगत बाधाओं को तोड़ना आवश्यक है, जबकि प्रौद्योगिकी, बाजारों और निर्णय लेने की भूमिकाओं तक उनकी पहुंच को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि समावेशी विकास हो सके।
जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी
साइफन-आधारित थर्मल जलविसर्जन प्रणाली
भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के शोधकर्ताओं ने एक नवीन साइफन-आधारित थर्मल जलविसर्जन प्रणाली विकसित की है। यह नई प्रणाली सिलीकरण की समस्याओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करती है, जो ताजे पानी की कमी के लिए एक कम लागत और स्केलेबल समाधान प्रदान करती है।
- पारंपरिक सौर जलवाष्पीकरण की दक्षता को बढ़ाने के लिए विकसित।
- ऑफ-ग्रिड और जल-तनावग्रस्त क्षेत्रों के लिए एक सतत ताजे पानी का स्रोत के रूप में डिजाइन किया गया।
- सिद्धांत: यह प्रणाली साइफन के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें एक कपड़े की बत्ती खारे पानी को खींचती है जबकि गुरुत्वाकर्षण निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करता है।
- नवाचार: एक खांचे वाली धातु की सतह खारे पानी के जमाव को क्रिस्टलीकरण से पहले प्रभावी ढंग से धो देती है, जिससे अवरोधन को रोका जा सके।
- प्रक्रिया: खारे पानी को गर्म सतह पर एक पतली परत के रूप में वाष्पित किया जाता है और इसके बाद ठंडी सतह पर केवल 2 मिमी की दूरी पर संघनित होता है, जिससे उच्च दक्षता प्राप्त होती है।
- उच्च दक्षता: सूर्य के प्रकाश में प्रति वर्ग मीटर प्रति घंटे 6 लीटर से अधिक ताजा पानी उत्पन्न करती है - जो पारंपरिक सौर जलवाष्पीकरण से काफी बेहतर है।
- मल्टीस्टेज डिजाइन: समग्र उत्पादन बढ़ाने के लिए गर्मी को पुनर्चक्रित करने के लिए ढेर में रखे गए वाष्पीकरण- संघनन जोड़े शामिल हैं।
- नमक प्रतिरोध: 20% तक की नमकता को संभालने में सक्षम, जिससे यह खार वाले पानी के उपचार के लिए उपयुक्त बनती है।
- सस्ती सामग्री: एल्युमिनियम और कपड़े से निर्मित, जो उत्पादन लागत को कम रखने में मदद करती है।
- ऊर्जा लचीलापन: सौर ऊर्जा या अपशिष्ट गर्मी पर काम कर सकती है, जिससे यह विभिन्न वातावरणों के लिए अनुकूल हो जाती है।
- स्केलेबल अनुप्रयोग: गांवों, आपदा क्षेत्रों और द्वीप समुदायों में उपयोग के लिए आदर्श।
- स्थिरता: जटिल मशीनरी पर निर्भरता के बिना जलविसर्जन के लिए एक साफ और कम-रखरखाव दृष्टिकोण प्रदान करती है।
यह साइफन-आधारित थर्मल जलविसर्जन प्रणाली पानी की शुद्धि प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है, जो ताजे पानी की कमी का सामना कर रहे क्षेत्रों के लिए स्थायी समाधान प्रदान करने का वादा करती है।
UPSC 2008
भारत में पहली जलविसर्जन प्लांट कहां स्थापित किया गया था, जो निचले तापमान थर्मल जलविसर्जन सिद्धांत पर प्रतिदिन एक लाख लीटर ताजा पानी उत्पादन करता था?
- (a) कवरत्ती
- (b) पोर्ट ब्लेयर
- (c) मैंगलोर
- (d) वलसाड
|
3433 docs|1075 tests
|
FAQs on Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): (29th September 2025 to 5th October 2025) - 1 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC
| 1. भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? |  |
| 2. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा दरें बनाए रखने का क्या प्रभाव पड़ता है? |  |
| 3. भारत में स्मारक संरक्षण के लिए नई नीति में क्या बदलाव किए गए हैं? |  |
| 4. BRO प्रोजेक्ट स्वस्तिक का महत्व क्या है? |  |
| 5. कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन से उपाय किए जा रहे हैं? |  |















