Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): September 15th to 21st, 2025 - 2 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download
जीएस3/अर्थव्यवस्था
NPS से UPS: सरकार ने एक बार विकल्प बढ़ाया
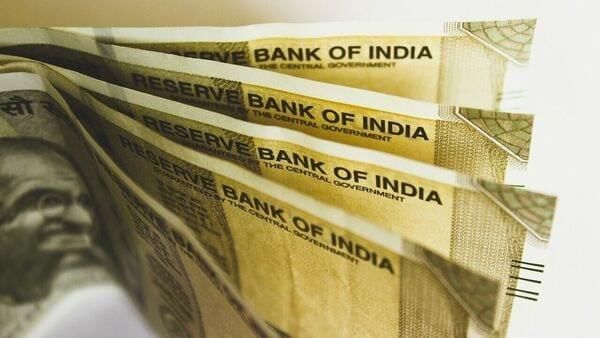 क्यों समाचार में?
क्यों समाचार में?
केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के लिए कर्मचारियों के विकल्प चुनने की समय सीमा को 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। लगभग 23.94 लाख कर्मचारी इस विकल्प के लिए योग्य हैं, लेकिन वर्तमान में केवल लगभग 40,000 ने स्विच किया है। UPS चुनने वाले कर्मचारियों के सेवा मामलों का प्रबंधन करने के लिए, पेंशन और पेंशनभोगियों की कल्याण विभाग ने 2 सितंबर को केंद्रीय सिविल सेवाएं (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 जारी किए हैं।
- सरकार ने NPS के तहत 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2025 के बीच शामिल केंद्रीय कर्मचारियों को UPS में स्थानांतरित होने की अनुमति दी है।
- यह एक बार का विकल्प अन्य योग्य श्रेणियों के लिए मौजूदा कट-ऑफ के साथ मेल खाता है और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय योजना में लचीलापन सुनिश्चित करता है।
- UPS से NPS में स्विच विकल्प: UPS के सदस्य को NPS में स्विच करने का एक बार का विकल्प है लेकिन वे UPS में वापस नहीं जा सकते। स्विच सेवानिवृत्ति से कम से कम एक वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) से तीन महीने पहले किया जाना चाहिए। यह विकल्प बर्खास्तगी या लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के मामलों में उपलब्ध नहीं है।
- पुरानी पेंशन योजना से अंतर: UPS से पहले, 1 जनवरी 2004 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत रखा गया था, जो निश्चित पेंशन की गारंटी देती थी। अप्रैल 2025 में पेश किया गया UPS, अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% गारंटीकृत पेंशन प्रदान करता है, बशर्ते कि कर्मचारी ने न्यूनतम 25 वर्ष सेवा की हो।
- वित्तीय योगदान: NPS के तहत, कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं, जबकि नियोक्ता 14% योगदान करता है। UPS के अंतर्गत, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से 10% समान योगदान की आवश्यकता होती है, इसके अलावा सरकार से 8.5% अतिरिक्त सुनिश्चित पेंशन के लिए।
- UPS 10 वर्षों की सेवा के बाद न्यूनतम ₹10,000 का मासिक भुगतान सुनिश्चित करता है, जो NPS की तुलना में अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें न्यूनतम भुगतान की गारंटी नहीं होती है।
सरकार के UPS को बढ़ावा देने के प्रयासों और समय सीमा बढ़ाने के बावजूद, Uptake कम है क्योंकि कई कर्मचारी OPS को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि इसमें आवश्यक योगदान और गारंटीकृत लाभ नहीं होते। केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम ने NPS और UPS दोनों के बारे में चिंताएं व्यक्त की हैं, OPS की पूर्ण वापसी की वकालत की है।
जीएस3/अर्थव्यवस्था
भारत के अधिग्रहण सुधारों के साथ नवाचार को अनलॉक करना
भारत के सामान्य वित्तीय नियमों (GFR) में हालिया सुधार अधिग्रहण के प्रति दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, विशेष रूप से अनुसंधान और विकास (R&D) के क्षेत्र में। ये सुधार अधिग्रहण को एक अनुपालन-आधारित कार्य से वैज्ञानिक प्रगति के लिए एक रणनीतिक चालक में बदलने का लक्ष्य रखते हैं।
- अधिग्रहण नवाचार के लिए एक उत्प्रेरक हो सकता है, न कि केवल एक अनुपालन तंत्र।
- भारत के सुधार R&D अधिग्रहण पर प्रतिबंधों को आसान बनाते हैं, जिससे शोधकर्ताओं के लिए अधिक लचीलापन मिलता है।
- वैश्विक उदाहरण सफल अधिग्रहण रणनीतियों को प्रदर्शित करते हैं जो तकनीकी प्रगति को प्रेरित करते हैं।
- अधिग्रहण की द्वैतीय प्रकृति: लागत दक्षता और नवाचार के बीच का तनाव अधिग्रहण प्रक्रियाओं में अंतर्निहित है। कठोर ढांचे वैज्ञानिक प्रगति में बाधा डाल सकते हैं, जैसा कि भारत की पिछली प्रणाली में देखा गया, जिसमें शोधकर्ताओं को आवश्यक विशिष्ट उपकरणों की अनुपलब्धता के बावजूद सरकारी ई-बाजार (GeM) का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया।
- हालिया सुधार: जून 2025 में महत्वपूर्ण सुधार पेश किए गए, जैसे कि संस्थागत प्रमुखों को विशेष उपकरणों के लिए GeM को बायपास करने की अनुमति देना और सीधे खरीद के लिए सीमा बढ़ाना। यह अनुसंधान में अनुकूलित अधिग्रहण समाधान की आवश्यकता को स्वीकार करता है।
- वैश्विक सबक: जर्मनी, अमेरिका, और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य देशों ने नवाचारी अधिग्रहण रणनीतियों को लागू किया है जो तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देती हैं, यह दिखाते हुए कि मिशन-उन्मुख अधिग्रहण के संभावित लाभ हैं।
- भविष्य की दिशा: अधिग्रहण को और बढ़ाने के लिए, भारत परिणाम-भारित टेंडर लागू कर सकता है, प्रमुख संस्थानों के लिए सैंडबॉक्स छूट प्रदान कर सकता है, स्रोत में एआई का उपयोग कर सकता है, और सह-अधिग्रहण गठबंधन स्थापित कर सकता है।
अंत में, जबकि भारत के GFR सुधार अनुसंधान में अधिग्रहण की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं, वे आवश्यक परिवर्तन की शुरुआत मात्र हैं। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारी रणनीतियों को अपनाकर, भारत अधिग्रहण को वैज्ञानिक खोज के एक शक्तिशाली सक्षमकर्ता में बदल सकता है।
GS2/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध
चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंध
समाचार में क्यों?
ट्रंप प्रशासन ने चाबहार बंदरगाह के लिए प्रतिबंध छूट को रद्द कर दिया है, जिससे भारत की अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रभावित हो रही है और क्षेत्र में इसकी स्ट्रैटेजिक स्थिति कमजोर हो रही है। 2018 में ईरान फ्रीडम और काउंटर-प्रोलिफरेशन एक्ट (IFCA) के तहत दी गई यह छूट भारत को चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक द्वार के रूप में विकसित करने के अपने दीर्घकालिक योजना को आगे बढ़ाने की अनुमति देती थी।
चाबहार बंदरगाह पर लगाए गए प्रतिबंधों के विमोचन के भारत के लिए क्या परिणाम हैं?
- स्ट्रैटेजिक परिणाम: चाबहार के विमोचन का निरसन भारत की क्षेत्रीय ताकत को कमजोर कर सकता है, जिससे इसकी क्षमता ग्वादर बंदरगाह का मुकाबला करने, रूस और यूरोप को जोड़ने वाले अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) में एकीकृत होने, और अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया में प्रभाव बनाए रखने में सीमित हो जाएगी।
- आर्थिक और व्यापारिक परिणाम: भारत के ईरान और अफगानिस्तान के लिए निर्यात—जिसमें वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान, औषधियां, और खाद्य उत्पाद शामिल हैं—को बाधा का सामना करना पड़ सकता है, जबकि 120 मिलियन USD का निवेश और 250 मिलियन USD की प्रतिबद्धताएं जोखिम में हैं। यह विमोचन भारत-यूएस व्यापार वार्ताओं और श्रम-गहन वस्तुओं पर 50% शुल्क के साथ मेल खाता है, जिससे भारत की निर्यात रणनीति पर दबाव बढ़ता है।
- संचालन और कानूनी जोखिम: भारतीय पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) जैसी कंपनियों को IFCA के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रति संवेदनशीलता का सामना करना पड़ सकता है, जिससे चाबहार व्यापार और विस्तार परियोजनाओं में देरी या निलंबन हो सकता है।
- भौगोलिक राजनीतिक परिणाम: विमोचन भारत-यूएस संबंधों पर दबाव डालता है और भारत की योजना को एक महत्वपूर्ण व्यापार और मानवीय सहायता के द्वार के रूप में चाबहार बंदरगाह का उपयोग करने के लिए एक बड़ा झटका है, विशेष रूप से अफगानिस्तान के लिए।
चाबहार बंदरगाह
बारे में: यह एक गहरे पानी का बंदरगाह है जो ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान में, ओमान की खाड़ी के पास मक़रान तट पर स्थित है, जो हार्मुज़ जलडमरूमध्य से बाहर है। यह ईरान का एकमात्र गहरे समुद्र का बंदरगाह है जिसका सीधा खुला महासागर तक पहुंच है, जो भारत को बड़े मालवाहक जहाजों के लिए सुरक्षित और सीधे पहुंच प्रदान करता है। इसमें दो मुख्य टर्मिनल हैं—शहीद बेहेश्ती और शहीद कलंतरी—जहां भारत सक्रिय रूप से शहीद बेहेश्ती टर्मिनल के विकास में शामिल है।
विकास एवं प्रबंधन: चाबहार समझौता (2016) भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और ट्रांजिट गलियारे की स्थापना के लिए हस्ताक्षरित किया गया। आईपीजीएल, अपनी सहायक कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री ज़ोन (IPGCFZ) के माध्यम से, दिसंबर 2018 में चाबहार बंदरगाह के संचालन का अधिग्रहण किया।
संचालन प्रदर्शन: अब तक, चाबहार बंदरगाह ने भारत से अफगानिस्तान के लिए 2.5 मिलियन टन गेहूं और 2,000 टन दालों का ट्रांसशिप किया है, 2021 में ईरान के लिए 40,000 लीटर मलेटोन (पर्यावरण-अनुकूल कीटनाशक) का प्रावधान किया है, और मानवीय सहायता का समर्थन किया है, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान भी शामिल है।
चाबहार पोर्ट का भारत के लिए महत्व क्या है?
- वैकल्पिक व्यापार मार्ग: यह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, पाकिस्तान को обход करते हुए, और कांडला पोर्ट से छोटे मार्गों के माध्यम से ईरान और INSTC तक पहुंच को बेहतर बनाता है।
- संयोग सुनिश्चित करना: पश्चिम एशियाई क्षेत्र में चल रहे संघर्ष और तनाव, जैसे यमन संकट और ईरान और पाकिस्तान के बीच हाल की बढ़ती तनाव, महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों को बाधित कर चुके हैं। चाबहार भारत को इसके वाणिज्यिक हितों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, जिससे पारंपरिक चोकपॉइंट्स जैसे होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भरता कम होती है।
- आर्थिक लाभ: यह भारत के मध्य एशिया और अफगानिस्तान के साथ व्यापार को मजबूत करता है, मार्गों को विविधता प्रदान करता है, और रूस, यूरोप, ईरान और अफगानिस्तान तक पहुंच को बढ़ाता है। चाबहार पोर्ट, एक प्रमुख INSTC नोड, भारतीय महासागर को उत्तरी यूरोप से जोड़ता है, जिससे व्यापार लागत में 30% और पारगमन समय में 40% की कमी आती है, जबकि भूमि लॉक देशों को भारतीय महासागर और भारतीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करता है।
- मानवीय सहायता: यह अफगानिस्तान में मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है।
- सामरिक प्रभाव: यह भारतीय महासागर में भारत की सामरिक उपस्थिति को मजबूत करता है, चीन के ग्वादर पोर्ट और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का मुकाबला करता है, और समुद्री डकैती के खिलाफ क्षमता को बढ़ाता है।
निष्कर्ष
चाबहार पोर्ट भारत के क्षेत्रीय प्रभाव, व्यापार संभावनाओं और संपर्क की आकांक्षाओं के लिए केंद्रीय बना हुआ है। इसके रणनीतिक संतुलन के रूप में भूमिका, यूएस प्रतिबंधों, क्षेत्रीय अस्थिरता और प्रतिस्पर्धी परियोजनाओं के बावजूद, स्थायी अवसर प्रदान करती है।
GS1/इतिहास और संस्कृति
भारत ने UNESCO की अस्थायी सूची में 7 प्राकृतिक स्थलों को जोड़ा
भारत ने UNESCO की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में सात प्राकृतिक स्थलों को शामिल किया है, जिससे इसकी कुल संख्या 69 हो गई है। यह भारत की अपने समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर स्थलों की सूची क्या है?
अस्थायी सूची यूनेस्को विश्व धरोहर नामांकन की दिशा में पहला कदम है। देश विशेष वैश्विक मूल्य वाले स्थलों की पहचान करते हैं और उन्हें यूनेस्को के लिए विचार हेतु प्रस्तुत करते हैं। केवल इस सूची में शामिल स्थलों को पूर्ण नामांकन के लिए नामित किया जा सकता है। भारत में, पुरातत्व सर्वेक्षण भारत (ASI) इन नामांकनों को संकलित और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है।
भारत के नए जोड़े गए स्थल
- डेक्कन ट्रैप्स, पचगनी और महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। ये स्थल अपने भली-भांति संरक्षित लावा प्रवाहों के लिए जाने जाते हैं और डेक्कन ट्रैप्स का हिस्सा हैं, जो कोयना वन्यजीव अभयारण्य में स्थित हैं, जो पहले से ही एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
- सेंट मैरीज़ आइलैंड क्लस्टर का भूवैज्ञानिक धरोहर, कर्नाटक। यह द्वीप समूह अपने अद्वितीय स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टान संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो लेट क्रेटेशियस काल में, लगभग 101 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व की हैं।
- मेघालयन युग की गुफाएँ, मेघालय। मेघालय में गुफाओं के प्रणाली, विशेषकर माव्मलुह गुफा, महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे होलोसीन युग में मेघालयन युग के लिए वैश्विक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करती हैं, जो पिछले 11,000 वर्षों में महत्वपूर्ण जलवायु और भूवैज्ञानिक परिवर्तनों को दर्शाती हैं।
- नागा हिल ओफिओलाइट, नगालैंड। यह स्थल ओफिओलाइट चट्टानों का दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो महासागरीय क्रस्ट को महाद्वीपीय प्लेटों पर उठाए गए दर्शाते हैं, जिससे टेक्टोनिक प्रक्रियाओं और मध्य महासागर रिज की गतियों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
- एर्रा मत्ति डिब्बालु (लाल बालू की पहाड़ियाँ), आंध्र प्रदेश। विशाखापत्तनम के पास ये लाल बालू संरचनाएँ अद्वितीय पैलियो-जलवायु और तटीय भूआकृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करती हैं, जो पृथ्वी के जलवायु इतिहास और विकास के बारे में जानकारी देती हैं। एर्रा मत्ति डिब्बालु को 2016 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा एक भू-धरोहर स्मारक के रूप में नामित किया गया था।
- तिरुमाला पहाड़ियों का प्राकृतिक धरोहर, आंध्र प्रदेश। इस स्थल में एपारचियन असंगति और सिलाथोरनम (प्राकृतिक मेहराब) शामिल है, जो भूवैज्ञानिक महत्व रखता है और पृथ्वी के 1.5 बिलियन से अधिक वर्षों के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्थल शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व और वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है।
- वारकला चट्टानें, केरल। केरल के तट पर ये चट्टानें मियो-प्लायोसीन युग के वार्कल्ली गठन को उजागर करती हैं, साथ ही प्राकृतिक झरने और विशिष्ट कटावीय भूआकृतियाँ प्रदर्शित करती हैं, जो वैज्ञानिक और पर्यटन दोनों के लिए मूल्यवान हैं।
विश्व धरोहर स्थलों (WHS) को विशेष वैश्विक मूल्य के स्थानों के रूप में मान्यता दी जाती है, जो उनके महत्व के लिए संरक्षित होते हैं ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सकें। ये स्थल सांस्कृतिक, प्राकृतिक, या मिश्रित हो सकते हैं और 1972 के विश्व धरोहर सम्मेलन के तहत संरक्षित होते हैं, जिसे यूनेस्को के सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया था। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति इस सूची के रखरखाव का संचालन करती है। भारत ने इस सम्मेलन की पुष्टि 1977 में की थी।
सितंबर 2025 तक, भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 44 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से मराठा सैन्य परिदृश्य भारत का 44वां और नवीनतम स्थल है।
GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध
भारत अमेरिका की फेंटेनाइल संबंधी ब्लैकलिस्ट में

हालिया रिपोर्ट, जिसे मेजर की लिस्ट कहा जाता है, में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान जैसे 22 अन्य देशों के साथ गैरकानूनी ड्रग्स, विशेष रूप से फेंटेनाइल, के महत्वपूर्ण स्रोत या ट्रांजिट हब के रूप में पहचान किया है। यह वर्गीकरण अमेरिका और उसके नागरिकों के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।
- मेजर की लिस्ट उन राष्ट्रों को रेखांकित करती है जो नशीले पदार्थों या पूर्ववर्ती रासायनिक प्रवाह में शामिल हैं।
- फेंटेनाइल एक सिंथेटिक ओपियोइड है, जो अमेरिका में ओवरडोज मौतों का प्रमुख कारण बन गया है।
- फेंटेनाइल को नियंत्रित करना इसकी सिंथेटिक प्रकृति और पूर्ववर्ती रसायनों की उपलब्धता के कारण चुनौतीपूर्ण है।
- फेंटेनाइल: 1960 के दशक में गंभीर दर्द को प्रबंधित करने के लिए विकसित किया गया एक शक्तिशाली सिंथेटिक ओपियोइड, यह अब अमेरिका में ओवरडोज मौतों की एक महत्वपूर्ण संख्या का जिम्मेदार है, जो हेरोइन से लगभग 50 गुना अधिक मजबूत है। केवल 2 मिलीग्राम इसका सेवन करना घातक हो सकता है।
- अगस्त 2023 से अगस्त 2024 के बीच, 57,000 से अधिक अमेरिकियों की ओपियोइड ओवरडोज से मौत हुई, जो मुख्यतः फेंटेनाइल से संबंधित थी।
- आपूर्ति श्रृंखला की जटिलता: फेंटेनाइल व्यापार में एक नेटवर्क शामिल है जहां चीन और भारत जैसे देश पूर्ववर्ती रसायनों का उत्पादन करते हैं, जिन्हें फिर मेक्सिकन कार्टेल द्वारा फेंटेनाइल में प्रोसेस किया जाता है और अमेरिका में तस्करी की जाती है।
- अमेरिका की प्रतिक्रिया में DEA द्वारा बढ़ी हुई जब्ती और ओपियोइड नशे के लिए उपचार कार्यक्रमों तथा नालोक्सोन वितरण जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शामिल हैं।
भारत का मेजर की लिस्ट में समावेश फेंटेनाइल तस्करी से उत्पन्न चुनौतियों और इसके सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव के समाधान के लिए बढ़ती जांच और सहयोग की आवश्यकता को संकेत देता है।
जीएस3/अर्थव्यवस्था
सरकार नई नीति के तहत भू-तापीय पायलट परियोजनाओं को बढ़ावा देगी
नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने भारत में भू-तापीय संसाधनों के विकास और नियमन के लिए एक ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी पहली राष्ट्रीय नीति पर भू-तापीय ऊर्जा की शुरुआत की है।
- यह नीति सितंबर 2025 में आधिकारिक रूप से घोषित की गई थी।
- यह भारत के 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य का समर्थन करती है।
- इसका दायरा विद्युत उत्पादन और प्रत्यक्ष उपयोग के अनुप्रयोगों दोनों को शामिल करता है।
- MNRE कार्यान्वयन का नेतृत्व करेगा, विभिन्न भागीदारों के साथ सहयोग करते हुए।
- वित्तीय समर्थन में कर प्रोत्साहन और अनुदान शामिल हैं।
- वित्तीय और नियामक समर्थन: नीति कर प्रोत्साहन, अनुदान, और रियायती वित्तपोषण प्रदान करती है, इसके साथ ही 30 वर्षों तक के दीर्घकालिक पट्टे भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, उच्च प्रारंभिक लागतों को कवर करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) प्रदान की जाती है, जिसकी अनुमानित लागत ₹36 करोड़ प्रति मेगावाट है।
- नीति का जोर परित्यक्त तेल और गैस कुओं को भू-तापीय ऊर्जा के लिए पुनः उपयोग करने पर है, जिसमें पहले से ही ONGC और वेदांता लिमिटेड के साथ सहयोग स्थापित किया गया है।
- वैश्विक भागीदारी देशों जैसे आइसलैंड, नॉर्वे, अमेरिका, और इंडोनेशिया के साथ अनुसंधान और विकास के लिए स्थापित की गई है, जो Enhanced और Advanced Geothermal Systems में है।
- वर्तमान में, विभिन्न क्षेत्रों में संसाधन मूल्यांकन और प्रदर्शन के लिए पांच पायलट परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
भारत की भू-तापीय ऊर्जा की क्षमता का अनुमान 10.6 GW है, जैसा कि भूगर्भीय सर्वेक्षण भारत (GSI) द्वारा पहचाना गया है, जिसमें देश भर में 381 से अधिक गर्म झरनों का मानचित्रण किया गया है। हालांकि, अभी तक कोई ग्रिड से जुड़े भू-तापीय संयंत्र नहीं हैं, लेकिन चल रही परियोजनाओं में तेलंगाना के मनुगुरु में 20 kW की पायलट बाइनरी-साइकिल संयंत्र और लद्दाख, गुजरात, और राजस्थान में अन्य पायलट परियोजनाएं शामिल हैं। भविष्य का रोडमैप 2030 तक भू-तापीय क्षमता को 10 GW और 2045 तक लगभग 100 GW तक पहुंचाने का लक्ष्य रखता है।
निम्नलिखित पर विचार करें:
- 1. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण
- 2. भू-तापीय ऊर्जा
- 3. गुरुत्वाकर्षण बल
- 4. प्लेटों की गति
- 5. पृथ्वी का घूर्णन
- 6. पृथ्वी का क्रांति
उपरोक्त में से कौन सी तत्व पृथ्वी की सतह पर गतिशील परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं?
(a) केवल 1, 2, 3 और 4
(b) केवल 1, 3, 5 और 6
(c) केवल 2, 4, 5 और 6
(d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6
जीएस2/शासन
अपराध मामलों में DNA साक्ष्य पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश
 समाचार में क्यों?
समाचार में क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने कत्तावेल्लाई @ देवाकर बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि अपराध मामलों में DNA साक्ष्य के प्रबंधन को मानकीकृत किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य महत्वपूर्ण मामलों में साक्ष्य के क्षतिग्रस्त होने के बाद होने वाली संदूषण और देरी को रोकना है।
- इस मामले में बलात्कार, हत्या, और डकैती जैसे गंभीर आरोप शामिल थे।
- कोर्ट ने फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) में प्रस्तुतियों में देरी, अनुचित चेन ऑफ कस्टडी, और साक्ष्य के संदूषण का खतरा जैसे मुद्दों को उजागर किया।
- राज्यों में समान प्रक्रियाओं की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि मौजूदा दिशा-निर्देश बिखरे हुए और असंगत हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने DNA साक्ष्य के प्रबंधन में राष्ट्रीय एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप किया है।
- संग्रह और दस्तावेजीकरण: DNA नमूनों को सही तरीके से पैक किया जाना चाहिए, FIR विवरण के साथ लेबल किया जाना चाहिए, और चिकित्सा अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी (IO), तथा गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- परिवहन: अनुसंधान अधिकारी को नमूनों को FSL में 48 घंटे के भीतर पहुंचाना आवश्यक है, और किसी भी देरी के कारणों को दर्ज करना चाहिए।
- मुकदमे के लिए भंडारण: साक्ष्य के पैकेज को बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति के खोला या फिर से सील नहीं किया जा सकता।
- चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर: इसे सजा या बरी होने तक बनाए रखना चाहिए, और IO को किसी भी कमी का समाधान करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।
DNA साक्ष्य पर सुप्रीम कोर्ट की पिछली टिप्पणियाँ
- अनिल बनाम महाराष्ट्र (2014): DNA साक्ष्य को तभी विश्वसनीय माना जाता है जब प्रयोगशाला प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जाए।
- मनोज बनाम मध्य प्रदेश (2022): DNA साक्ष्य को संदूषण के जोखिम के कारण अस्वीकार किया गया क्योंकि पुनर्प्राप्ति एक खुले क्षेत्र से की गई थी।
- राहुल बनाम दिल्ली (2022): पुलिस हिरासत में दो महीने तक रखने के बाद DNA साक्ष्य को स्वीकार्य नहीं माना गया।
- पट्टू राजन बनाम तमिलनाडु (2019): DNA साक्ष्य का मूल्य सहायक साक्ष्य पर निर्भर करता है; इसकी अनुपस्थिति किसी मामले के लिए अनिवार्यतः घातक नहीं है।
- शारदा बनाम धर्मपाल (2003): DNA परीक्षण के आदेश वैध हैं और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करते।
- दास @ अनु बनाम केरल (2022): अनुच्छेद 20(3) के तहत DNA संग्रह को आत्म-प्रवर्तन नहीं माना जाता; दुष्कर्म मामलों में संग्रह के लिए CrPC की धारा 53A की अनुमति है।
बैक2बेसिक्स: DNA प्रोफाइलिंग
- सारांश: DNA प्रोफाइलिंग, जिसे DNA फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है, एक फोरेंसिक विधि है जिसका उपयोग व्यक्तियों की पहचान करने के लिए विशिष्ट DNA क्षेत्रों का विश्लेषण करके किया जाता है, विशेष रूप से शॉर्ट टेंडम रिपीट्स (STRs)।
- कैसे काम करता है: मानव DNA 99.9% समान होता है; 0.1% वैरिएबिलिटी ही व्यक्तिगत पहचान को संभव बनाती है।
- स्रोत: DNA को विभिन्न जैविक सामग्रियों से निकाला जा सकता है, जैसे कि रक्त, वीर्य, लार, बाल, हड्डी, त्वचा, या यहां तक कि "टच DNA"।
- प्रक्रियाएँ: DNA प्रोफाइलिंग प्रक्रिया में आइसोलेशन, शुद्धिकरण, अम्लन, दृश्यमानता, और DNA मार्कर्स की सांख्यिकीय तुलना शामिल होती है।
- विधियाँ: मिनीSTRs और माइटोकॉन्ड्रियल DNA (mtDNA) जैसी तकनीकें क्षीण या सीमित नमूनों का विश्लेषण करने के लिए उपयोगी होती हैं।
- कानूनी स्थिति: DNA साक्ष्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 (अब BSA 2023 की धारा 39) के तहत विशेषज्ञ राय के रूप में माना जाता है, जो सहायक साक्ष्य के रूप में कार्य करता है न कि मुख्य साक्ष्य के रूप में।
संक्षेप में, सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उद्देश्य आपराधिक कार्यवाही में DNA साक्ष्य की अखंडता और विश्वसनीयता को बढ़ाना है, मौजूदा खामियों को संबोधित करना और देशभर में प्रक्रियाओं में एकरूपता सुनिश्चित करना है।
GS3/Environment
वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संकट कितनी गंभीर है?
वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण का संकट एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक चुनौती में बदल गया है। एक समय में इसकी सुविधा के लिए प्रशंसा की गई, प्लास्टिक की गैर-बायोडिग्रेडेबल प्रकृति और बढ़ती खपत दरों ने गंभीर पारिस्थितिकी परिणामों को जन्म दिया है। इस वर्ष की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम, प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करना, इस संकट के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकतानुसार जोर देती है, जो स्वास्थ्य, शासन और पर्यावरणीय स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है।
- प्लास्टिक उत्पादन 2024 में 500 मिलियन टन तक पहुँच गया, जिससे 400 मिलियन टन कचरा उत्पन्न हुआ।
- वर्तमान प्रवृत्तियों के अनुसार, प्लास्टिक कचरा 2060 तक 1.2 बिलियन टन तक तीन गुना हो सकता है।
- विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मध्य सदी तक, महासागरों में मछलियों की तुलना में अधिक प्लास्टिक हो सकता है।
- बढ़ती खपत: 2000 से 2019 के बीच, प्लास्टिक उत्पादन दोगुना होकर 460 मिलियन टन तक पहुँच गया।
- कचरा वृद्धि: 2019 में, वैश्विक प्लास्टिक कचरा 353 मिलियन टन था, जिसमें पैकेजिंग का हिस्सा 40% था।
- पुनर्चक्रण की विफलता: केवल 9% प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण किया जाता है, जबकि 50% लैंडफिल में चला जाता है और 22% पर्यावरण में भाग जाता है।
- महासागरीय खतरा: प्रत्येक वर्ष लगभग 11 मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों में जाता है, जो पहले से मौजूद 200 मिलियन टन में जोड़ता है।
- जलवायु संबंध: प्लास्टिक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 3.4% योगदान करते हैं और 2040 तक वैश्विक कार्बन बजट का 19% उपभोग कर सकते हैं।
प्लास्टिक प्रदूषण की चुनौती इसकी गैर-बायोडिग्रेडेबल प्रकृति के कारण और बढ़ जाती है, जो प्लास्टिक को सूक्ष्म और नैनो-कणों में टूटने की अनुमति देती है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण फैलता है, जो सबसे ऊँची चोटियों से लेकर सबसे गहरे महासागर की खाइयों तक फैला हुआ है। सूक्ष्मप्लास्टिक्स से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम खाद्य श्रृंखलाओं और जल सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, जबकि गरीब देश अपर्याप्त कचरा प्रबंधन प्रणालियों का आर्थिक बोझ उठाते हैं।
वैश्विक उपायों का प्रस्तावित
- कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता: UNEA-5 में, 2022 में, सभी 193 यूएन सदस्य राज्यों ने प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई।
- UNEP लक्ष्य: नवाचार और पुनर्चक्रण के माध्यम से अगले दो दशकों में प्लास्टिक अपशिष्ट को 80% तक कम करने का लक्ष्य।
- एकल-उपयोग प्लास्टिक में कमी: अनावश्यक पेट्रोकेमिकल उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की तत्काल आवश्यकता।
- विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR): विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से निर्माताओं को जवाबदेह ठहराना।
- पुनर्चक्रण क्रांति: वर्तमान में, केवल 6% प्लास्टिक पुनर्चक्रित स्रोतों से आते हैं, जिससे इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए तकनीकी उन्नति और बाजार प्रोत्साहनों की आवश्यकता है।
व्यक्तियों और मीडिया की भूमिका
- हरे विकल्प: पारंपरिक, पुन: उपयोग होने वाले उत्पादों और पर्यावरण-अनुकूल सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- जागरूकता अभियान: मीडिया उपभोक्ता आदतों को आकार देने और सरकारी नीतियों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- व्यवहार परिवर्तन: प्लास्टिक के उपभोग में सामूहिक कमी आवश्यक है, साथ ही प्रणालीगत सुधार भी।
अंत में, प्लास्टिक प्रदूषण आधुनिक विकास के विरोधाभासों को उजागर करता है, जहां सुविधा ने एक संकट को जन्म दिया है। डेटा यह दर्शाता है कि मानवता एक मोड़ पर है: अस्थायी प्रथाओं को जारी रखना या वृत्ताकार, सतत अर्थव्यवस्थाओं की ओर संक्रमण करना। भारत जैसे देशों के लिए, जो अनोखे विकासात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करना पर्यावरण शासन, जलवायु कार्रवाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।
UPSC प्रासंगिकता
UPSC 2023 के संदर्भ में, तेल प्रदूषण और इसके समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक और तेल प्रदूषण दोनों पेट्रोकेमिकल स्रोतों से उत्पन्न होते हैं और जैव विविधता, मत्स्य पालन, और तटीय आजीविका को खतरे में डालते हैं। भारत के लिए, इसके गंभीर परिणाम हैं क्योंकि इसकी व्यापक तटरेखा और समुद्री संसाधनों पर निर्भरता है, जिससे आजीविका का नुकसान और पारिस्थितिक असंतुलन का जोखिम बढ़ता है।
जीएस3/अर्थव्यवस्था
जीएसटी 2.0 — तात्कालिक दर्द, संभावित दीर्घकालिक लाभ
 क्यों समाचार में?
क्यों समाचार में?
वस्तु और सेवा कर (GST), जो एक गंतव्य-आधारित कर प्रणाली स्थापित करने के लिए बनाया गया था, ने यह सुनिश्चित किया कि करों का अंतिम बोझ अंत उपभोक्ताओं पर पड़े। प्रारंभिक कार्यान्वयन में कई कर दरों, उल्टे शुल्क संरचनाओं, और महत्वपूर्ण अनुपालन लागतों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नया GST दर ढांचा, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होगा, उपभोग, उत्पादन, सरकारी राजस्व, और समग्र मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता पर व्यापक प्रभाव डालने वाला एक महत्वपूर्ण संशोधन है।
- 2025 का सुधार GST दर संरचना को सरल बनाता है, जिसमें अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं को तीन मुख्य कर दरों: 0%, 5%, और 18% में समेकित किया गया है, साथ ही विलासिता और पाप के सामानों के लिए 40% की दंडात्मक दर है।
- 546 वस्तुओं की समीक्षा में से लगभग 80% वस्तुएं कर दर में कमी देखेंगे, जिनसे वस्त्र, ऑटोमोबाइल, और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा।
- हालांकि संभावित उपभोक्ता लाभ हैं, लेकिन सुधार सरकार के लिए महत्वपूर्ण राजस्व हानि और वित्तीय अस्थिरता पैदा कर सकते हैं।
- राजस्व प्रभाव:GST राजस्व (R) को कर दर (r) और कर आधार (E) के गुणनफल के रूप में गणना किया जाता है। जबकि कम कर दरों से मांग को उत्तेजना मिल सकती है, वे समग्र राजस्व में समान अनुपात में वृद्धि नहीं कर सकते, जो संभावित राजस्व कमी का कारण बन सकता है।
- कमियों की पूर्वानुमान: वित्त मंत्रालय वार्षिक राजस्व हानि ₹48,000 करोड़ का अनुमान लगाता है, जो वित्तीय स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
- आय प्रभाव: सुधार से प्रारंभ में आवश्यक वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए ख़र्च करने योग्य आय में वृद्धि हो सकती है, लेकिन कम GST दरें उच्च दर वाली वस्तुओं की ओर उपभोग में बदलाव ला सकती हैं, जो दीर्घकाल में सरकार को लाभ पहुंचा सकती हैं।
- कैस्केडिंग मुद्दे: संशोधित GST ढांचा सभी कैस्केडिंग प्रभावों को समाप्त करने में विफल है, क्योंकि छूट प्राप्त वस्तुएं इनपुट कर क्रेडिट (ITC) की अनुमति नहीं देतीं, जिससे व्यवसायों के लिए दावा करने की प्रक्रिया जटिल हो जाती है।
- मैक्रोइकोनॉमिक चुनौतियाँ: नाममात्र जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमानों से कम होने के कारण, GST राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है, जो केंद्रीय और राज्य बजट पर दबाव डालता है।
निष्कर्षतः, 2025 के GST सुधार कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास हैं। ये कम कीमतें और ख़र्च करने योग्य आय में वृद्धि का वादा करते हैं, विशेषकर श्रम-गहन क्षेत्रों में। हालाँकि, संबंधित वित्तीय लागतें और अनसुलझी अस्थिरताएँ चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं जो इन सुधारों की दीर्घकालिक प्रभावशीलता को कमजोर कर सकती हैं। सतत विकास अंततः निवेश क्षमता और उत्पादकता में सुधार पर निर्भर करेगा।
GS1/History & Culture
ASI द्वारा सारनाथ पट्टिका का संशोधन, बनारस शासक के परिवार को श्रेय
भारतीय पुरातात्त्विक सर्वेक्षण (ASI) सारनाथ की पट्टिका को अपडेट करने जा रहा है, ताकि बनारस शासक के परिवार के योगदान को विरासत स्थल के संरक्षण में मान्यता दी जा सके, न कि इस श्रेय को केवल ब्रिटिश अधिकारियों को दिया जाए, यूनेस्को टीम की यात्रा से पहले।
- सारनाथ: सारनाथ एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है जो वाराणसी, उत्तर प्रदेश के निकट स्थित है।
- अपडेट की गई पट्टिका 18वीं शताब्दी के अंत से जगत सिंह के योगदान को मान्यता देगी।
- यह संशोधन भारत में ऐतिहासिक naratives के उपनिवेशीकरण के लिए एक व्यापक आंदोलन को दर्शाता है।
- सारनाथ: वाराणसी से लगभग 10 किमी दूर, सारनाथ को उस स्थल के रूप में पूजा जाता है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपनी पहली उपदेश दिया था, जो बौद्ध समुदाय की शुरुआत को चिह्नित करता है।
- बुद्ध का पहला उपदेश: लगभग 528 ई.पू. में, बुद्ध ने यहाँ चार आर्य सत्य और आठfold पथ को साझा किया, जो बौद्ध दर्शन की नींव स्थापित करता है।
- मौर्य समर्थन: सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ई.पू. में सारनाथ का दौरा किया, स्तूपों और स्तंभों का निर्माण किया, जिसमें प्रसिद्ध अशोक का सिंहासन शामिल है, जो अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है।
- ऐतिहासिक श्रेय: हालिया शोध से पता चलता है कि जगत सिंह की खुदाई 1787-88 में सारनाथ के अवशेषों को उजागर करने में महत्वपूर्ण थी, जो पिछले naratives को चुनौती देती है जो ब्रिटिश अधिकारियों को श्रेय देती थीं।
- संशोधन का महत्व: आगामी पट्टिका परिवर्तन स्थानीय योगदानों को विरासत संरक्षण में मान्यता देने और भारत की सांस्कृतिक कूटनीति के प्रयासों के साथ मेल खाने का एक बड़ा हिस्सा है।
यह संशोधन न केवल ऐतिहासिक रिकॉर्ड को सही करने का प्रयास है, बल्कि यह विरासत स्थलों के लिए स्वदेशी योगदानों को मान्यता देने के महत्व पर भी जोर देता है, विशेष रूप से क्योंकि सारनाथ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार है।
|
7 videos|3454 docs|1081 tests
|
FAQs on Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): September 15th to 21st, 2025 - 2 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC
| 1. NPS से UPSC का क्या संबंध है और यह विकल्प कैसे बढ़ा गया ? |  |
| 2. चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंधों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है ? |  |
| 3. भारत ने UNESCO की अस्थायी सूची में 7 प्राकृतिक स्थलों को क्यों जोड़ा ? |  |
| 4. DNA साक्ष्य पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का क्या महत्व है ? |  |
| 5. जीएसटी 2.0 के संभावित दीर्घकालिक लाभ क्या हैं ? |  |















