एनसीईआरटी सारांश: भारत में शेयर बाजार - 3 | UPSC CSE (हिंदी) के लिए पुरानी और नई एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें PDF Download
कर संग्रहण
भारत सरकार के कर राजस्व ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 32.61 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया, जो मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और बढ़ी हुई कर अनुपालन उपायों के कारण महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। प्रत्यक्ष करों ने कुल कर राजस्व का 58.4% हिस्सा बनाया, जो सामाजिक और विकासात्मक पहलों के लिए आय और कॉर्पोरेट कर संग्रहण पर बढ़ती निर्भरता को रेखांकित करता है।
कर संग्रहण में वृद्धि के कारण:
- मजबूत आर्थिक वृद्धि: भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले दशक में औसत वार्षिक दर 7% की वृद्धि की है।
- बढ़ती आय: उच्च निपटान आय ने प्रत्यक्ष कर योगदान में वृद्धि की है।
- सुधरे हुए अनुपालन: ई-फाइलिंग जैसे सरल कर प्रक्रियाओं ने अनुपालन दरों को बढ़ाया है।
- तकनीकी एकीकरण: कुशल कर प्रशासन के लिए उन्नत विश्लेषण और AI-आधारित सिस्टम का उपयोग किया जाता है और कर चोरी की पहचान के लिए।
- कर आधार का विस्तार: अधिक व्यक्तियों और व्यवसायों को कर जाल में लाने के लिए निरंतर प्रयास।
प्रत्यक्ष कर
प्रत्यक्ष कर सरकार के राजस्व में एक प्रमुख योगदानकर्ता बने हुए हैं।
- कॉर्पोरेट कर: कॉर्पोरेट कर संग्रहण में वृद्धि महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरीकरण और स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए प्रोत्साहनों के कारण निरंतर बनी हुई है।
- व्यक्तिगत आय कर: हाल के बजट में संशोधित कर स्लैब ने संग्रहण में वृद्धि की है जबकि करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाया है।
हाल के सुधारों में शामिल हैं:
अपडेटेड कर स्लैब (2025):
- 0% आय के लिए ₹3 लाख तक
- 5% आय के लिए ₹3 लाख से ₹7.5 लाख के बीच
- 10% आय के लिए ₹7.5 लाख से ₹15 लाख के बीच
- 20% आय के लिए ₹15 लाख से अधिक
- Ultra-high incomes पर 30% अधिभार जो ₹2 करोड़ से अधिक हैं
- E-उद्यम: मानव हस्तक्षेप को कम करने के लिए वास्तविक समय निगरानी और बिना चेहरे के आकलन प्रणाली का कार्यान्वयन।
अप्रत्यक्ष कर
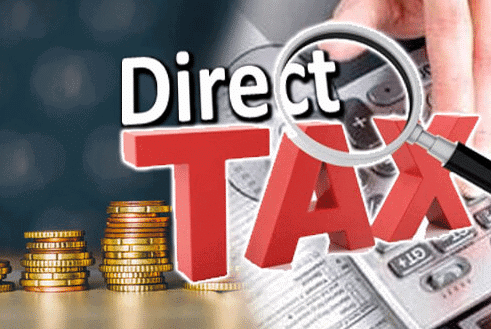
वस्तु एवं सेवा कर (GST): 2017 में पेश किया गया, GST ने अप्रत्यक्ष कराधान में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाते हुए VAT, उत्पाद शुल्क, और सेवा कर जैसे कई करों को समाप्त कर दिया है। 2025 में GST संरचना में शामिल हैं:
- दरें: चार-स्तरीय दर संरचना — 5%, 12%, 18%, और 28%।
- संकलन: GST राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है, 2024-25 में औसतन प्रति माह ₹1.6 लाख करोड़ से अधिक।
GST के लाभ:
- व्यवसायों के लिए कर अनुपालन को सरल बनाता है।
- करों का चक्रवृद्धि प्रभाव कम करता है।
- व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ाता है।
चुनौतियाँ:
- पेट्रोलियम उत्पादों, शराब, और बिजली को GST के तहत लाना विवादित बना हुआ है।
- एक समान दर प्राप्त करने के लिए कर स्लैब को तर्कसंगत बनाना जारी है।
सेवा कर और इसका संक्रमण: सेवा कर, जो GST से पहले का था, GST प्रणाली में समाहित हो गया है। हालाँकि, 2017 से पहले सेवा कर संग्रह से संबंधित कुछ विरासत विवाद अभी भी समर्पित न्यायाधिकरणों के माध्यम से सुलझाए जा रहे हैं।
प्रौद्योगिकी और कर प्रशासन: आयकर विभाग और GST नेटवर्क (GSTN) दक्षता बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों पर निर्भर करते हैं। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:
- ई-इनवॉइसिंग: उन व्यवसायों के लिए अनिवार्य, जिनकी वार्षिक टर्नओवर ₹5 करोड़ से अधिक है।
- स्वचालित रिफंड प्रणाली: निर्यातकों और MSMEs के लिए रिफंड प्रक्रिया को तेज करना।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: गैर-अनुपालन करने वाले करदाताओं की पहचान और धोखाधड़ी का पता लगाना।
वस्तु एवं सेवा कर परिषद और सुधार: GST परिषद देश भर में करों के सामंजस्यपूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाल के सुधारों में शामिल हैं:
- कर की दरों में कमी: कुछ वस्तुओं और सेवाओं को मांग को बढ़ावा देने के लिए निम्न कर श्रेणियों में स्थानांतरित किया गया।
- संरचना योजना का विस्तार: छोटे व्यवसाय जो 2 करोड़ रुपये तक की टर्नओवर रखते हैं, अब सरल जीएसटी अनुपालन से लाभान्वित होते हैं।
जीएसटी और संवैधानिक ढांचा
जीएसटी, अनुच्छेद 246A के अंतर्गत, केंद्र और राज्यों दोनों को जीएसटी लगाने और संग्रह करने का अधिकार देता है। पेट्रोलियम उत्पाद और शराब जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, जबकि इन्हें इस प्रणाली में लाने के प्रयास जारी हैं।
उभरती चुनौतियाँ और समाधान
- नए क्षेत्रों का एकीकरण: उभरते क्षेत्रों जैसे कि क्रिप्टोक्यूरेंसी को जीएसटी ढांचे में शामिल करने के लिए प्रयास चल रहे हैं।
- करदाता शिक्षा: अनुपालन आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- राज्य-केंद्र समन्वय: राजस्व-शेयरिंग चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करना।
- कर दरों को सरल बनाना: बेहतर दक्षता के लिए कर स्लैब को एकीकृत करने के लिए जारी प्रयास।
जीएसटी का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
- कर-से-जीडीपी अनुपात में वृद्धि: 2011-12 में 11.8% से बढ़कर 2024-25 में 13.7% हो गया।
- निर्यात को बढ़ावा: निर्यातकों को जीएसटी के तहत शून्य-रेटिंग से लाभ होता है, जिससे भारतीय वस्तुएं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनती हैं।
- आर्थिक वृद्धि: कम अनुपालन लागत और सरल प्रक्रियाओं ने निवेश को प्रोत्साहित किया है।
[आंतरिक प्रश्न] भविष्य की दृष्टि: भारत की कर पारिस्थितिकी प्रणाली प्रौद्योगिकी, नीति सरलीकरण, और बेहतर करदाता सेवाओं के एकीकरण के साथ अधिक उन्नतियों के लिए तैयार है। ध्यान एक ऐसा कराधान प्रणाली बनाने पर है जो निष्पक्ष, पारदर्शी, और विकास उन्मुख हो, जो तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करे।
|
389 docs|527 tests
|
















