कला और वास्तुकला के विकास में प्रमुख चरण | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download
प्राचीन भारतीय वास्तुकला: अतीत की एक झलक
भारत की वास्तुकला की यात्रा लगभग चार हजार वर्षों में फैली हुई है, जिसकी जड़ें प्राचीन काल में गहराई से जुड़ी हुई हैं। इस प्रारंभिक अवधि में भारतीय वास्तुकला की नींव रखी गई।
इंडस घाटी सभ्यता उन्नत वास्तु कौशल के पहले प्रमाण प्रदान करती है। खुदाई में अच्छी तरह से योजनाबद्ध नगरों और प्रभावशाली संरचनाओं के अवशेष मिले हैं। इस युग की उल्लेखनीय वास्तु उपलब्धियों में शामिल हैं:
- महान स्नानागार: मोहनजोदड़ो में एक महत्वपूर्ण संरचना, जिसका माप 11.88 x 7.01 x 2.43 मीटर है। इसमें जिप्सम में सेट जलाए गए ईंटों का फर्श था, जो सामग्री के नवोन्मेषी उपयोग को दर्शाता है।
- अन्न भंडार: हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य में किले के भीतर छह अन्न भंडारों की उपस्थिति से उन्नत भंडारण समाधानों का संकेत मिलता है।
- बहु-स्तंभ सभा हॉल: एक बड़ा सभा हॉल जिसमें कई स्तंभ थे, जो उस समय की वास्तुशिल्प कीSophistication को प्रदर्शित करता है।
- डॉकयार्ड: लोथल में खुदाई में एक डॉकयार्ड का अस्तित्व मिला, जो सभ्यता की समुद्री क्षमताओं को दर्शाता है।
निर्माण में जलाए गए ईंटों का व्यापक उपयोग इस अवधि में भारतीय वास्तुकला की एकRemarkable विशेषता थी, जिसने उपमहाद्वीप में भविष्य की वास्तुकला के विकास के लिए मंच तैयार किया।
प्राचीन भारत में वास्तुकला का विकास
प्रोटो-ऐतिहासिक से प्रारंभिक ऐतिहासिक चरण: वास्तुकला के प्रोटो-ऐतिहासिक चरण और प्रारंभिक ऐतिहासिक चरण के बीच एक महत्वपूर्ण अंतराल है।
वेदिक आर्य, जो इसके बाद आए, लकड़ी, बांस और रेड़ों से बने सरल घरों में रहते थे। उनकी सरल धार्मिक प्रथाओं के कारण ये बुनियादी संरचनाएँ उनके दैनिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त थीं, जिसने वास्तुकला के विकास में बहुत कम योगदान दिया।
दूसरी शहरीकरण और मौर्य काल: भारत में वास्तुकला ने छठी सदी ई.पू. में दूसरी शहरीकरण और आर्थिक गतिविधियों के विकास के दौरान और अधिक विकास देखा। समकालीन ग्रंथों जैसे जातक में उस समय के शहरों में सुंदर भवनों की उपस्थिति का उल्लेख है।
मौर्य काल में वास्तुकला की उपलब्धियाँ: मौर्य काल वास्तुकला की उपलब्धियों का एक उच्च बिंदु था, जो स्तूपों, गुफाओं और आवासीय भवनों में स्पष्ट था।
- स्तूप: ये ईंट या पत्थर की masonry से बने ठोस गुंबद थे, जिन्हें पवित्र स्थलों को श्रद्धांजलि देने या बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए बनाया गया था। सम्राट अशोक ने कई स्तूपों का निर्माण किया, जिसमें सांची का महान स्तूप सबसे प्रसिद्ध है, जिसे उनके द्वारा बनाया गया माना जाता है। ऐतिहासिक खंडों जैसे ह्युएन त्सांग की रचनाएँ इस समय बनाए गए स्तूपों की विशाल संख्या का उल्लेख करती हैं।
- गुफा निवास: अशोक और उनके पोते ने भिक्षुओं के लिए गुफा निवास भी बनाए। प्रमुख उदाहरणों में बाराबर पहाड़ियों की गुफाएँ शामिल हैं, जैसे सुदामा गुफा, जो अजिविका संप्रदाय के व्यापारियों के लिए समर्पित है, और कर्ण-चौपर गुफा, जो एक मेहराबदार छत के साथ आयताकार हॉल के लिए जानी जाती है। ये गुफाएँ कठोर गनीस से खोदी गई थीं और इनके आंतरिक दीवारों को दर्पण की तरह चमकदार बनाया गया था।
- आवासीय भवन: जबकि मौर्य आवासीय भवनों के कोई भौतिक उदाहरण नहीं बचे हैं, प्राचीन लेखकों जैसे मेगस्थनीज के खंडों में पाटलिपुत्र की राजधानी में महलों की भव्यता का वर्णन है। हाल की पुरातात्त्विक खुदाइयों में इन संरचनाओं के अवशेष मिले हैं, जिनमें से सबसे उल्लेखनीय सौ स्तंभों वाले हॉल के अवशेष हैं।
भारतीय वास्तुकला का विकास: मौर्य के बाद से गुप्त काल तक
भारतीय वास्तुकला का विकास मौर्य के बाद के काल से जारी है, जिसमें स्तूपों, गुफाओं और मंदिरों के निर्माण में महत्वपूर्ण विकास हुआ।
मौर्य के बाद की अवधि: वास्तु विकास
मौर्य के बाद की अवधि में, विशेष रूप से शुंगों के शासन के दौरान, स्तूपों के निर्माण में उल्लेखनीय वास्तु विकास हुआ।
- भारहुत स्तूप: भारहुत में एक बड़ा स्तूप बनाया गया, हालांकि आज केवल इसकी रेलिंग और एक द्वार के टुकड़े बचे हैं। बचे हुए रेलिंग, जो लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं, में सीधी स्तंभ, क्रॉसबार और कोपिंग पत्थर हैं।
- बोधगया: बोधगया में एक अन्य उदाहरण है, जहाँ स्तूप के चारों ओर की रेलिंग भी इस अवधि की है।
- सांची स्तूप: सांची में तीन बड़े स्तूप हैं, जो सभीRemarkably संरक्षित हैं। प्रमुख स्तूप, जिसे पहले सम्राट अशोक ने बनाया था, को मौर्य के बाद की अवधि में विस्तारित किया गया, जिसमें चार जटिल डिजाइन वाले द्वार जोड़े गए, प्रत्येक cardinal दिशा में।
- गुफा खुदाई: इस समय कई बड़े गुफाएँ खोदी गईं, जिनमें बेडसा, भाजा, कोंडाने, जुनार, नासिक, अजंता और एलोरा की गुफाएँ शामिल हैं। ये गुफाएँ चैत्य (प्रार्थना हॉल) या विहार (मठ) के रूप में कार्य करती थीं।
गुप्त काल: मंदिर वास्तुकला का उदय
गुप्त काल भारतीय वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण क्षण है, विशेष रूप से मंदिर निर्माण के क्षेत्र में। इस युग में दो प्रमुख मंदिर शैलियों का उदय हुआ: नागरा शैली और द्रविड़ शैली।
गुप्त मंदिरों की विशेषताएँ: गुप्त काल के मंदिर आमतौर पर सरल और विनम्र डिज़ाइन में होते हैं। इस अवधि से कई स्पष्ट प्रकार के मंदिरों की पहचान की जा सकती है, जो बाद में मध्यकालीन भारतीय मंदिर शैलियों में विकसित हुए।
गुप्त मंदिरों के प्रकार:
- चपटी छत वाला चौकोर मंदिर: एक चौकोर मंदिर जिसमें चपटी छत और सामने एक उथला स्तंभित बरामदा है।
- चपटी छत वाला चौकोर मंदिर जिसमें ढका हुआ परिक्रमा: एक चौकोर मंदिर जिसमें गर्भगृह के चारों ओर ढका हुआ परिक्रमा है, सामने एक स्तंभित बरामदा और कभी-कभी ऊपर एक दूसरा मंजिल होता है।
- निम्न शिखर वाला चौकोर मंदिर: एक चौकोर मंदिर जिसके ऊपर एक निम्न और स्थूल शिखर है।
- आयताकार मंदिर: एक आयताकार मंदिर जिसमें एक गोलाकार पीछे और एक बैरल-वॉल्टेड छत है।
- गोलाकार मंदिर: एक गोलाकार मंदिर जिसमें इसके चार cardinal चेहरों पर उथले आयताकार प्रक्षिप्तियाँ हैं।
बाद की शैलियों पर प्रभाव: पहले तीन प्रकार के मंदिर मध्यकालीन भारतीय मंदिर शैलियों के पूर्ववर्ती माने जाते हैं। विशेष रूप से, दूसरा प्रकार नागरा शैली का पूर्ववर्ती माना जाता है, जबकि तीसरा प्रकार द्रविड़ शैली की नींव रखता है।
संक्षेप में, मौर्य के बाद से गुप्त काल तक भारतीय वास्तुकला का विकास स्तूपों और गुफाओं से मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की ओर एक संक्रमण को दर्शाता है, जिसने बाद में आने वाली समृद्ध वास्तुकला की धरोहर के लिए आधार तैयार किया।
नागरा, द्रविड़, और वेसारा शैलियों का उदय
गुप्त के बाद की अवधि में प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण चरण रहा, जिसमें तीन मुख्य शैलियों का उदय हुआ: नागरा उत्तर भारत में, द्रविड़ दक्षिण भारत में, और वेसारा डेक्कन क्षेत्र में।
नागरा शैली: नागरा शैली की पहचान चौकोर आधार और प्रत्येक चेहरे पर कई ग्रैजुएटेड प्रक्षिप्तियों (रथक) के साथ होती है, जो बाहरी रूप को क्रॉस-फॉर्म आकार देती है।
इसकी ऊँचाई में, इसमें एक टॉवर (शिखर) होता है जो धीरे-धीरे भीतर की ओर झुकता है और इसे एक गोलाकार स्लैब से ढका जाता है जिसके किनारे रिब्ड होते हैं (अमलका)।
नागरा शैली के उल्लेखनीय उदाहरणों में शामिल हैं:
- दसावतारा मंदिर: देवगढ़ में
- ईंट का मंदिर: भितरगांव में
द्रविड़ शैली: द्रविड़ शैली की पहचान एक गर्भगृह के चारों ओर की परिक्रमा से होती है जिसमें पीछे की ओर घटते हुए मंजिल होते हैं।
द्रविड़ शैली के उल्लेखनीय उदाहरणों में शामिल हैं:
- पार्वती मंदिर: नच्नकुंथर में
- शिव मंदिर: भुमारा और ऐहोल में
- पल्लव मंदिर: जैसे कैलाशनाथ मंदिर कांची में और वैकुंट-परमल मंदिर
वेसारा शैली: वेसारा शैली नागरा और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है।
उल्लेखनीय उदाहरणों में शामिल हैं ऐहोल और वातापी के मंदिर, जैसे:
- लध्कान मंदिर
- हुचिंतालिगुड़ी मंदिर
- पापनाथ मंदिर
गुप्त के बाद की अवधि: गुप्त के बाद की वास्तुकला में महाबलीपुरम में पाए जाने वाले सात रथ मंदिर और पल्लवों के गुफा-शैली के मंदिर भी शामिल हैं। इस अवधि ने भारतीय संस्कृति और परंपरा की वास्तुकला में एक मजबूत आधार तैयार किया, जो आगे चलकर विकसित होती रही और अगले युगों में समृद्ध अंतःक्रियाएँ प्राप्त करती रही।
I'm sorry, but it seems there was a misunderstanding. Please provide the chapter notes you would like to have translated into Hindi, and I will assist you with that.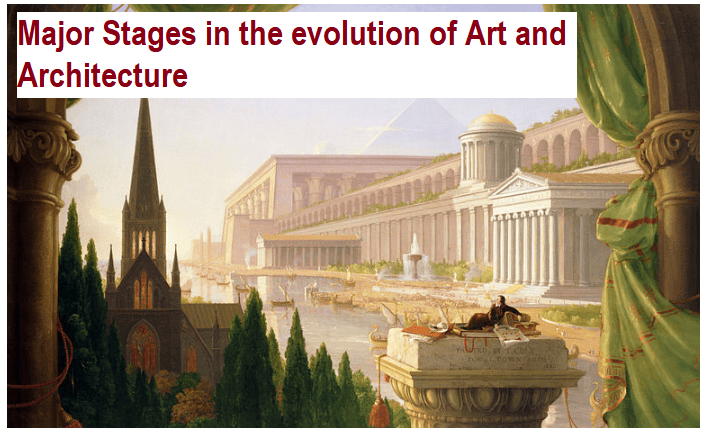
|
28 videos|739 docs|84 tests
|















