दो विश्व युद्धों के बीच अंतरराष्ट्रीय संबंध | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download
परिचय
दो विश्व युद्धों के बीच अंतरराष्ट्रीय संबंधों को दो स्पष्ट चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जो जनवरी 1933 के महत्वपूर्ण क्षण से चिह्नित हैं, जब एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में सत्ता ग्रहण की।
इससे पहले, विश्व शांति बनाए रखने की एक उचित आशा थी, हालांकि राष्ट्रों के संघ ने मांचूरिया में जापानी आक्रामकता को संबोधित करने में असफलता दिखाई। हालांकि, एक बार जब हिटलर ने अपने नियंत्रण को मजबूत किया, तो किसी भी प्रकार के युद्ध को रोकने की संभावना, चाहे वह सीमित हो या पूर्ण पैमाने पर, काफी हद तक कम हो गई।
पहले चरण को तीन अवधि में विभाजित किया जा सकता है:
- 1919-23: पहले विश्व युद्ध के बाद, अंतरराष्ट्रीय संबंध शांति समझौते से उत्पन्न मुद्दों से अस्थिर हो गए, जबकि नए स्थापित राष्ट्रों के संघ ने इन चुनौतियों को संभालने में संघर्ष किया।
- तुर्की और इटली ने अपने उपचार को लेकर असंतोष व्यक्त किया:
- तुर्की समझौते को नकारने के लिए तैयार था।
- इटली, जो 1922 में मुसोलिनी के शासन में आ गया, ने अपनी नाराजगी को प्रदर्शित किया:
- फियमे को जब्त किया, जिसे यूगोस्लाविया को दिया गया था।
- कॉर्फू घटना में संलग्न हुआ।
- बाद में, इटली की आक्रामकता 1935 में एबिसिनिया की ओर निर्देशित होगी।
जर्मन पुनर्प्राप्तियों का मुद्दा और जर्मनी की भुगतान क्षमता का सवाल ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संबंधों को तनाव में डालता है, क्योंकि उनके जर्मन पुनर्प्राप्ति के प्रति अलग दृष्टिकोण थे:- फ्रांस को कमजोर जर्मनी चाहिए।
- ब्रिटेन को एक मजबूत जर्मनी चाहिए जो ब्रिटिश निर्यात खरीद सके।
- लॉयड जॉर्ज का फ्रांस और जर्मनी के बीच सुलह करने का प्रयास 1922 के जिनोआ सम्मेलन में असफल रहा।
1923 में, फ्रांसीसी सैनिकों ने रुहर में कब्जा कर लिया, जो एक महत्वपूर्ण जर्मन औद्योगिक क्षेत्र है, जर्मनी से नकद भुगतान की मांग के बदले सामान जब्त करने के प्रयास में। यह कार्रवाई जर्मन मुद्रा के पतन में योगदान करती है।
इस बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका, जबकि राजनीतिक रूप से अलगाव में था, ने यूरोप पर महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव डाला, यूरोपीय युद्ध ऋणों के पूर्ण भुगतान पर जोर देते हुए।
रूस, अब बोल्शेविक (कम्युनिस्ट) शासन के अधीन, पश्चिमी देशों द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा गया, जिनमें से कई, जापान के साथ मिलकर, 1918 से 1920 तक रूस में गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों के खिलाफ हस्तक्षेप किया।
युद्ध और शांति समझौते से उभरने वाले नए राज्यों, जिनमें यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और पोलैंड शामिल थे, गंभीर आंतरिक समस्याओं और विभाजन का सामना करना पड़ा, जिनका अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।
- 1924 से 1929: इस अवधि में, अंतरराष्ट्रीय वातावरण में महत्वपूर्ण सुधार हुआ, आंशिक रूप से राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव के कारण।
- फ्रांस में, एडौर्ड हेरियट और आरीस्टाइड ब्रियंड ने सत्ता ग्रहण की, जबकि जर्मनी में, गुस्ताव स्ट्रेसेमैन और ब्रिटेन में, रामसे मैकडोनाल्ड ने भी नेतृत्व संभाला, सभी ने संबंधों को बढ़ाने के लिए तत्पर थे।
- इस समय के दौरान कुछ प्रमुख विकास शामिल थे:
- डॉज प्लान (1924): अमेरिकी सहायता से तैयार किया गया, इस योजना ने जर्मन पुनर्प्राप्तियों के चारों ओर तनाव को कम किया।
- लोकार्नो संधियाँ (1925): इन संधियों ने वर्साय में स्थापित पश्चिमी यूरोप की सीमाओं की गारंटी दी, जिससे फ्रांस की जर्मन इरादों के संबंध में चिंताओं को प्रभावी रूप से कम किया गया।
- राष्ट्रों के संघ की सदस्यता (1926): जर्मनी को राष्ट्रों के संघ में शामिल किया गया, जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय में पुनः एकीकरण का एक महत्वपूर्ण कदम था।
- केलॉग-ब्रियन संधि (1928): कुल 65 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, युद्ध को विवादों को सुलझाने के एक साधन के रूप में त्यागते हुए, और शांति के प्रति प्रतिबद्धता को और अधिक बल दिया।
- यंग प्लान (1929): इस योजना ने जर्मन पुनर्प्राप्तियों को अधिक प्रबंधनीय स्तर तक कम किया, जिससे एक अधिक स्थिर अंतरराष्ट्रीय वातावरण में योगदान मिला।
1930 से 1933: जब 1929 का अंत आया, दुनिया आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने लगी, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के पतन में एक भूमिका निभाई। आर्थिक कारक आंशिक रूप से जापान के 1931 में मांचूरिया पर आक्रमण के लिए जिम्मेदार थे, जबकि जर्मनी में व्यापक बेरोजगारी ने एडोल्फ हिटलर के सत्ता में आने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में, विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन 1932 में convened हुआ, केवल 1933 में जर्मन प्रतिनिधियों के बाहर जाने के बाद असफलता में समाप्त हुआ, जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक निम्न बिंदु था।
अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सुधार के प्रयास
राष्ट्रों का संघ: राष्ट्रों का संघ विभिन्न अंतरराष्ट्रीय विवादों और समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। हालांकि, इसकी प्राधिकरण कमजोर हुई क्योंकि कई देशों ने संघ से स्वतंत्र रूप से समझौतों पर हस्ताक्षर करना पसंद किया, जो इसकी प्रभावशीलता पर विश्वास की कमी को दर्शाता है।
देश आक्रामकताओं को रोकने के लिए सैन्य समर्थन प्रदान करने के लिए भी अनिच्छुक थे, जिससे संघ की प्राधिकरण और कमजोर हो गई।
- वाशिंगटन सम्मेलन (1921-22): वाशिंगटन सम्मेलन (1921–22) का उद्देश्य नौसैनिक हथियारों की दौड़ को सीमित करना और प्रशांत में शक्तियों के बीच विरोधी हितों को संबोधित करना था। इसमें नौ राष्ट्र शामिल थे: संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और पुर्तगाल।
- वाशिंगटन सम्मेलन का एक लक्ष्य अमेरिका और जापान के बीच संबंधों में सुधार करना था। अमेरिका जापान की बढ़ती शक्ति और चीन में उसके प्रभाव के प्रति संदेह कर रहा था, विशेष रूप से जब जापान ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कियाओचौ और प्रशांत में जर्मन द्वीपों पर कब्जा कर लिया था।
एक नौसैनिक निर्माण दौड़ को रोकने के लिए, यह सहमति हुई थी कि जापानी नौसेना अमेरिकी और ब्रिटिश नौसेनाओं के आकार के तीन-पांचवें तक सीमित होगी। इसके बदले में, जापान ने कियाओचौ और शानटुंग प्रांत से हटने पर सहमति दी, जिसे उसने 1914 से कब्जा कर रखा था। - चीन के संदर्भ में, एक नौ-शक्ति संधि स्थापित की गई, जहां हस्ताक्षरकर्ताओं ने \"ओपन डोर\" सिद्धांत को स्वीकार करने और चीन की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, और प्रशासनिक स्वतंत्रता का सम्मान करने पर सहमति व्यक्त की।
- एंग्लो-जापानी संधि ने अमेरिका और कनाडा के लिए चिंता पैदा की, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया कि ब्रिटिश निष्क्रिय समर्थन ने जापानी प्रभाव को दूर पूर्व में बढ़ाया। यह संधि, जो 1921 में समाप्त होने वाली थी, को नवीनीकरण नहीं मिला। इसके बजाय, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, और अमेरिका द्वारा चार-शक्ति संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें प्रशांत द्वीपों में एक-दूसरे के अधिकारों का सम्मान करने और विवाद समाधान के लिए संयुक्त सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति दी गई।
- वाशिंगटन सम्मेलन ने अस्थायी रूप से दूर पूर्व के प्रश्न पर शक्तियों के बीच मतभेदों को हल किया, और समझौतों को उस समय एक महत्वपूर्ण सफलता माना गया। अमेरिका ने अपनी \"ओपन डोर\" नीति की मान्यता प्राप्त की और एंग्लो-जापानी संधि की समाप्ति हुई।
चीन, कागज पर, आगे के शोषण से सुरक्षित था और शानटुंग की बहाली प्राप्त की, जो जापान के लिए उसकी चीनी नीति में एक राजनीतिक असफलता थी। हालांकि, जापान की शक्ति को रोकने के प्रयासों के बावजूद, सम्मेलन ने अनजाने में जापान की शक्ति को दूर पूर्व में बढ़ा दिया।
स्थापित नौसैनिक शक्ति अनुपात और प्रशांत द्वीपों को सुदृढ़ न करने की सहमति ने दूर पूर्व में जापान की नौसैनिक श्रेष्ठता सुनिश्चित की। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नौसेना के साथ उभरा, जो प्रशांत में केंद्रित थी, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका, बड़े नौसेनाओं के बावजूद, अपनी सेनाओं को अधिक व्यापक रूप से फैलाने में लगे थे। यह स्थिति को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण बना देता था यदि जापान आक्रामक कार्रवाई करने की कोशिश करता, जिसके परिणामस्वरूप 1930 के दशक में चीन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम आए, जब अमेरिका जापानी आक्रामकता के खिलाफ हस्तक्षेप करने से कतराता था।
- जिनोआ सम्मेलन (1922): जिनोआ सम्मेलन का प्रस्ताव ब्रिटिश प्रधान मंत्री लॉयड जॉर्ज ने फ्रांसीसी-जर्मन शत्रुता, यूरोपीय युद्ध ऋणों को अमेरिका, और सोवियत रूस के साथ कूटनीतिक संबंधों को फिर से शुरू करने की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए किया था।
- हालांकि, सम्मेलन फ्रांसीसी के पूर्ण पुनर्प्राप्तियों पर जोर देने, अमेरिकी गैर-उपस्थिति, और रूसियों और जर्मनों के किसी अन्य स्थान पर आपसी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बाहर जाने के कारण विफल रहा।
बाद में, जब जर्मनों ने पुनर्प्राप्तियों का भुगतान करने से इनकार किया, तो फ्रांसीसी सैनिकों ने रुहर पर कब्जा कर लिया, जिससे जर्मनों ने निष्क्रिय प्रतिरोध के साथ प्रतिक्रिया दी। - डॉज प्लान (1924): डॉज योजना जिनोआ सम्मेलन के बाद के गतिरोध का एक उत्तर था। इसका उद्देश्य पुनर्प्राप्तियों के मुद्दे को संबोधित करना था, जिससे जर्मनी केवल वही भुगतान कर सके जो वह वहन कर सके।
जर्मनी को मुख्य रूप से अमेरिका से 800 मिलियन स्वर्ण मार्क का एक विदेशी ऋण प्रदान किया गया था। योजना जर्मन अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और अंतरराष्ट्रीय तनाव को कम करने में सफल रही। - लोकार्नो संधियाँ (1925): लोकार्नो संधियाँ जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन, इटली, पोलैंड, और चेकोस्लोवाकिया के बीच शांति की गारंटी देने के लिए समझौते थे।
सबसे महत्वपूर्ण समझौता जर्मनी, फ्रांस, और बेल्जियम के बीच सीमाओं का आपसी सम्मान था, जिसमें ब्रिटेन और इटली उल्लंघन की स्थिति में सहायता प्रदान करने की पेशकश की।
जर्मनी ने पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के साथ मध्यस्थता पर सहमति व्यक्त की, लेकिन इन देशों के साथ सीमाओं की गारंटी नहीं दी। - ये संधियां प्रारंभ में स्वागत की गईं और जर्मन विदेश मंत्री स्ट्रेसेमैन के लिए एक सफलता मानी गईं।
लोकार्नो संधि की आलोचना: लोकार्नो संधि को वर्साय संधि और संघ के संधि को कमजोर करने के रूप में देखा गया। यह जर्मनी की पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं के बीच भेद करती थी, जर्मनी ने अपनी पश्चिमी सीमाओं को स्वीकार किया लेकिन अपनी पूर्वी सीमाओं के पुनरीक्षण की मांग की।
ब्रिटेन के बेल्जियम और फ्रांस की रक्षा करने के वादे ने पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के प्रति इसके समर्पण के बारे में चिंताएं उठाईं।
स्ट्रेसेमैन और ब्रियंड: स्ट्रेसेमैन और फ्रांसीसी विदेश मंत्री ब्रियंड, साथ ही ब्रिटिश विदेश मंत्री चेम्बरलेन, को उनके कूटनीतिक प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
सितंबर 1926 में, उन्होंने राइनलैंड से फ्रांसीसी सैनिकों की वापसी पर सहमति व्यक्त की, जो \"लोकार्नो आत्मा\" को दर्शाता है।
केलॉग-ब्रियन संधि (1928): केलॉग-ब्रियन संधि, जिसे प्रारंभिक रूप से ब्रियंड द्वारा अमेरिका और फ्रांस के बीच युद्ध से इनकार करने के लिए प्रस्तावित किया गया था, इसे पूरे विश्व में विस्तार दिया गया।
अंततः, 65 राज्यों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, जो युद्ध को राष्ट्रीय नीति उपकरण के रूप में त्यागने पर सहमति व्यक्त करते हैं।
हालांकि इसकी प्रभावशाली उपस्थिति थी, लेकिन संधि ने उल्लंघनों के खिलाफ प्रवर्तन उपायों की कमी थी। जापान के हस्ताक्षर ने इसके बाद के चीन के खिलाफ युद्ध को रोकने में मदद नहीं की।
- यंग प्लान (1929): यंग योजना ने डॉज योजना द्वारा अनसुलझे पुनर्प्राप्तियों के मुद्दों को हल करने का लक्ष्य रखा।
सुधरे हुए हालात के तहत, पुनर्प्राप्तियों को £6600 मिलियन से £2000 मिलियन तक कम किया गया, जो 59 वर्षों में ग्रेडेड स्केल पर भुगतान किया जाना था।
यह कमी मित्र राष्ट्रों द्वारा एक गलती के रूप में स्वीकृति थी और कीन्स के पहले के सुझावों के साथ मेल खाती थी।
जबकि इसे जर्मनी में कई लोगों द्वारा स्वागत किया गया, नाजी पार्टी ने योजना का विरोध किया, जिसमें शांति समझौते के अधिक तेज और अधिक कट्टर संशोधन की मांग की। - लोकार्नो आत्मा का पतन: स्ट्रेसेमैन की अक्टूबर 1929 में मृत्यु, जो यूरोप में शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, लोकार्नो आत्मा के लिए एक झटका था।
उसी महीने में वॉल स्ट्रीट क्रैश ने ग्रेट डिप्रेशन को जन्म दिया, जिससे जर्मनी में व्यापक बेरोजगारी उत्पन्न हुई और लोकार्नो की नाजुक सद्भावना का अंत हुआ।
विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन (1932-33)
जब राष्ट्रों के संघ के सदस्य राज्यों ने संधि को स्वीकार किया, तो उन्होंने सभी ने हथियारों को कम करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि, केवल जर्मनी ने निरस्त्रीकरण की दिशा में कोई वास्तविक प्रयास किया।
वास्तव में, इस अवधि में अधिकांश अन्य देशों ने अपने सैन्य खर्च को बढ़ाया। 1925 से 1933 के बीच, वैश्विक हथियारों पर व्यय $3.5 बिलियन से लगभग $5 बिलियन तक बढ़ गया।
विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन जिनेवा में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य हथियारों को कम करने का एक तरीका खोजना था। हालांकि, यदि लोकार्नो हनीमून के दौरान प्रगति संभव नहीं थी, तो 1930 के दशक के अशांत वातावरण में यह असंभव प्रतीत हुआ।
- ब्रिटिशों ने तर्क किया कि उन्हें अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अधिक हथियारों की आवश्यकता थी।
- फ्रांसीसी, जो जर्मनी में नाजी समर्थन की तेज वृद्धि के बारे में चिंतित थे, ने निरस्त्रीकरण से इनकार कर दिया या जर्मनी को उनके साथ समान हथियार रखने की अनुमति नहीं दी।
- अक्टूबर 1933 में, हिटलर ने, ब्रिटेन और इटली की जर्मनी के प्रति सहानुभूति के प्रति जागरूक होकर, सम्मेलन से बाहर निकलने का निर्णय लिया, जो इसकी विफलता की शुरुआत के रूप में चिह्नित हुआ।
एक सप्ताह बाद, जर्मनी ने राष्ट्रों के संघ से भी बाहर निकल गया।
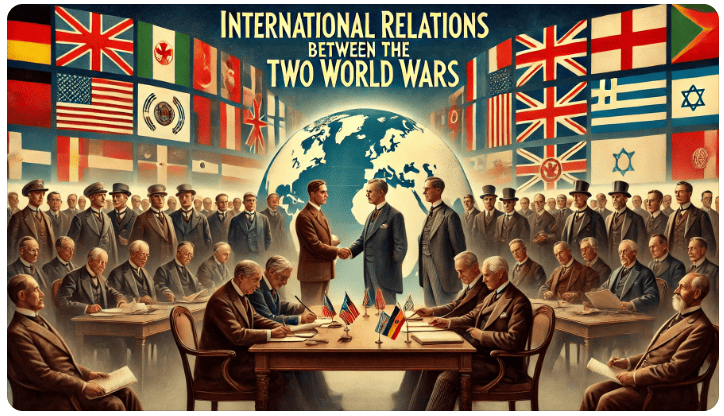
|
28 videos|739 docs|84 tests
|















