दो शक्ति समूहों का उदय (द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया) | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download
परिचय
शीत युद्ध एक ऐसा समय था जब अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों के नेतृत्व में पश्चिमी ब्लॉक और सोवियत संघ और उसके वारसॉ पैक्ट सहयोगियों के नेतृत्व में पूर्वी ब्लॉक के बीच गहन राजनीतिक और सैन्य तनाव था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का था। जबकि इतिहासकार सटीक तिथियों पर बहस करते हैं, शीत युद्ध को सामान्यतः 1947 से 1991 तक माना जाता है। "शीत" शब्द का अर्थ है कि दोनों पक्षों के बीच सीधे बड़े पैमाने पर संघर्ष का अभाव था, हालाँकि कोरिया, वियतनाम, और अफगानिस्तान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संघर्षों में दोनों पक्षों ने विरोधी गुटों को समर्थन दिया।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों से लड़ने के लिए बनाए गए अस्थायी गठबंधन से उभरते हुए, शीत युद्ध ने USSR और USA को सुपरपावर बना दिया, जिनके बीच आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण में स्पष्ट अंतर था। सोवियत संघ एक एक-पार्टी मार्क्सवादी-लेनिनवादी राज्य था, जबकि अमेरिका एक पूंजीवादी लोकतंत्र था जिसमें आम तौर पर स्वतंत्र चुनाव होते थे। सीधे पूर्ण युद्ध में शामिल हुए बिना, दोनों सुपरपावरों ने संभावित परमाणु विश्व युद्ध के लिए खुद को भारी रूप से सशस्त्र किया। इससे आपसी नाश के सिद्धांत (MAD) का विकास हुआ, जहाँ प्रत्येक पक्ष का परमाणु निरोधक दूसरे को हमले के लिए मजबूर नहीं करता था, क्योंकि उन्हें पता था कि इससे कुल विनाश होगा।
शीत युद्ध को परमाणु भंडारों के विकास, पारंपरिक सैन्य बलों की तैनाती, और प्रॉक्सी युद्धों, मनोवैज्ञानिक युद्ध, प्रचार, जासूसी, और स्पेस रेस जैसी तकनीकी प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रभुत्व की लड़ाई के रूप में चिह्नित किया गया।
शब्द के उत्पत्ति: "शीत युद्ध" शब्द का उपयोग पहले बार सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच के युद्धोत्तर भू-राजनीतिक संघर्ष का वर्णन करने के लिए बर्नार्ड बारुच के भाषण में किया गया था, जो डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति के प्रभावशाली सलाहकार थे। समाचार पत्र के स्तंभकार वाल्टर लिपमैन ने अपने पुस्तक "The Cold War" में इस शब्द को लोकप्रिय किया। जब 1947 में इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में पूछा गया, तो लिपमैन ने इसे 1930 के दशक के एक फ़्रांसीसी शब्द से जोड़ा।
एक आत्म-घोषित तटस्थ ब्लॉक गैर-आलंबन आंदोलन के साथ उभरा, जिसे मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, और यूगोस्लाविया जैसे देशों ने स्थापित किया। इस आंदोलन ने अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम या सोवियत के नेतृत्व वाले पूर्व के साथ संरेखण को अस्वीकार किया।
शीत युद्ध का कारण बनने वाले घटनाएँ
रूसी क्रांति:
1917 में, रूस में बोल्शेविकों के अधिग्रहण ने देश को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलगाव में डाल दिया। उस समय के नेता व्लादिमीर लेनिन का मानना था कि सोवियत संघ शत्रुतापूर्ण पूंजीवादी देशों से घिरा हुआ था। उन्होंने सोवियत दुश्मनों को विभाजित रखने के लिए कूटनीति को एक उपकरण के रूप में देखा, जिससे विदेशी क्रांतिकारी आंदोलनों को बढ़ावा देने के लिए सोवियत कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का निर्माण हुआ।
लेनिन के उत्तराधिकारी, जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ को पूंजीवादी दुनिया के भीतर "साम्यवादी द्वीप" के रूप में देखा। उन्होंने विश्वास किया कि पूंजीवादी घेराबंदी को सामाजिक घेराबंदी से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता थी। 1925 तक, स्टालिन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पूंजीवादी और साम्यवादी देशों के बीच संघर्ष के रूप में देखा, पूंजीवाद के अंत की भविष्यवाणी की।
संदेह द्वितीय विश्व युद्ध से पहले:
द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, घटनाओं ने पश्चिमी शक्तियों और सोवियत संघ के बीच आपसी अविश्वास को बढ़ा दिया।
• पश्चिम ने रूसी गृह युद्ध के दौरान एंटी-बोल्शेविक बलों का समर्थन किया।
• 1926 में, ब्रिटेन में श्रमिकों की हड़ताल के लिए सोवियत वित्त पोषण के कारण कूटनीतिक संबंध टूट गए।
• अन्य कारकों में स्टालिन की 1927 की शांति सह-अस्तित्व की घोषणा का मिटना, 1928 के शख्ति परीक्षण के दौरान ब्रिटिश-फ्रांसीसी कूप के आरोप, 1933 तक सोवियत संघ को मान्यता देने से अमेरिकी इनकार, और स्टालिन के शुद्धिकरण के दौरान जासूसी के आरोप शामिल थे।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संदेह:
सोवियत संघ ने शुरू में जर्मनी के साथ एक गैर-आक्रमण संधि पर हस्ताक्षर किया लेकिन बाद में 1941 में जर्मनी द्वारा आक्रमण के बाद ब्रिटेन और अमेरिका के साथ गठबंधन किया। स्टालिन पश्चिमी सहयोगियों पर संदेह करता रहा, विश्वास करते हुए कि वे जर्मनी के खिलाफ दूसरे मोर्चे को विलंबित करके सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए साजिश कर रहे थे।
सिद्धांतों में भिन्नता:
मुख्य संघर्ष साम्यवादी और पूंजीवादी राज्यों के बीच मौलिक भिन्नताओं से उत्पन्न हुआ।
• साम्यवाद, जो मार्क्स के विचारों पर आधारित है, सामूहिक स्वामित्व और केंद्रीय योजना का समर्थन करता है ताकि श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा की जा सके।
• इसके विपरीत, पूंजीवाद निजी स्वामित्व, लाभ-प्रेरित उद्यम, और निजी धन की शक्ति पर निर्भर करता है।
• रूस में 1917 में पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना के बाद, पूंजीवादी राज्यों ने साम्यवाद को संदेह और उसके प्रसार के डर के साथ देखा।
स्टालिन की विदेश नीति:
स्टालिन ने जितना संभव हो सके जर्मन क्षेत्र पर कब्जा करने और पड़ोसी देशों जैसे फिनलैंड, पोलैंड, और रोमानिया से भूमि को जोड़ने के लिए सोवियत प्रभाव का विस्तार करने का प्रयास किया। इस विस्तारवादी दृष्टिकोण ने पश्चिम को चिंतित कर दिया, जिसने स्टालिन के कार्यों को आक्रामक और वैश्विक स्तर पर साम्यवाद फैलाने की इच्छा के रूप में देखा।
शीत युद्ध का आरोप:
1950 के दशक में, कई पश्चिमी इतिहासकारों ने शीत युद्ध के लिए स्टालिन को दोषी ठहराया।
• जॉर्ज केन्नन ने USSR के निरोध की वकालत की, जिसके परिणामस्वरूप NATO का गठन और कोरियाई युद्ध में अमेरिका की भागीदारी हुई।
• कुछ सोवियत इतिहासकारों और 1960 और 1970 के दशक में अमेरिकी इतिहासकारों ने तर्क किया कि शीत युद्ध केवल स्टालिन की गलती नहीं थी।
• उन्होंने विश्वास किया कि रूस के युद्धकालीन नुकसान ने स्टालिन के प्रयासों को उचित ठहराया।
• पुनरीक्षणवादी इतिहासकारों ने तर्क किया कि अमेरिका की कार्रवाई, विशेष रूप से उसका परमाणु एकाधिकार और औद्योगिक शक्ति, ने रूसी शत्रुता को बढ़ावा दिया और शीत युद्ध में योगदान दिया।
द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की स्थितियाँ (1945–47)
द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद, सहयोगियों के बीच यूरोप को पुनर्गठित करने के बारे में महत्वपूर्ण असहमतियां थीं। प्रत्येक पक्ष के पास युद्ध के बाद की दुनिया में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विचार थे।
पश्चिमी सहयोगियों की दृष्टि:
पश्चिमी सहयोगियों ने एक ऐसा प्रणाली चाहता था जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें व्यापक रूप से स्थापित हों।
• उन्होंने मानवीय संगठनों के माध्यम से संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की विश्वास किया।
सोवियत संघ का दृष्टिकोण:
विपरीत रूप से, सोवियत संघ, जिसने युद्ध के दौरान immense नुकसान (लगभग 27 मिलियन लोग) और विनाश का सामना किया, सुरक्षा बढ़ाने के लिए पड़ोसी देशों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया।
• युद्ध के दौरान, स्टालिन ने विभिन्न देशों के कम्युनिस्टों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए थे ताकि लाल सेना के कब्जे के बाद मॉस्को के प्रति वफादार गुप्त पुलिस बल स्थापित किए जा सकें।
• स्टालिन का उद्देश्य ब्रिटेन और अमेरिका के साथ शांति बनाए रखना था ताकि आंतरिक पुनर्निर्माण और आर्थिक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।
याल्टा सम्मेलन (4-11 फरवरी 1945):
याल्टा सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तीन प्रमुख सहयोगी शक्तियों—यू.एस. राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, और सोवियत प्रीमियर जोसेफ स्टालिन—के बीच महत्वपूर्ण बैठक थी।
• सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी, जिनमें शामिल हैं:
- संयुक्त राष्ट्र का गठन: एक नई संस्था, संयुक्त राष्ट्र, स्थापित की जानी थी।
- जर्मनी का विभाजन: जर्मनी को ज़ोन में विभाजित किया जाना था।
- जर्मन सैन्य उद्योग: जर्मन सैन्य उद्योग को समाप्त किया जाना था।
- पुनर्प्राप्ति: पुनर्प्राप्तियों का निर्धारण एक आयोग को सौंपा गया।
- स्वतंत्र चुनाव: पूर्वी यूरोपीय राज्यों में स्वतंत्र चुनाव कराए जाने थे। जापान में सोवियत भागीदारी: स्टालिन ने जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने पर सहमति दी।
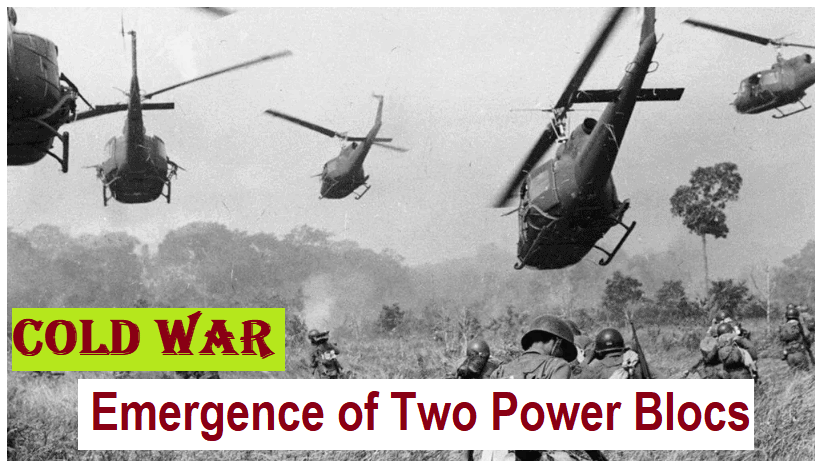
|
28 videos|739 docs|84 tests
|















