प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में व्यापार और वाणिज्य | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download
परिचय
व्यापार और वाणिज्य पर मुख्य बिंदु (700-1300 ई.पू.):
- व्यापार और वाणिज्य इस अवधि के दौरान फ्यूडलाइजेशन द्वारा चिह्नित थे, जो एक फ्यूडल प्रणाली की ओर बढ़ने का संकेत देता है।
- व्यापार को दो चरणों के माध्यम से समझा जा सकता है:
- चरण 1 (700-900 ई.पू.): व्यापार में गिरावट, धातु मुद्रा का सीमित उपयोग, शहरी केंद्रों का कमजोर होना, और एक अधिक अलग-थलग गांव की अर्थव्यवस्था का विशेषता।
- चरण 2 (900-1300 ई.पू.): व्यापार आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर पुनर्जीवित हुआ, जिसमें धातु के सिक्कों का उपयोग बढ़ा, हालांकि मौद्रिक अर्थव्यवस्था अभी भी मौर्य साम्राज्य के बाद की अवधि की तरह प्रमुख नहीं थी।
- फ्यूडलाइजेशन के संकेत शामिल थे:
- पैसे के लेनदेन और उनकी प्रकृति।
- राज्य अधिकारियों और शासक chiefs द्वारा भूमि के हितों में हेरफेर।
- शासक अभिजात वर्ग का बड़े व्यापारियों और वाणिज्यिकों के हितों की सेवा करना।
- कलाकारों और कारीगरों पर प्रतिबंध।
प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में व्यापार और वाणिज्य (700-1300 ई.पू.):
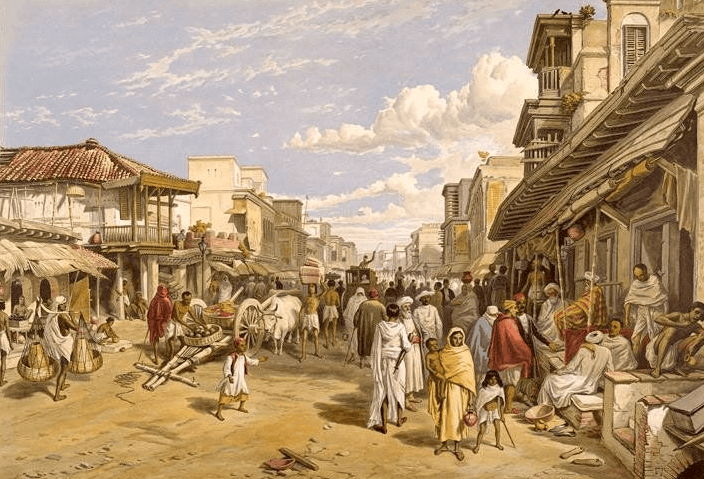
फ्यूडलाइजेशन: यह अवधि फ्यूडलाइजेशन की प्रक्रिया से चिह्नित थी, जो सामाजिक-आर्थिक संरचना में बदलाव को दर्शाती है।
व्यापार के चरण:
- 700-900 ई.पू.: इस चरण में व्यापार में अपेक्षाकृत गिरावट आई, जिसमें धातु मुद्रा का उपयोग, शहरी केंद्रों की कमजोरी, और एक प्रकार की बंद गांव की अर्थव्यवस्था का विशेषता थी।
- 900-1300 ई.पू.: व्यापार ने देश के भीतर और बाहर गति पकड़ी, जिसमें धातु के सिक्कों की संख्या में वृद्धि हुई। हालांकि, मौद्रिक अर्थव्यवस्था मौर्य काल के बाद के पांच शताब्दियों की तरह गहराई से नहीं फैली थी।
फ्यूडलाइजेशन के संकेत:
- पैसों के लेन-देन की प्रकृति।
- राज्य के अधिकारियों और शासक chiefs द्वारा भूमि के हितों में हेरफेर।
- बड़े व्यापारी और व्यवसायियों के हितों के लिए शासक वर्ग के कार्य।
- कारीगरों और शिल्पकारों पर लगाए गए प्रतिबंध।
कुल मिलाकर, इस अवधि के दौरान व्यापार और वाणिज्य फ्यूडल संरचनाओं, मौद्रिक प्रथाओं में बदलाव और ग्रामीण तथा शहरी अर्थव्यवस्थाओं के विभिन्न गतिशीलताओं द्वारा आकारित हुए।
पहला चरण (लगभग 700-900 ईस्वी)
भूमि अनुदान का विस्तार (750-1000 ईस्वी):
- इस अवधि के दौरान, भूमि को न केवल पुरोहितों और मंदिरों को बल्कि योद्धा chiefs और राज्य अधिकारियों को भी व्यापक रूप से दिया गया।
- भूमि मालिकों की एक पदानुक्रम उभरी, जिसमें विभिन्न स्तरों के राज्य अधिकारी शामिल थे जैसे महामंडलेश्वर, मंडलिका, समंत, महासमंत, और ठाकुर।
- ये अधिकारी किसानों से निकाली गई अधिशेष पर निर्भर थे, जिससे किसानों के पास व्यापार के लिए बहुत कम बचता था।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:
- भूमि मालिकों के हाथों में अधिशेष के संकेंद्रण ने एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास किया जहाँ स्थानीय आवश्यकताओं को स्थानीय रूप से पूरा किया गया।
- वास्तविक उत्पादकों की गतिशीलता पर कई प्रतिबंध लगे, जिससे इस स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिली।
- विनिमय के माध्यम की कमी, विशेष रूप से धातु के सिक्के, ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा दिया।
विनिमय के माध्यम:
विनिमय के माध्यम:
गुप्त काल के बाद व्यापार में गिरावट के सबूत:
- वास्तविक सिक्कों की कमी और पुरातात्विक खोजों में सिक्का-आकार के अभाव ने अध्ययन की गई अवधि के दौरान व्यापार में गिरावट का सुझाव दिया।
D.D. कोसांबी और R.S. शर्मा के योगदान:
- D.D. Kosambi ने प्रारंभ में गुप्त काल के बाद सीमित सिक्काकरण का विचार प्रस्तुत किया।
- R.S. Sharma ने 1965 में गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी और इसके व्यापार, वाणिज्य और सामंतवादी सामाजिक संरचनाओं के उदय से जुड़े पहलुओं पर जोर दिया।
सिक्कों की कमी के विवाद पर प्रतिक्रियाएँ:
- उड़ीसा का केस अध्ययन: यह c.A.D. 600 से 1200 के बीच सिक्कों की पूर्ण अनुपस्थिति की जांच करता है, लेकिन दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापार का तर्क देता है। विदेशी व्यापार में बदली के महत्व पर जोर दिया गया है।
- कश्मीर का केस अध्ययन: यह लगभग आठवीं शताब्दी A.D. के आसपास तांबे के सिक्कों के उदय को दर्शाता है। इस सिक्काकरण की खराब गुणवत्ता को व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था के पतन और कृषि गतिविधियों के बढ़ने से जोड़ा गया है।
- मध्य-पूर्वी भारत का दृष्टिकोण: यह A.D. 750-1200 के बीच बिहार, पश्चिम बंगाल और वर्तमान बांग्लादेश से मिले प्रमाणों के आधार पर सिक्कों की कमी और व्यापार के पतन के विचार को चुनौती देता है। हालांकि सिक्कों की अनुपस्थिति और पालों और सेनाओं द्वारा सिक्के न ढलाई जाने को स्वीकार करते हुए, यह तर्क करता है कि विनिमय के माध्यमों की कमी नहीं थी।
- हारीकेला के चांदी के सिक्कों, गुड़िया और चूर्णि (सोने/चांदी के धूल के रूप में धन) के प्रमाण के रूप में विनियम के माध्यमों को प्रस्तुत किया गया है।
लेकिन इन क्षेत्रों में भी:
लेकिन इन क्षेत्रों में भी:
स्थानीय लोगों की समुद्री व्यापार में भागीदारी:
- स्रोतों में इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या स्थानीय लोग क्षेत्र के समुद्री व्यापार में शामिल थे।
- यहां तक कि जो सीमित व्यापारिक गतिविधियाँ थीं, वे शासक वर्ग तक सीमित थीं।
- सामान्य लोगों की दुर्दशा इस बात में स्पष्ट है कि “वांगाली” शब्द का अर्थ होता था "बहुत गरीब और दुखी"।
- हालांकि कुछ क्षेत्रीय अपवाद हो सकते हैं, समग्र स्थिति प्रोफेसर R.S. शर्मा के सामान्य परिकल्पना के अनुरूप है।
दक्षिण-पूर्व एशिया के मामले में भी यही स्थिति थी।
कंबोडिया का विस्तृत अध्ययन और खमेर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में सिक्कों और बार्टर की भूमिका:
- गुप्त काल के बाद (ई.पू. 600-800) दक्षिणपूर्व एशिया, जिसमें कंबोडिया भी शामिल है, ने सिक्कों की प्रणाली विकसित नहीं की।
- खमेर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पैडी (चावल) और सीमित रूप से कपड़े के बार्टर पर निर्भर थी।
- जबकि प्रारंभिक मध्यकालीन सिक्कों जैसे कि इंडो-सासनियन, श्री विग्रह, श्री आदिवराह, बुल और हॉर्समैन, तथा गढईया का उदय पश्चिम और उत्तर-पश्चिमी भारत में हुआ, इनका समग्र अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा।
- सिक्कों की गुणवत्ता खराब थी और उनकी क्रय शक्ति कम थी, जो अर्थव्यवस्था में उनकी घटती भूमिका को दर्शाती है।
- जनसंख्या में वृद्धि और बस्तियों के विस्तार के बावजूद, इस दौरान धन के प्रवाह का मात्रा नगण्य था।
- प्रथम चरण में धातु के धन के प्रवाह में यह कमी भारत की व्यापारिक गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।
व्यापार में सापेक्ष कमी
राजनीतिक सत्ता का विखंडन:
- स्थानीय प्रमुखों और धार्मिक अनुदानकर्ताओं को शक्ति का वितरण भूमि अनुदान अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक शताब्दियों में नकारात्मक प्रभाव डालता है।
व्यापारियों और व्यापारियों की उत्साह में कमी:
- कई मध्यस्थ जमींदार, विशेषकर कम उत्पादक क्षेत्रों में, लूट और डकैती का सहारा लेते थे या अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले सामान पर अत्यधिक कर लगाते थे।
- संभावित शासक प्रमुखों के बीच लगातार युद्धों ने इस कमी में योगदान दिया।
जैन ग्रंथ और व्यापार:
- आठवीं शताब्दी के दो जैन ग्रंथ, समरैच्कहा और कुवलायमाला, त्वरित व्यापार और व्यस्त नगरों का उल्लेख करते हैं।
- हालांकि, इन ग्रंथों को पूर्व के स्रोतों से भारी रूप से प्रेरित माना जाता है और ये शायद आठवीं शताब्दी की वास्तविक आर्थिक स्थिति को सटीक रूप से नहीं दर्शाते हैं।
विदेशी व्यापार में कमी के कारण
भारत के पश्चिमी बाजारों की हानि और व्यापार पर प्रभाव
- ईसाई युग के प्रारंभिक सदियों में, भारत का पश्चिम के साथ एक लाभकारी व्यापार संबंध था, जिसने महत्वपूर्ण मात्रा में सोना लाया।
- 4वीं सदी में, रोमन साम्राज्य के पतन ने इस व्यापार को प्रभावित किया।
- 6वीं सदी के मध्य तक, बाईज़ेंटाइन साम्राज्य (पूर्व रोमन साम्राज्य) ने रेशम बनाने की कला सीखी, जिसने भारत के व्यापार को और प्रभावित किया।
- 7वीं और 8वीं सदी में, भारत के उत्तर-पश्चिम सीमाओं पर अरबों का विस्तार व्यापार को बाधित कर रहा था: अरब लुटेरों ने भारतीय व्यापारियों को पकड़ लिया और व्यापार मार्गों को बाधित कर दिया।
- ब्रोच और ठाणे जैसे बंदरगाहों पर हमले हुए, और सौराष्ट्र तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह वलभी को नष्ट कर दिया गया।
- हालांकि अरबों ने 10वीं सदी के बाद भारतीय समुद्री व्यापार के विकास में योगदान दिया, लेकिन उनके प्रारंभिक लूटपाट ने भारतीय वाणिज्यिक गतिविधियों को गंभीर रूप से बाधित किया।
- इस अवधि के दौरान तिब्बती और चीनी के बीच संघर्षों ने मध्य एशियाई व्यापार मार्गों पर सामान के प्रवाह को भी प्रभावित किया।
- हालांकि इस समय के दौरान साउथ-ईस्ट एशिया के साथ भारत के संपर्क का संदर्भ साहित्य में मिलता है, यह निश्चित नहीं है कि क्या यह पश्चिम के साथ व्यापार की हानि की भरपाई कर सकता था।
शहरी बस्तियाँ: गिरावट
शहरी बस्तियाँ: गिरावट
कई नगरों की गिरावट और निर्जनता का पहला चरण वाणिज्यिक मंदी का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि नगर मुख्य रूप से हस्तशिल्प और वाणिज्य में लगे व्यक्तियों द्वारा आबाद थे।
- व्यापार कम हुआ और हस्तशिल्प वस्तुओं की मांग में कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप व्यापारी और कारीगर वैकल्पिक आजीविका के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवास करने लगे।
- यह प्रवास नगरों के गिरने और नगरवासियों के गांव की अर्थव्यवस्था में एकीकृत होने का कारण बना।
- हियूएन त्सांग और पुराणिक रिकॉर्डों की गिनती ने काली युग के दौरान प्रमुख शहरों की जनसंख्या में कमी का संकेत दिया।
- इस गिरावट की प्रवृत्ति को 5वीं सदी में वराहमिहिर ने नोट किया था।
- वैशाली, पाटलिपुत्र और वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण नगरों के पतन के संकेत पुरातात्विक खुदाई से स्पष्ट हैं।
- खुदाई से संरचनाओं और पुरातात्विक वस्तुओं की कमी का पता चलता है।
- 3वीं से 8वीं सदी के बीच, शहरी केंद्रों ने निर्जनता या गिरावट का सामना किया।
- पंजाब में रोपर और उत्तर प्रदेश में भीटा जैसे बस्तियों को अंततः छोड़ दिया गया।
- कन्नौज की मध्यकालीन प्रासंगिकता अभी भी पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से पुष्टि की प्रतीक्षा कर रही है।
- गिरावट के बावजूद, व्यावसायिक गतिविधियाँ जारी रहीं, विशेष रूप से अभिजात वर्ग के लिए लक्जरी वस्तुओं के व्यापार में।
- कीमती पत्थरों, हाथी दांत, और घोड़ों जैसी वस्तुएँ दीर्घकालिक व्यापार में महत्वपूर्ण थीं।
- हालांकि, इस अवधि में दैनिक वस्तुओं के लेन-देन के लिए साक्ष्य दुर्लभ हैं।
- शिलालेखों में उल्लेखनीय वस्तुओं में नमक और तेल शामिल हैं, जिन्हें आयात करना पड़ा।
- यदि अर्थव्यवस्था आत्म-निर्भर होती, तो अनाज, चीनी, वस्त्र, और हस्तशिल्प के व्यापार के संदर्भ में अधिक साक्ष्य होते।
- A.D. 750-1000 के दौरान वाणिज्यिक गतिविधियाँ मुख्य रूप से भू-स्वामियों और सामंतों की आवश्यकताओं को पूरा करती थीं।
- हरियाणा में पेहोआ और उत्तर प्रदेश में आहर जैसे कुछ व्यापारिक केंद्र थे, जहाँ व्यापारी एकत्रित होते थे।
- हालांकि, ये केंद्र देश की मुख्यतः बंद अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डाल पाए।
दूसरा चरण (लगभग A.D. 900 – 1300)
व्यापार और वाणिज्य का पुनरुद्धार (9वीं-13वीं सदी):
- इस अवधि में व्यापार और वाणिज्य का पुनरुद्धार देखा गया, जिसे कृषि विस्तार, धन के उपयोग में वृद्धि, और एक बाजार अर्थव्यवस्था की पुनः उपस्थिति के द्वारा चिह्नित किया गया, जहां वस्तुएं अदला-बदली के लिए उत्पादित की जाती थीं न कि स्थानीय उपभोग के लिए।
- उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में शहरी बस्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।
- हालांकि क्षेत्रीय भिन्नताएँ थीं, अनाज, दालों और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसने आंतरिक और बाह्य व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बनाया।
कला और उद्योग:
- कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ शिल्प उत्पादन में भी वृद्धि हुई, जिसने क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय अदला-बदली को उत्तेजित किया।
- कपड़ा उद्योग, जो प्राचीन काल से स्थापित था, एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि बन गया।
- गांधी और गुजरात जैसे क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त हुई, जिसमें मोटे और महीन कपास के सामान का उत्पादन किया गया।
- मार्को पोलो और अरबी लेखकों ने बंगाल और गुजरात के कपास के कपड़ों की गुणवत्ता की प्रशंसा की, जबकि 'मनसोल्लासा' जैसे ग्रंथों ने महत्वपूर्ण कपड़ा केंद्रों को उजागर किया।
- तेल उद्योग भी प्रमुखता प्राप्त करने लगा, जिसमें दसवीं सदी से तेलबीज की खेती और तेल मिलों का उल्लेख बढ़ा।
- गुड़ और अन्य चीनी रूपों का बड़े पैमाने पर उत्पादन, गन्ने की खेती और गन्ना क्रशरों के उल्लेख से स्पष्ट होता है।
- धातु और चमड़े की कारीगरी उच्च स्तरों पर पहुंच गई, जिसमें विभिन्न धातुओं जैसे तांबा, पीतल, लोहे, सोने, और चांदी के साथ काम करने वाले कारीगरों का उल्लेख है।
- उच्च गुणवत्ता वाले शस्त्र और हथियार बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया गया, जिसमें मगध, वाराणसी, कलिंग, और सौराष्ट्र जैसे क्षेत्रों को उनकी तलवारों के लिए जाना जाता था।
- गुजरात अपनी चमड़े की उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, जो कढ़ाई वाले चमड़े के चटाई का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता था।
- सिक्के और अन्य अदला-बदली के माध्यमों में पुनरुत्थान देखा गया, जिसमें विभिन्न सिक्कों के साहित्यिक और शिलालेख संदर्भ शामिल थे।
- धातु मुद्रा पुनः उभरी, जिसमें विभिन्न प्रकार के सिक्कों और उनके गुणकों का संदर्भ ग्रंथों और शिलालेखों में पाया गया।
- सिक्कों के संदर्भों की प्रचुरता के बावजूद, चलन में मुद्रा की कुल मात्रा सीमित थी, और सिक्कों को अक्सर घटित किया जाता था और उनका वजन कम किया जाता था।
- विनिमय का एक महत्वपूर्ण साधन बार्टर बना रहा, और वाणिज्य को सुगम बनाने के लिए बिना नकद पैसे के लिए हंडीका (बिल ऑफ एक्सचेंज) जैसे क्रेडिट उपकरण विकसित किए गए।
- इस अवधि के ग्रंथों में उपभोग और वाणिज्यिक उद्यमों के लिए ऋण उठाने के विभिन्न साधनों का संकेत मिलता है, जो उस समय की आर्थिक प्रथाओं को दर्शाता है।
व्यापार के पहलू
व्यापार के पहलू
- कृषि उत्पादन में वृद्धि और औद्योगिक तथा कारीगरी उत्पादन द्वारा उत्पन्न गति ने विनिमय केंद्रों की एक पदानुक्रम बनाने में योगदान दिया।
- अंतर-क्षेत्रीय और अंतःक्षेत्रीय विनिमय नेटवर्क ने पहले चरण (लगभग 750-900 ई. के आस-पास) की अपेक्षाकृत बंद गांव अर्थव्यवस्था में दरारें उत्पन्न कीं।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
व्यापार की वस्तुएं:
- व्यापारी विभिन्न वस्तुओं जैसे कि खाद्य अनाज, तेल, मक्खन, नमक, नारियल, सुपारी, पान के पत्ते, मेहंदी, नीला रंग, शक्कर, गुड़, धागा, कपास के कपड़े, कंबल, धातु और मसाले एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे, और इसके लिए कर और टोल का भुगतान करते थे।
- चावल, गेहूं, जौ, दालें, अलसी की फाइबर, कपास का कपड़ा, ताड़ का चीनी, नीला रंग, और रस्सियों के लिए नारियल का रेशे भी महत्वपूर्ण व्यापार आइटम थे।
भारतीय वस्तुओं के उपभोक्ता:
- भारतीय वस्तुओं के प्रमुख उपभोक्ता चीन, अरब और मिस्र के धनवान निवासी थे।
- कई भारतीय उत्पाद संभवतः भूमध्य सागर के माध्यम से यूरोप पहुंचे।
- घरेलू स्तर पर, उपभोक्ताओं में नई भूमि मालिक वर्ग, शासक chiefs, उभरते व्यापारिक वर्ग, और ब्राह्मणिक एवं गैर-ब्राह्मणिक धार्मिक संस्थाएँ शामिल थीं।
- देवताओं को अर्पित करने या प्रसाद के रूप में वितरित करने के लिए खाद्य सामग्री की बढ़ती आवश्यकता थी।
व्यापार मार्ग:
- एक विशाल सड़क नेटवर्क ने विभिन्न बंदरगाहों, बाजारों और नगरों को जोड़ा, जिससे व्यापार और वाणिज्य में सुविधा हुई।
- चinese तीर्थयात्री हियु एन त्सांग ने सातवीं शताब्दी में भारत में भूमि संपर्कों का दस्तावेजीकरण किया, जिसमें उन्होंने उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कांची, और पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में सिंध तक के नगरों का दौरा किया।
- कश्मीर के ग्यारहवीं शताब्दी के कवि बिल्हण ने भी भारत के विभिन्न भागों में अपनी यात्राओं के बारे में लिखा।
- अल-बिरुनी ने 1030 ई. में कन्नौज, मथुरा, और बयाना जैसे स्थानों से उत्पन्न होने वाले पंद्रह व्यापार मार्गों का उल्लेख किया।
- एक महत्वपूर्ण मार्ग कन्नौज से शुरू होता था, प्रयाग के माध्यम से गुजरता था, और ताम्रलिप्ति के बंदरगाह (आधुनिक तमलुक, पश्चिम बंगाल) की ओर जाता था, फिर पूर्वी तट के साथ कांची तक। यह मार्ग असम, नेपाल, और तिब्बत से भी जुड़ता था, जिससे चीन के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाया जा सके।
- राजस्थान के बयाना से एक मार्ग मारवाड़ के रेगिस्तान से गुजरते हुए सिंध के आधुनिक बंदरगाह कराची तक जाता था, जिसमें गुजरात और उत्तरी भारत के बंदरगाहों और नगरों से जुड़ने वाली शाखाएँ थीं।
- मथुरा और प्रयाग से पश्चिमी तट पर ब्रोच के बंदरगाह तक उज्जैन के माध्यम से जाने वाले मार्ग ने आंतरिक भारत को अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उत्तर भारत में नदियाँ और दक्षिण भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के साथ समुद्री मार्ग भी अंतर-क्षेत्रीय संपर्क के लिए महत्वपूर्ण थे।
संचार के साधन:
मैदानी क्षेत्रों में, बैल गाड़ियों का प्राथमिक परिवहन साधन था, लेकिन जहाँ इनका उपयोग नहीं हो सकता था, वहाँ मानव श्रमिकों का उपयोग सामानों को ले जाने के लिए किया जाता था। नदी यातायात के लिए विभिन्न प्रकार की नावों का उपयोग किया जाता था, जबकि विशाल जहाज समुद्र में चलते थे। दसवीं सदी के बाद, शासकों ने राजमार्गों की सुरक्षा बनाए रखने, चोरों और डाकुओं को सजा देने, और व्यापारियों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने में बढ़ती रुचि दिखाई। गुजरात में, चालुक्य राजाओं ने राजमार्गों की देखरेख के लिए 'जियाला-पथ-कारण' नामक एक विभाग स्थापित किया, महत्वपूर्ण बंदरगाहों और बाज़ारों को जोड़ने के लिए नए रास्ते बनाए, और यात्रियों के लाभ के लिए तालाबों और कुओं का खुदाई की। जैसे-जैसे व्यापार एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत बन गया, राजनीतिक अधिकारियों ने व्यापारियों और वाणिज्यिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया। मार्को पोलो ने कंबे को एक समुद्री डाकू-मुक्त क्षेत्र के रूप में नोट किया, जो इस बात का संकेत है कि भारतीय राजाओं ने समुद्र मार्ग पर समुद्री डाकुओं से बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए, जो दक्षिण चीन से फारसी खाड़ी तक के समुद्री रास्ते पर एक बड़ा खतरा था।
- वृहद स्तर पर समुद्री व्यापार गतिविधियाँ संचालित की गईं। इस अवधि में फारसी खाड़ी और दक्षिण चीन के बीच समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ, जिसमें भारत को अपनी स्ट्रैटेजिक स्थिति से लाभ हुआ।
- एशियाई व्यापार मुख्यतः अरबों द्वारा नियंत्रित था, जिन्होंने आठवीं सदी में महत्वपूर्ण बंदरगाह वलभी को नष्ट करने के बाद अरब सागर में प्रमुख समुद्री शक्ति प्राप्त की।
- बारहवीं सदी में, चीन इस व्यापार में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभरा, लेकिन अरबों ने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी।
- अरब प्रतिस्पर्धा के बावजूद, भारतीयों ने दसवीं सदी से समुद्री व्यापार में भाग लेना शुरू किया। अरब लेखकों जैसे अबू ज़ैद ने फारसी खाड़ी में भारतीय व्यापारियों का उल्लेख किया, और यात्रियों जैसे इब्न बतूता ने अदन जैसे स्थानों पर भारतीय व्यापारी उपनिवेशों का उल्लेख किया।
- दक्षिण भारत में चोल विशेष रूप से समुद्री व्यापार में सक्रिय थे, जिन्होंने मलय और सुमात्रा जैसे क्षेत्रों के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित किए और व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए चीन के लिए दूतावास भेजे।
- सीमित भौतिक भागीदारी के बावजूद, भारतीय उत्पादों की विश्व स्तर पर उच्च मांग थी, जो अक्सर अरब और चीनी मध्यस्थों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुँचते थे।
वस्तुएँ जो विनिमय की गईं
पूर्व से आयात:
- चीनी
- मार्को पोलो हमें बताते हैं कि पूर्व से आने वाले जहाजों ने गुजरात के कंबे पोर्ट पर सोना, चाँदी और तांबा लाया।
- टिन एक अन्य धातु थी जो दक्षिण-पूर्व एशिया से भारत आई।
पूर्व को निर्यात:
- अरोमेटिक्स और मसाले (विशेष रूप से काली मिर्च)। मार्को पोलो के अनुसार, काली मिर्च का सेवन केवल कुरीसाई (हांग-चौ) शहर में ही प्रतिदिन 10,000 पाउंड की दर से होता था।
- भारत से चीन को कपास का कपड़ा: एक चीनी बंदरगाह अधिकारी (चौ जू कुआ) की रिपोर्ट में कहा गया है कि इब्न बतूता (ई. स. 1333) के अनुसार, चीन के शहरों में सुस्त कपास के कपड़े रेशम से कमतर और अधिक मूल्यवान थे।
- भारत भी चीन को हाथी दांत, गैंडे के सींग और कुछ कीमती तथा अर्ध-कीमती पत्थर निर्यात करता था।
पश्चिम में व्यापार के प्रमाण (यानी अरब):
- कंबे, समराथा और जूनागढ़ में मिले अरबी लेखन से पता चलता है कि फारसी खाड़ी के व्यापारी और शिपर बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी में पश्चिमी भारत आए थे।
- लेखापद्धति में उल्लेख है कि फारसी खाड़ी के होर्मुज से गुजरात तट पर जहाज आ रहे थे।
पश्चिम को निर्यात:
- यहूदी व्यापारी पश्चिमी भारत के तट से कई सामान जैसे: मसाले, अरोमेटिक्स, रंग, औषधीय जड़ी-बूटियाँ, कांस्य और पीतल की बर्तन, वस्त्र, मोती, मनके, नारियल आदि को मिस्र के बाजारों में ले जाते थे।
- भारत ने तटीय क्षेत्रों में जहाज निर्माण और घरों के निर्माण के लिए आवश्यक टीक की लकड़ी का भी निर्यात किया।
- कुछ अधिशेष खाद्यान्न, मुख्य रूप से चावल भी निर्यात किया गया।
- मार्को पोलो के अनुसार, गुजरात की सुंदर और कढ़ाई की गई चमड़े की चटाइयाँ अरब जगत में अत्यधिक मूल्यवान थीं।
- लोहे और स्टील के उत्पाद, विशेष रूप से तलवारें और भाले, पश्चिमी देशों में व्यापक बाजार का आनंद लेते थे।
पश्चिम से आयात:
- सबसे महत्वपूर्ण वस्तु घोड़ा था। जैसे-जैसे प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि में सामंतों और प्रमुखों की संख्या बढ़ी, घोड़ों की मांग भी कई गुना बढ़ गई। घोड़ों को भूमि और समुद्र दोनों के द्वारा लाया गया। इब्न बतूता हमें बताते हैं कि उत्तर-पश्चिमी भूमि मार्गों से आने वाले घोड़े के व्यापारी बड़े लाभ कमाते थे। वसाफ (ई. 1328, एक अरब लेखक) के अनुसार, तेरहवीं सदी में हर साल 10,000 से अधिक घोड़ों को कोरोमंडल तट, कंबे और भारत के अन्य बंदरगाहों पर लाया जाता था। घोड़ों को बहरीन, मुस्कट, अदन, फारस आदि जैसे स्थानों से लाया गया। खजूर, हाथी दांत, मूंगा, पन्ना आदि भी पश्चिम से भारत में लाए गए।
बंदरगाह:
- डेबल बंदरगाह (इंडस के मुहाने पर): इसे अरब और चीन के साथ-साथ भारत के अन्य बंदरगाहों से जहाजों द्वारा देखा गया। गुजरात के तट पर सोमनाथ, ब्रॉच और कंबे थे। सोमनाथ की पूर्व में चीन और पश्चिम में ज़ांज़ीबार (अफ्रीका) के साथ संबंध थे। ब्रॉच (या प्राचीन भृगुकच्छ) का बहुत लंबा इतिहास रहा है। कंबे (अरबी स्रोतों में खंभायत और संस्कृत स्रोतों में स्तंभतीर्थ): इसका सबसे पुराना उल्लेख नौवीं सदी ईस्वी में मिलता है। सोपारा और थाणे अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाह थे।
मलाबार तट पर:
- क्विलोन सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में उभरा था। अरब लेखकों और चीनी स्रोतों में क्विलोन बंदरगाह के महत्व का उल्लेख है।
पूर्वी बंदरगाह:
- दसवीं और तेरहवीं सदी के बीच तीन शताब्दियों में, कोरोमंडल तट पूर्व और पश्चिम से आने वाले जहाजों के लिए एक वास्तविक क्लियरिंग हाउस के रूप में विकसित हुआ। वसाफ: हमें बताता है कि फारसी खाड़ी के द्वीपों की समृद्धि और यूरोप तक के अन्य देशों की सुंदरता को कोरोमंडल तट से प्राप्त किया गया है। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह नागापट्टिनम था।
उड़ीसा तट पर:
- पुरी और कालिंगपट्टम महत्वपूर्ण बंदरगाह थे।
बंगाल में तम्रलिप्ति की किस्मत फिर से जागृत हो रही थी, हालाँकि कुछ विद्वानों के अनुसार, इसे साप्तग्राम के एक अन्य बंदरगाह द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा था।
व्यापारियों की सुरक्षा और सुरक्षा:
- भारी लाभ के मद्देनजर, समकालीन राजनीतिक अधिकारियों ने विदेशी व्यापार में लगे व्यापारियों को प्रदान की गई सुविधाओं में गहरी रुचि दिखाई।
- गुजरात के चालुक्य (10वीं-13वीं शताब्दी) ने शाही नियंत्रण के तहत बंदरगाहों का एक अलग विभाग (वेलाकुलकरना) स्थापित किया।
- उन्होंने अपने राज्य में मुस्लिम व्यापारियों को धार्मिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान की।
- कोला राजाओं ने भी अपने बंदरगाहों का प्रबंधन शाही अधिकारियों के माध्यम से किया, जिन्होंने स्थानीय व्यापारी संगठनों की मदद से विदेशी व्यापारियों का ध्यान रखा और बंदरगाह कर (port-cesses) एकत्र किया।
- अरब लेखकों ने एकमत से राष्ट्रकूट राजाओं की अरबों के प्रति शांति और सहिष्णुता की नीति की प्रशंसा की।
- इब्न बत्तूता हमें बताते हैं कि जब भी कोई विदेशी व्यापारी मर जाता, उसकी संपत्ति को जब्त नहीं किया जाता था, बल्कि उसे सुरक्षित रखकर वारिस को सौंपा जाता था।
- आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में मोटुपल्ली में मिले एक शिलालेख (A.D. 1244) से पता चलता है कि राजा ने तूफान में फंसी जहाजों की सुरक्षा की गारंटी दी और विदेशी व्यापारियों का विश्वास जीतने के लिए भूमि के कानून के अनुसार शुल्क एकत्र करने का आश्वासन दिया।
नगरों का पुनरुद्धार:
- प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का दूसरा चरण (लगभग 900-1300 ईस्वी) पिछले दो शताब्दियों से एक महत्वपूर्ण भिन्नता था, क्योंकि यह शहरी केंद्रों के एक विशेष पुनरुद्धार द्वारा चिह्नित है।
- यह पुनरुद्धार लगभग सम्पूर्ण भारत में एक घटना बन गया।
- इसे अक्सर भारतीय उपमहाद्वीप की “तीसरी शहरीकरण” के रूप में वर्णित किया जाता है।
व्यापारी समुदाय और संगठन
व्यापारी समुदाय और संगठन
प्राचीन भारत में व्यापारियों और वाणिज्यिकों की भूमिका:
- व्यापारी उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।
- वे कृषि अधिशेष और शिल्पकारों एवं कारीगरों के उत्पादों को एकत्रित करते हैं, जिन्हें व्यापक क्षेत्र में वितरित किया जाता है।
- समाज में व्यापारियों और वाणिज्यिकों की स्थिति दो वाणिज्यिक गतिविधियों के चरणों से जुड़ी हुई है:
- पहला चरण (700-900): व्यापारियों को सीमित वाणिज्यिक आदान-प्रदान के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- दूसरा चरण (900-1300): व्यापार के पुनरुद्धार ने वाणिज्यिक समुदायों की स्थिति और शक्ति में सुधार किया।
- प्राचीन भारतीय ग्रंथों में व्यापार को, कृषि और पशुपालन के साथ, वैश्याओं के लिए आजीविका के वैध साधनों के रूप में मान्यता दी गई है।
- सातवीं सदी में, चीनी यात्री हियूएन त्सांग ने वैश्याओं को व्यापारियों और शूद्रों को कृषकों के रूप में उल्लेख किया।
- गुप्त काल के बाद ब्राह्मणical वर्ण व्यवस्था की बाधाएँ कमजोर हो गईं, जिससे एक अधिक तरल सामाजिक संरचना बनी जहाँ लोग वर्ण विभाजनों के पार पेशे अपनाने लगे।
पहले चरण के दौरान व्यापारियों की स्थिति (लगभग 700-900 ईस्वी):
- इस अवधि के दौरान व्यापार के गिरावट ने समाज में व्यापारियों की भूमिका को काफी हद तक कम कर दिया।
- व्यापार में गिरावट और बाजारों के गायब होने के साथ, व्यापारियों को मंदिरों और उभरते जमींदारों से संरक्षण प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ा।
- यह परिवर्तन व्यापारियों को उनकी स्वतंत्र वाणिज्यिक गतिविधियों से वंचित कर दिया, जिससे उन्हें अपने संरक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- उड़ीसा और मध्य भारत से प्राप्त लेखों से पता चलता है कि व्यापारियों, कारीगरों और वाणिज्यिकों को दाताओं के पास स्थानांतरित किया गया।
- इस अवधि के दौरान व्यापारियों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिकाएँ सौंपे जाने का कोई सबूत नहीं है, जो गुप्त काल में उनकी प्रशासनिक भूमिकाओं के विपरीत है।
- कुछ व्यापारी, विशेष रूप से तट पर, सक्रिय रहे लेकिन संख्या में कम थे, और मुख्य रूप से राजाओं, प्रमुखों और मंदिरों के लिए विलासिता के सामान पर ध्यान केंद्रित किया।
- दक्षिण भारत में, व्यापार एक प्रमुख गतिविधि नहीं थी, जैसा कि समकालीन रिकॉर्ड में व्यापारियों की एक विशिष्ट वर्ग के रूप में अनुपस्थिति से स्पष्ट है।
- प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि का पहला चरण समृद्ध और स्वतंत्र व्यापारी वर्ग के गिरावट का प्रतीक है।
दूसरे चरण के दौरान व्यापारियों की स्थिति (लगभग 900-1300 ईस्वी):
- वाणिज्यिक समुदाय ने पुनः महत्व प्राप्त किया, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी लक्जरी और आवश्यक वस्तुओं के व्यापार में सक्रिय रूप से शामिल थे।
- कई व्यापारियों ने विभिन्न स्तरों पर प्रशासन में भाग लिया और शाही अदालतों में मंत्री पद धारण किए।
- व्यापारियों ने मंदिरों और पुरोहितों को महत्वपूर्ण उपहार देकर सामाजिक मान्यता प्राप्त की।
- इस अवधि के साहित्य और शिलालेखों में कई व्यापारियों का उल्लेख है जो उनके विशेष व्यापारों के लिए जाने जाते थे।
- पैसे उधार देना व्यापारियों के लिए एक प्रमुख गतिविधि बन गया, जिसमें पश्चिमी भारत में Nikshepa-vanika जैसे विशेष समूहों का उदय हुआ।
- क्षेत्रीय व्यापारी समूह, विशेष रूप से पश्चिमी भारत से, उस क्षेत्र के विशाल भूमि मार्ग नेटवर्क के कारण प्रमुखता प्राप्त करते गए जो तटीय बंदरगाहों को उत्तरी भारत से जोड़ते थे।
- ओसिया, पट्ली, श्रीमाला और मोढेरा जैसे स्थानों से व्यापारियों को मिलकर मारवाड़ी के रूप में जाना जाने लगा।
- इन व्यापारियों को संदर्भित करने के लिए श्रेठी और सार्थवह जैसे शब्दों का सामान्य रूप से उपयोग किया जाता था।
- श्रेष्ठी: एक समृद्ध थोक व्यापारी जो छोटे व्यापारियों को सामान या पैसे उधार देते हुए बैंक के रूप में भी कार्य करता था।
- सार्थवह: एक कारवां नेता जो दूर के व्यापारिक यात्राओं में व्यापारियों का मार्गदर्शन करता था, जिसके पास मार्गों, भाषाओं और क्षेत्रीय व्यापार नियमों का ज्ञान होता था।
- दक्षिण भारत में, 8वीं/9वीं शताब्दी से कृषि का विस्तार और अधिशेष उत्पादन ने व्यापार के आदान-प्रदान में वृद्धि की।
- दक्षिण भारतीय व्यापारी विशेष वस्तुओं जैसे कि वस्त्र, तेल, घी, सुपारी और घोड़ों में विशेषज्ञता रखते थे।
- क्षेत्रीय बाजार जिन्हें नागरम कहा जाता था, आदान-प्रदान के केंद्र बन गए, और उनकी संख्या कोला अवधि के दौरान काफी बढ़ गई।
व्यापारियों की सामाजिक भूमिका:
- व्यापार के विकास के साथ आर्थिक समृद्धि बढ़ी, जिससे व्यापारी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए मंदिरों, पुजारियों और धार्मिक कार्यों के रखरखाव में योगदान देने लगे। कई शिलालेख इन उद्देश्यों के लिए व्यापारियों द्वारा नकद या सामान के दान का दस्तावेजीकरण करते हैं। कुछ व्यापारी प्रभावशाली बन गए और राज्य अधिकारियों और मंत्रियों की श्रेणी में शामिल हो गए। उदाहरण के लिए, एक दसवीं शताब्दी का शिलालेख एक मोढ़ा जाति के व्यापारी का उल्लेख करता है जो महाराष्ट्र के ठाणे के पास संजन का प्रमुख बन गया। गुजरात में, विमला का व्यापारी परिवार क्षेत्र के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके वंशज जैसे वस्तुपाल और ताजपाल महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर रहे और माउंट आबू में जैन देवताओं के लिए प्रसिद्ध संगमरमर के मंदिरों का निर्माण किया। मध्य गुजरात से एक तेरहवीं शताब्दी का शिलालेख दर्शाता है कि कई महत्वपूर्ण व्यापारी, व्यापारी और कारीगर स्थानीय प्रशासनिक निकायों का हिस्सा थे।
व्यापारियों का चरित्र और आचरण:
- विदेशी लेखक और यात्री, जैसे अल-इद्रीसी (बारहवीं शताब्दी) और मार्को पोलो (तेरहवीं शताब्दी), भारतीय व्यापारियों की सत्यता और व्यापारिक लेन-देन में ईमानदारी की प्रशंसा करते हैं। हालांकि, समकालीन भारतीय साहित्य में लालची और बेईमान व्यापारियों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। उदाहरण के लिए, कश्मीर के लेखक क्षेमेन्द्र एक स्वार्थी व्यापारी का वर्णन करते हैं जो अकाल के समय खाद्यान्न का भंडारण करके लाभ प्राप्त करता है। पश्चिमी भारत के ग्यारहवीं शताब्दी के ग्रंथ व्यापारियों को उनके स्थान और चरित्र के आधार पर उच्च और निम्न में वर्गीकृत करते हैं, जिसमें धनी व्यापारी जो बड़े पैमाने पर व्यापार में लगे होते हैं, उन्हें बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जबकि छोटे व्यापारी और कारीगर जो लोगों को धोखा देते हैं, उन्हें तिरस्कृत किया जाता है।
व्यापारियों का संगठन
व्यापारी और गिल्ड:
- व्यापारी केवल धन से नहीं, बल्कि अपने हितों की सुरक्षा के लिए गठित गिल्ड से भी शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करते थे।
- प्रारंभिक चरण में, व्यापार में गिरावट ने व्यापारी कॉर्पोरेट गतिविधियों को कमजोर कर दिया, जिससे गिल्ड क्षेत्रीय या व्यावसायिक उपजातियों में सीमित हो गईं।
- हालांकि, जैसे-जैसे व्यापार में पुनरुद्धार हुआ, व्यापारी गिल्ड आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण रूप से पुनः उभरीं।
गिल्ड: परिभाषा और कार्य:
- गिल्ड समान प्रकार के वस्त्रों का व्यापार करने वाले व्यापारियों के स्वैच्छिक संघ थे, जैसे अनाज, वस्त्र, पान की पत्तियाँ, घोड़े, इत्र, आदि।
- ये स्थानीय (अधिक स्थायी) और यात्रा करने वाले (विशिष्ट यात्राओं के लिए अस्थायी) व्यापारियों द्वारा गठित किए गए थे।
- गिल्ड ने सदस्यता और आचरण के संबंध में अपने नियम स्थापित किए।
- वे वस्तुओं के लिए मूल्य निर्धारित करते थे और बिक्री के लिए विशेष दिनों की मांग कर सकते थे।
- यदि स्थानीय प्राधिकरण सहयोग नहीं करते थे, तो वे कुछ क्षेत्रों में व्यापार करने से मना कर सकते थे।
- गिल्ड के व्यापारी धार्मिक हितों के संरक्षक के रूप में कार्य करते थे, अक्सर मंदिर की देखभाल के लिए अतिरिक्त कर चुकाने पर सहमत होते थे।
- प्रत्येक गिल्ड का नेतृत्व एक प्रमुख द्वारा किया जाता था, जिसे सदस्यों द्वारा चुना जाता था, जो एक मजिस्ट्रेट की तरह कार्य करता था, आर्थिक विवादों को सुलझाता था और गिल्ड का प्रतिनिधित्व राजा के समक्ष करता था।
- गिल्ड के सदस्य एक सख्त अनुशासन को मानते थे लेकिन बाजार में सुरक्षा और विश्वसनीयता का आनंद लेते थे।
- हालांकि गिल्ड के प्रमुख कभी-कभी अधिनायकत्व दिखाते थे, व्यापारी गिल्ड को शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्व देते थे।
- व्यापारियों के कॉर्पोरेट निकाय का वर्णन करने के लिए विभिन्न शब्दों जैसे नाईगमा, श्रेणी, समूह, सार्थ, संघ का उपयोग किया जाता था।
- नाईगमा विभिन्न जातियों के कारवाँ व्यापारियों का संघ था जो अन्य देशों के साथ व्यापार करते थे।
- श्रृंखला को समान पेशे में लोगों के समूह के रूप में देखा जाता था, हालांकि व्याख्याएँ भिन्न थीं।
- पश्चिमी भारत में राजाओं ने गिल्ड गतिविधियों की निगरानी के लिए श्रेणी-करण विभाग स्थापित किया।
- कुछ व्यापारी गिल्ड ने सुरक्षा के लिए अपनी खुद की सेना श्रेणीबल बनाए रखी।
- लेखों में व्यापारी कॉर्पोरेट गतिविधियों का उल्लेख है, जिसमें वाणिज्य- मंडल जैसे संदर्भ स्थानीय व्यापारी गिल्ड को दर्शाते हैं।
दक्षिण भारत में व्यापार गिल्डों का संगठन:
दक्षिण भारत में व्यापार संघों का संगठन:
दक्षिण भारत में व्यापारी संघ:
- दसवीं सदी में कृषि और व्यापार के विस्तार के कारण दक्षिण भारत में व्यापारी संघों का उदय हुआ।
- इन संघों को समय के रूप में जाना जाता था, जो सदस्यों के बीच विशेष नियमों का पालन करने के लिए सहमति द्वारा बनाए गए थे।
- मुख्य व्यापारी संघों में Ayyavole और Manigraman शामिल थे, जो वर्तमान महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश में संचालित होते थे।
- चोल राजाओं ने विभिन्न पहलों के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा दिया, और व्यापार संघों ने भारतीय संस्कृति के निर्यात में भूमिका निभाई।
- Ayyavole संघ, जिसे 500 स्वामी के रूप में जाना जाता था, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के समुदायों के बीच व्यापार लिंक के रूप में कार्य करता था।
- यह दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में संचालित होता था, चोलों के अधीन अपनी शक्ति प्राप्त करता था।
- Ayyavole संघ ने स्थानीय व्यापार संघों को शामिल करते हुए विस्तार किया, और चोल समर्थन के साथ एक समुद्री शक्ति बन गया।
- संघ श्री विजया, बर्मा और थाई प्रायद्वीप जैसे स्थानों में सक्रिय था।
- Ayyavole संघ ने एक संघ का गठन किया और व्यापार के विकास के कारण एक घुमंतू समूह से एक समुदाय में विकसित हुआ।
- शब्द नानादेसी संघ की विविध सदस्यता का संदर्भ देता है।
- संघ का प्रभाव दक्षिण भारत से परे फैला, जैसा कि बर्मा, जावा, सुमात्रा और श्रीलंका में पाए गए शिलालेखों में देखा गया।
- कुछ सदस्यों ने समय चक्रवर्ती का शीर्षक धारण किया, जो संघों पर नियंत्रण का संकेत देता है।
- मनिग्रामण संघ, जो प्रारंभ में केरल तट के साथ था, ने अपनी गतिविधियों का विस्तार किया और लंबी दूरी के समुद्री व्यापार में भी संलग्न हुआ।
- एक अन्य समूह, Anjuvannam, केरल तट के साथ उभरा और स्थानीय व्यापारियों और संघों के साथ बातचीत की।
- व्यापार संघ महत्वपूर्ण बन गए, जिनमें संघों ने उच्च वंशावली का पता लगाया, जैसे कि Ayyavole के विरा बनंजा।
- ये संघ विशाल व्यापार नेटवर्क को नियंत्रित करते थे, एक-दूसरे के साथ सहयोग करते थे और शाही घरानों के साथ निकटता से जुड़े रहते थे।
व्यापारियों और कारीगरों के बीच संबंध:
व्यापारियों और कारीगरों के बीच संबंध:
- प्रारंभिक मध्यकालीन काल में कारीगरों और व्यापारियों के बीच संबंध की सटीक प्रकृति समकालीन स्रोतों में स्पष्ट रूप से दस्तावेजित नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि जैसे कि बुनकर और धातु श्रमिक, कारीगर स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे या व्यापारियों के निर्देशन में, जो उन्हें पैसे, कच्चे माल, या दोनों प्रदान करते थे।
- कुछ साक्ष्य यह सुझाव देते हैं कि जैसे-जैसे व्यापारियों ने कच्चे माल और तैयार उत्पादों के संचलन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त किया, उनके प्रभाव का कारीगरों की गतिविधियों पर महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई।
- ऐतिहासिक व्यक्तित्व जैसे कि अल्बिरुनी और 12वीं सदी के न्यायविद लक्ष्मिधर यह संकेत देते हैं कि कारीगर व्यापारियों के बीच रहते थे। यह निकटता सुझाव देती है कि व्यापारी पूंजी और कच्चे माल की आपूर्ति करते थे, जबकि कारीगर व्यापारी की मांग और विनिर्देशों के अनुसार सामान का उत्पादन करते थे।
- तमिलनाडु के एरोड से 11वीं सदी की एक लेख inscription कारीगरों की व्यापारी संगठनों पर निर्भरता को उजागर करती है, क्योंकि यह कारीगरों के लिए व्यापारियों द्वारा प्रदान किए गए आश्रय का उल्लेख करती है।
- जैसे-जैसे व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ, व्यापारियों ने खरीदने और बेचने के वाणिज्यिक नेटवर्क का एकाधिकार करने की प्रवृत्ति दिखाई, जिससे कारीगरों की स्वतंत्र रूप से अपने सामान को बाजार में बेचने की क्षमता सीमित हो गई।
- कुछ तेल विक्रेताओं और बुनकरों के उदाहरण हैं जिन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने सामान को बेचने में सफलता पाई और इतने अमीर हो गए कि उन्होंने मंदिरों और पुजारियों को दान देने में सक्षम हो गए।
- सामान्यतः, प्रारंभिक मध्यकालीन काल में कारीगर और शिल्पकार बड़े व्यापारियों पर आर्थिक रूप से निर्भर थे।
|
28 videos|739 docs|84 tests
|





















