भारत में पुर्तगाली | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download
पुर्तगालीयों का आगमन
- वास्को दा गामा का 1498 में मलाबार तट पर कालीकट में आगमन, तीन जहाजों के साथ और एक गुजराती नाविक अब्दुल मजीद द्वारा मार्गदर्शित, एशिया और यूरोप के बीच संबंधों में एक नए युग की शुरुआत मानी जाती है।
समुद्री मार्ग खोजने के उद्देश्य और पुर्तगाली आगमन के पीछे के कारक:
- एशिया और यूरोप प्राचीन काल से व्यापार में लगे हुए थे।
- दोनों के बीच प्रत्यक्ष समुद्री संबंध एक पुरानी आकांक्षा की पूर्ति थे।
- ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने 6वीं सदी ईसा पूर्व में फिनिशियन द्वारा अफ्रीका के चारों ओर यात्रा करने का उल्लेख किया।
- 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल का ओटोमन तुर्कों द्वारा पतन मौजूदा व्यापार मार्गों में अवरोध उत्पन्न करता है।
- भारतीय वस्तुएँ अरब मुस्लिम बिचौलिए के माध्यम से यूरोपीय बाजारों तक पहुँचती थीं।
- रेड सी का व्यापार मार्ग इस्लामी शासकों के लिए एक लाभकारी राज्य एकाधिकार बन गया।
- भारत के लिए भूमि मार्ग भी अरबों द्वारा नियंत्रित थे।
- यूरोपियन सीधे भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजने के लिए उत्सुक थे।
- भारत के साथ प्रत्यक्ष समुद्री लिंक अरब और तुर्कों के पूर्वी वस्तुओं के व्यापार पर एकाधिकार को कमजोर करेगा।
- पुर्तगालियों के लिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग स्थापित करना मुसलमानों को गंभीर चोट पहुँचाएगा।
- अरब और तुर्क पारंपरिक रूप से ईसाई धर्म के विरोधी थे।
- तुर्कों की बढ़ती सैन्य और नौसैनिक शक्ति के कारण यूरोप के लिए एक बढ़ती हुई धमकी थी।
- पुर्तगालियों को उम्मीद थी कि अफ्रीका में उनकी खोजें उन्हें प्रेस्टेर जॉन के प्रसिद्ध राज्य तक ले जाएँगी।
- यह उन्हें मुसलमानों पर दो मोर्चों से हमले करने में सक्षम बनाएगा।
- इस प्रकार, व्यावसायिक और धार्मिक उद्देश्य एक दूसरे को मजबूत और सही ठहराते थे।
पोप द्वारा दिखाया गया रुचि:
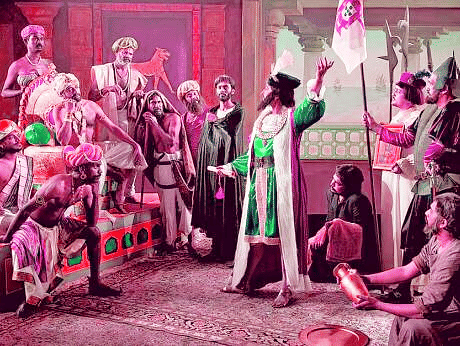
- 1453 में, पोप ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज में बढ़ती रुचि व्यक्त की, जब उन्होंने एक बुल जारी किया जिसने पुर्तगाल को अफ्रीका में केप के पार \"सदा के लिए\" भूमि पर दावा करने का अधिकार दिया। यह स्थानीय \"अधर्मियों\" को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की शर्त पर था।
पुनर्जागरण का प्रभाव:
- 15वीं शताब्दी के यूरोप में फैले पुनर्जागरण ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज में रुचि को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने स्थापित सोच के तरीकों को चुनौती दी और अन्वेषण की भावना को बढ़ावा दिया। पुनर्जागरण काल ने अन्वेषण को प्रोत्साहित किया, और पूर्वी व्यापार में बढ़ती रुचि देखी गई, जिसका प्रमाण 13वीं शताब्दी से भारतीय महासागर में जेनेज़ व्यापारियों की आमद थी। इस दौरान, विनीशियन निकोलो कांटि और बारबोसा, साथ ही रूसी निकितिन जैसे प्रमुख व्यक्तित्वों ने भारतीय महासागर की यात्रा की और भारत पहुंचे।
यूरोप का आर्थिक विकास:
- इस समय कई यूरोपीय क्षेत्रों में तेजी से आर्थिक विकास हो रहा था। इसे खेती योग्य भूमि के विस्तार, बेहतर हल के परिचय, और फसल प्रबंधन की वैज्ञानिक तकनीकों जैसे फसल चक्र द्वारा चिह्नित किया गया। मांस की बढ़ती आपूर्ति ने इस आर्थिक समृद्धि में योगदान दिया। इस आर्थिक समृद्धि ने पूर्वी लक्जरी वस्तुओं की मांग को बढ़ा दिया। जैसे-जैसे आहार की आदतें अधिक मांस खाने की ओर बढ़ी, नमकीन मांस के स्वाद को बढ़ाने के लिए मसालों की आवश्यकता भी बढ़ी। सर्दियों के चारे की कमी के कारण, यूरोप में अधिकांश मवेशियों का वध करना पड़ा। मांस को नमक डालकर संरक्षित किया गया, जिससे पूर्वी मसाले और भी आवश्यक हो गए। पूर्वी मसाले नमकीन मांस को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए महत्वपूर्ण हो गए।
जहाज निर्माण और नौवहन में उन्नतियाँ:
इस अवधि के दौरान, यूरोप ने जहाज निर्माण और नौवहन तकनीकों में महत्वपूर्ण प्रगति की। इस प्रगति ने यूरोप में अव्यक्त समुद्री यात्राओं के लिए व्यापक उत्साह को जन्म दिया, जिसका उद्देश्य पूर्व के अनजाने क्षेत्रों की खोज करना था।
जेनोईज़ की रुचि:
- जेनोईज़ यूरोप में विनीशियनों के मुख्य प्रतिस्पर्धी थे।
- हालाँकि जेनोईज़ पूर्वी वस्तुओं के वितरण में संलग्न थे, लेकिन वे विनीशियनों द्वारा overshadowed हो गए थे।
- वेनिस और जेनोआ, अपने व्यापार में सफलता के बावजूद, शक्तिशाली ओटोमन तुर्कों को चुनौती देने के लिए बहुत छोटे थे।
- 1453 में तुर्कों द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करने का जेनोईज़ पर गंभीर प्रभाव पड़ा।
- काले सागर के बंदरगाह, जो उनके व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थे, धीरे-धीरे अप्राप्य होते गए।
- इस नुकसान ने, साथ ही विनीशियों के साथ चल रही प्रतिद्वंद्विता ने जेनोआ को पुर्तगाल और स्पेन की सहायता करने के लिए प्रेरित किया।
- जेनोआ ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज में जहाज, वित्तीय सहायता, और नौवहन विशेषज्ञता प्रदान की।
- क्रिस्टोफर कोलंबस, एक जेनोईज़ अन्वेषक, ने 1492 में भारत का मार्ग खोजते समय अमेरिका की 'खोज' की।
- इस अवधि के दौरान, पुर्तगाल ईसाई धर्म के इस्लाम के प्रति प्रतिरोध में एक नेता के रूप में उभरा।
- भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी, जिन्हें 'नेविगेटर' कहा जाता है, का एक fixation बन गई।
- उन्होंने पूर्वी भूमध्यसागर पर मुस्लिम नियंत्रण को दरकिनार करने का लक्ष्य रखा।
वास्को दा गामा का भारत में आगमन (1498)

- वास्को दा गामा मई 1498 में तीन जहाजों के साथ भारत के कालीकट में पहुंचे, जिनका मार्गदर्शन एक गुजराती पायलट अब्दुल मजीद ने किया।
- कालीकट के हिंदू शासक, जामोरिन (समुथिरी), ने दा गामा का स्वागत किया, व्यापार के पारस्परिक लाभों में विश्वास करते हुए।
- जामोरिन ने पुर्तगालियों को मसालों के व्यापार की अनुमति दी और तट पर एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी।
- अरब व्यापारियों के विरोध के बावजूद, दा गामा ने जामोरिन से व्यापार अधिकार प्राप्त किए।
- उन्हें सीमा शुल्क और सोने की कीमतों का भुगतान करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।
- पुर्तगालियों का लक्ष्य यूरोप के लिए मसाले के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना था।
- उन्होंने अरब व्यापारिक जहाजों की खोज करने का प्रयास किया, जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई।
- एक हिंसक टकराव के बाद, जहाँ फैक्ट्री में पुर्तगालियों की हत्या कर दी गई थी, पुर्तगालियों ने प्रतिशोध लिया।
- दा गामा ने भारत में तीन महीने बिताए और लाभकारी सामान के साथ पुर्तगाल लौटे।
- लाए गए मसाले पूरे अभियान की लागत का साठ गुना मूल्यवान थे।
- इस सफलता ने अन्य यूरोपीय व्यापारियों को भारत में सीधे व्यापार करने के लिए प्रेरित किया।
- 1502 में, दा गामा एक बड़े बेड़े के साथ लौटे और मुस्लिम व्यापारियों को निष्कासित करने की मांग की।
- जामोरिन ने मना कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप दा गामा ने कालीकट पर एक भयानक हमला किया।
- उन्होंने कोचीन, क्विलोन, और अन्य स्थानों पर किलों की स्थापना की ताकि मलाबार व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके।
- दा गामा के कार्यों ने एशियाई खुले व्यापार की परंपरा से भूमध्यसागरीय दृष्टिकोण की ओर एक बदलाव को चिह्नित किया।
- पुर्तगालियों का लक्ष्य पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना था, विशेषकर अरब प्रतियोगियों के खिलाफ।
- इसके परिणामस्वरूप कालीकट, कन्नूर, और कोचीन को महत्वपूर्ण पुर्तगाली व्यापार केंद्रों के रूप में स्थापित किया गया।
- अपने व्यापारिक गतिविधियों की सुरक्षा के बहाने, पुर्तगालियों ने इन केंद्रों को मजबूत किया।
- इसने भारतीय महासागर में मौजूदा व्यापार गतिशीलता को बदल दिया।
भारत में पुर्तगाली गवर्नर
फ्रांसिस्को डी अल्मेइडा
- 1505 में, पुर्तगाल के राजा ने भारत में तीन साल के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति की, जिसमें दक्षिण-पश्चिम भारतीय तट पर चार किलों की स्थापना की शर्त थी: अंजेदिवा द्वीप, कन्नूर, कोचीन, और क्विलोन।
- उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त सैन्य बल दिया गया था।
- अल्मेइडा का लक्ष्य भारतीय महासागर में पुर्तगालियों को प्रमुख शक्ति बनाना था, जिसके लिए उन्होंने ब्लू वाटर नीति (कार्टेज प्रणाली) को अपनाया।
- उन्होंने माना कि नौसैनिक शक्ति भारत पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है, stating, “जब तक आप समुद्र में शक्तिशाली रहेंगे, आप भारत को अपने पास रखेंगे; और यदि आपके पास यह शक्ति नहीं है, तो तट पर एक किला भी आपके लिए कम मूल्यवान होगा।”
- पुर्तगाली शक्ति के बढ़ते प्रभाव का जवाब देते हुए, मिस्र के सुलतान ने उन्हें चुनौती देने के लिए एक बेड़ा तैयार किया, जिसमें गुजरात के शासक, कालीकट का ज़ामोरिन और बीजापुर और अहमदनगर के शासक शामिल थे।
- प्रारंभिक सफलता के बाद, जहां अल्मेइडा का बेटा मारा गया, संयुक्त बेड़े को 1509 में पुर्तगालियों द्वारा पराजित किया गया।
- यह विजय भारतीय महासागर में पुर्तगाली नौसैनिक श्रेष्ठता को स्थापित करने में सफल रही, जिससे उन्हें फारसी खाड़ी और लाल सागर में अपने संचालन का विस्तार करने की अनुमति मिली।
अल्फोंसो डी अल्बुकर्क
- अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जिन्होंने अल्मेइडा की जगह पुर्तगाली गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला, पूर्व में पुर्तगाली शक्ति के सच्चे संस्थापक माने जाते हैं।
- उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले इस कार्य को पूरा किया।
- अल्बुकर्क ने एक नीति की वकालत की, जिसका उद्देश्य एशिया और अफ्रीका में रणनीतिक स्थानों पर किलों की स्थापना के माध्यम से पूर्वी व्यापार पर नियंत्रण हासिल करना था।
- यह नीति एक मजबूत नौसेना द्वारा समर्थित थी।
- उन्होंने कहा कि केवल नौसेना पर आधारित एक शासन नहीं टिकेगा।
- अल्बुकर्क ने तर्क किया कि बिना किलों के, शासक न तो व्यापार करेंगे और न ही मित्रवत संबंध बनाए रखेंगे।
- अल्बुकर्क के तहत, पुर्तगालियों ने अन्य जहाजों के लिए एक परमिट प्रणाली पेश करके अपने नियंत्रण को मजबूत किया।
- उन्होंने क्षेत्र के प्रमुख जहाज निर्माण केंद्रों पर प्रभाव डाला।
- गुल्फ और लाल सागर क्षेत्रों में जहाज निर्माण के लिए लकड़ी की कमी ने पुर्तगाली उद्देश्यों में मदद की।
- अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुलतान से गोवा को आसानी से प्राप्त कर इस नीति की शुरुआत की।
- यह अधिग्रहण यूरोपीय नियंत्रण में भारतीय क्षेत्र का पहला टुकड़ा था, जो एलेक्ज़ांडर द ग्रेट के बाद का था।
- गोवा, अपने उत्कृष्ट प्राकृतिक बंदरगाह और किले के साथ, मलाबार व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित था।
- गोवा से, पुर्तगालियों ने डेक्कन के शासकों की गतिविधियों पर नज़र रखी।
- उन्होंने मुख्य भूमि पर अपने प्रभाव का विस्तार करते हुए बीजापुरी बंदरगाहों दंडा-राजौरी और दाभोल पर नाकाबंदी और लूटपाट की।
- इस कार्रवाई ने बीजापुर के समुद्री व्यापार को कमजोर कर दिया।
- गोवा के अपने आधार से, पुर्तगालियों ने श्रीलंका के कोलंबो, सुमात्रा के अचिन और मलक्का बंदरगाह पर किलों की स्थापना की।
- इन किलों ने उन्हें मलेशिया प्रायद्वीप और सुमात्रा के बीच के संकीर्ण खाड़ी पर नियंत्रण रखने की अनुमति दी।
- पुर्तगालियों ने लाल सागर के मुहाने पर सोकोटरा द्वीप पर एक स्टेशन भी स्थापित किया।
- उन्होंने अदन पर घेराबंदी की, जिसे वास्को दा गामा ने पकड़ने में असफल रहे थे।
- हालांकि, उन्होंने ओरमूज़ के शासक को मजबूर किया कि वह पुर्तगालियों को वहां एक किला स्थापित करने की अनुमति दे।
- इस अवधि के दौरान, पुर्तगालियों का लक्ष्य दीव और कंबे के किलों पर नियंत्रण प्राप्त करना था, जो गुजराती व्यापार के प्रमुख केंद्र थे।
- उन्होंने 1520-21 में दीव पर कब्जा करने के लिए दो असफल प्रयास किए।
- इन प्रयासों का सामना इसके गवर्नर, अहमद अयाज़ ने किया।
- महत्वपूर्ण रूप से, अल्बुकर्क ने सती प्रथा को समाप्त किया।
- उन्होंने अपने पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि भारत में एक स्थायी पुर्तगाली जनसंख्या सुनिश्चित की जा सके।
निनो दा कुन्हा
निनो दा कुन्हा ने 1528 से 1538 तक भारत में पुर्तगाली क्षेत्रों के गवर्नर के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत में पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। जब गुजरात-तुर्की गठबंधन बन रहा था, तब मुगलों से एक बड़ा खतरा उत्पन्न हुआ। हुमायूँ ने गुजरात पर हमला किया। गुजरात के बहादुर शाह ने 1534 में पुर्तगालियों से सहायता मांगी, उन्हें बास्सीन द्वीप और इसकी निर्भरताएँ और राजस्व प्रदान करके। उन्होंने दिउ में एक आधार की भी पेशकश की। बहादुर शाह का पुर्तगालियों के साथ संबंध 1536 में हुमायूँ के गुजरात से लौटने के बाद बिगड़ गया। मुगलों के गुजरात से निष्कासन के बाद, बहादुर शाह ने ओटोमन सुलतान से मदद मांगी। उन्होंने दियू में पुर्तगाली विस्तार को सीमित करने का प्रयास किया। पुर्तगालियों ने बातचीत की, जिसके दौरान बहादुर शाह 1537 में मारे गए। दियू को पुनः प्राप्त करने के प्रयास असफल रहे।
- पुर्तगालियों ने गुजरात के सुल्तानों से कई क्षेत्रों पर कब्जा किया, जिनमें शामिल हैं:
- (i) दमन (1531 में कब्जा, 1539 में औपचारिक रूप से सौंपा);
- (ii) सलसेट, बॉम्बे, बेस्साइम (1534 में कब्जा);
- (iii) दिउ (1535 में सौंपा)।
- दा कुन्हा ने बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया, जहाँ उन्होंने कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाया, हुगली को उनके मुख्यालय के रूप में रखते हुए।
- इस अवधि के दौरान, ओटोमन तुर्क, सुलतान सुलेमान के तहत, यूरोप पर हमले की तैयारी कर रहे थे।
- तुर्कों ने 1514 में ईरान के शासक को हराया और सीरिया, मिस्र, अरब पर कब्जा कर लिया।
- गुजरात के सुलतान ने ओटोमन शासक को उनके विजय पर बधाई देने के लिए एक दूतावास भेजा।
- ओटोमन शासक ने पुर्तगालियों से लड़ने की इच्छा व्यक्त की।
- दोनों देशों के बीच दूतावासों और पत्रों का निरंतर आदान-प्रदान हुआ।
- 1529 में पुर्तगालियों को लाल सागर से निकालने के बाद, बहादुर शाह की सहायता के लिए सुलेमान राइस के तहत एक मजबूत बेड़ा भेजा गया।
- बहादुर शाह ने इस सहायता का स्वागत किया, दो तुर्की अधिकारियों को सूरत और दिउ के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया।
- इन अधिकारियों में से एक, रूमी खान, बाद में एक प्रसिद्ध तोपची के रूप में प्रसिद्ध हुए।
- 1531 में, पुर्तगालियों ने दमन और दिउ पर हमला किया, लेकिन रूमी खान ने सफलतापूर्वक हमले को पीछे धकेल दिया।
- पुर्तगालियों ने तट पर चौल में एक किला स्थापित किया।
- तुर्कों ने 1536 में भारतीय जल में पुर्तगालियों के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी नौसैनिक प्रदर्शनी दिखाई।
- इस बेड़े में कई नाविकों को अलेक्ज़ैंड्रिया में वेनिसी गैलियों से सेवा में लिया गया था।
- 1538 में, काहिरा के गवर्नर 82 वर्षीय सुलेमान पाशा के नेतृत्व में बेड़ा दियू के समक्ष आया।
- तुर्की एडमिरल का घमंड गुजरात के सुलतान को अपनी सहायता वापस लेने के लिए प्रेरित किया।
- दो महीने की घेराबंदी के बाद, तुर्की बेड़ा एक शक्तिशाली पुर्तगाली आर्मडा के आने की खबर सुनकर पीछे हट गया।
नोट:

- < />तुर्कों से पुर्तगाली लोगों को खतरा अगले बीस वर्षों तक जारी रहा। इस दौरान, पुर्तगालियों ने दमन पर नियंत्रण प्राप्त करके अपनी स्थिति मजबूत की।
- ऑटोमन साम्राज्य का अंतिम हमला अली रायस के नेतृत्व में 1554 में हुआ।
पुर्तगालियों के लिए अनुकूल स्थितियाँ
- भारत में, गुजरात को छोड़कर, जिसे शक्तिशाली महमूद बेगड़हा ने शासित किया था, उत्तरी भाग कई छोटे शक्तियों में बंटा हुआ था।
- दक्कन में, बहमनी साम्राज्य छोटे राज्यों में बंट रहा था।
- इन शक्तियों में से किसी के पास भी एक प्रभावशाली नौसेना नहीं थी, न ही उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति को विकसित करने का विचार किया।
- दूर पूर्व में, चीनी सम्राट का साम्राज्यिक आदेश चीनी जहाजों की नौवहन क्षमता को सीमित करता था।
- जहाँ तक अरब व्यापारियों और जहाज मालिकों की बात है, जो तब तक भारतीय महासागर के व्यापार में प्रमुख थे, उनके पास पुर्तगालियों की संगठन और एकता की तुलना में कुछ नहीं था।
- इसके अलावा, पुर्तगालियों ने अपने जहाजों पर तोपें लगाई थीं।
प्रौद्योगिकी की तुलना:
- प्रौद्योगिकी की दृष्टि से, इंडो-अरब जहाज और चीनी जंक अपनी ताकत, माल ले जाने की क्षमता, और लेटीन पालों के साथ हवा के खिलाफ चलने की क्षमता में पुर्तगाली गैलन और कैरेवेल के बराबर थे।
- हालांकि, पुर्तगालियों की जहाजों की मैन्युवरबिलिटी बेहतर थी, जो इंडो-अरब जहाजों की तुलना में तेज और अधिक कुशल थीं।
- पुर्तगाली जहाजों की हल भी मजबूत थी, जो दुश्मनों की तोप की आग को बेहतर ढंग से सहन कर सकती थी।
पुर्तगालियों की दृढ़ता:
- आखिरकार, पुर्तगाली नाविकों की दृढ़ता और संकल्प ने उनकी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- भारतीय शक्तियाँ, जो समुद्री डाकुओं से लड़ने की अधिक अभ्यस्त थीं, अपनी खुद की शासकों के समर्थन के बिना लंबे समुद्री युद्धों में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थीं।
भारतीय शक्तियों की प्रतिक्रिया:
भारतीय शक्तियों ने पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व को स्वीकार किया क्योंकि यह उनके मुख्यभूमि पर राजनीतिक स्थितियों को खतरे में डालता नहीं था। पुर्तगाली उपस्थिति ने उनके विदेशी व्यापार से होने वाली आय पर भी नकारात्मक प्रभाव नहीं डाला। पुर्तगालियों के साथ नौसैनिक संघर्ष में शामिल होना कठिन प्रतीत होता था, सफलता की संभावना अनिश्चित थी, और यह महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ देने की संभावना नहीं थी।
पुर्तगाली धार्मिक नीति
- पुर्तगाली ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक थे और सभी मुसलमानों को सताने का प्रयास कर रहे थे।
- प्रारंभ में, पुर्तगाली मुसलमानों के प्रति असहिष्णु थे लेकिन हिंदुओं के प्रति अपेक्षाकृत सहिष्णु थे।
- हालांकि, गोवा में इंक्विज़िशन के आगमन के साथ यह स्थिति बदल गई, जिसके परिणामस्वरूप हिंदुओं का भी उत्पीड़न हुआ।
- अपनी असहिष्णुता के बावजूद, जीसुइट लोगों ने अकबर, मुग़ल सम्राट, के दरबार में सकारात्मक प्रभाव डाला, जो धार्मिक चर्चाओं में रुचि रखते थे।
- सितंबर 1579 में, अकबर ने गोवा में अधिकारियों को पत्र लिखा, जिसमें दो विद्वान पुजारियों की उपस्थिति की मांग की।
- गोवा के चर्च के अधिकारियों ने इसे सम्राट और उसके दरबार को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का अवसर देखा और उत्सुकता से निमंत्रण स्वीकार कर लिया।
- जीसुइट पुजारी रोडोल्फो एक्वविवा और एंटोनियो मोंसर्रेट 1580 में फतेहपुर सीकरी पहुंचे लेकिन 1583 में लौट आए, जिससे पुर्तगालियों की अकबर को परिवर्तित करने की आशाएँ निराश हुईं।
- जीसुइट पुजारियों ने जहाँगीर के शासनकाल में भी मुग़ल सम्राटों के साथ संपर्क बनाए रखा।
पुर्तगालियों का मुग़लों के साथ संबंध खराब होना
- 1608 में, कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स I के पत्र के साथ सूरत पहुंचे, जिसमें भारत में व्यापार की अनुमति मांगी गई थी।
- पुर्तगालियों ने हॉकिंस को मुग़ल दरबार तक पहुँचने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे।
- जहाँगीर, मुग़ल सम्राट, ने 1609 में हॉकिंस का स्वागत किया, उनके उपहारों को स्वीकार किया और उन्हें 400 का मंसबदार नियुक्त किया।
- इंग्लैंड को व्यापार अधिकार दिए गए, जिससे पुर्तगालियों में नाराजगी बढ़ी।
- आखिरकार, पुर्तगालियों और मुग़ल सम्राट के बीच एक संधि स्थापित की गई।
- 1612 में, इंग्लिश जहाज ड्रैगन, कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में, एक पुर्तगाली बेड़े को पराजित किया।
- जहाँगीर इंग्लिश जीत से प्रभावित हुए, क्योंकि उनके पास खुद का कोई नौसेना नहीं था।
- 1613 में, पुर्तगालियों ने मुग़ल जहाजों पर हमला करके और मुसलमानों को जेल में डालकर जहाँगीर को नाराज किया।
- शाहजहाँ के शासनकाल में, पुर्तगालियों ने मुग़ल दरबार में अपने लाभ खो दिए।
हुगली का कब्जा:
- 1579 में, पुर्तगालियों ने बंगाल के सटगांव के निकट एक व्यापार पोस्ट स्थापित की, जो बाद में नए बंदरगाह हुगली में व्यापार स्थानांतरित कर दी गई। उन्होंने नमक उत्पादन का एकाधिकार स्थापित किया, अपना खुद का कस्टम हाउस बनाया, और तंबाकू पर कर लागू किए। पुर्तगालियों ने एक क्रूर दास व्यापार में भी संलग्नता दिखाई, हिंदू और मुस्लिम बच्चों को पकड़कर उन्हें ईसाई बनाने के लिए उठाया। उन्होंने मुमताज महल से दो दास लड़कियों को भी जब्त किया। 24 जून, 1632 को, शाह जहान ने हुगली की घेराबंदी का आदेश दिया, जो तीन महीने तक चली। मुगलों को 1,000 हताहत हुए लेकिन 400 कैदियों को पकड़ लिया गया, जिन्हें इस्लाम में रूपांतरित होने या दास बनने का विकल्प दिया गया। ईसाइयों का उत्पीड़न एक समय तक जारी रहा, लेकिन अंततः समाप्त हो गया।
भारतीय व्यापार पर पुर्तगालियों का प्रभाव
- निहत्थे व्यापार का अंत: पुर्तगालियों ने भारतीय जल में निहत्थे खुले समुद्री व्यापार के युग को बाधित किया, पश्चिमी भारतीय महासागर में व्यापार पर मुस्लिम एकाधिकार को चुनौती दी और पूर्वी वस्तुओं का यूरोप में व्यापार किया।
- एकाधिकार की मांग: जब वे कालिकट में पहुंचे, तब से पुर्तगालियों ने व्यापार में पूर्ण एकाधिकार की मांग की, अन्य व्यापारियों, भारतीय और विदेशी, को बाहर करने का प्रयास किया।
- संयुक्त व्यापार: पुर्तगाली जहाजों ने हथियार और गोला-बारूद के साथ अन्य व्यापारियों को धमकी दी, उनके माल और जहाजों को जब्त किया, जो सशस्त्र व्यापार की शुरुआत का संकेत था।
- कार्टाज़ प्रणाली का परिचय: 1502 में, पुर्तगालियों ने कार्टाज़ प्रणाली का परिचय दिया, जो कालिकट में विशेष व्यापार अधिकार की मांग करती थी। जब ज़ामोरिन ने अस्वीकार कर दिया, तो वास्को दा गामा ने अरब सागर और भारतीय महासागर में सभी जहाजों पर युद्ध की घोषणा की।
- कार्टाज़ की व्याख्या: कार्टाज़ एक समुद्री पास या व्यापार लाइसेंस था जो पुर्तगालियों द्वारा जारी किया गया था, जिससे जहाजों को हमले का भय के बिना व्यापार करने की अनुमति मिलती थी। यह पहली बार 1502 में जारी किया गया।
- शाही एकाधिकार: पुर्तगालियों ने मसालों, औषधियों, रंगों (जिसमें नीला भी शामिल है), तांबा, चांदी, सोना, हथियार, गोला-बारूद और युद्ध घोड़ों पर शाही एकाधिकार की घोषणा की।
- व्यापार प्रतिबंध: किसी भी देश के व्यापारियों, जिसमें पुर्तगाली निजी व्यापारी और शाही अधिकारी शामिल थे, को बिना अनुमति के इन वस्तुओं में व्यापार करने से प्रतिबंधित किया गया।
- नियंत्रण और प्रवर्तन: कार्टाज़ का उद्देश्य भारतीय महासागर में पुर्तगाली व्यापार एकाधिकार को नियंत्रित और प्रवर्तन करना था, यह सुनिश्चित करना कि व्यापारी पुर्तगाली व्यापार पोस्ट पर कर चुकाएं।
- छानबीन और जब्ती: पुर्तगालियों ने उन जहाजों की छानबीन की, जो बिना कार्टाज़ के या प्रतिबंधित वस्तुओं में व्यापार करने के संदेह में थीं। संदिग्ध जहाजों को डुबोया या जब्त किया जा सकता था, और चालक दल को दास बना लिया जा सकता था।
- पास खरीदना: अकबर, अहमदनगर के नीलम शाह, बीजापुर के आदिल शाह, कोचिन के राजाओं, कालिकट के ज़ामोरिन, कैननोर के शासकों जैसे शासकों ने पुर्तगालियों से अपने जहाजों को विभिन्न स्थानों पर भेजने के लिए पास खरीदे।
एकाधिकार व्यापार
- जब पुर्तगाली भारत में पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि विभिन्न हिस्सों के व्यापारी तटीय क्षेत्रों में व्यापार कर रहे थे। वास्को दा गामा ने 1498 में रिपोर्ट किया कि मेका, टेनासेरी, पेगू, सीलोन, तुर्की, मिस्र, फारस, इथियोपिया, ट्यूनीशिया, और भारत के विभिन्न हिस्सों के व्यापारी कालीकट के बंदरगाह पर व्यापार कर रहे थे। चीनी व्यापारी और लाल समुद्र क्षेत्रों के व्यापारी भी भारतीय बंदरगाहों पर आते थे, लेकिन किसी समूह ने विशिष्ट व्यापार अधिकारों की मांग नहीं की या विशेष व्यापारियों के लिए वस्तुओं को अलग नहीं किया। हालाँकि, पुर्तगालियों के आगमन के साथ स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया। पुर्तगालियों ने भारतीय राजाओं पर दबाव डाला कि वे अन्य व्यापारियों को अपने बंदरगाहों पर व्यापार करने से रोकें और कुछ वस्तुओं को अन्य व्यापारियों के लिए प्रतिबंधित घोषित किया। उन्होंने भारतीय शासकों के साथ संधियों के माध्यम से व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। रणनीतिक स्थानों पर पुर्तगाली किलों की स्थापना, उनके जहाजों द्वारा गश्त और अन्य जहाजों के लिए पास की आवश्यकता सभी प्रयास थे जो उन्होंने एशियाई जलों में अपने एकाधिकार को लागू करने के लिए किए।
भारतीय शासकों और व्यापारियों का व्यापार:
- पुर्तगालियों के एक पूर्ण एकाधिकार स्थापित करने के प्रयासों ने भारतीय शासकों और व्यापारियों द्वारा किए गए व्यापार को पूरी तरह से खत्म नहीं किया। कन्नूर के राजा ने अपने जहाजों को कम्बे और होर्मुज में वस्तुओं के साथ भेजने के लिए पुर्तगालियों से पास प्राप्त किया। उसने इन स्थानों से घोड़े आयात किए, हालाँकि इसे पुर्तगालियों द्वारा एकाधिकार वस्तु के रूप में पहचाना गया था। कभी-कभी, ऐसे जहाजों को पुर्तगालियों द्वारा जब्त किए जाने का जोखिम होता था। तटीय मालाबार में तानूर, चाल्ले और कालीकट के राजाओं को समान परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। गुजरात के nobles ने पुर्तगाली एकाधिकार के बावजूद व्यापार करना जारी रखा। मलिक गोपी, मलिक अयाज़, ख्वाजा सोफर और अन्य व्यापार में रुचि रखने वाले अपने जहाजों को पुर्तगालियों के पास के साथ या बिना चलाते थे।
एकाधिकार बहुत प्रभावी नहीं था:
स्थानीय और विदेशी व्यापारी जो भारत में बसे थे, वे कार्ताज के साथ या बिना व्यापार करते थे। पुर्तगाली व्यापारियों को जल्द ही पता चला कि वे भूमि पर अधिक नुकसान उठाते हैं बनिस्बत समुद्र पर लाभ उठाने के, क्योंकि समुद्र में नुकसान उठाने वाले व्यापारी अपने सरकारों पर दबाव डालते थे कि वे पुर्तगाली व्यापार के खिलाफ प्रतिशोध करें। एशिया के विशाल तटों पर व्यापार की निगरानी करना संभव नहीं था। समुद्री डाकू जो पुर्तगाली जहाजों पर हमला करते थे, वे ओमान, मलाबार, दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में सक्रिय थे। पुर्तगाली नीतियों ने व्यापारियों और छोटे शासकों से उन्हें अधिक प्रोत्साहन और समर्थन प्राप्त करने में मदद की।
काली मिर्च का व्यापार:
- काली मिर्च का वार्षिक उत्पादन कैलिकट और केप कॉमोरिन के बीच 60,000 क्विंटल होता था।
- केवल 15,000 क्विंटल पुर्तगाली कारखानों को वितरित किया जाता था।
- बाकी तीन-चौथाई अन्य बंदरगाहों पर ले जाया जाता था।
- इस प्रथा को पुर्तगालियों द्वारा अवैध माना गया।
- पुर्तगाली 1503 में सहमति की गई काली मिर्च की कीमत को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे।
- उत्पादकों के पास व्यापारियों को काली मिर्च देने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था।
- व्यापारी पुर्तगाली की जानकारी के बिना काली मिर्च को अन्य व्यापार केंद्रों पर भेजते थे।
अरबों और गुजराती व्यापारियों द्वारा व्यापार:
- अरब और गुजराती व्यापारी पुर्तगाली व्यापार प्रतिबंध और नियमों को दरकिनार करने के तरीके खोजते थे।
- यहां तक कि पुर्तगाली निजी व्यापारी भी शाही एकाधिकार और कार्ताज के कारण असंतुष्ट थे।
- शाही अधिकारियों को छोटी वेतन मिलने के कारण अक्सर निजी व्यापारियों (पुर्तगाली, अरब, गुजराती आदि) द्वारा रिश्वत दी जाती थी।
- कई पुर्तगाली अधिकारी अपनी सरकार की जानकारी के बिना विभिन्न वस्तुओं में निजी व्यापार करते थे।
पुर्तगाली नियंत्रण की चुनौतियाँ:
भारतीय महासागर पर पुर्तगाली नियंत्रण अधूरा रहा क्योंकि वे अदन पर कब्जा करने में असफल रहे। अदन पर कब्जा करने में विफलता ने उनके लिए लाल समुद्र में प्रवेश को नियंत्रित करना कठिन बना दिया। तुर्की का सीरिया, मिस्र और अरब पर विजय प्राप्त करना पुर्तगाली प्रयासों को जटिल बनाता है। पूर्वी भूमध्य सागर और लाल समुद्र में तुर्की की नौसैनिक शक्ति का विस्तार पुर्तगाली नाकेबंदी पर प्रभाव डालता है। लाल समुद्र क्षेत्र में पुर्तगाली एकाधिकार कभी प्रभावी नहीं रहा। भारतीय महासागर के दूसरे छोर पर, मसाले के द्वीपों पर पुर्तगाली नियंत्रण कमजोर हुआ।
नौसेना संघर्ष:
- पुर्तगालियों को एक नौसैनिक शक्ति का सामना करना पड़ा, जो उनके युद्धपोतों से टकराने के लिए तैयार थी।
- पारंपरिक जावा की नौसैनिक क्षमताओं का उपयोग करते हुए, सुमात्रा के शासक, सुलतान अली मुगायत शाह ने कई नौसैनिक मुठभेड़ों में पुर्तगालियों को हराया और अच्हे को मजबूत करने के लिए पुर्तगालियों से बड़ी संख्या में तोपें कब्जा कीं।
- उन्होंने ओटोमन सुलतान से सैन्य उपकरणों के लिए भी संपर्क किया। ओटोमन ने अच्हे को एक घेराबंदी का सामना करने में सक्षम करने के लिए एक विशेष कैलिबर की कांस्य तोपें प्रदान कीं।
अच्हे का उदय:
- इससे अच्हे मसालों के निर्यात का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जो पुर्तगाली नियंत्रण में मलक्का के साथ प्रतिस्पर्धा करता था।
- अरब और गुजराती, जो मलक्का में अच्छी तरह से स्थापित थे, ने अच्हे को लाल समुद्र में लक्कादिव्स के माध्यम से मसालों के निर्यात के लिए एक केंद्र के रूप में उपयोग किया, इस प्रकार पुर्तगाली नियंत्रित मलाबार जल क्षेत्र को बायपास किया।
पुर्तगाली सफलता को सीमित करने वाले कारक:
- पुर्तगाली सफलता को सीमित करने वाले महत्वपूर्ण कारक थे:
- एशियाई व्यापार नेटवर्क की संरचना
- एशियाई व्यापारियों, अरबों, गुजराती, तमिलों और अन्य की शक्ति और संसाधनशीलता, जिनके पास इस प्रणाली का संचालन करने का लंबा अनुभव था
- तुर्की और उत्तर सुमात्रा के शासक की नौसेना और सैन्य शक्ति
- पुर्तगाली और पुर्तगाली साम्राज्य (Estado da India) में कार्ताज प्रणाली के कार्यों की आंतरिक सीमाएं
- कार्ताज प्रणाली का उपयोग करके महासागरीय व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने में बहुत सफलता नहीं मिली और स्थानीय व्यापारियों को कार्ताज देने के नियमों को उदार बनाना पड़ा। इसमें मुस्लिम व्यापारियों को भी शामिल किया गया।
- घोड़ों का व्यापार, जो विशेष रूप से मुस्लिमों के हाथ में था, एक अत्यधिक लाभकारी व्यापार था।
- मुस्लिम कई अन्य वस्तुओं, जैसे कपड़ा उत्पाद, कांच, सुगंधित वस्तुएं और कॉफी के व्यापार में भी सक्रिय थे, जिसमें पुर्तगालियों के पास न तो पैसा था और न ही जहाज।
- इसलिए, व्यापार और लाभ की आवश्यकताएँ जल्द ही धार्मिक पूर्वाग्रहों पर हावी हो गईं।
पुर्तगाली प्रयास और व्यापार:
पुर्तगाली प्रयास ने मुस्लिम व्यापारियों को पूर्वी वस्तुओं के व्यापार से बाहर करने की कोशिश की। पश्चिम एशिया में व्यापार पर पुर्तगाली एकाधिकार की स्थापना केवल सीमित सफलता प्राप्त कर सकी। सोलहवीं सदी के मध्य तक, बड़ी मात्रा में मसाले लिस्बन लाए गए। यूरोप में मसालों का विपणन मुख्य रूप से एंटवर्प, काला सागर के बंदरगाहों, लेवेंट और मिस्र के बाजारों के माध्यम से किया गया। पुर्तगालियों ने महासागरीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कार्टाज़ प्रणाली का उपयोग किया। नियंत्रण तब तक पूर्ण नहीं हुआ जब तक 17वीं सदी में अन्य यूरोपीय शक्तियाँ जैसे डच और अंग्रेज़ नहीं आए।
पुर्तगाल की व्यापारिक सीमाएँ
- पुर्तगाल एक छोटा देश था, जिसकी वित्तीय संसाधन सीमित थे, इसके बावजूद इसकी व्यापार में तेजी से विकास हुआ।
- जर्मन और इतालवी व्यापारी पूर्वी वस्तुओं के मुख्य वितरक बन गए, क्योंकि पुर्तगाल के पास ऐसा करने के लिए साधन नहीं थे।
- पूर्वी उत्पादों के लिए यूरोपीय वस्तुओं की सीमित मांग ने कीमती धातुओं, विशेष रूप से चाँदी के निर्यात की आवश्यकता को जन्म दिया।
- स्पेन के विपरीत, पुर्तगाल के पास अमेरिका में चाँदी की खदानें नहीं थीं और यह इटालियन और जर्मन वित्तीय समर्थकों पर निर्भर था।
- पुर्तगाली राजा की यह अपेक्षा कि भारत के तटीय व्यापार पर नियंत्रण पूर्वी वस्तुओं के यूरोप में निर्यात को वित्तपोषित करेगा, गलत थी।
- प्रारंभ में, लिस्बन से भारत की ओर पुर्तगाली व्यापार 12-13 जहाजों तक सीमित था।
- 16वीं सदी के अंत तक, निजी पुर्तगाली व्यापारियों ने यूरोप के साथ व्यापार में अपनी हिस्सेदारी 90 प्रतिशत से अधिक बढ़ा दी, जो वस्त्र और कीमती पत्थरों पर केंद्रित थी।
- निजी व्यापारियों ने एशियाई व्यापार में व्यापक भागीदारी के माध्यम से इस व्यापार को वित्तपोषित किया।
- पुर्तगाली सरकार ने पश्चिमी भारतीय महासागर में अपने उद्यम को पुनर्वितरणात्मक उद्यम के रूप में देखा, जो दूसरों के व्यापार पर कर लगाकर आय अर्जित करता था, न कि व्यापार का विस्तार करता था।
- यूरोप और पूर्व के बीच व्यापार का सच्चा विस्तार 17वीं सदी में डच और अंग्रेज़ों के आगमन के बाद ही हुआ।
पुर्तगाली का महत्व
राजनैतिक प्रणाली में योगदान:
- पुर्तगालियों का एशिया में राजनैतिक प्रणाली पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनकी संख्या कम थी।
- भारत या अन्य स्थानों पर बड़े क्षेत्रों को पकड़ना और बनाए रखना उनके लिए कठिन था।
- उन्होंने बुद्धिमानी से अपने नियंत्रण को सुरक्षित द्वीपों और तटीय किलों तक सीमित कर दिया, जिन्हें समुद्र के द्वारा आपूर्ति की जा सकती थी।
- इसका प्रमुख उदाहरण गोवा द्वीप है, जो उनकी सरकार का मुख्यालय बना।
- धमक और persuasion के माध्यम से, पुर्तगालियों ने छोटे राज्यों जैसे कि कालीकट, कोचिन, और क्रागानोर के शासकों को मसाले व्यापार में उनके एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया।
- गोवा में पुर्तगाली व्यवस्था का पर्यवेक्षण एक गवर्नर-जनरल द्वारा किया जाता था, जिसे एक काउंसिल सहायता करती थी, जिसमें धार्मिक प्रमुख भी शामिल होता था।
- उनकी संख्या कम होने के कारण, पुर्तगालियों ने मिश्रित विवाह को बढ़ावा दिया, जिससे एक नई इंडो-पुर्तगाली या गोअन समाज का उदय हुआ।
- यह समाज और सरकार कठोर जातीय रेखाओं के अनुसार व्यवस्थित थी, जिसमें शुद्ध पुर्तगाली उत्पत्ति के लोग शीर्ष पर थे।
- मिश्रित उत्पत्ति के लोग नीचे थे और राजनीतिक शक्ति से बाहर थे।
- गिरजाघर कभी-कभी क्रूर "auto da fe" या जलाने की सजा का सहारा लेता था, ताकि ईसाइयों में हरिसी को समाप्त किया जा सके।
- कुल मिलाकर, पुर्तगालियों का राजनीति और वैश्विक व्यापार के विस्तार में योगदान नगण्य था।
भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग का महत्व:
- पुर्तगालियों द्वारा भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग का उद्घाटन भारत को विस्तृत विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता से एकीकृत करने में सहायक था।
- इसने भारत में एक बाजार अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया।
- यह विकास भारत की पूर्ववर्ती आत्म-नियंत्रण की अवधि से एक परिवर्तन का भी प्रतीक था।
- इतिहासकारों का कहना है कि पुर्तगालियों का आगमन न केवल भारत में यूरोपीय युग की शुरुआत की, बल्कि समुद्री शक्ति के उदय का भी संकेत दिया।
- हालांकि चोलों ने अतीत में एक समुद्री शक्ति के रूप में कार्य किया था, पुर्तगाली पहले विदेशी शक्ति थे जो समुद्र द्वारा भारत आए।
- नए व्यापारिक संबंध: पुर्तगालियों ने भारत के जापान, फिलीपींस, और लैटिन अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए।
- उन्होंने अन्य यूरोपीय शक्तियों जैसे कि स्पेन, डच, अंग्रेज़, और फ्रेंच के आगमन के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया।
- गोवा और आस-पास के क्षेत्रों में, पुर्तगालियों ने अपना सिक्का "Cruzado" पेश किया, जिसे विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों में भी स्वीकार किया गया।
प्रौद्योगिकी का परिचय:
पुर्तगाली उन्नत समुद्री तकनीकों में विशेषज्ञ थे।
- कोचीन में उनके मार्गदर्शन में पश्चिमी तरीकों का उपयोग करके जहाज निर्माण की शुरुआत हुई।
- उनके बहु-डेक वाले जहाज मजबूत बनाए गए थे, जिससे वे भारी हथियार ले जा सकते थे।
- सोलहवीं सदी के मलाबार में, पुर्तगालियों ने शरीर कवच, मैचलॉक सैनिकों, और अपने जहाजों से लाए गए तोपों के उपयोग के साथ सैन्य नवाचार प्रदर्शित किए।
- उन्होंने मुगल तोपों और स्टिरप की तोपखाने के उपयोग को प्रभावित किया हो सकता है।
- प्रिंटिंग और घड़ियों जैसी तकनीकों को गोवा में पेश किया गया, लेकिन ये मुख्य भूमि पर स्वीकार नहीं की गईं।
- पुर्तगालियों को नई सड़कें और सिंचाई कार्य बनाने के लिए भी जाना जाता है।
कृषि में योगदान:
- पुर्तगालियों ने भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कई उत्पाद पेश किए, जैसे मक्का, आलू, अनानास, तम्बाकू, मिर्च।
- इनमें से, तम्बाकू एक प्रमुख व्यापार वस्तु बन गया।
- अन्य पौधे जिन्हें पुर्तगालियों ने पेश किया, उनमें पपीता (पहली बार मैक्सिको में उगाया गया), काजू (ब्राज़िल का मूल), अमरुद (केंद्र और दक्षिण अमेरिका का मूल) शामिल हैं।
- आम और सिट्रस फलों की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ, बेहतर नारियल के पौधों की किस्में पेश की गईं, साथ ही बड़े बागों की स्थापना भी हुई।
- भारतीय किसान नए उत्पादों के प्रति receptive थे यदि वे लाभ का वादा करते थे।
संस्कृति में योगदान:
- भारत में मिशनरियों और चर्च न केवल शिक्षक थे, बल्कि कला के संरक्षक भी थे, जैसे कि चित्रकला, नक्काशी, शिल्प।
- संगीत में, उन्होंने भारत में यूरोपीय कला की व्याख्या और परिचय में एक भूमिका निभाई, न कि केवल पुर्तगाली कला में।
पुर्तगाली का पतन
18वीं सदी तक, भारत में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक प्रभाव खो दिया, हालांकि कुछ ने व्यक्तिगत रूप से व्यापार जारी रखा, जबकि अन्य समुद्री डकैती और लूटपाट की ओर मुड़ गए। हुगली का उपयोग कुछ पुर्तगालियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए एक अड्डे के रूप में किया गया। पुर्तगालियों के पतन के कई कारण थे:
- शक्तिशाली राजवंशों का उदय: भारत में पुर्तगालियों के पास जो स्थानीय लाभ थे, वे मिस्र, फारस, उत्तरी भारत में मजबूत राजवंशों के उदय के साथ घट गए, साथ ही उग्र मराठे उनके पड़ोसी बन गए। मराठों ने 1739 में पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन पर कब्जा कर लिया।
- धार्मिक नीतियाँ: पुर्तगालियों की धार्मिक नीतियों, विशेषकर जीसुइट्स की गतिविधियों ने राजनीतिक भय उत्पन्न किया। उनके मुसलमानों के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख और हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की नीति ने हिंदुओं में भी नाराजगी पैदा की।
- बेईमान व्यापार प्रथाएँ: पुर्तगालियों को उनकी बेईमान व्यापार प्रथाओं के लिए बदनामी मिली और उन्हें समुद्री डाकू के रूप में देखा जाने लगा।
- अहंकार और हिंसा: उनके अहंकार और हिंसक व्यवहार ने छोटे राज्य के शासकों और सम्राट मुगलों के प्रति उनकी दुश्मनी उत्पन्न की।
- ब्राज़ील की खोज: ब्राज़ील की खोज ने पुर्तगाली उपनिवेशी गतिविधियों को पश्चिम की ओर मोड़ दिया।
- स्पेन और पुर्तगाल का संघ: 1580-81 में स्पेन और पुर्तगाल का संघ ने पुर्तगाल को इंग्लैंड और डच के साथ स्पेन के युद्धों में शामिल होने के लिए मजबूर किया, जिससे भारत में पुर्तगाली व्यापार एकाधिकार पर गंभीर प्रभाव पड़ा।
- नौसेना मार्ग का रहस्य: भारत के लिए समुद्री मार्ग पर पुर्तगालियों का एकाधिकार हमेशा के लिए गुप्त नहीं रह सकता था; जल्द ही डच और अंग्रेजों ने नौवहन कौशल सीखा और मार्ग की खोज की।
- नई यूरोपीय व्यापारिक समुदायों का आगमन: भारत में नए यूरोपीय व्यापारिक समुदायों का आगमन हुआ, जिसने तीव्र प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। पुर्तगालियों को अधिक शक्तिशाली और उद्यमी प्रतिस्पर्धियों के सामने झुकना पड़ा।
- डच और अंग्रेजों के संसाधन: डच और अंग्रेजों के पास अधिक संसाधन और विदेशों में विस्तार के लिए मजबूत प्रेरणाएँ थीं, जिन्होंने अंततः पुर्तगाली प्रतिरोध को पार कर लिया।
- गोवा की स्थिति: गोवा, जो पुर्तगालियों के पास रहा, विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद एक बंदरगाह के रूप में महत्व खो बैठा, जिससे इसका अधिग्रहण बेमतलब हो गया।
|
28 videos|739 docs|84 tests
|





















