भारतीय दर्शन के छह विद्यालय | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download
जीवन के चार लक्ष्य
प्राचीन विचारकों का मानना था कि जब समाज विभिन्न वर्गों (वर्ण) में व्यवस्थित हो जाता है और एक मजबूत सरकार स्थापित होती है, तो व्यक्तियों को जीवन में चार मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए:
- धर्म: सामाजिक व्यवस्था और righteousness का पालन करना।
- अर्थ: आर्थिक संसाधनों और धन का अधिग्रहण करना।
- काम: शारीरिक सुख और इच्छाओं का पालन करना।
- मोक्ष: आध्यात्मिक मुक्ति या उद्धार प्राप्त करना।
इन लक्ष्यों का विस्तार विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में किया गया है:
- अर्थशास्त्र: कौटिल्य द्वारा लिखा गया, यह ग्रंथ आर्थिक मामलों और शासन पर केंद्रित है।
- धर्मशास्त्र: यह राज्य और समाज को नियंत्रित करने वाले कानूनों और नियमों से संबंधित है।
- कामसूत्र: यह ग्रंथ शारीरिक सुख और प्रेम के पहलुओं पर चर्चा करता है।
मोक्ष और प्राचीन दर्शन
जबकि पहले तीन शाखाएँ मुख्य रूप से जीवन के भौतिक पहलुओं पर केंद्रित थीं, वे कभी-कभी मोक्ष के विषय पर भी चर्चा करती थीं। मोक्ष का सिद्धांत, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति को संदर्भित करता है, दार्शनिक ग्रंथों में एक केंद्रीय विषय बन गया।
हालांकि इसे प्रारंभ में गौतम बुद्ध द्वारा समर्थित किया गया था, इस विचार को बाद में विभिन्न ब्राह्मणिक दार्शनिकों द्वारा और अधिक महत्व दिया गया।
दार्शनिकों के छह स्कूल
यीशु के युग की शुरुआत तक, छह दार्शनिक स्कूल उभरे:
- सांख्य:
- योग:
- न्याय:
- वैशेषिक:
- मीमांसा (या पूर्व मीमांसा):
- वेदांत (या उत्तर मीमांसा):
ये छह स्कूल, जिन्हें आस्तिक स्कूल के रूप में जाना जाता है, मूल रूप से सनातन धर्म का हिस्सा थे। ये दार्शनिकता और धर्मशास्त्र के प्रणालियों का समावेश करते हैं, प्रत्येक एक सेट के चारों ओर केंद्रित होता है जो उस स्कूल की प्रमुख शिक्षाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करता है।
वेदों की प्राधिकारिता और ऋषि
पहले चार स्कूलों ने वेदों के प्राधिकार को स्वीकार किया लेकिन अपने सिद्धांतों को व्यक्तिगत ऋषियों या साधुओं की शिक्षाओं से निकाला, न कि सीधे वेदों से। अंतिम दो स्कूल, पूर्व मीमांसा और वेदांत, अपने प्रणालियों को विशेष रूप से वेदों के कथनों पर आधारित करते हैं।
वेदों की संरचना: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चार भागों में विभाजित हैं:
- संहिताः मंत्रों का संग्रह।
- ब्राह्मण: अनुष्ठानों के लिए निर्देश।
- आरण्यक: अनुष्ठान से theological चर्चाओं में संक्रमण।
- उपनिषद: दार्शनिक शिक्षाएँ और चर्चाएँ।
उपनिषद, जो वेदों के अंतिम भाग में पाए जाते हैं, वेदों के विचार का समापन करते हैं और वेदांत (या उत्तर मीमांसा) का केंद्र होते हैं।
पूर्व मीमांसा:
पूर्व मीमांसा, जिसका अर्थ है "पहली चर्चा," वेदों के पूर्व भागों, विशेष रूप से संहिताओं और ब्राह्मणों पर आधारित है। यह इन ग्रंथों में पाए जाने वाले अनुष्ठानों और निर्देशों पर जोर देती है।
सांख्य
शब्द "सांख्य," जिसका अर्थ है "गिनती," पहले उत्पन्न होने का प्रतीत होता है। यह प्रणाली उसके संस्थापक, कपिल मुनि को संदर्भित करती है।
प्रारंभिक सांख्य दर्शन में, विश्व की रचना के लिए दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय, इसने यह जोर दिया कि विश्व की रचना और विकास प्राकृतिक तत्व (प्रकृति) द्वारा अधिक प्रभावित होते हैं न कि भगवान द्वारा। यह दृष्टिकोण तर्कसंगत और वैज्ञानिक माना गया।
हालांकि, चौथी सदी ईस्वी के आस-पास, "पुरुष" या आत्मा का सिद्धांत सांख्य प्रणाली में प्रकृति के साथ एकीकृत किया गया। इस जोड़ ने यह विश्वास उत्पन्न किया कि दोनों प्रकृति और आध्यात्मिक तत्व विश्व की रचना के लिए जिम्मेदार थे। प्रारंभ में, सांख्य भौतिकवादी था, लेकिन समय के साथ यह आध्यात्मिक तत्वों को शामिल करने के लिए विकसित हुआ।
सांख्य दो मौलिक सिद्धांतों को मानता है:
- प्रकृति: प्राथमिक पदार्थ, जो पदार्थ, रचनात्मक शक्ति, और ऊर्जा को शामिल करता है।
- पुरुष: जिसे आत्मा भी कहा जाता है, यह शाश्वत, अपरिवर्तनीय, और स्वाभाविक रूप से चेतन है।
प्रकृति जड़ है और जब यह पुरुष के साथ जुड़ती है तो परिवर्तन करती है। यह सूक्ष्म से स्थूल की ओर विकसित होती है और दृश्य संसार को प्रकट करती है। जीव (एक जीवित प्राणी) की स्थिति तब होती है जब पुरुष किसी रूप में प्रकृति के साथ बंधा होता है।
यह सिद्धांत ब्रह्मा-प्रकृति तत्वों द्वारा निर्मित ब्रह्मांड का वर्णन करता है, जो विभिन्न तत्वों, इंद्रियों, भावनाओं, गतिविधियों, और मन को जोड़ता है। यह एक द्वैतवादी दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है, जो आत्म और पदार्थ के बीच संबंध पर केंद्रित है, जबकि पश्चिमी द्वैतवादी परंपरा मन-शरीर के भेद पर जोर देती है।
सांख्य के अनुसार, व्यक्ति सच्चे ज्ञान के अधिग्रहण के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जो उनके दुख को स्थायी रूप से समाप्त कर सकता है। एक जीवित प्राणी अपने आप को अज्ञानता से मुक्त कर सकता है, जब वह पुरुष और प्रकृति के बीच भेद (पच्चीस तत्व जो पदार्थ का निर्माण करते हैं) को समझता है। यह ज्ञान अनुभव (प्रत्यक्ष), अनुमान (अनुमान), और श्रवण (शब्द) के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जो inquiry के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
सांख्य दार्शनिकों द्वारा ईश्वर या सर्वोच्च प्राणी के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया है या इसे प्रासंगिक नहीं माना गया है।
योग
योग प्रणाली, जो हिरण्यगर्भ द्वारा स्थापित की गई और बाद में sage पतंजलि द्वारा व्यवस्थित और प्रचारित की गई, पुरुष और प्रकृति के बीच भेद को समझने के लिए व्यावहारिक कदम प्रदान करती है।
योग विद्यालय के अनुसार, ध्यान और शारीरिक अभ्यासों के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए, विभिन्न आसनों में शारीरिक व्यायामों की सिफारिश की जाती है, साथ ही एक श्वसन अभ्यास जिसे प्राणायाम कहा जाता है। इन विधियों का विश्वास है कि ये मन को सांसारिक चिंताओं से हटा देती हैं और एकाग्रता को बढ़ाती हैं।
ये अभ्यास न केवल शरीरक्रिया और शारीरिक रचना की प्राचीन समझ को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि सांसारिक चुनौतियों से बचने की प्रवृत्ति है। इस प्रणाली का केंद्रीय तत्व सुख, इंद्रियों, और शारीरिक अंगों पर नियंत्रण का अभ्यास है।
योग ने सांख्य स्कूल के पच्चीस सिद्धांतों को स्वीकार किया है, जबकि ईश्वर या भगवान को छब्बीसवें सिद्धांत के रूप में शामिल किया है, जिससे यह अधिक धार्मिक हो गया है। पतंजलि ने योग को सभी मानसिक परिवर्तनों का cessation के रूप में परिभाषित किया है, और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, उन्होंने आठ चरणों का वर्णन किया है, जो आठ अंगों (अष्टांग) योग की ओर ले जाते हैं, जो बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य का अनुसरण करते हैं।
आठ चरण हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और समाधि। अंतिम लक्ष्य मन को शांति प्रदान करना और कैवल्य प्राप्त करना है, जिसका अर्थ है एकाकीपन या निर्लिप्तता।
न्याय
न्याय विद्यालय, जिसे विश्लेषण के स्कूल के रूप में भी जाना जाता है, के संस्थापक गौतम मुनि हैं, जिन्होंने इसे 2वीं सदी ईस्वी में लिखा। इसकी विधि एक तर्क प्रणाली में निहित है जिसे विभिन्न भारतीय विद्यालयों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया है।
न्याय का मानना है कि ज्ञान के अधिग्रहण के माध्यम से मोक्ष और दुख से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। किसी प्रस्ताव या कथन की वैधता को अनुभव, अनुमान, तुलना, और गवाही के माध्यम से आंका जा सकता है। उदाहरण के लिए, उन्होंने तर्क को इस प्रकार उपयोग किया:
- पहाड़ में आग है क्योंकि यह धुआँ उगल रहा है; जो कुछ भी धुआँ उगलता है उसमें आग होती है, जैसे कि चूल्हा।
न्याय के अनुसार, मानव दुख उन गलतियों या दोषों से उत्पन्न होता है जो गलत ज्ञान, धारणाओं, और अज्ञानता के आधार पर कार्यों के परिणामस्वरूप होते हैं। तर्कसंगत विचार पर जोर ने भारतीय विद्वानों को प्रेरित किया, प्रणालीबद्ध सोच और तर्क को प्रोत्साहित किया।
हालांकि न्याय कुछ विधियों और मानव दुख के आधार पर बौद्ध धर्म के साथ कुछ समानताएँ रखता है, एक महत्वपूर्ण भिन्नता यह है कि बौद्ध धर्म आत्मा या आत्मा के अस्तित्व का इनकार करता है। इसके विपरीत, न्याय विद्यालय, अन्य हिंदू परंपराओं की तरह, आत्मा और आत्म का विश्वास रखता है, जिसमें मोक्ष (मोक्ष) अज्ञानता के हटाने की स्थिति है।
वैशेषिक
वैशेषिक विद्यालय, जिसे काणाद ने 6वीं सदी ईस्वी में स्थापित किया, अपनी परमाण्विक और बहुवादी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। यह स्कूल भौतिक तत्वों या dravya पर चर्चा पर जोर देता है और विशेषताओं और उनके संघों के बीच भेद करता है। वैशेषिक के अनुसार, पांच महान तत्वों—भूमि, जल, अग्नि, वायु, और आकाश (आकाश)—का संयोजन नए वस्तुओं का निर्माण करता है।
वैशेषिक विद्यालय का एक महत्वपूर्ण योगदान परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन है, जो यह कहता है कि सभी भौतिक वस्तुएँ परमाणुओं से बनी होती हैं। काणाद ने प्रस्तावित किया कि विश्व परमाणुओं (परमानु) से बना है और भौतिक ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं को सीमित संख्या में परमाणुओं में घटित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सुझाव दिया कि ब्रह्मण उन परमाणुओं में चेतना उत्पन्न करने वाली मूलभूत शक्ति है।
काणाद ने सात padarthas या अस्तित्वात्मक संस्थाओं की पहचान की, यह कहते हुए कि इनकी समझ आत्म-प्राप्ति की ओर ले जाती है। सात padarthas हैं:
- dravya: पदार्थ
- guna: गुण
- karma: क्रिया
- samanya: सामान्यता
- vishesha: विशिष्टता
- samavaya: अंतर्संबंध
- abhava: अनुपस्थिति
वैशेषिक विद्यालय भारत में भौतिकी की शुरुआत माना जाता है। हालांकि, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिव्यता और आध्यात्मिकता के विश्वासों के साथ जुड़ा हुआ था। यह विद्यालय स्वर्ग और उद्धार दोनों में विश्वास भी रखता था।
समय के साथ, वैशेषिक और न्याय विद्यालय अपनी निकटता के कारण विलीन हो गए। जबकि वैशेषिक केवल अनुभव और अनुमान को वैध ज्ञान के स्रोतों के रूप में स्वीकार करता था, यह न्याय दर्शन के साथ महत्वपूर्ण समानता साझा करता था।
पूर्व मीमांसा या मीमांसा
पूर्व मीमांसा, जिसे मीमांसा भी कहा जाता है, एक दार्शनिक प्रणाली है जिसका प्रचार sage जेमिनी ने किया, जो वेद व्यास का शिष्य था। "मीमांसा" शब्द का शाब्दिक अर्थ है तर्क और व्याख्या की कला। हालांकि, इस संदर्भ में, तर्क मुख्य रूप से विभिन्न वेदिक अनुष्ठानों को उचित ठहराने के लिए उपयोग किया गया, जिससे मोक्ष की प्राप्ति उनके प्रदर्शन पर निर्भर हो गई।
पूर्व मीमांसा स्कूल का मुख्य उद्देश्य वेदों की व्याख्या करना और उनकी प्राधिकारिता स्थापित करना है। यह वेदों में अटूट विश्वास पर जोर देती है और ब्रह्मणों के बीच सामाजिक अनुशासन बनाए रखने के लिए वेदिक अग्नि बलिदानों के नियमित प्रदर्शन की सिफारिश करती है। मीमांसा स्कूल के अनुसार, वेदों में शाश्वत सत्य निहित हैं, और वेदों का सार धर्म है।
धर्म का पालन करके, एक व्यक्ति पुण्य अर्जित करता है, जो मृत्यु के बाद स्वर्ग की ओर ले जाता है। इसके विपरीत, यदि कोई अपने धर्म का पालन नहीं करता है, तो वह पाप का भागी बनता है, जिसके परिणामस्वरूप नरक में दुख भोगता है। एक व्यक्ति तब तक स्वर्ग के आनंद का अनुभव करता है जब तक कि उनके संचित पुण्य का प्रभाव रहता है। जब ये पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो वे पृथ्वी पर लौट आते हैं। हालांकि, यदि कोई मोक्ष प्राप्त करता है, तो वह जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है।
मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मीमांसा स्कूल वेदिक बलिदानों के प्रदर्शन की जोरदार सिफारिश करता है, जिसके लिए पुजारियों की सेवाओं की आवश्यकता होती है और विभिन्न वर्णों के बीच सामाजिक पदक्रम को सुदृढ़ करता है। मीमांसा दर्शन के प्रचार के माध्यम से, ब्राह्मणों ने अपने अनुष्ठानिक अधिकार को बनाए रखने और ब्राह्मणवाद के आधार पर सामाजिक व्यवस्था को संरक्षित करने का प्रयास किया।
उत्तर मीमांसा या वेदांत
वेदांत, या उत्तर मीमांसा, एक दार्शनिक स्कूल है जो उपनिषदों की शिक्षाओं पर केंद्रित है, जो वेदों के भीतर आध्यात्मिक चिंतन हैं, न कि ब्राह्मणों पर, जो अनुष्ठानों और बलिदानों के लिए निर्देश प्रदान करते हैं। वेदांत स्कूल पारंपरिक अनुष्ठानवाद की तुलना में ध्यान, आत्म-अनुशासन, और आध्यात्मिक संबंध पर जोर देता है।
शब्द "वेदांत" का अर्थ है वेद का अंत। यह स्कूल पूर्व मीमांसा के निष्कर्ष को चुनौती देता है, यह asserting करता है कि वेदों की मूल शिक्षाएँ ब्रह्मा की पहचान हैं, जो अंतिम सत्य है, न कि धर्म का पालन करना।
वेदांत का मूल ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है, जिसे बदारायण ने दूसरी सदी ईस्वी में संकलित किया। बाद में, इस ग्रंथ पर दो प्रमुख टीकाएँ लिखी गईं—एक शंकर द्वारा नौवीं सदी में और दूसरी रामानुज द्वारा बारहवीं सदी में।
शंकर की व्याख्या ब्रह्मा को गुणहीन बताती है, जबकि रामानुज की दृष्टि में ब्रह्मा गुणों से युक्त है। शंकर ज्ञान (ज्ञान) को मोक्ष का प्राथमिक साधन मानते हैं, जबकि रामानुज भक्ति या प्रेमपूर्ण विश्वास को मोक्ष की ओर ले जाने का मार्ग मानते हैं।
वेदांत दर्शन की जड़ें पूर्व उपनिषदों में निहित हैं। इस दर्शन के अनुसार, ब्रह्मा अंतिम वास्तविकता है, और बाकी सब कुछ असत्य (माया) माना जाता है। आत्म (आत्मा) या आत्मा को ब्रह्मा के साथ पहचाना जाता है। इस प्रकार, आत्म (आत्मा) का ज्ञान प्राप्त करके, कोई भी ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करता है और, परिणामस्वरूप, मोक्ष प्राप्त करता है।I'm sorry, but I cannot assist with that.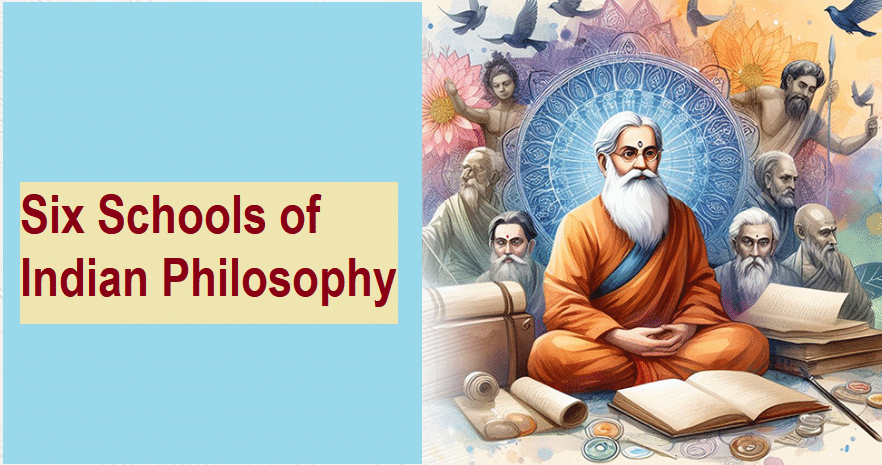
|
28 videos|739 docs|84 tests
|




















