मध्य पूर्व में संघर्ष | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download
मध्य पूर्व संघर्ष का अवलोकन
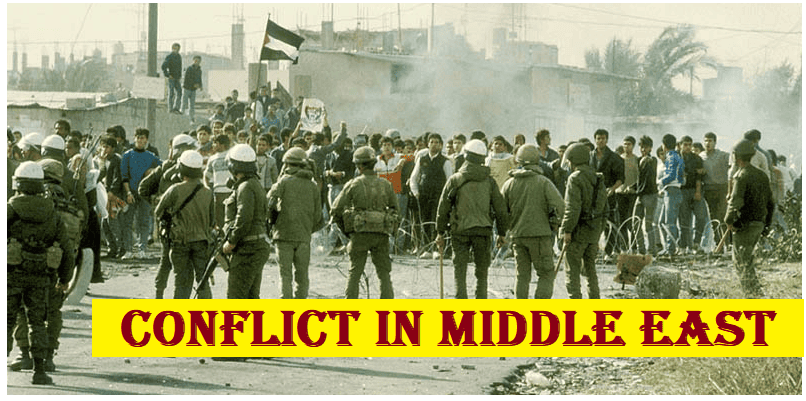
मध्य पूर्व एक परेशान क्षेत्र रहा है, जहां 1945 से लगभग निरंतर युद्ध और नागरिक युद्ध चल रहे हैं। इस क्षेत्र में मिस्र, सूदान, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, तुर्की, यमन, संयुक्त अरब अमीरात, और ओमान जैसे देश शामिल हैं। इनमें से अधिकांश देश, तुर्की और ईरान को छोड़कर, मुख्यतः अरब हैं। ईरान, जबकि अरब नहीं है, के उत्तरी फारसी खाड़ी के आसपास एक महत्वपूर्ण अरब जनसंख्या है। इस क्षेत्र में इज़राइल भी शामिल है, जो 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा फिलिस्तीन में स्थापित एक छोटा यहूदी राज्य है।
इज़राइल का निर्माण और अरब प्रतिक्रिया:
- फिलिस्तीन में अरब भूमि पर इज़राइल की स्थापना ने विश्व भर के अरब देशों में आक्रोश पैदा किया।
- अरबों ने यहूदियों का समर्थन करने के लिए ब्रिटेन और यहूदी राज्य के विचार को मजबूती से समर्थन देने के लिए अमेरिका पर आरोप लगाया।
- अरब राज्यों ने इज़राइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया और इसे नष्ट करने की शपथ ली।
संघर्ष और युद्ध:
- इज़राइल और अरब राज्यों के बीच चार बड़े युद्ध हुए (1948-49, 1956, 1967, और 1973), लेकिन इज़राइल इन हमलों से बच गया।
- इज़राइल और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष बिना स्थायी शांति समझौते के जारी रहा।
मध्य पूर्व मामलों में अन्य विषय:
- राजनीतिक और आर्थिक एकता: कुछ अरब देशों ने अरब राज्यों के बीच एकता की कोशिश की।
- विदेशी हस्तक्षेप: कई अरब देशों ने अपने देशों में विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना चाहा।
पश्चिमी और कम्युनिस्ट रुचि:
- मध्य पूर्व ने अपनी रणनीतिक स्थिति और समृद्ध तेल संसाधनों के कारण पश्चिमी और कम्युनिस्ट शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया।
व्यक्तिगत अरब राज्यों से संबंधित संघर्ष:
- लेबनान में गृह युद्ध (1975-1990)।
- ईरान और इराक के बीच युद्ध (1980-1988)।
- पहला खाड़ी युद्ध (1990-1991) जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया और अमेरिका के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन द्वारा खदेड़ा गया।
विभिन्न दृष्टिकोण:
- मध्य पूर्व की स्थिति की व्याख्या दृष्टिकोण के अनुसार भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और पत्रकारों ने अक्सर मिस्र के कर्नल नासेर को एक खतरनाक व्यक्ति के रूप में देखा, जबकि कई अरबों ने उन्हें अरब एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हुए एक नायक के रूप में देखा।
अरब एकता और बाहरी दुनिया से हस्तक्षेप
अरबों के बीच समानताएँ:
- सभी अरबों की संवाद का माध्यम अरबी भाषा है।
- अधिकांश मुसलमान हैं, लेबनान की लगभग आधी आबादी के अपवाद के साथ, जो ईसाई हैं।
- कई अरब इजराइल को नष्ट करने की इच्छा रखते हैं ताकि फिलिस्तीनी अरब उन भूमि को पुनः प्राप्त कर सकें, जिसे वे अपना अधिकार मानते हैं।
- कई अरबों के बीच राजनीतिक और आर्थिक एकता की एक मजबूत इच्छा है, जो यूरोपीय समुदाय के समान है।
ऐतिहासिक अरब एकता के लिए आह्वान:
- 1931 में, यरूशलेम में एक इस्लामी सम्मेलन ने अरब भूमि को एक संपूर्ण और अविभाज्य एकता के रूप में घोषित किया, जो उनकी पूर्ण स्वतंत्रता और एकीकरण के लिए वकालत करता था।
अरब लीग:
- 1945 में स्थापित, अरब लीग ने अरब राज्यों के बीच एकता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा, जिसमें प्रारंभ में मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक, लेबनान, सऊदी अरब, और यमन शामिल थे।
- 1980 तक सदस्यता बढ़कर 20 राज्यों तक पहुँच गई।
- अपने उदात्त लक्ष्यों के बावजूद, अरब लीग आंतरिक संघर्षों से जूझती रही और सीमित राजनीतिक सफलता प्राप्त की।
गमाल अब्देल नासेर और पैन-अरबिज़्म:
- 1950 के मध्य में, मिस्र के कर्नल गमाल अब्देल नासेर पैन-अरब आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे, जब उन्होंने 1956 के सुएज़ संकट के बाद प्रतिष्ठा हासिल की।
- 1958 में, नासेर ने सीरिया और मिस्र को एकीकृत करके संयुक्त अरब गणराज्य का गठन किया, जिसमें नासेर राष्ट्रपति बने।
- हालांकि, यह संघ अल्पकालिक था, क्योंकि सीरिया ने 1961 में नासेर के प्रभुत्व के प्रति नाराजगी के कारण बाहर निकल गया।
नासेर के बाद एकता के प्रयास:
- 1970 में नासेर की मृत्यु के बाद, उनके उत्तराधिकारी राष्ट्रपति सदात ने मिस्र, लीबिया और सीरिया के बीच एक ढीली संघ बनाने का प्रयास किया, जिसे अरब गणराज्यों का संघ कहा गया, लेकिन इस पहल का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।
अरब राज्यों के बीच भिन्नता:
- अपनी समानताओं के बावजूद, गहरे मतभेदों ने अरब राज्यों के बीच निकटता की एकता को रोका।
- जोर्डन और सऊदी अरब, जो पारंपरिक शाही परिवारों द्वारा शासित हैं, अक्सर मिस्र और सीरिया की आलोचना का सामना करते थे, जिनका शासन राष्ट्रीयतावादी और सोशलिस्ट था।
- 1979 में, अधिकांश अरब राज्यों ने मिस्र के साथ अपने संबंध तोड़ लिए, जब उसने इज़राइल के साथ एक अलग शांति संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसके परिणामस्वरूप मिस्र को अरब लीग से बाहर कर दिया गया।
ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा ऐतिहासिक हस्तक्षेप:
- मध्य पूर्व में ब्रिटिश और फ्रांसीसी भागीदारी का इतिहास कई वर्षों पुराना है।
- प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ब्रिटेन और फ्रांस को वर्साय समझौते द्वारा मध्य पूर्व के बड़े क्षेत्रों का प्रबंधन करने के लिए जनादेश दिया गया।
- हालांकि ब्रिटेन ने 1932 में इराक और 1946 में जोर्डन को स्वतंत्रता दी, लेकिन दोनों देश ब्रिटिश समर्थक बने रहे।
- फ्रांस ने 1945 में सीरिया और लेबनान को स्वतंत्रता दी, लेकिन क्षेत्र में कुछ प्रभाव बनाए रखने की कोशिश की।
मध्य पूर्व का सामरिक महत्व:
- मध्य पूर्व की रणनीतिक स्थिति पश्चिमी देशों, साम्यवादी गुट और तीसरी दुनिया के देशों के बीच एक चौराहे के रूप में इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाती है।
- एक समय, यह विश्व के एक तिहाई से अधिक तेल का उत्पादन करता था, जिसमें प्रमुख उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कुवैत थे।
- उत्तर सागर के तेल की उपलब्धता और परमाणु ऊर्जा के आगमन से पहले, यूरोपीय देशों की मध्य पूर्व से तेल आपूर्ति पर भारी निर्भरता थी।
- एक स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, उन्होंने तेल उत्पादक राज्यों में मित्रवत सरकारें स्थापित करना चाहा।
शक्ति संतुलन में परिवर्तन:
- अरब राज्यों के बीच एकता की कमी ने अन्य देशों को मध्य पूर्व में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी।
- कई अरब राज्यों में राष्ट्रीयता की सरकारें थीं जो पश्चिमी प्रभाव को गहराई से अस्वीकार करती थीं।
- एक के बाद एक, ऐसे सरकारें जो बहुत अधिक प्र-Western मानी जाती थीं, गिरा दी गईं और उनके स्थान पर गैर-संरेखित शासन स्थापित किए गए जो पूर्व (साम्यवादी गुट) और पश्चिम दोनों से स्वतंत्र रूप से कार्य करने का प्रयास कर रहे थे।
मिस्र:
- द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में, ब्रिटिश सैनिकों का एक समूह नहर क्षेत्र में बना रहा, जो सुएज़ नहर को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण था।
- 1952 में, एक समूह ने मिस्री सेना के अधिकारियों ने राजा फ़ारूक को अपदस्थ कर दिया, जिन्हें ब्रिटिश के प्रति बहुत नरम माना गया।
- 1954 तक, कर्नल नासिर राष्ट्रपति बन गए और उनके ब्रिटेन के प्रति विद्रोह ने 1956 के सुएज़ युद्ध को जन्म दिया, जिसने मिस्र में ब्रिटिश प्रभाव का अंत किया।
जॉर्डन:
- राजा अब्दुल्ला को 1946 में ब्रिटिश द्वारा सिंहासन पर बैठाया गया।
- उन्हें 1951 में उन राष्ट्रवादियों द्वारा हत्या कर दी गई जो महसूस करते थे कि वह ब्रिटेन के साथ बहुत अधिक जुड़े हुए थे।
- राजा हुसैन, अब्दुल्ला के उत्तराधिकारी, को जीवित रहने के लिए सावधान रहना पड़ा।
- उन्होंने 1957 में ब्रिटिश सैनिकों को जॉर्डन में आधार उपयोग की अनुमति देने वाले संधि को समाप्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप सभी ब्रिटिश सैनिकों की वापसी हुई।
इराक:
- इराक के किंग फैसल और उनके प्रधानमंत्री, नूरी-एस-सैद, ब्रिटिश समर्थक थे। 1955 में, उन्होंने तुर्की के साथ बगदाद पैक्ट पर हस्ताक्षर किए ताकि एक संयुक्त रक्षा और आर्थिक नीति स्थापित की जा सके। 1956 का सुएज़ युद्ध ब्रिटेन के लिए अपमानजनक था और इसने इराक में ब्रिटिश विरोधी भावना को बढ़ावा दिया। फैसल और नूरी-एस-सैद की हत्या कर दी गई, और 1958 में इराक एक गणराज्य बन गया। नई सरकार ने बगदाद पैक्ट से बाहर निकलने का निर्णय लिया और वह मिस्र के प्रति सहानुभूतिपूर्ण थी।
ईरान:
- 1945 में, रूस ने उत्तरी ईरान में एक कम्युनिस्ट सरकार स्थापित करने का प्रयास किया, जो सोवियत संघ के साथ सीमांत था और वहां एक बड़ा कम्युनिस्ट पार्टी थी। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त शाह रेज़ा पहलवी ने इसका विरोध किया और 1950 में अमेरिका के साथ एक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका ने ईरान को आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान की, जिसमें टैंक और जेट फाइटर्स शामिल थे। ईरान में एक मजबूत राष्ट्रीयतावाद आंदोलन ने विदेशी प्रभाव, विशेष रूप से अमेरिका और ब्रिटेन के प्रति नाराजगी व्यक्त की। 1951 में, डॉ. मुसद्दिक, जो ईरान के प्रधानमंत्री थे, ने एंग्लो-ईरानियन ऑइल कंपनी और उसके रिफाइनरी को अबादन में राष्ट्रीयकरण किया। 1954 में, एक समझौता हुआ जिसमें ब्रिटिश पेट्रोलियम को शेयरों का 40 प्रतिशत और ईरान को लाभ का 50 प्रतिशत प्राप्त हुआ। शाह ने इस लाभ का उपयोग आधुनिकीकरण और भूमि सुधार के लिए किया, लेकिन अमेरिका के साथ उनके करीबी संबंधों और उनकी संपत्ति के प्रति संदेह के कारण नाराजगी बढ़ी। 1979 में, उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, और आयातुल्ला खुमैनी के तहत एक इस्लामी गणराज्य स्थापित किया गया, जो नासिर की तरह एक गैर-संरेखित देश की इच्छा रखते थे।
अरब-इजरायल संघर्ष: इजरायल का निर्माण और अरब-इजरायली युद्ध, 1948-1949
इजरायल राज्य के निर्माण ने युद्ध क्यों छेड़ा?
- संघर्ष की जड़ें लगभग 2,000 साल पहले AD 71 में जाती हैं, जब अधिकांश यहूदी पलस्तीन, जो उनका जन्मभूमि थी, से रोमन द्वारा निकाल दिए गए थे।
- समय के साथ, पलस्तीन में कुछ छोटे यहूदी समुदाय बने रहे, और यहूदियों की निर्वासन से धीरे-धीरे वापसी हुई।
- हालांकि, 19वीं सदी के अंत तक, यहूदियों की संख्या इतनी नहीं थी कि वे अरबों के लिए खतरा बन सकें, जो पलस्तीन को अपनी मातृभूमि मानते थे।
- 1897 में, कुछ यूरोपीय यहूदियों ने स्विट्ज़रलैंड के बासेल में विश्व सियोनिस्ट संगठन की स्थापना की। सियोनिस्ट मानते थे कि यहूदियों को पलस्तीन लौटकर एक 'राष्ट्रीय मातृभूमि' या यहूदी राज्य स्थापित करना चाहिए।
- रूस, फ्रांस, और जर्मनी में उत्पीड़न का सामना करने के बाद, यहूदियों ने सुरक्षित आश्रय की खोज की।
- समस्या यह थी कि पलस्तीन पहले से ही अरबों द्वारा बसा हुआ था, जो स्वाभाविक रूप से यहूदियों के हाथों अपनी भूमि खोने से डरते थे।
- ब्रिटेन की भूमिका 1917 में सामने आई जब विदेश मंत्री आर्थर बालफोर ने पलस्तीन में यहूदी राष्ट्रीय घर के लिए समर्थन व्यक्त किया (जिसे बालफोर घोषणा कहा जाता है)।
- 1919 के बाद, जब पलस्तीन ब्रिटिश जनादेश बना, तो बड़ी संख्या में यहूदियों का आगमन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप यहूदी आव्रजन के खिलाफ अरबों द्वारा जोरदार विरोध हुआ।
- ब्रिटिश सरकार ने 1922 में आश्वासन दिया कि यहूदी पूरे पलस्तीन पर कब्जा नहीं करेंगे और पलस्तीन के अरबों के अधिकारों का समझौता नहीं होगा।
- बालफोर की घोषणा ने यह भी जोर दिया कि पलस्तीन में गैर-यहूदी समुदायों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों को नुकसान नहीं पहुँचाया जाना चाहिए।
- ब्रिटिशों का उद्देश्य यहूदियों और अरबों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना था, लेकिन उन्होंने गहरी धार्मिक विभाजन को कमतर आंका और बालफोर के वादे को पूरा करने में असफल रहे।
- 1933 के बाद जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ नाज़ी उत्पीड़न के कारण पलस्तीन में यहूदी शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई, जिससे 1940 तक यहूदी आबादी लगभग आधी हो गई।
- 1936 से, अरबों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किए, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिशों द्वारा कठोर कार्रवाई की गई, जिससे 3,000 से अधिक अरबों की मौत हुई।
- 1937 में, ब्रिटिश पील आयोग ने पलस्तीन को अलग अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने का सुझाव दिया, लेकिन अरबों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
- 1939 में, ब्रिटिशों ने दस वर्षों के भीतर एक स्वतंत्र अरब राज्य की पेशकश की और यहूदी आव्रजन को प्रति वर्ष 10,000 तक सीमित किया, जिसे यहूदियों ने भी अस्वीकार कर दिया।
- द्वितीय विश्व युद्ध ने स्थिति को और बढ़ा दिया क्योंकि नाज़ी-स्थापित यूरोप से यहूदियों की एक बड़ी संख्या शरण लेने आई।
- 1945 में, अमेरिका ने ब्रिटेन पर 100,000 यहूदियों को पलस्तीन में प्रवेश देने का दबाव डाला।
- डेविड बेन-गुरियन जैसे यहूदी नेताओं के समर्थन के बावजूद, ब्रिटिशों ने अरबों को नाराज करने से बचने के लिए मना कर दिया।
- यहूदियों ने अपने 'राष्ट्रीय घर' के लिए लड़ाई लड़ने का संकल्प किया और अरबों और ब्रिटिशों दोनों के खिलाफ हिंसा का अभियान शुरू किया।
- प्रसिद्ध घटनाओं में यरूशलेम में किंग डेविड होटल को बम से उड़ा देना शामिल था, जिसमें 91 लोग मारे गए।
- ब्रिटिशों ने यहूदी नेताओं को गिरफ्तार करके और यहूदियों को पलस्तीन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे जहाजों जैसे Exodus को वापस मोड़कर जवाब दिया।
- द्वितीय विश्व युद्ध से कमजोर होकर, ब्रिटिशों ने स्थिति को प्रबंधित करने में असमर्थता व्यक्त की।
- विदेश सचिव अर्नेस्ट बेविन ने संयुक्त राष्ट्र से इस मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध किया।
- नवंबर 1947 में, संयुक्त राष्ट्र ने पलस्तीन को विभाजित करने के लिए मतदान किया, जिसमें लगभग आधा यहूदी राज्य के लिए आवंटित किया गया।
- 1948 की शुरुआत में, ब्रिटिशों ने पूरी तरह से हटने और यूएन योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।
- जब यहूदियों और अरबों के बीच लड़ाई छिड़ गई, जबकि अरबों ने पलस्तीन का आधा हिस्सा खोने का विरोध किया, ब्रिटिशों ने अपनी सेनाएँ वापस ले लीं।
- मई 1948 में, बेन-गुरियन ने इजरायल की स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसके तुरंत बाद इस पर मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक, और लेबनान ने हमला किया।
इस त्रासदी के लिए किसे दोषी ठहराया जाए?
- दुनिया में कई लोगों ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन में उठे तूफान के लिए जिम्मेदार ठहराया। यहां तक कि उन ब्रिटिश समाचार पत्रों ने भी, जो कंजर्वेटिव पार्टी के समर्थन में थे, बेविन और लेबर सरकार की स्थिति को लेकर आलोचना की।
- यह सुझाव दिया गया कि ब्रिटिश सैनिकों को फिलिस्तीन के सुगम विभाजन को सुनिश्चित करने के लिए वहां रहना चाहिए था।
- अरबों ने ब्रिटिशों पर यह आरोप लगाया कि वे प्रो-यहूदी हैं, बहुत अधिक यहूदियों को फिलिस्तीन में आने की अनुमति दी, और इस कारण से उन्हें अपने घर का आधा हिस्सा खोना पड़ा।
- वहीं, यहूदियों ने ब्रिटिशों पर प्रो-अरब होने का आरोप लगाया, यह कहते हुए कि उन्होंने यहूदी प्रवासन को सीमित करने का प्रयास किया।
- बेविन ने अमेरिका को इस अराजकता के लिए जिम्मेदार ठहराया। उनके इस विचार का समर्थन करने के लिए सबूत हैं।
- यह राष्ट्रपति ट्रूमैन थे जिन्होंने अप्रैल 1946 में ब्रिटेन पर दबाव डाला कि वह फिलिस्तीन में 100,000 अतिरिक्त यहूदियों को स्वीकार करे।
- अरबों के गुस्से को बढ़ाने के बावजूद, ट्रूमैन ने फिलिस्तीन में व्यवस्था बनाए रखने के लिए अमेरिकी सैनिक भेजने से इनकार कर दिया, अमेरिका में और यहूदी प्रवासन पर रोक लगा दी, और ब्रिटिश मॉरिसन योजना (जुलाई 1946) को अस्वीकार कर दिया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश निगरानी में अलग-अलग अरब और यहूदी प्रांत स्थापित करना था।
- अमेरिकियों ने सभी अरब राष्ट्रों के विरोध के बावजूद संयुक्त राष्ट्र में विभाजन के लिए भी दबाव डाला, जिससे फिलिस्तीन में हिंसा और बढ़ गई।
- कुछ इतिहासकार ब्रिटिशों का बचाव करते हैं, यह तर्क करते हुए कि उन्होंने दोनों पक्षों के प्रति निष्पक्ष रहने का प्रयास किया और यह कि अरबों और यहूदियों को एक शांतिपूर्ण समाधान स्वीकार करने के लिए मनाना असंभव था।
- ब्रिटिशों की वापसी को एक ऐसे तरीके के रूप में देखा गया, जिससे अमेरिकियों और संयुक्त राष्ट्र को उस स्थिति की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया जा सके, जिसे उन्होंने बनाने में मदद की थी, और 1945 के बाद 100 मिलियन पाउंड से अधिक खर्च करने के बाद ब्रिटिशों को और अधिक वित्तीय बोझ से बचाने के लिए।
युद्ध और इसके परिणाम:
- शुरुआत में, बहुत से लोगों ने उम्मीद की थी कि अरब आसानी से जीतेंगे, लेकिन इसके विपरीत, इजराइलियों ने उन्हें हराया और अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जितना कि संयुक्त राष्ट्र ने विभाजन में आवंटित किया था। अंततः इजराइल ने लगभग तीन-चौथाई फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया, जिसमें लाल सागर पर स्थित मिस्र का बंदरगाह ईलात भी शामिल था।
- इजराइलियों की विजय का कारण यह था कि वे भयंकर संघर्ष कर रहे थे, जिनमें से कई को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में सेवा का सैन्य अनुभव था।
- अरब राज्यों में विभाजन था, वे खराब रूप से सुसज्जित थे, और फिलिस्तीनी demoralized थे, क्योंकि उनकी सैन्य संगठन को 1936-1939 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश द्वारा भंग कर दिया गया था।
- सबसे दुखद परिणाम फिलिस्तीनी अरबों का विस्थापन था, जिन्होंने अपनी मातृभूमि का तीन-चौथाई हिस्सा खो दिया। अधिकांश लोग राज्यविहीन हो गए, कुछ नए इजराइली राज्य में और अन्य वेस्ट बैंक में, जो कि जॉर्डन द्वारा कब्जा किया गया था।
- लगभग एक मिलियन लोग मिस्र, लेबनान, जॉर्डन, और सीरिया में भाग गए, जहाँ वे भयानक शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे।
- यरूशलेम इजराइल और जॉर्डन के बीच विभाजित था।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, और फ्रांस ने इजराइल की सीमाओं की गारंटी दी, लेकिन अरब राज्यों ने युद्धविराम को स्थायी नहीं माना। उन्होंने इजराइल की वैधता को मान्यता देने से इनकार कर दिया, इस युद्ध को इजराइल को नष्ट करने और फिलिस्तीन को पुनः प्राप्त करने के संघर्ष की शुरुआत के रूप में देखा।
1967 का छह-दिन युद्ध
पृष्ठभूमि:
- 1948-49 के युद्ध के बाद, अरब देशों ने शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए और इज़राइल को मान्यता देने से मना कर दिया।
- 1967 में, इराक, सीरिया, और मिस्र ने इज़राइल को नष्ट करने के उद्देश्य से अरब देशों का एक गठबंधन बनाया।
युद्ध की पूर्वपीठिका:
- इराक: 1963 में एक बाथ से प्रभावित सरकार सत्ता में आई, जिसका उद्देश्य अरब एकता और सामाजिक सुधार था। राष्ट्रपति अरेफ ने इज़राइल को समाप्त करने का लक्ष्य घोषित किया।
- सीरिया: बाथ पार्टी ने 1966 में सत्ता पर कब्जा कर लिया और फतह के साथ फिलिस्तीनी मुक्ति आंदोलन का समर्थन किया। सीरिया ने गोलान हाइट्स से यहूदी बस्तियों पर बमबारी की।
- मिस्र: राष्ट्रपति नासेर, जो अपनी नेतृत्व क्षमता और समाजवादी सुधारों के लिए लोकप्रिय थे, ने सिनाई सीमा पर सैनिकों को तैनात किया और अकाबा की खाड़ी को बंद कर दिया, इज़राइल पर हमले की योजना बनाई। सोवियत संघ ने मिस्र और सीरिया को प्रचार और संभावित सैन्य सहायता के साथ समर्थन दिया।
युद्ध:
- अरब बलों के एकत्र होने के साथ, इज़राइल ने पहले हमला करने का निर्णय लिया, 5 जून को हवाई हमले शुरू किए, जिससे अधिकांश मिस्री वायु सेना नष्ट हो गई।
- इज़राइली सैनिकों ने तेजी से गाज़ा पट्टी, सिनाई, पश्चिम किनारा, जेरूसलम, और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया।
- युद्ध 10 जून को संयुक्त राष्ट्र की संघर्ष विराम के साथ समाप्त हुआ, जो एक सप्ताह से भी कम समय में हुआ।
इज़राइल की सफलता के कारण:
- अरब सैनिकों का जमाव धीमा था, जिसने इज़राइल को तैयारी का समय दिया।
- इज़राइली वायु श्रेष्ठता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- अरब संचार और तैयारी की कमी ने उनकी हार में योगदान दिया।
युद्ध के परिणाम:
- इज़राइल ने कब्जे में लिए गए क्षेत्रों को लौटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के आदेश की अनदेखी की, और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बफर क्षेत्रों की स्थापना की।
- इज़राइल को लगभग एक मिलियन नए अरब निवासियों का शासन करने की चुनौती का सामना करना पड़ा, जिनमें से कई शरणार्थी शिविरों में रहते थे।
- यह हार अरब देशों के लिए एक अपमान थी, विशेष रूप से नासेर के लिए, जिन्होंने महसूस किया कि अरबों को इज़राइल को चुनौती देने के लिए बाहरी समर्थन की आवश्यकता है।
- सोवियत संघ, जो फिर से प्रभाव प्राप्त करना चाहता था, ने मिस्र और सीरिया को आधुनिक हथियारों की आपूर्ति शुरू की।
- अरब देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र कराने के लिए फिर से कोशिश करने का संकल्प लिया, जिसमें अगला बड़ा प्रयास 1973 के योम किप्पुर युद्ध में हुआ।
1973 का योम किप्पुर युद्ध
युद्ध की पृष्ठभूमि:
- फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन (PLO), जिसका नेतृत्व यासिर अराफात कर रहे थे, ने अरब देशों पर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाला।
- जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो PLO के अधिक चरमपंथी घटक अपनी आवाज उठाने के लिए आतंकवादी हमलों का सहारा लेने लगे।
- जॉर्डन के राजा हुसैन, जो PLO के आतंकवाद से शर्मिंदा थे, ने 1970 में जॉर्डन से PLO के सदस्यों को निकाल दिया।
- 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में इजराइली एथलीटों की हत्या जैसे चरम हिंसा के कृत्यों ने तनाव को बढ़ा दिया।
- मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात, जिन्होंने 1970 में नासेर का स्थान लिया, इजराइल के साथ एक शांति समझौते की आवश्यकता में विश्वास रखते थे।
- उन्हें डर था कि PLO का आतंकवाद फिलिस्तीनी कारण के लिए वैश्विक सहानुभूति को प्रभावित कर सकता है।
- सादात ने अरब हितों के लिए अमेरिकी समर्थन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा, आशा करते हुए कि अमेरिका इजराइल को बातचीत के लिए मनाएगा। हालांकि, अमेरिका ने हस्तक्षेप नहीं किया।
- सीरिया के सहयोग से, सादात ने इजराइल पर हमला करने का निर्णय लिया, यह मानते हुए कि एक सैन्य संघर्ष अमेरिकी मध्यस्थता को मजबूर करेगा।
- मॉडर्न रूसी हथियारों और रूसी सैन्य विशेषज्ञों से मिली प्रशिक्षण के कारण मिस्र का आत्मविश्वास बढ़ गया।
युद्ध का प्रारंभ:
- युद्ध 6 अक्टूबर 1973 को शुरू हुआ, जब मिस्री और सीरियाई बलों ने योम किप्पुर, एक महत्वपूर्ण यहूदी उत्सव, के दौरान आश्चर्यजनक हमला किया।
- प्रारंभिक अरब सफलताओं का इजराइली प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो मुख्य रूप से अमेरिकी-आपूर्तित हथियारों का उपयोग कर रहा था।
- प्रारंभिक लाभ के बावजूद, इजराइल ने 1967 में कब्जा किए गए सभी क्षेत्रों को बनाए रखा और यहां तक कि सुएज़ नहर के पार मिस्र में भी बढ़त हासिल की।
- एक तरह से, सादात की रणनीति सफल रही, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने शांति समझौते के लिए मध्यस्थता की आवश्यकता को पहचाना।
- संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से, एक संघर्ष विराम स्थापित किया गया, जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार किया।
युद्ध के बाद:
युद्ध के समापन ने स्थायी शांति के लिए आशा को जगाया। मिस्र और इज़रायली नेताओं ने जिनेवा में (हालाँकि एक ही कमरे में नहीं) शर्तों पर चर्चा करने के लिए बैठक की।
- इज़राइल ने 1967 के युद्ध के बाद से बंद पड़े सुएज़ नहर से अपने सैनिकों को वापस लेने पर सहमति जताई, जिससे 1975 में मिस्र द्वारा इसका पुनः उद्घाटन संभव हुआ (हालाँकि यह इज़रायली जहाजों के लिए नहीं था)।
- अरब तेल उत्पादक राष्ट्रों ने अमेरिका और पश्चिमी यूरोप पर दबाव डालने के लिए तेल की आपूर्ति में कमी लाने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से यूरोप में महत्वपूर्ण कमी आई।
- साथ ही, तेल निर्यातक देशों का संगठन (OPEC) ने तेल की कीमतों में वृद्धि की, जिससे वैश्विक महंगाई और औद्योगिक देशों में ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ।
कैम्प डेविड समझौते और मिस्र-इजरायली शांति (1978-1979)
बातचीत की शुरुआत:
- राष्ट्रपति सदात ने पहचाना कि मिस्र सैन्य साधनों से इजराइल को पराजित नहीं कर सकता और निरंतर संघर्ष संसाधनों की बर्बादी है।
- जोखिमों के बावजूद, सदात ने इजराइल के साथ बातचीत करने का साहसिक कदम उठाया, उसकी वैधता को मान्यता दी।
- इजरायली सरकार उच्च रक्षा खर्च और वैश्विक मंदी के कारण आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही थी, और अरब राज्यों के साथ शांति खोजने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से दबाव था।
- सदात की बातचीत की तत्परता ने उनके नवंबर 1977 में इजराइल की यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया, इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री मेनाचेम बेगिन दिसंबर में मिस्र आए।
- यू.एस. राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने मिस्र और इजराइल के बीच औपचारिक वार्ता को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो सितंबर 1978 में कैम्प डेविड में शुरू हुई।
शांति संधि और इसके परिणाम:
- कार्टर के मध्यस्थता में, वार्ता ने मार्च 1979 में वाशिंगटन में हस्ताक्षरित शांति संधि की ओर अग्रसर किया।
- मुख्य समझौतों में शामिल थे:
- 1948 से जारी मिस्र और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति को समाप्त करना।
- इजराइल का सिनाई प्रायद्वीप से अपनी सेनाओं को वापस खींचने का वचन देना।
- मिस्र का इजराइल पर हमला न करने और दक्षिण सिनाई में नए खोले गए कुओं से तेल आपूर्ति की गारंटी देना।
- इजरायली जहाजों को सुएज़ नहर का उपयोग करने की अनुमति देना।
प्रतिक्रियाएँ और चुनौतियाँ:
- इस संधि का PLO और अधिकांश अरब राज्यों द्वारा निंदा की गई, सिवाय सूडान और मोरक्को के।
- इजराइल को सीरिया और जॉर्डन के साथ समान शांति संधियाँ स्थापित करने के लिए लंबा रास्ता तय करना था।
- विश्व की राय इजराइल के खिलाफ बदलने लगी, PLO की स्थिति को मान्यता देने लगी।
- जब अमेरिका ने PLO और इजराइल को एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए एक साथ लाने का प्रयास किया, तब इजराइल ने सहयोग करने से इनकार कर दिया।
- नवंबर 1980 में, बेगिन ने घोषणा की कि इजराइल गोलान हाइट्स को सीरिया को कभी नहीं लौटाएगा या पश्चिमी तट को स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य बनने की अनुमति नहीं देगा, इसके अस्तित्व के लिए इसे खतरे के रूप में देखते हुए।
- पश्चिमी तट के अरबों में इजराइली बस्तियों की नीतियों को लेकर असंतोष बढ़ा।
- चिंताएँ उठीं कि यदि इजराइली सरकार अधिक मध्यम दृष्टिकोण अपनाने में विफल रही, तो हिंसा फिर से भड़क सकती है।
जारी तनाव और इंटिफ़ादा:
- शांति के प्रारंभिक चरणों के बावजूद, सादात को संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद धमकियों का सामना करना पड़ा। अक्टूबर 1981 में, उन्हें कट्टरपंथी मुस्लिम सैनिकों ने हत्या कर दी, जो मानते थे कि उन्होंने अरब और मुस्लिम कारणों के साथ विश्वासघात किया है। उनके उत्तराधिकारी, होस्नी मुबारक, ने कैंप डेविड समझौते को बनाए रखा, जो शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 1980 के दशक के दौरान, ईरान-इराक युद्ध ने अरब ध्यान को हीन कर दिया, जिससे अरब-इजराइली तनाव पीछे छूट गया। हालांकि, दिसंबर 1987 में, गाजा और पश्चिमी तट पर फिलिस्तीनियों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसे इंटिफ़ादा के नाम से जाना गया, जिसमें हड़तालें, कर न चुकाने और इजरायली उत्पादों का बहिष्कार शामिल था। इजरायली कार्रवाई ने इंटिफ़ादा को दबाने में असफलता का सामना किया, जो तीन साल से अधिक समय तक चली और इजरायली कार्रवाइयों के लिए अंतरराष्ट्रीय निंदा को आकर्षित किया।
इजराइल और PLO के बीच शांति
जून 1992 में इजराइल में एक कम आक्रामक सरकार (लेबर) के चुनाव ने फिलिस्तीनियों के साथ बेहतर संबंधों की उम्मीदें बढ़ाईं। प्रधानमंत्री यित्ज़ाक राबिन और विदेश मंत्री शिमोन पेरेस दोनों ने वार्ता में विश्वास किया और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए रियायतें देने के लिए तैयार थे। पीएलओ के नेता यासिर अराफात ने प्रतिक्रिया दी, और वार्ता शुरू हुई।
सितंबर 1993 का शांति समझौता:
यह ओस्लो में एक सम्मेलन के दौरान पहला महत्वपूर्ण सफलता का क्षण था, जिसे ओस्लो समझौतों के नाम से जाना गया। मुख्य समझौतों में शामिल थे:
- इजराइल ने आधिकारिक रूप से पीएलओ को मान्यता दी।
- पीएलओ ने इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को स्वीकार किया और आतंकवाद से दूर रहने का संकल्प लिया।
- फिलिस्तीनियों को जेरिको (पश्चिमी तट में) और गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों में सीमित आत्म-शासन दिया गया, जो 1967 के युद्ध के बाद से इजराइल द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र थे, जिसमें इजरायली सैनिकों का इन क्षेत्रों से हटना शामिल था।
दोनों पक्षों के कट्टरपंथी समूहों, जैसे कि फिलिस्तीनी मुक्ति के लिए लोकप्रिय मोर्चा, जो एक पूरी तरह स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की मांग कर रहा था, और पश्चिमी तट पर इजरायली बस्तियाँ, जो पीएलओ को किसी भी रियायत का विरोध कर रहे थे, के बावजूद, दोनों पक्षों के मध्यम नेताओं ने उल्लेखनीय साहस और दृढ़ता का प्रदर्शन किया। इजराइली उप विदेश मंत्री योसी बेइलिन और अराफात के सलाहकारों में से एक महमूद अब्बास (जिसे अबू माज़ेन भी कहा जाता है) जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं। अगले वर्षों में, उन्होंने ओस्लो समझौतों की नींव पर और भी महत्वपूर्ण कदम उठाए।
|
28 videos|739 docs|84 tests
|















