राष्ट्रीय आंदोलन का चरण 2 (1915-1922) - 1 | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download
नागपुर सत्र (Nagpur Session) का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress) का आयोजन दिसंबर 1920 में हुआ, जो भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जिन्होंने कांग्रेस की संगठनात्मक संरचना, उद्देश्यों और विधियों को पुनः आकार दिया।

1. कांग्रेस के उद्देश्य की पुनर्परिभाषा: इस सत्र में कांग्रेस की स्वराज (Swaraj) के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई, लेकिन एक नई समझ के साथ। स्वराज अब इस रूप में व्यक्त किया गया कि "साम्राज्य के भीतर स्व-सरकार की तलाश करना यदि संभव हो और आवश्यक होने पर बाहर।" यह स्वतंत्रता के प्रति एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
2. विधियों में विकास: इस सत्र में 'संवैधानिक साधनों' पर निर्भरता से 'सभी शांतिपूर्ण और वैध विधियों' को अपनाने की ओर एक बदलाव देखा गया। यह व्यापक दृष्टिकोण स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक विभिन्न रणनीतियों को स्वीकार करता है।
3. संगठनात्मक सुधार
- कार्य समिति का गठन: एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन था कार्य समिति का गठन, जिसमें पंद्रह सदस्य शामिल थे। इस समिति को पार्टी के प्रमुख कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया।
- अखिल भारतीय समिति का निर्माण: 350 सदस्यों की एक अखिल भारतीय समिति बनाई गई, जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए जिम्मेदार थी। यह शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करती थी, जिसके पास कार्य समिति के निर्णयों और कार्यप्रणाली की समीक्षा करने का अधिकार था, जिससे जवाबदेही और समावेशिता सुनिश्चित होती थी।
- ग्राउंड स्तर को मजबूत करना: विभिन्न स्तरों पर कांग्रेस समितियों का गठन किया गया, जो नगरों से लेकर गांवों तक फैली हुई थीं, स्थानीय समुदायों के साथ व्यापक भागीदारी और जुड़ाव को सुविधाजनक बनाया। यह विकेन्द्रीकृत संरचना समर्थन को जुटाने और कांग्रेस के विचारधाराओं को प्रभावी ढंग से फैलाने के लिए लक्षित थी।
- भाषाई पुनर्गठन: प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया, जिसका उद्देश्य स्थानीय भाषाओं में कांग्रेस के आदर्शों को बढ़ावा देना था। हिंदी पर जोर दिया गया, जिससे शिक्षित अभिजात वर्ग और जनसामान्य के बीच की खाई को पाटा जा सके, और पहुँच और सामंजस्य बढ़ाया जा सके।
- समावेशी सदस्यता: इस सत्र ने सभी पुरुषों और महिलाओं को, जो इक्कीस वर्ष या उससे अधिक उम्र के थे, नाममात्र वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करने पर कांग्रेस की सदस्यता खोल दी। यह सदस्यता का लोकतंत्रीकरण पार्टी के आधार को व्यापक बनाने और समावेशिता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता था।
4. नेतृत्व में परिवर्तन: अगस्त 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद, कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में चला गया। यह भारतीय राजनीति में गांधीवादी युग की शुरुआत का प्रतीक था, जो अहिंसात्मक प्रतिरोध और जन आंदोलन की विशेषता के लिए जाना जाता है।
5. संगठनात्मक ढांचे का आधुनिकीकरण: नागपुर सत्र ने कांग्रेस पार्टी को आधुनिकता की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिसमें समकालीन संगठनात्मक प्रथाओं को अपनाया गया। स्थानीय, क्षेत्रीय, और राष्ट्रीय समितियों की स्थापना ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ तालमेल बैठाया और कुशल कार्यप्रणाली को सुगम बनाया।
स्वराज पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन के परिणामस्वरूप स्वराज पार्टी का उदय, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। इसके प्रमुख योगदान और विरासत का विवरण नीचे दिया गया है:
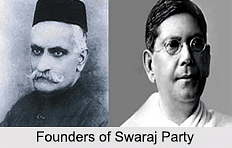
1. गठन और उद्देश्य
- विभाजन का पृष्ठभूमि: गैर-सहयोग आंदोलन के निलंबन के परिणामस्वरूप कांग्रेस में विभाजन हो गया, जिसके चलते मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी नामक एक अलग समूह का गठन किया।
- चुनाव में भाग लेने का उद्देश्य: स्वराजवादी विधान परिषद चुनावों में भाग लेने और उपनिवेशी सरकार को भीतर से बाधित करने का प्रयास कर रहे थे। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास जैसे नेताओं के नेतृत्व में, उन्होंने परिषदों में भागीदारी का समर्थन किया ताकि सरकार की अक्षमताओं को उजागर किया जा सके और सुधारों के लिए दबाव डाला जा सके।
2. चुनावी सफलता और विधायी कार्रवाई
- प्रभावशाली चुनावी लाभ: नवंबर 1923 के चुनावों में, स्वराज पार्टी ने विशेष रूप से बंगाल और केंद्रीय विधायी परिषद में उल्लेखनीय सफलताएँ प्राप्त की, जिसमें मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने क्रमशः नेतृत्व की भूमिकाएँ ग्रहण कीं।
- जवाबदेह सरकार की मांग: स्वराज पार्टी ने भारत में जवाबदेह सरकार की स्थापना की मांग की, 1919 के भारतीय प्रशासन अधिनियम में आवश्यक परिवर्तनों के लिए समर्थन किया।
- विधायी प्रस्ताव: परिषदों के भीतर, पार्टी ने दमनकारी कानूनों के खिलाफ सफलतापूर्वक प्रस्ताव पारित किए और ड्यार्की प्रणाली की कमियों को उजागर करते हुए सुधारों के लिए समर्थन किया।
3. चुनौतियाँ और पतन
- नेतृत्व की हानि का प्रभाव: पार्टी को जून 1925 में C.R. दास के निधन से एक झटका लगा, जिससे इसकी एकता और नेतृत्व कमजोर हुआ।
- साम्प्रदायिक विभाजन: स्वराज पार्टी के भीतर आंतरिक विभाजन उभरे, जिसमें कुछ सदस्यों, जिन्हें 'जिम्मेदारवादी' कहा जाता था, ने सरकार के साथ सहयोग की पेशकश की ताकि साम्प्रदायिक हितों की रक्षा की जा सके, जिससे पार्टी की एकता कमजोर हुई।
- सिविल नाफरमानी का संक्रमण: स्वराजियों ने 1930 में लाहौर कांग्रेस के प्रस्ताव के बाद और सिविल नाफरमानी आंदोलन की शुरुआत के दौरान विधानसभाओं से बाहर निकलने का निर्णय लिया, जिससे रणनीति में बदलाव आया।
4. विरासत और उपलब्धियाँ
- राजनीतिक रिक्तता को भरना: स्वराज पार्टी ने उस समय राजनीतिक रिक्तता को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जब राष्ट्रीय आंदोलन अपनी ताकत को पुनर्गroupित कर रहा था, और उपनिवेशी सहानुभूति के सामने झुकने के बिना लचीलापन दर्शाया।
- व्यवस्थित विधान सभा सहभागिता: उन्होंने विधानसभाओं में व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से कार्य किया, आवश्यकतानुसार रणनीतिक रूप से पीछे हटते हुए, जो संस्थागत ढांचों के भीतर राजनीतिक सक्रियता का एक मॉडल प्रस्तुत करता है।
- उपनिवेशी कानूनों का पर्दाफाश: अपने कार्यों के माध्यम से, स्वराज पार्टी ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की अक्षमताओं को प्रभावी ढंग से उजागर किया और उपनिवेशी शासन की दमनकारी प्रकृति को उजागर किया, जिससे इसके खिलाफ सार्वजनिक राय को जागरूक किया।
- नेतृत्व और संगठन: स्वराज पार्टी एक संगठित और अनुशासित राजनीतिक इकाई के रूप में उभरी, जिनके स्पष्ट उद्देश्य और कार्यक्रम थे, और उन्होंने एक विखंडित राजनीतिक परिदृश्य के बीच संरचित दृष्टिकोण के लिए साइमन आयोग से भी मान्यता प्राप्त की।
संक्षेप में, स्वराज पार्टी की विरासत उपनिवेशी संस्थाओं के साथ उसकी रणनीतिक भागीदारी, जिम्मेदार सरकार के लिए वकालत, और स्वतंत्रता की लड़ाई के एक महत्वपूर्ण चरण के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन को बनाए रखने और पुनर्जीवित करने में उसकी भूमिका में निहित है।
साइमन आयोग
साइमन आयोग
ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में साइमन आयोग की नियुक्ति ने भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, जिससे व्यापक विरोध और अंततः विधायी परिवर्तन हुए। यहाँ इसका संक्षिप्त विवरण है:

1. गठन और संरचना
- पृष्ठभूमि: 1927 में, ब्रिटिश सरकार ने 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए साइमन आयोग की नियुक्ति की। महत्वपूर्ण रूप से, आयोग के सभी सात सदस्य अंग्रेज थे, जिसने भारतीय राजनीतिक दलों से तत्काल आलोचना को जन्म दिया।
2. व्यापक विरोध
- भारतीय प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति: आयोग में भारतीय सदस्यों की कमी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों सहित विभिन्न राजनीतिक गुटों से निंदा को आकर्षित किया, क्योंकि इसे भारतीय दृष्टिकोण और हितों की अनदेखी के रूप में देखा गया।
- देशव्यापी विरोध प्रदर्शन: 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग के बंबई आगमन पर, देशभर में एक सामान्य हड़ताल का आयोजन किया गया। आयोग का स्वागत काले झंडों और 'साइमन वापस जाओ' के नारे के साथ किया गया, जो भारतीयों के बीच व्यापक असंतोष को दर्शाता है।
- लाहौर में दुखद घटना: 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक बड़ी एंटी-साइमन आयोग डेमोंस्ट्रेशन हिंसक हो गई, जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया। लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आईं और एक महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसने जनता के आक्रोश को और बढ़ा दिया।
3. रिपोर्ट का प्रकाशन और विधायी निहितार्थ
- साइमन आयोग की सिफारिशें: साइमन आयोग की रिपोर्ट, जो मई 1930 में प्रकाशित हुई, ने डायार्की प्रणाली की विफलता को स्वीकार किया और एक वैकल्पिक के रूप में स्वायत्त सरकार की स्थापना की सिफारिश की।
- विधायी प्रभाव: साइमन आयोग की सिफारिशें 1935 के भारत सरकार अधिनियम के मसौदे का आधार बनीं, जो भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण विधायी मील का पत्थर था।
नेहरू रिपोर्ट
नेहरू समिति का भारत के लिए संविधान तैयार करने का प्रयास राजनीतिक आत्म-निर्णय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यहाँ इसके कार्यवाहियों और परिणामों का एक अवलोकन प्रस्तुत है:
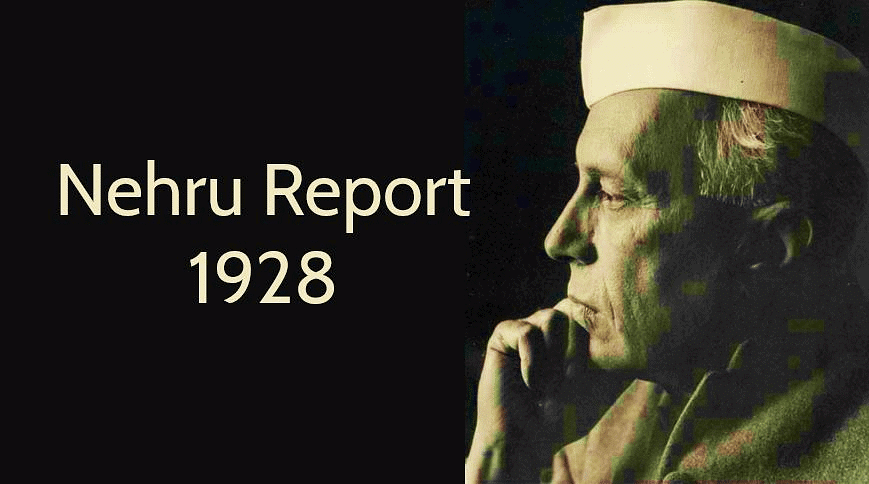
- लॉर्ड बर्केनहेड द्वारा शुरुआत: लॉर्ड बर्केनहेड की चुनौती का जवाब देते हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 28 फरवरी, 1928 को सभी दलों की बैठक बुलाई ताकि एक ऐसा संविधान तैयार किया जा सके जो सभी के लिए स्वीकार्य हो।
- मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता: आठ सदस्यों की एक समिति, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की, को भारत के भविष्य के संविधान का खाका तैयार करने का कार्य सौंपा गया। इसमें तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम, और सुभाष चंद्र बोस जैसे प्रमुख सदस्य शामिल थे।
2. मुख्य सिफारिशें
- डोमिनियन स्थिति: नेहरू समिति की रिपोर्ट ने भारत के संविधान के विकास में अगले कदम के रूप में डोमिनियन स्थिति की सिफारिश की, जो आत्म-शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
- जिम्मेदार सरकार और प्रांतीय स्वायत्तता: रिपोर्ट में केंद्र में पूरी जिम्मेदार सरकार के साथ-साथ प्रांतों को स्वायत्तता देने की सिफारिश की गई, जिससे केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन सुनिश्चित हो सके।
- द्व chambersीय विधानमंडल: रिपोर्ट में केंद्र में द्व chambersीय विधानमंडल की स्थापना की सिफारिश की गई, जिसका उद्देश्य प्रतिनिधित्व और शासन का संतुलित प्रणाली बनाना था।
- अल्पसंख्यक अधिकारों पर ध्यान: रिपोर्ट में अल्पसंख्यक अधिकारों पर एक अलग अध्याय शामिल किया गया, इसके साथ ही मौलिक अधिकारों की गणना की गई, जो समिति की समावेशी शासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
3. चुनौतियाँ और विरोध
- सभी दलों के सम्मेलन में टकराव: कोलकाता में सभी दलों के सम्मेलन में रिपोर्ट पेश करते समय, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों, जिनका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, और हिंदू महासभा के M.R. जयकर के बीच तनाव बढ़ गया। जिन्ना की केंद्रीय विधान मंडलों में मुसलमानों के लिए कुल सीटों का एक तिहाई मांगने के कारण एक हिंसक टकराव हुआ और उनके प्रस्तावित संशोधनों का बाद में खारिज कर दिया गया।
- सहमति प्राप्त करने में असफलता: विभिन्न दृष्टिकोणों को समायोजित करने के प्रयासों के बावजूद, नेहरू समिति की रिपोर्ट सहमति प्राप्त करने में असफल रही, मुख्यतः जिन्ना और मुस्लिम लीग के विरोध के कारण। रिपोर्ट एक प्रारंभिक दस्तावेज बनकर रह गई।
4. प्रतिक्रिया और मुस्लिम लीग के चौदह बिंदु
- जिन्ना का असहमति: मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम हितों के लिए इस रिपोर्ट को हानिकारक मानते हुए, मुसलमानों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया, जहां उन्होंने मुस्लिम लीग की मांगों के रूप में चौदह बिंदुओं को प्रस्तुत किया, जिसमें किसी भी भविष्य के संवैधानिक ढांचे में मुसलमानों के लिए सुरक्षा और प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर जोर दिया।
अंत में, जबकि नेहरू समिति के प्रयास संवैधानिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थे, विभिन्न हितों, विशेष रूप से मुस्लिम लीग के हितों को सुलझाने में उनकी असमर्थता ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य की जटिलताओं और विविध समाज में सहमति बनाने की चुनौतियों को उजागर किया।
जिन्ना के चौदह बिंदु
M.A. जिन्ना का मार्च 1929 में दिल्ली में मुस्लिम लीग की बैठक में चौदह बिंदुओं का प्रस्तुतिकरण मुख्य मांगों को रेखांकित करता है, जो भारत के भविष्य के प्रशासन के ढांचे में मुस्लिम प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हैं। यहाँ बिंदुओं का विश्लेषण है:
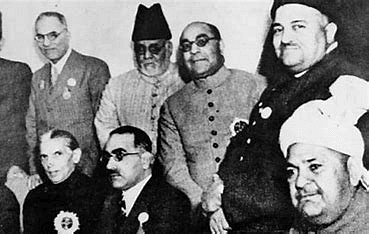
1. संघीय प्रणाली और प्रांतीय स्वायत्तता: संघीय प्रणाली और संविधान की आवश्यकता पर जोर दिया, जहां प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जिससे विकेंद्रीकृत शासन सुनिश्चित हो सके।
2. अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व: सभी विधायिकाओं और चुने गए निकायों में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों, के लिए उचित प्रतिनिधित्व की वकालत की गई, ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके।
3. प्रांतों के लिए समान स्वायत्तता: सभी प्रांतों को समान स्वायत्तता देने की मांग की गई, जिससे समान उपचार और शासन संरचनाएँ सुनिश्चित हो सकें।
4. मुस्लिम प्रतिनिधित्व केंद्रीय विधायिका में: मांग की गई कि केंद्रीय विधायिका में मुस्लिम प्रतिनिधित्व एक-तिहाई से कम नहीं होना चाहिए, ताकि उनकी भागीदारी और प्रभाव सुनिश्चित हो सके।
5. सामुदायिक प्रतिनिधित्व की निरंतरता: यह स्पष्ट किया गया कि जब तक संविधान में मुसलमानों के अधिकारों और हितों की उचित सुरक्षा नहीं की जाती, तब तक मतदाता प्रणाली के माध्यम से सामुदायिक प्रतिनिधित्व की निरंतरता आवश्यक है।
6. मुस्लिम बहुलता वाले प्रांतों का संरक्षण: पंजाब, बंगाल और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत जैसे महत्वपूर्ण प्रांतों में मुस्लिम बहुलता के संरक्षण पर जोर दिया गया, ताकि उनके जनसंख्यात्मक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक प्रभाव की रक्षा की जा सके।
7. सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता: सभी समुदायों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता देने की वकालत की गई, ताकि विश्वास और आचार की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके।
8. अल्पसंख्यक वीटो शक्ति: प्रस्तावित किया गया कि किसी भी निर्वाचित निकाय में कोई भी विधेयक तब तक पारित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उस निकाय के किसी भी समुदाय के तीन-चौथाई सदस्य उसका विरोध न करें, जो अल्पसंख्यक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है।
9. सिंध का बंबई प्रेसीडेंसी से विभाजन: सिंध को बंबई प्रेसीडेंसी से अलग करने का सुझाव दिया गया, प्रशासनिक स्वायत्तता और प्रतिनिधित्व का समर्थन किया गया।
10. उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांतों और बलूचिस्तान में सुधार: उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांतों और बलूचिस्तान में सुधारों की मांग की गई ताकि विकास और प्रतिनिधित्व में समानता सुनिश्चित की जा सके।
11. सेवाओं में पर्याप्त मुस्लिम प्रतिनिधित्व: सभी सरकारी सेवाओं में मुसलमानों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग की गई, ताकि उनकी भागीदारी और प्रभाव सुनिश्चित हो सके।
12. मुस्लिम संस्कृति की सुरक्षा: मुस्लिम संस्कृति, धरोहर और पहचान की सुरक्षा के लिए उचित उपायों की वकालत की गई।
13. मंत्रिमंडल में मुस्लिम समावेश: यह निर्धारित किया गया कि कोई भी मंत्रिमंडल बिना कम से कम एक-तिहाई मुस्लिम मंत्रियों के नहीं बनाया जाएगा, ताकि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में मुस्लिम भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
14. संघीय राज्यों की सहमति से संवैधानिक परिवर्तन: यह asserted किया गया कि संविधान में कोई भी परिवर्तन संघीय राज्यों की सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए, ताकि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और संवैधानिक संशोधनों में सहमति सुनिश्चित हो सके।
M.A. जिन्ना के चौदह अंक मुस्लिमों के लिए भारत के भविष्य के शासन के ढांचे के भीतर महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मांगों का एक व्यापक सेट था। इन अंकों ने संघीयता, अल्पसंख्यक अधिकारों और समान प्रतिनिधित्व के महत्व को उजागर किया, जो स्वतंत्रता की व्यापक संघर्ष में साम्प्रदायिक तनावों को संबोधित करने की जटिलताओं और चुनौतियों को दर्शाता है।
लाहौर सत्र
जवाहरलाल नेहरू के गतिशील नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने अपने ऐतिहासिक लाहौर सत्र का आयोजन किया, जो भारत की स्वतंत्रता की संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। यहाँ प्रमुख घटनाओं का एक अवलोकन है:

1. पूरना स्वराज की घोषणा: जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, INC के लाहौर सत्र ने 19 दिसंबर 1929 को पूरना स्वराज (पूर्ण स्वतंत्रता) को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया। यह साहसी घोषणा ब्रिटिश उपनिवेशी शासन से भारत के लिए पूर्ण संप्रभुता की मांग की दिशा में एक निर्णायक बदलाव को दर्शाती है।
2. त्रिकोणीय ध्वज का अपनाना: लाहौर सत्र में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने त्रिकोणीय ध्वज को भारत की राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता की आकांक्षा का प्रतीक माना। यह ध्वज, जो भारत की एकता और विविधता का प्रतिनिधित्व करता है, 31 दिसंबर 1929 को समारोहपूर्वक फहराया गया, जो भारतीयों के बीच प्रतिरोध और एकता की भावना का प्रतीक था।
3. पहला स्वतंत्रता दिवस: लाहौर सत्र ने 26 जनवरी 1930 को पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में निर्धारित किया, जिसे हर वर्ष मनाया जाएगा ताकि भारत की संप्रभुता और आत्म-शासन प्राप्त करने की अडिग प्रतिबद्धता की याद दिलाई जा सके। इस दिन को पूर्ण स्वराज की घोषणा और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाने के लिए चुना गया।
4. प्रतीकवाद और महत्व
- एकता का प्रतीक: पूर्ण स्वराज की घोषणा और त्रिकोणीय ध्वज का अपनाना भारतीय लोगों की स्वतंत्रता की खोज में एकता और संकल्प का प्रतीक था, जो भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक विभाजन को पार करता है।
- स्वतंत्रता संघर्ष में मील का पत्थर: लाहौर सत्र ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया, जिसने आंदोलन के लिए स्पष्ट दृष्टि और दिशा प्रदान की, और लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
5. विरासत और प्रभाव
- भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा: लाहौर सत्र और इसकी घोषणाएँ भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं, जो स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों और स्वतंत्रता और न्याय की प्राप्ति में प्रदर्शित संकल्प की याद दिलाती हैं।
- स्वतंत्रता की नींव: लाहौर सत्र में पारित प्रस्तावों ने बाद के आंदोलनों की नींव रखी, जिसमें नागरिक अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन शामिल हैं, जो अंततः 1947 में भारत की स्वतंत्रता की ओर ले गए।
अंत में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में INC का लाहौर सत्र भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में एक निर्णायक क्षण था, जो पूर्ण स्वराज को प्राप्त करने की राष्ट्र की अडिग प्रतिबद्धता का प्रतीक है और उपनिवेशी शासन से मुक्ति की दिशा में अंतिम प्रयास के लिए आधार तैयार करता है।
|
198 videos|620 docs|193 tests
|
















