UPSC Exam > UPSC Notes > भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) UPSC CSE के लिए > विवेक सिंह सारांश: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
विवेक सिंह सारांश: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) | भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) UPSC CSE के लिए PDF Download
जन वितरण प्रणाली (PDS)
भारत में जन वितरण प्रणाली (PDS) का आरंभ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में हुआ जब खाद्यान्न की कमी थी। सरकार ने खाद्य और आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए हस्तक्षेप किया। प्रारंभ में, PDS ने 1960 के दशक में खाद्य की कमी के दौरान, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के युद्धों और इसके बाद के सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। हरित क्रांति और कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ, PDS ने 1970 और 1980 के दशक में जनजातीय क्षेत्रों और उच्च गरीबी वाले क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया।
समय के साथ, PDS सरकार की खाद्य अर्थव्यवस्था प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जो कमी को प्रबंधित करने और खाद्यान्न का वितरण सस्ती कीमतों पर करने के लिए विकसित हुआ है। यह क्रमिक है, जिसका अर्थ है कि यह किसी परिवार को किसी भी वस्तु की संपूर्ण आवश्यकता प्रदान नहीं करता है, बल्कि उन्हें प्रबंधनीय मात्राओं में वितरित करता है। PDS के अंतर्गत वितरित वस्तुओं में मुख्य रूप से गेहूं, चावल, चीनी, और केरोसिन शामिल हैं, जबकि कुछ राज्यों में दालें, खाद्य तेल, आयोडीनयुक्त नमक, मसाले, आदि भी वितरित किए जाते हैं।
PDS का विकास:
अंत्योदय अन्न योजना के तहत, पात्र परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें गेहूं की कीमत ₹2 प्रति किलोग्राम और चावल की कीमत ₹3 प्रति किलोग्राम है। यह कार्यक्रम समाज के सबसे वंचित वर्गों के बीच भूख और कुपोषण की समस्या को संबोधित करने का उद्देश्य रखता है, उन्हें सस्ती खाद्य का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करके।
वर्षों के दौरान, AAY को अधिक परिवारों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है, जो सरकार की सबसे गरीब जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा में सुधार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह योजना भारत में व्यापक जन वितरण प्रणाली (PDS) का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या वर्गों को सब्सिडी दरों पर खाद्यान्न वितरित करना है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग शामिल हैं।
AAY भारत के भूख से लड़ने और यह सुनिश्चित करने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि सभी नागरिकों को पर्याप्त और पोषक खाद्य उपलब्ध हो, विशेष रूप से एक ऐसे देश में जहाँ आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहा है।
पृष्ठभूमि
लक्षित जन वितरण प्रणाली (TPDS) को और अधिक प्रभावी बनाने और सबसे कमजोर जनसंख्या की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए, सरकार ने दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना (AAY) पेश की। यह पहल 2000 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के निष्कर्षों पर आधारित थी, जिसमें यह संकेत मिला कि भारतीय जनसंख्या का लगभग 5% दो समय के भोजन को सुरक्षित करने में संघर्ष कर रहा था, जो देश में भूख की उपस्थिति को उजागर करता है।
AAY को प्रारंभ में 1 करोड़ (10 मिलियन) सबसे गरीब परिवारों को लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया था, उन्हें प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न अत्यधिक सब्सिडी दरों पर प्रदान करने के लिए—गेहूं के लिए ₹2 प्रति किलोग्राम और चावल के लिए ₹3 प्रति किलोग्राम। यह योजना TPDS को अधिक केंद्रित और लक्षित बनाने का लक्ष्य रखती थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि सबसे कमजोर परिवारों को उचित खाद्य आपूर्ति प्राप्त हो।
समय के साथ, AAY को अतिरिक्त 1.5 करोड़ (15 मिलियन) परिवारों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है, जो सरकार की सबसे गरीब जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा में सुधार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। AAY के तहत, खाद्यान्न केंद्रीय मुद्दा मूल्य (CIP) पर वितरित किया जाता है, जिसमें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं होता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि लाभार्थी सब्सिडी दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करें।
यह कार्यक्रम भारत में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है और यह सुनिश्चित करता है कि सबसे कमजोर जनसंख्या आवश्यक खाद्य वस्तुओं तक पहुँच प्राप्त करें, इस प्रकार देश में भूख और कुपोषण की महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करते हुए।
कार्यान्वयन
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) लक्षित जन वितरण प्रणाली (TPDS) के अंतर्गत काम करती है, जिसमें खाद्यान्न की अंतः खुदरा कीमत संबंधित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों (UTs) द्वारा निर्धारित की जाती है। मूल्य निर्धारण में थोक और खुदरा मार्जिन, परिवहन शुल्क, स्थानीय कर और अन्य शुल्क जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है।
TPDS के तहत, राज्यों को निर्धनता रेखा (BPL) वाले परिवारों को खाद्यान्न वितरित करने की आवश्यकता होती है, जिसकी कीमत केंद्रीय मुद्दा मूल्य (CIP) से 50 पैसे प्रति किलोग्राम अधिक नहीं होनी चाहिए। AAY के अंतर्गत परिवारों के लिए, खुदरा मूल्य CIP पर बनाए रखा जाता है, जो गेहूं के लिए ₹2 प्रति किलोग्राम और चावल के लिए ₹3 प्रति किलोग्राम है। गरीबी रेखा से ऊपर (APL) परिवारों और TPDS के अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिससे राज्यों को अपनी विवेकानुसार CIP से ऊपर खुदरा मूल्य निर्धारित करने की अनुमति मिलती है।
AAY यह सुनिश्चित करता है कि सबसे कमजोर परिवारों को आवश्यक खाद्यान्न सब्सिडी दरों पर प्राप्त हो, जो सबसे गरीब जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण समर्थन में योगदान देता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013
अवलोकन: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, पूर्व के लक्षित जन वितरण प्रणाली (TPDS) योजना का सुधार और विस्तार है। इसका उद्देश्य जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, जो भारत में लगभग 84 करोड़ लोगों को कवर करता है।
कवरेज: यह अधिनियम 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या पर लागू होता है, कुल मिलाकर लगभग 84 करोड़ लोग। इसके लिए लगभग 60 मिलियन टन (MT) खाद्यान्न की आवश्यकता है, जिसकी लागत सरकार को लगभग ₹1.90 लाख करोड़ है। अधिनियम से पहले, TPDS ने लगभग 40 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया।
लाभार्थी परिवारों की श्रेणियाँ: NFSA के तहत परिवारों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
केंद्रीय सरकार प्रत्येक राज्य के लिए अधिनियम के तहत प्रतिशत कवरेज निर्धारित करती है, ग्रामीण जनसंख्या के लिए 75% और शहरी जनसंख्या के लिए 50% के सीमाओं के भीतर। राज्य सरकारें विशेष दिशानिर्देशों के आधार पर AAY और प्राथमिकता श्रेणियों के तहत कवर किए जाने वाले परिवारों की पहचान करती हैं।
अस्थायी प्रावधान (2023): केंद्रीय सरकार ने NFSA 2013 के तहत 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक खाद्यान्न (चावल, गेहूं, और मोटे अनाज) मुफ्त में प्रदान किए। यह प्रावधान समाप्त हो गया है।
अतिरिक्त लाभ: अधिनियम कुछ विशेष समूहों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है:
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत राशन कार्डों की राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी को सक्षम करने के लिए, केंद्रीय सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC) योजना प्रस्तुत की।
ONORC योजना का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सब्सिडी वाले राशन खरीदने की अनुमति देना है।
उदाहरण के लिए, कन्नौज का एक प्रवासी श्रमिक मुंबई में काम की तलाश करते समय जन वितरण प्रणाली (PDS) के लाभों का उपयोग कर सकता है।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC) योजना उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जो लाभार्थियों के राशन कार्ड, आधार नंबर, और देश भर में निर्बाध राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक बिक्री बिंदु (ePoS) प्रणालियों का एकीकरण करती है।
शांता कुमार समिति की सिफारिशें
अगस्त 2014 में, भारत सरकार (GOI) ने शांता कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (HLC) का गठन किया ताकि खाद्य निगम (FCI) को पुनर्गठित करने या बंडल करने के तरीके प्रस्तावित किए जा सकें ताकि परिचालन दक्षता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार हो सके। समिति ने 2015 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। यहाँ प्रमुख सिफारिशें हैं:
![विवेक सिंह सारांश: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) | भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) UPSC CSE के लिए]()

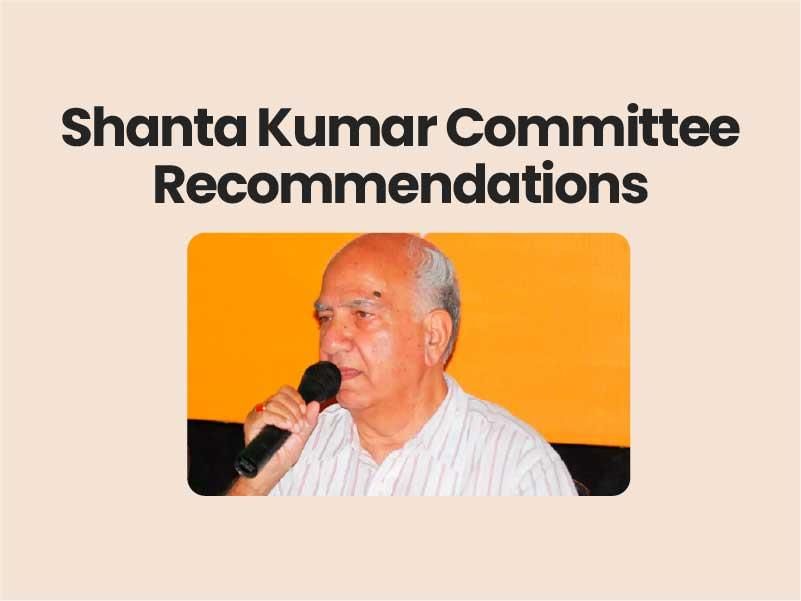

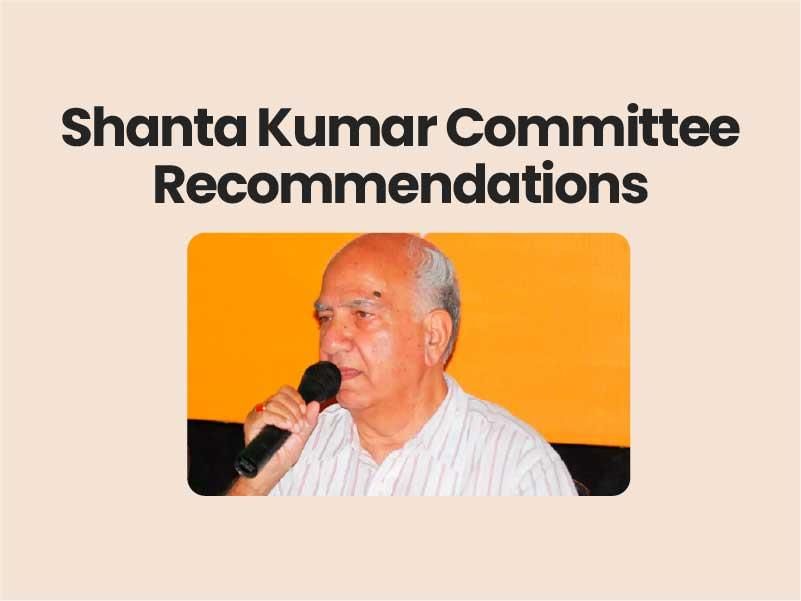
भारत में जन वितरण प्रणाली (PDS) का आरंभ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में हुआ जब खाद्यान्न की कमी थी। सरकार ने खाद्य और आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए हस्तक्षेप किया। प्रारंभ में, PDS ने 1960 के दशक में खाद्य की कमी के दौरान, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के युद्धों और इसके बाद के सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। हरित क्रांति और कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ, PDS ने 1970 और 1980 के दशक में जनजातीय क्षेत्रों और उच्च गरीबी वाले क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया।
समय के साथ, PDS सरकार की खाद्य अर्थव्यवस्था प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जो कमी को प्रबंधित करने और खाद्यान्न का वितरण सस्ती कीमतों पर करने के लिए विकसित हुआ है। यह क्रमिक है, जिसका अर्थ है कि यह किसी परिवार को किसी भी वस्तु की संपूर्ण आवश्यकता प्रदान नहीं करता है, बल्कि उन्हें प्रबंधनीय मात्राओं में वितरित करता है। PDS के अंतर्गत वितरित वस्तुओं में मुख्य रूप से गेहूं, चावल, चीनी, और केरोसिन शामिल हैं, जबकि कुछ राज्यों में दालें, खाद्य तेल, आयोडीनयुक्त नमक, मसाले, आदि भी वितरित किए जाते हैं।
PDS का विकास:
- सामान्य अधिकार योजना: 1992 तक, PDS एक सामान्य अधिकार योजना थी जो सभी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध थी बिना किसी विशेष समूह को लक्षित किए।
- पुनर्गठित PDS (1992): जून 1992 में शुरू किया गया ताकि PDS को मजबूत और सुव्यवस्थित किया जा सके, जिससे इसके पहुंच को दूरदराज और अपठनीय क्षेत्रों में सुधार किया जा सके।
- लक्षित जन वितरण प्रणाली (TPDS) (1997): गरीबों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पेश किया गया, राज्यों को जरूरतमंदों की पहचान करना और खाद्यान्न को पारदर्शी और जिम्मेदारी के साथ उचित मूल्य की दुकानों (FPS) पर वितरित करना आवश्यक था।
- पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से पहचान किए गए गरीबों को खाद्यान्न प्रदान करना।
- उचित मूल्य की दुकानों पर वितरण में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- भूमिहीन कृषि श्रमिकों, सीमांत किसानों और शहरी गरीबों जैसे कमजोर वर्गों को शामिल करना।
अंत्योदय अन्न योजना के तहत, पात्र परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें गेहूं की कीमत ₹2 प्रति किलोग्राम और चावल की कीमत ₹3 प्रति किलोग्राम है। यह कार्यक्रम समाज के सबसे वंचित वर्गों के बीच भूख और कुपोषण की समस्या को संबोधित करने का उद्देश्य रखता है, उन्हें सस्ती खाद्य का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करके।
वर्षों के दौरान, AAY को अधिक परिवारों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है, जो सरकार की सबसे गरीब जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा में सुधार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह योजना भारत में व्यापक जन वितरण प्रणाली (PDS) का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या वर्गों को सब्सिडी दरों पर खाद्यान्न वितरित करना है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग शामिल हैं।
AAY भारत के भूख से लड़ने और यह सुनिश्चित करने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि सभी नागरिकों को पर्याप्त और पोषक खाद्य उपलब्ध हो, विशेष रूप से एक ऐसे देश में जहाँ आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहा है।
पृष्ठभूमि
लक्षित जन वितरण प्रणाली (TPDS) को और अधिक प्रभावी बनाने और सबसे कमजोर जनसंख्या की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए, सरकार ने दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना (AAY) पेश की। यह पहल 2000 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के निष्कर्षों पर आधारित थी, जिसमें यह संकेत मिला कि भारतीय जनसंख्या का लगभग 5% दो समय के भोजन को सुरक्षित करने में संघर्ष कर रहा था, जो देश में भूख की उपस्थिति को उजागर करता है।
AAY को प्रारंभ में 1 करोड़ (10 मिलियन) सबसे गरीब परिवारों को लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया था, उन्हें प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न अत्यधिक सब्सिडी दरों पर प्रदान करने के लिए—गेहूं के लिए ₹2 प्रति किलोग्राम और चावल के लिए ₹3 प्रति किलोग्राम। यह योजना TPDS को अधिक केंद्रित और लक्षित बनाने का लक्ष्य रखती थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि सबसे कमजोर परिवारों को उचित खाद्य आपूर्ति प्राप्त हो।
समय के साथ, AAY को अतिरिक्त 1.5 करोड़ (15 मिलियन) परिवारों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है, जो सरकार की सबसे गरीब जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा में सुधार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। AAY के तहत, खाद्यान्न केंद्रीय मुद्दा मूल्य (CIP) पर वितरित किया जाता है, जिसमें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं होता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि लाभार्थी सब्सिडी दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करें।
यह कार्यक्रम भारत में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है और यह सुनिश्चित करता है कि सबसे कमजोर जनसंख्या आवश्यक खाद्य वस्तुओं तक पहुँच प्राप्त करें, इस प्रकार देश में भूख और कुपोषण की महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करते हुए।
कार्यान्वयन
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) लक्षित जन वितरण प्रणाली (TPDS) के अंतर्गत काम करती है, जिसमें खाद्यान्न की अंतः खुदरा कीमत संबंधित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों (UTs) द्वारा निर्धारित की जाती है। मूल्य निर्धारण में थोक और खुदरा मार्जिन, परिवहन शुल्क, स्थानीय कर और अन्य शुल्क जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है।
TPDS के तहत, राज्यों को निर्धनता रेखा (BPL) वाले परिवारों को खाद्यान्न वितरित करने की आवश्यकता होती है, जिसकी कीमत केंद्रीय मुद्दा मूल्य (CIP) से 50 पैसे प्रति किलोग्राम अधिक नहीं होनी चाहिए। AAY के अंतर्गत परिवारों के लिए, खुदरा मूल्य CIP पर बनाए रखा जाता है, जो गेहूं के लिए ₹2 प्रति किलोग्राम और चावल के लिए ₹3 प्रति किलोग्राम है। गरीबी रेखा से ऊपर (APL) परिवारों और TPDS के अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिससे राज्यों को अपनी विवेकानुसार CIP से ऊपर खुदरा मूल्य निर्धारित करने की अनुमति मिलती है।
AAY यह सुनिश्चित करता है कि सबसे कमजोर परिवारों को आवश्यक खाद्यान्न सब्सिडी दरों पर प्राप्त हो, जो सबसे गरीब जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण समर्थन में योगदान देता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013
अवलोकन: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, पूर्व के लक्षित जन वितरण प्रणाली (TPDS) योजना का सुधार और विस्तार है। इसका उद्देश्य जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, जो भारत में लगभग 84 करोड़ लोगों को कवर करता है।
कवरेज: यह अधिनियम 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या पर लागू होता है, कुल मिलाकर लगभग 84 करोड़ लोग। इसके लिए लगभग 60 मिलियन टन (MT) खाद्यान्न की आवश्यकता है, जिसकी लागत सरकार को लगभग ₹1.90 लाख करोड़ है। अधिनियम से पहले, TPDS ने लगभग 40 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया।
लाभार्थी परिवारों की श्रेणियाँ: NFSA के तहत परिवारों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY):
आवंटन: प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न।
मूल्य निर्धारण: चावल के लिए ₹3/किलोग्राम, गेहूं के लिए ₹2/किलोग्राम, और मोटे अनाज के लिए ₹1/किलोग्राम। - प्राथमिकता परिवार:
आवंटन: प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न।
मूल्य निर्धारण: AAY के समान (चावल के लिए ₹3/किलोग्राम, गेहूं के लिए ₹2/किलोग्राम, और मोटे अनाज के लिए ₹1/किलोग्राम)।
केंद्रीय सरकार प्रत्येक राज्य के लिए अधिनियम के तहत प्रतिशत कवरेज निर्धारित करती है, ग्रामीण जनसंख्या के लिए 75% और शहरी जनसंख्या के लिए 50% के सीमाओं के भीतर। राज्य सरकारें विशेष दिशानिर्देशों के आधार पर AAY और प्राथमिकता श्रेणियों के तहत कवर किए जाने वाले परिवारों की पहचान करती हैं।
अस्थायी प्रावधान (2023): केंद्रीय सरकार ने NFSA 2013 के तहत 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक खाद्यान्न (चावल, गेहूं, और मोटे अनाज) मुफ्त में प्रदान किए। यह प्रावधान समाप्त हो गया है।
अतिरिक्त लाभ: अधिनियम कुछ विशेष समूहों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है:
- गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ:
गर्भावस्था के दौरान और childbirth के बाद छह महीनों तक स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से मुफ्त भोजन।
किस्तों में ₹6,000 की वित्तीय सहायता। - 6 महीने से 6 वर्ष के बच्चे:
स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्रों पर मुफ्त भोजन। - 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे:
स्कूलों में मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है।
- महिला सशक्तिकरण: पात्र परिवारों में, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे बड़ी महिला को राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए परिवार का मुखिया माना जाएगा। यदि परिवार में 18 वर्ष से अधिक कोई महिला नहीं है, और केवल 18 वर्ष से कम की एक महिला है, तो सबसे बड़े पुरुष सदस्य को राशन कार्ड प्राप्त होगा। जब महिला 18 वर्ष की हो जाएगी, तब उसे राशन कार्ड प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- शिकायत निवारण तंत्र: प्रत्येक राज्य सरकार को एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें कॉल सेंटर, हेल्पलाइन नंबर, नामित नोडल अधिकारी, या अन्य निर्धारित तरीके शामिल हो सकते हैं।
हर राज्य सरकार द्वारा एक राज्य खाद्य आयोग का गठन किया जाना चाहिए जो अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करेगा। यह आयोग एक अध्यक्ष और पांच अन्य सदस्यों का होगा। - केंद्रीय और राज्य सरकारों की जिम्मेदारियाँ: राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के निर्धारित डिपो से केंद्रीय मुद्दा मूल्य (CIP) पर खाद्यान्न प्राप्त करने और उचित मूल्य की दुकानों (FPS) पर वितरण के लिए अंतर-राज्य आवंटन का आयोजन करने की जिम्मेदार हैं। उन्हें निर्दिष्ट कीमतों पर हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न का वास्तविक वितरण सुनिश्चित करना होगा।
केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को अंतर-राज्य आंदोलन, खाद्यान्न के हैंडलिंग, और FPS डीलरों को दिए गए मार्जिन से संबंधित खर्चों को कवर करने में सहायता करेगी, जैसा कि निर्धारित मानदंडों के अनुसार। - विविध प्रावधान: इस अधिनियम के प्रावधान केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को अन्य खाद्य-आधारित कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने या तैयार करने से नहीं रोकेंगे।
राज्य सरकार अपनी संसाधनों से इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए लाभों से अधिक लाभ देने वाली खाद्य या पोषण आधारित योजनाओं को जारी रख सकती है या तैयार कर सकती है।
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के तहत हकदार होने के दावे के लिए उत्तरदायी होंगी, सिवाय युद्ध, बाढ़, सूखा, आग, चक्रवात, भूकंप के मामलों के जो ऐसे व्यक्ति को खाद्यान्न या भोजन की नियमित आपूर्ति प्रभावित करते हैं।
केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण, खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को फायदेमंद कीमतों, इनपुट्स, ऋण, सिंचाई, बिजली, फसल बीमा आदि के माध्यम से जीवनयापन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेंगे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत राशन कार्डों की राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी को सक्षम करने के लिए, केंद्रीय सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC) योजना प्रस्तुत की।
ONORC योजना का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सब्सिडी वाले राशन खरीदने की अनुमति देना है।
उदाहरण के लिए, कन्नौज का एक प्रवासी श्रमिक मुंबई में काम की तलाश करते समय जन वितरण प्रणाली (PDS) के लाभों का उपयोग कर सकता है।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC) योजना उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जो लाभार्थियों के राशन कार्ड, आधार नंबर, और देश भर में निर्बाध राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक बिक्री बिंदु (ePoS) प्रणालियों का एकीकरण करती है।
शांता कुमार समिति की सिफारिशें
अगस्त 2014 में, भारत सरकार (GOI) ने शांता कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (HLC) का गठन किया ताकि खाद्य निगम (FCI) को पुनर्गठित करने या बंडल करने के तरीके प्रस्तावित किए जा सकें ताकि परिचालन दक्षता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार हो सके। समिति ने 2015 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। यहाँ प्रमुख सिफारिशें हैं:
- खरीद: FCI को गेहूं, धान, और चावल की सभी खरीद गतिविधियों को उन राज्य सरकारों को स्थानांतरित करना चाहिए जिन्होंने पर्याप्त अनुभव प्रदर्शित किया है और खरीद के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा विकसित किया है।
FCI केवल उन राज्य सरकारों से अधिशेष भंडार स्वीकार करेगा जिनकी अपनी आवश्यकताओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पूरा किया गया है, जो कि घाटे वाले राज्यों में वितरण के लिए है। - जन वितरण प्रणाली (PDS) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA): HLC वर्तमान में NFSA के तहत 67 प्रतिशत जनसंख्या की कवरेज का पुनर्मूल्यांकन करने की सिफारिश करती है, यह सुझाव देते हुए कि इसे लगभग 40 प्रतिशत तक कम किया जाए, जो अभी भी गरीबी रेखा (BPL) के परिवारों और उससे ऊपर कुछ को कवर करेगा।
अनाज वितरण की समस्या को संबोधित करने के लिए, समिति ने सुझाव दिया कि BPL परिवारों को प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए वर्तमान 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के मुकाबले 7 किलोग्राम अनाज मिलना चाहिए।
प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए अनाज वितरण की कीमत को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें 50 प्रतिशत MSP की दर की सिफारिश की गई है। यह समायोजन सरकारी खजाने पर अत्यधिक वित्तीय दबाव से बचने और कृषि और खाद्य क्षेत्रों में निरंतर निवेश सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
HLC ने PDS के भीतर नकद हस्तांतरण की क्रमिक शुरुआत का भी समर्थन किया है, जिससे दक्षता और लचीलापन बढ़ सके। - भंडारण और आंदोलन:
FCI को अपनी भंडारण गतिविधियों को केंद्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम, और निजी क्षेत्र जैसी विभिन्न एजेंसियों को आउटसोर्स करना चाहिए।
FCI के कई पुराने पारंपरिक भंडारों को निजी क्षेत्र और अन्य भंडारण एजेंसियों की मदद से सिलो में परिवर्तित किया जा सकता है।
सभी सिलो और पारंपरिक भंडारों में बेहतर यांत्रिकी की आवश्यकता है।
अनाज के आंदोलन को धीरे-धीरे कंटेनर में परिवर्तित करने की आवश्यकता है ताकि परिवहन हानि को कम किया जा सके और मोड़ने का समय सुधारा जा सके।
यह रेलवे साइडिंग पर अधिक यांत्रिक सुविधाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। - बफर भंडारण और तरलता नीति: एक पारदर्शी तरलता नीति आवश्यक है, जिसे FCI को बफर मानकों से अधिक अधिशेष भंडार का सामना करने पर स्वचालित रूप
- समय के साथ, PDS (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) सरकार की खाद्य अर्थव्यवस्था प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जो कमी को प्रबंधित करने और खाद्यान्नों का वितरण सस्ती कीमतों पर करने के लिए विकसित हुआ है।
- यह क्रमिक है, जिसका अर्थ है कि यह किसी भी वस्तु की पूरी आवश्यकता को किसी परिवार को प्रदान नहीं करता है, बल्कि इसे प्रबंधनीय मात्रा में वितरित करता है।
- PDS के तहत वितरित किए जाने वाले मुख्य वस्तुएं हैं: गेहूं, चावल, चीनी, और केरोसिन, जबकि कुछ राज्यों में दालें, खाद्य तेल, आयोडाइज्ड नमक, मसाले आदि भी वितरित किए जाते हैं।
सामान्य अधिकार योजना: 1992 से पहले, PDS एक सामान्य अधिकार योजना थी जो सभी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध थी, बिना किसी विशेष समूह को लक्षित किए।
- नवीनीकृत PDS (1992): जून 1992 में लॉन्च किया गया था ताकि PDS को मजबूत और सुव्यवस्थित किया जा सके, जिससे इसकी पहुंच दूरदराज और कठिन क्षेत्रों में बेहतर हो सके।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) (1997): गरीबों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पेश की गई, जिसमें राज्यों को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से गरीबों को खाद्यान्न वितरित करने के लिए आवश्यक किया गया।

अतिरिक्त लाभ: अधिनियम विशेष समूहों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है:
- महिला सशक्तिकरण: महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपाय।
- शिकायत निवारण तंत्र: नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए स्पष्ट और प्रभावी तंत्र की स्थापना।
- केंद्रीय और राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां: सभी संबंधित सरकारी निकायों की जिम्मेदारियों का स्पष्ट विवरण।
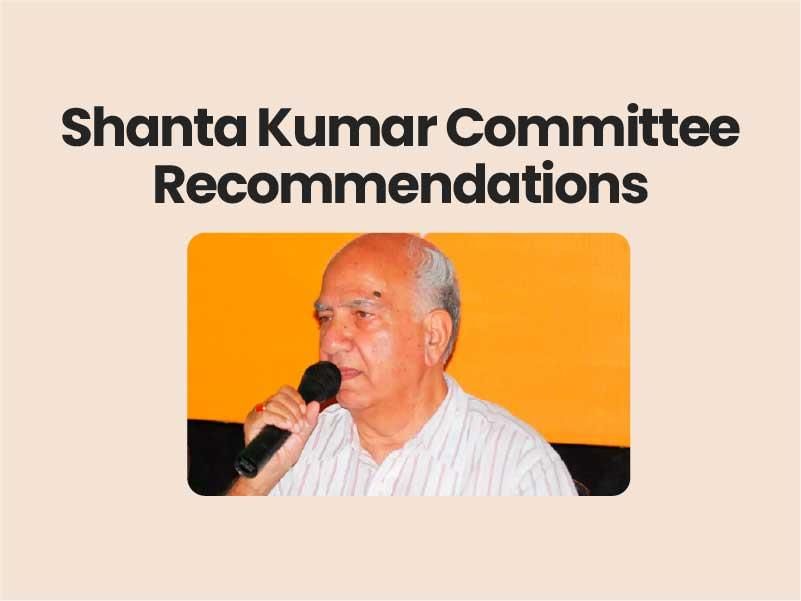

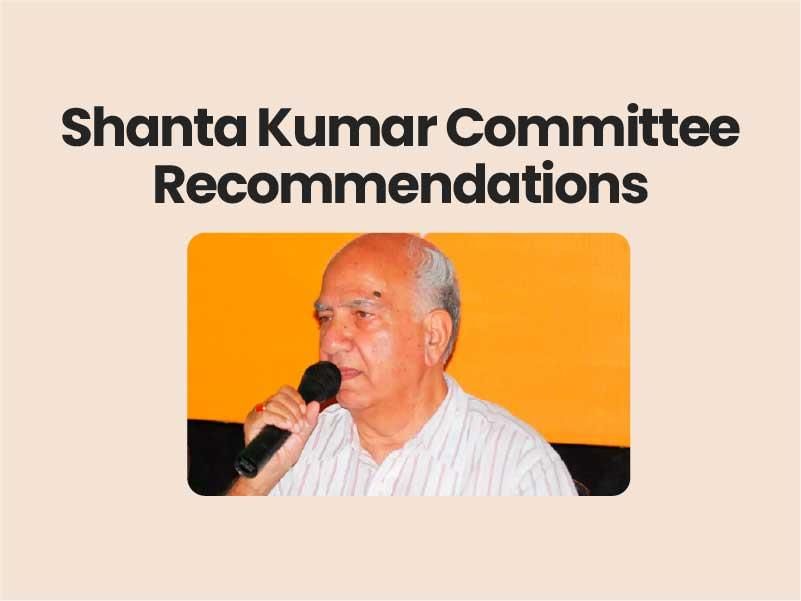
The document विवेक सिंह सारांश: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) | भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) UPSC CSE के लिए is a part of the UPSC Course भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) UPSC CSE के लिए.
All you need of UPSC at this link: UPSC
|
289 docs|166 tests
|
Related Searches





















