वेदिक काल: राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download
प्रारंभिक वेदिक युग (1500-1000 ई. पू.) में राजनीतिक जीवन
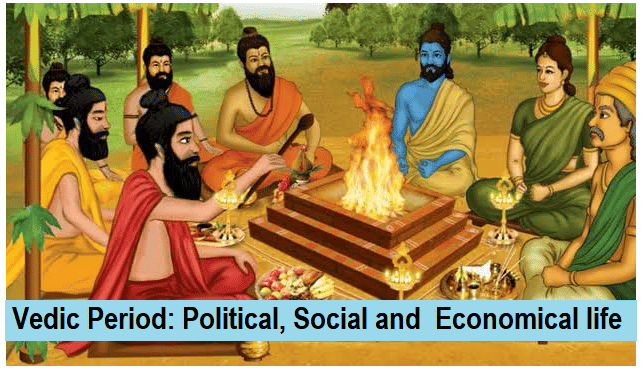
प्रशासनिक विभाजन
- प्रारंभिक राजनीतिक इकाई कुल या परिवार था।
- कई परिवार कुल के आधार पर एकजुट होकर एक गांव बनाते थे, जिसे ग्राम कहा जाता था।
- एक ग्राम के नेता को ग्रामणी कहा जाता था।
- गांवों के समूह को एक बड़ी इकाई विशु या जिला कहा जाता था, जिसका नेतृत्व विशयपति करता था।
- उच्चतम राजनीतिक इकाई जना या जनजाति थी, जिसमें भरत, मत्स्य, यादु, और पुरु जैसी विभिन्न जनजातीय राज्य शामिल थे।
- राज्य का प्रमुख राजन या राजा के रूप में जाना जाता था।
शासन का रूप
- राजनीतिक प्रणाली जनजातीय थी, जिसमें एक मजबूत सैन्य उपस्थिति थी।
- किसी भी नागरिक प्रणाली या भौगोलिक प्रशासन का अभाव था, क्योंकि लोग लगातार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास कर रहे थे।
- प्रशासनिक संरचना जनजातीय प्रमुख के चारों ओर केंद्रित थी, जिसे राजन कहा जाता था।
राजा/राजन/मुखिया
- राजा जनजाति के भीतर एक प्रमुख स्थान रखता था, जिसे अक्सर अभिषेक समारोह के दौरान एक पुरोहित द्वारा नियुक्त किया जाता था।
- हालांकि राजा की स्थिति वंशानुगत प्रतीत होती थी, राजन को जनजातीय संगठन पर विचार करना पड़ता था और उसके पास पूर्ण शक्ति नहीं होती थी।
- राजा के चुनाव के संकेत समिति नामक जनजातीय सभा द्वारा होने के थे।
- राजा की जिम्मेदारी जनजाति, उसके मवेशियों की सुरक्षा, युद्ध में नेतृत्व करना, और जनजाति के लिए अनुष्ठान करना थी।
- उसे इंद्र में वीरता, मित्र में दया, और वरुण में सदाचार का प्रतीक माना जाता था।
- कानून और व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी थी, जिसे अक्सर पुरोहित द्वारा समर्थन प्राप्त होता था।
अधिकारी
- राजा को विभिन्न अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की गई, जिनमें पुरोहित (पादरी), सेनानी (जनरल), ग्रामणी (गाँव के मुखिया) और जासूस शामिल थे। पुरोहित एक महत्वपूर्ण राज्य अधिकारी था, जिसमें वशिष्ठ और विष्वामित्र जैसे पादरी ऋग्वेदिक काल के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। पादरी प्रमुख को कार्रवाई के लिए प्रेरित करते थे और पुरस्कार के रूप में गाय और महिला दासियों के बदले में उपलब्धियों का जश्न मनाते थे।
सेनानी
- सेनानी, या सेना का कमांडर, एक और महत्वपूर्ण अधिकारी था। सेना में पत्ति (पैदल सेना) और रथिन्स (रथ) शामिल थे। सेना या सेना एक स्थायी बल नहीं थी, बल्कि युद्ध के लिए सक्षम जनजातियों के लोगों का समूह था। तक्षन, बढ़ई, और रथकार, रथ बनाने वाले, रथ उत्पादन के लिए जिम्मेदार थे। सैनिकों ने धनुष, तीर, तलवार, कुल्हाड़ी और भाले जैसे हथियारों का उपयोग किया। कोई आधिकारिक कर संग्रहकर्ता नहीं था; इसके बजाय, लोग विशेष अवसरों पर bali नामक योगदान स्वेच्छा से देते थे। ऋग्वेद में न्याय का प्रशासन करने वाले किसी आधिकारिक का उल्लेख नहीं है। इसके बावजूद, समाज में चोर और डकैती जैसी समस्याएँ थीं, विशेष रूप से गायों की चोरी। जासूसों को ऐसे विरोधी सामाजिक गतिविधियों की निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया गया था। जो अधिकारी बड़े गौचर क्षेत्रों की देखरेख करता था, उसे व्रजपति कहा जाता था, जो परिवार के मुखिया या लड़ाई की टोली को युद्ध में ले जाता था।
लोक Assemblies
- राजन का समर्थन जनजातीय सभाओं द्वारा किया गया, जैसे सभा, समिति, विदाथ, गण, और परिषद। सभा संभवतः बुजुर्गों का एक परिषद थी, जबकि समिति पूरी जनसंख्या की एक सामान्य सभा थी। ये सभाएँ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करती थीं, जिसमें युद्ध, युद्ध के लूट के वितरण, न्यायिक मामले, और धार्मिक गतिविधियाँ शामिल थीं। ये प्रमुखों के अधिकारों को सीमित करने का कार्य करती थीं। दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं को भी सभा और समिति की चर्चाओं में भाग लेने की अनुमति थी।
उपरांत वेदिक युग में परिवर्तन
उपरांत वेदिक काल के दौरान, समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसमें एक पशुपालन जीवनशैली से स्थायी कृषि समाज की ओर बदलाव शामिल है। कृषि एक केंद्रीय गतिविधि बन गई, जो स्थायी खेती के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।
कृषि समाज की ओर संक्रमण
- उपरांत वेदिक काल में एक पशुपालन समाज से स्थायी कृषि समाज की ओर परिवर्तन देखा गया, जिसमें कृषि एक महत्वपूर्ण गतिविधि बन गई। यह संक्रमण लोगों की जीवनशैली और आर्थिक प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।
सामाजिक विभेदन और वर्ण व्यवस्था
- इस दौरान एक गहरा परिवर्तन वर्ण व्यवस्था के रूप में सामाजिक विभेदन का उदय था। समाज चार वर्णों में विभाजित हो गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय (या राजन्य), वैश्य, और शूद्र। इन वर्णों की उत्पत्ति एक स्तोत्र में वर्णित है, जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्याओं और शूद्रों को संसार के सृष्टिकर्ता, प्रजापति के शरीर के विभिन्न भागों के रूप में दर्शाता है।
- स्तोत्र में दर्शाया गया है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुँह से, क्षत्रियों की भुजाओं से, वैश्याओं की जाँघों से, और शूद्रों की पैरों से हुई है, जो उनके समाज में भूमिकाओं का प्रतीक है।
ब्राह्मणों की भूमिका
- इस अवधि के दौरान, बलिदानों और अनुष्ठानों की बढ़ती संख्या ने ब्राह्मणों की शक्ति को बढ़ाया, जो विभिन्न अनुष्ठान करते थे, जिनमें कृषि कार्य से संबंधित अनुष्ठान भी शामिल थे। ब्राह्मणों ने इन अनुष्ठानों की देखरेख करके समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उनकी स्थिति और बढ़ गई।
क्षत्रियों की भूमिका
क्षत्रिय सामाजिक पदानुक्रम में अगली श्रेणी में थे, जो शासक थे और शासन तथा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ब्राह्मणों के साथ मिलकर, उन्होंने प्रशासन और रक्षा सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित किया।
वैश्य की भूमिका
- वैश्य, जो सबसे अधिक संख्या में थे, कृषि, व्यापार और शिल्प गतिविधियों में लगे हुए थे।
- वे आर्थिकी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के लिए जिम्मेदार थे।
- ब्राह्मणों और क्षत्रियाओं को अपनी जीविका के लिए वैश्याओं द्वारा दिए गए उपहारों और करों पर निर्भर रहना पड़ता था।
शूद्र की भूमिका
- शूद्र सामाजिक पदानुक्रम में सबसे नीचे थे और उन्हें तीन उच्च वर्गों की सेवा करने के लिए ordained किया गया था।
- उन्हें उपनयन संस्कार जैसे अनुष्ठान में भाग लेने का अधिकार नहीं था, जो शिक्षा के लिए आवश्यक था, और इस प्रकार वे कुछ सामाजिक विशेषाधिकारों से वंचित थे।
- अन्य तीन वर्गों को द्विज कहा जाता था क्योंकि वे इस समारोह के लिए योग्य थे।
वर्ण का सिद्धांत
- वर्ण प्रणाली को जन्म के अनुसार स्थिति, वर्णों का एक पदानुक्रम (ब्राह्मण शीर्ष पर और शूद्र आधार पर) और अंतोगामी तथा अनुष्ठानिक पवित्रता के नियमों से परिभाषित किया गया था।
वर्णधर्म प्रणाली
- वर्णधर्म प्रणाली ने समाज के व्यवस्थित कार्य के लिए एक सामाजिक कानून स्थापित करने का प्रयास किया।
- हालांकि, उत्तर वैदिक काल में, यह प्रणाली पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी।
- सामाजिक समूह मुख्यतः व्यवसाय के आधार पर विभाजित थे, और समाज लचीला बना रहा, जिससे व्यक्तियों को जन्म के बंधन के बिना व्यवसाय बदलने की अनुमति मिली।
जाति प्रणाली
- जाति का विचार बाद के वेदिक ग्रंथों में उभरा, जो विस्तारित परिवारों को संदर्भित करता है और संबंधों के बंधनों पर जोर देता है। जबकि वरना ने धार्मिक स्थिति को निर्धारित किया, जाति ने वास्तविक स्थिति का निर्णय किया। समय के साथ, जाति सामाजिक-आर्थिक स्थिति का एक अधिक सटीक माप बन गया और यह अंतोगामी संबंध समूहों और विशेषीकृत व्यवसायों से जुड़ा हुआ था।
गैर-वेदिक जनजातियों के साथ अंतःक्रियाएँ
- बाद के वेदिक काल में, वेदिक लोग विभिन्न गैर-वेदिक जनजातियों से मिले, जिससे महत्वपूर्ण अंतःक्रियाएँ हुईं जो एक मिश्रित समाज के निर्माण में योगदान करती थीं। अथर्ववेद इन अंतःक्रियाओं को दर्शाते हुए विभिन्न गैर-वेदिक धार्मिक प्रथाओं का चित्रण करता है, जिन्हें पुरोहितों द्वारा अनुमोदित किया गया।
- इन अंतःक्रियाओं के बावजूद, जनजातीय अंतोगामी पर बल दिया गया ताकि जनजातियों की शुद्धता बनी रहे, जबकि क्षत्रिय और ब्राह्मण का बढ़ता प्रभाव उनकी श्रेष्ठ स्थिति के संरक्षण की आवश्यकता को दर्शाता है।
आवास
- लोग लकड़ी या ताड़ की छत वाले घरों में रहना जारी रखते थे, जिनकी दीवारें मिट्टी से प्लास्टर की जाती थीं। बेहतर घरों में एक भंडारण कक्ष, एक महिलाओं का कमरा, पुरुषों के लिए एक सामान्य बैठक कक्ष, और अग्नि पूजा के लिए एक हॉल शामिल थे।
परिवार की संरचना और गृहपति की भूमिका
- परिवार वेदिक समाज की मूल इकाई बना रहा, लेकिन बाद के वेदिक काल में इसकी संरचना में बदलाव आया। पितृसत्तात्मक परिवार अच्छी तरह से स्थापित था, और गृहपति (घर के प्रमुख) को विशेष स्थिति प्राप्त हुई।
- पिताओं की बढ़ती शक्ति स्पष्ट थी, क्योंकि वे अपने पुत्रों को भी वंचित कर सकते थे। परिवार की अर्थव्यवस्था के उभार के साथ, गृहस्वामी की स्थिति आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बन गई।
- भूमि पर अधिकार उपयोग के आधार पर थे, और भूमि का सामूहिक स्वामित्व प्रचलित था। गृहपति धनवान थे और उन्होंने अपना धन अपनी मेहनत से प्राप्त किया, न कि उपहारों के माध्यम से।
- उन्होंने यज्ञ (बलिदान) किए ताकि पुण्य प्राप्त कर सकें, और अपने धन का एक हिस्सा ब्राह्मणों को दिया। आत्रांजिखेड़ा और आहिच्छत्र जैसे स्थलों पर पाए गए सामूहिक चूल्हे बड़े परिवारों के लिए सामूहिक भोजन या खाना पकाने के लिए बनाए गए थे।
राजसी परिवार और प्रथमज
राजसी परिवारों में, प्रथमजन्म का अधिकार (primogeniture) मजबूत होता जा रहा था। पुरुष पूर्वजों की पूजा आम हो गई। कुछ महिला दार्शनिकों और कुछ रानियों के राजतिलक समारोह में भाग लेने के कुछ उदाहरणों के बावजूद, महिलाओं को आमतौर पर पुरुषों के अधीन माना जाता था और प्रमुख पारिवारिक निर्णय-निर्माण से बाहर रखा गया।
गोत्र और विवाह प्रथाएं
- इस अवधि के दौरान गोत्र (कबीला) की संस्था विकसित हुई, जहां समान गोत्र वाले लोग एक सामान्य पूर्वज से उत्पन्न होते थे।
- गोत्र के बाहर विवाह करने की प्रथा (गोत्र बहिष्कार) विकसित हुई, जिसमें समान गोत्र के सदस्यों के बीच विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- हालांकि एकपत्नी विवाह को प्राथमिकता दी गई, बहुविवाह भी आम था।
महिलाओं की स्थिति में गिरावट
- बाद के वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, और कुछ प्रतिबंध लगाए गए।
- एक ग्रंथ में, महिलाओं को ताश और शराब के साथ एक दोष के रूप में देखा गया।
- एक अन्य ग्रंथ में, बेटियों को दुःख का स्रोत माना गया।
- महिलाओं को विवाह के बाद अपने पतियों के साथ रहने की अपेक्षा की गई, और उनके सार्वजनिक बैठकों (समिति) में भाग लेने पर प्रतिबंध था।
- महिलाओं को संपत्ति का अधिकार खो दिया, और वे अपने पिता, पति या पुत्रों की निर्भर बन गईं।
वर्णाश्रम धर्म
- आश्रम (जीवन के चरण) की संस्था का प्रारंभ होने लगा, जिसमें जीवन के चार चरणों का वर्णन किया गया: ब्रह्मचर्य (छात्र), गृहस्थ (गृहस्थ), वनप्रस्थ (सन्यासी) और संन्यासी (तपस्वी)।
- शुरू में, बाद के वैदिक ग्रंथों में केवल तीन आश्रमों का उल्लेख किया गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, और वनप्रस्थ।
- समय के साथ, चौथा चरण संन्यास जोड़ा गया, हालांकि यह तब तक ज्ञात नहीं था जब तक उपनिषद नहीं लिखे गए।
- यह अवधारणा वर्ण के साथ मिलकर वर्णाश्रम धर्म के रूप में जानी गई।
देवताओं और भौतिक जीवन में परिवर्तन
सामग्री जीवन में परिवर्तन ने देवताओं और देवी-देवियों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने में योगदान दिया। स्थानीय गैर-आर्यन जनसंख्याओं के साथ निरंतर बातचीत ने भी इन परिवर्तनों में योगदान दिया, जिससे विष्णु और रुद्र जैसे देवताओं की प्रमुखता बढ़ गई, जबकि ये पहले ऋग्वेद में छोटे देवता थे।
खाने की आदतें
- खाना और पेय पदार्थ प्रारंभिक वैदिक समय के समान ही रहे, जिसमें चावल, अनाज से बना दलिया, जौ, दूध, दही, घी, तिल और मांस सामान्य थे।
- मांस का सेवन आमतौर पर त्योहारों के अवसर पर किया जाता था, और सुरा (एक शराबी पेय) का सेवन immoral व्यवहार के कारण निंदा किया गया।
पहनावे की समझ
- पहनावा आमतौर पर तीन वस्त्रों में होता था: एक अंतर्वस्त्र (निवि), एक मुख्य वस्त्र (वासस), और एक ऊपरी वस्त्र (अधि-वासस)।
- पुरुष और महिलाएं दोनों अपनी वेशभूषा का हिस्सा के रूप में पगड़ी पहनते थे।
चिकित्सा ज्ञान और प्रथाएँ
- चिकित्सा का ज्ञान प्रारंभिक था, जिसमें औषधीय जड़ी-बूटियों के साथ जादुई मंत्रों का उपयोग रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता था, जो एक प्राइमिटिव प्रणाली को दर्शाता है।
- रक्तस्त्राव रोकने के लिए रेत बंधन का उपयोग उल्लेखनीय था।
- सांख्यायन ब्राह्मण ने यह नोट किया कि मौसमी परिवर्तनों के दौरान बीमारी विशेष रूप से प्रचलित थी, जो मानव स्वास्थ्य पर प्रकृति के प्रभाव को उजागर करता है।
वेदिक युग में आर्थिक जीवन
प्रारंभिक वेदिक युग (1500 – 1000 ई.पू.)
आर्थिक गतिविधियाँ
- प्रारंभिक वेदिक काल में, आर्य मुख्यतः पालनहार थे, जिसमें मवेशी पालन उनका मुख्य व्यवसाय था।
- उन्होंने दूध, मांस और चमड़े के लिए विभिन्न जानवरों जैसे मवेशियों, भेड़ों, बकरियों और घोड़ों का पालन किया।
- एक पालनहार समाज कृषि उत्पादों की तुलना में पशु धन पर अधिक निर्भर करता है।
- पालनहारिता एक उपजीविका की रणनीति है, जिसे उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहाँ बड़े पैमाने पर कृषि संभव नहीं है।
- ऋग्वेद से प्राप्त साहित्यिक साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि मवेशी कितना महत्वपूर्ण थे।
- कई शब्द गो से निकले हैं, जिसका अर्थ है गाय।
- एक अमीर व्यक्ति को गामत कहा जाता था, और उसकी बेटी को दुहित्री कहा जाता था, जिसका अर्थ है गाय का दूध निकालने वाली।
- संघर्ष और युद्ध के लिए शब्द, जैसे गविष्टि और गवेषणा, अक्सर गायों की खोज या उन पर लड़ाइयों को संदर्भित करते थे।
- मुखिया, या राजा, को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ है गायों का रक्षक।
- सामाजिक और धार्मिक जीवन, साथ ही ऋग्वेदिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलू, गाय पालन के चारों ओर केंद्रित थे।
साहित्यिक और पुरातात्त्विक साक्ष्य
- ऋग्वेदिक स्तोत्रों और प्रार्थनाओं में चरागाह भूमि, गायों के बाड़े, डेयरी उत्पादों, और पालतू जानवरों का उल्लेख सामान्य है।
- गायों को सब कुछ प्रदान करने वाले के रूप में देखा जाता था, और उनके संख्या में वृद्धि के लिए प्रार्थनाएँ की जाती थीं।
- गायों के लिए संघर्षों का संकेत पानी के संदर्भ में मिलता है, जो अपनी संपत्ति, मुख्यतः गायों, को पहाड़ों और जंगलों में छिपाते थे।
- इन गायों को पुनः प्राप्त करने के लिए इंद्र देवता का आवाहन किया जाता था।
- हालांकि प्रारंभिक वेदिक लोग कृषि के ज्ञान से अवगत थे, लेकिन इसके महत्व के संदर्भ में साक्ष्य सीमित हैं।
- कृषि के संदर्भ बाद में जोड़े गए प्रतीत होते हैं।
- ऋग्वेद में कुछ संदर्भ कृषि प्रथाओं जैसे बोने, काटने, और थ्रेशिंग के लिए ज्ञात हैं।
- हल का उल्लेख है, जो संभवतः लकड़ी का बना था, और यव या जौ ही एकमात्र अनाज है जिसका स्पष्ट उल्लेख है।
- जुताई की गई भूमि को उर्वरा या क्षेत्र के रूप में जाना जाता था।
- आयरन तकनीक की कमी और ताम्र उपकरणों पर निर्भरता कृषि के प्रदर्शन को सीमित करती थी।
- पत्थर के उपकरण, जैसे कुल्हाड़ी, का उपयोग किया जाता था, और स्थानांतरित कृषि का अभ्यास किया जाता था।
- ऋग्वेद में औजारों का उल्लेख है जैसे हंसिया, फावड़े, और कुल्हाड़ी, जो संभवतः फसल काटने या स्थानांतरित कृषि के लिए थे।
- क्षेत्र में कम वर्षा और सतलज, सिंधु, घग्गर, और रावी जैसी नदियों के बदलते मार्ग स्थायी कृषि को चुनौती देते थे।
- पालनहारिता और स्थानांतरित कृषि के साक्ष्य एक घुमंतू या अर्ध-घुमंतू जीवनशैली का सुझाव देते हैं, जिसमें लोग अपने झुंडों के साथ चराई के क्षेत्रों की खोज में चलते थे।
- साहित्यिक और पुरातात्त्विक स्रोत यह संकेत करते हैं कि जनसंख्या पूरी तरह से स्थायी नहीं थी, और गोतरा जैसे संबंध इकाइयाँ एक गतिशील चरित्र को दर्शाती हैं।
- उपहारों का आदान-प्रदान और पुनर्वितरण महत्वपूर्ण आर्थिक प्रथाएँ थीं, जिसमें जनजातीय संघर्षों में विजयी मुखियाओं को श्रद्धांजलि दी जाती थी।
- बलिदानों और अनुष्ठानों के दौरान भी पुनर्वितरण होता था।
- भूमि के स्वामित्व पर आधारित निजी संपत्ति का कोई विचार नहीं था।
- पुजारियों को दिए गए उपहार आमतौर पर गायें और महिला दास थीं, भूमि नहीं।
अन्य व्यवसाय
- प्रारंभिक वेदिक समाज में व्यापार और वाणिज्य के साक्ष्य सीमित हैं।
- ऋग्वेद में कारीगरों जैसे बढ़ई, रथ निर्माता, बुनकर, चमड़ा कारीगर, और मिट्टी के बर्तन बनाने वालों का उल्लेख है, जो विभिन्न शिल्पों के अभ्यास को दर्शाता है।
- आयास शब्द, जो ताम्र या कांस्य को संदर्भित करता है, धातु कार्य में ज्ञान का सुझाव देता है।
- वेदिक लोग भूमि मार्गों से अधिक परिचित थे, क्योंकि ऋग्वेद में समुद्र मुख्यतः जल के संग्रह को दर्शाता है।
- लोग लकड़ी और बांस के घरों में रहते थे, जिनकी छतें घास की और फर्श मिट्टी की होती थीं।
- ऋग्वेद में पुर का उल्लेख है, जो संभवतः किलाबंद स्थान थे जो आक्रमणों के दौरान शरण के रूप में काम करते थे, हालाँकि इन स्थलों की सटीक पहचान अभी भी अनुसंधान के अधीन है।
- ऋग्वेद में नगर (शहर) का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे संकेत मिलता है कि लोग शहरों में नहीं रहते थे।
- ग्रामणी गाँव का मुखिया था, जो नागरिक और सैन्य मामलों दोनों के लिए जिम्मेदार था।
- ऋग्वेदिक चरण पेंटेड ग्रे वेयर (PGW) संस्कृति के पूर्व-आयरन चरण के साथ मेल खाता है।
बाद का वेदिक युग कृषि
बाद के वैदिक चरण के दौरान, कृषि वैदिक लोगों का प्राथमिक व्यवसाय बन गया। कृषि के विस्तार में उपजाऊ नदी-तट के क्षेत्रों की उपलब्धता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से गंगा-यमुना दोआब और मध्य गंगा घाटी में।
बाद के वैदिक ग्रंथों में छह, आठ, बारह, और यहाँ तक कि चौबीस बैलों के जोड़ से हल चलाने का वर्णन किया गया है, हालांकि यह थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है। हल चलाने के लिए आमतौर पर लकड़ी के हल का उपयोग किया जाता था, जो ऊपरी गंगेटिक मैदानों की हल्की मिट्टी के लिए उपयुक्त था।
कृषि को प्राचीन समझा जाता था, लेकिन यह व्यापक थी। खेत (sita) का ज्ञान था, और कृषि प्रक्रियाओं की शुरुआत के लिए विभिन्न अनुष्ठान किए जाते थे, जैसा कि सतपथ ब्राह्मणा में विस्तृत रूप से वर्णित है।
- कृषि क्रियाओं में हल चलाना, बीज डालना, फसल काटना, और थ्रेशिंग शामिल थे।
- उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद का उपयोग अच्छी तरह से समझा जाता था।
- अलग-अलग अनाज उगाए जाते थे, जिनमें जौ, चावल, गेहूं, फलियाँ, तिल, और दालें शामिल थीं।
- प्रत्येक वर्ष आमतौर पर दो फसलें होती थीं।
कृषि में श्रम करना राजाओं और राजकुमारों के लिए भी छोटा नहीं माना जाता था। जनक, विग्रह का राजा, और बलराम, कृष्ण के भाई, हल चलाने से जुड़े हुए हैं।
हालांकि, बाद के समय में, ऊँचे वर्णों के सदस्यों के लिए हल चलाना निषिद्ध हो गया। कृषि के उद्देश्यों के लिए भैंसों का पालतू बनाना महत्वपूर्ण था, विशेषकर दलदली भूमि के लिए हल चलाने में।
इस अवधि में भगवान इंद्र को “हल का स्वामी” का उपाधि मिली, जो कृषि के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।
अनुष्ठानों में पके चावल जैसे सामग्री की पेशकश शुरू हुई, जो कृषि उत्पादों के महत्व को दर्शाती है। अथर्ववेद में भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित बारह बलिदानों में गायों, बछड़ों, बैलों, सोने, पके चावल, छप्पर वाले घरों, और अच्छी तरह से खेती की गई खेतों की ब्राह्मणों को भेंट शामिल थी।
ये भेंट स्थायी बस्तियों और कृषि के बढ़ते महत्व को दर्शाती हैं। कृषि गतिविधियाँ श्रम-गहन नहीं थीं, और खुदाई से प्राप्त चावल के अवशेष यह सुझाव देते हैं कि गीली चावल की खेती, जो श्रम-गहन होती है, अभी तक प्रचलित नहीं थी।
पौधों के खाद्य पदार्थों की संख्या और विविधता बढ़ी, चावल मुख्य फसल और स्थायी आहार बन गया। खुदाई से प्राप्त स्थलों जैसे PGW और Banas संस्कृति से जलकर खड़े चावल के दाने प्राप्त होते हैं।
वैदिक लोग दोआब में चावल के साथ परिचित हुए, और ग्रंथ विभिन्न प्रकार के चावल का उल्लेख करते हैं।
प्रारंभिक वैदिक युग में धार्मिक जीवन (1500 - 1000 ई.पू.)
परिचय
- वैदिक लोगों के धार्मिक विचार ऋग्वेद के hymns में परिलक्षित होते हैं।
- उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों (जैसे कि हवा, पानी, वर्षा, गरज, अग्नि आदि) की पूजा की, जो उनके नियंत्रण से परे थीं।
- ऋग्वेद के देवता इन प्राकृतिक शक्तियों के व्यक्तित्वकरण थे।
पितृसत्तात्मक समाज:
- ऋग्वेद में देवता जनजातीय और पितृसत्तात्मक समाज को दर्शाते हैं।
- पुरुष देवताओं जैसे कि इंद्र, अग्नि, वरुण, और यम का प्रमुख स्थान है, जबकि देवियों जैसे कि उषा और सरस्वती का स्थान द्वितीयक है।
प्रमुख देवता और उनके कार्य
- इंद्र: शक्ति, युद्ध, गरज, और वर्षा का देवता। युद्ध में विजय और वर्षा के लिए उनकी पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उनके लिए लगभग 250 hymns समर्पित हैं।
- अग्नि: अग्नि का देवता, जिसे देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ माना जाता है। घरेलू जीवन और शुद्धता से जुड़े। उनके लिए लगभग 200 hymns समर्पित हैं।
- वरुण: जल का देवता और ऋता (कॉस्मिक ऑर्डर) का रक्षक।
- यम: मृत्यु का देवता।
- मारुत: तूफान के देवता जो इंद्र की सहायता करते थे।
- सोमा: पौधों और जड़ी-बूटियों से संबंधित, विशेषकर बलिदानों में प्रयुक्त नशीला रस।
- पुशन: रास्तों, पशुपालकों, और पशुओं का देवता।
- अदिति और उषा: प्रात: के साथ जुड़ी छोटी देवियां।
वैदिक धर्म की विशेषताएँ
- वैदिक धर्म बलिदानात्मक (sacrificial) स्वभाव का था, जिसमें विभिन्न वरदानों के लिए देवताओं को बुलाने हेतु यज्ञ किए जाते थे।
- इन यज्ञों के दौरान हिम्न और प्रार्थनाएँ की जाती थीं, जिन्हें आमतौर पर पुजारियों द्वारा किया जाता था।
- बलिदानों की बढ़ती महत्ता ने पुजारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया।
- प्रार्थनाएँ सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से की जाती थीं, जो देवताओं के साथ सीधी संवाद पर जोर देती थीं।
- धर्म जादुई सूत्रों पर आधारित नहीं था, बल्कि बलिदानों और हुम्नों के माध्यम से देवताओं से सीधे अपील पर आधारित था।
- देवताओं को बच्चों, पशुओं, भोजन, धन, और स्वास्थ्य जैसे भौतिक लाभों के लिए बुलाया जाता था।
- पशुपालन समाज में पशु बलिदान आम था, जबकि पुराने जानवरों को आर्थिक बोझ कम करने के लिए मारा जाता था।
- वैदिक धर्म ने पितृसत्तात्मक पशुपालक समाज को दर्शाया और यह भौतिकवादी दृष्टिकोण का था।
बाद के वैदिक परिवर्तन
- कृषि के विकास के साथ, भौतिक जीवन में परिवर्तन और स्थानीय गैर-आर्यन जनसंख्या के साथ संपर्क ने धार्मिक प्रथाओं को प्रभावित किया।
- दो अलग-अलग धार्मिक परंपराएँ उभरीं: वैदिक (जो साम और यजुर्वेद संहिताओं और ब्राह्मणों में प्रलेखित हैं) और गैर-वैदिक या लोक परंपरा (जो अथर्ववेद में प्रलेखित हैं)।
- यज्ञों की आवृत्ति और पैमाना बढ़ गया, जिसमें अक्सर कई जानवरों का बलिदान होता था।
- सार्वजनिक यज्ञ जैसे राजसूय, वजापेया, और अश्वमेधा में सामुदायिक भागीदारी होती थी और यह प्रमुखों के अधिकार को सुदृढ़ करता था।
- निजी यज्ञ व्यक्तियों द्वारा उनके घरों में किए जाते थे, जो वैदिक लोगों के स्थायी जीवनशैली को दर्शाते थे।
- ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा, और यज्ञ उनके लिए उपहार और शुल्क के माध्यम से समृद्धि का स्रोत बन गए।
- बलिदानों में अनुष्ठान में प्रजनन पूजा के तत्व शामिल होने लगे, और कुछ वस्तुओं को दिव्यता के प्रतीक के रूप में पूजा जाने लगा, जो मूर्तिपूजा के विकास को दर्शाता है।
- इंद्र और अग्नि की प्राथमिकता कम हो गई, जबकि देवताओं जैसे प्रजापति, विष्णु, और रुद्र का महत्व बढ़ गया।
- पुशन शूद्रों का देवता बन गया, और अथर्ववेद की सामग्री लोक परंपराओं को दर्शाती है, जो जादू और व्यक्तिगत चिंताओं पर केंद्रित है।
- जटिल यज्ञों और पुजारीय प्रभुत्व के खिलाफ विरोध ने उपनिषदों में दार्शनिक सिद्धांतों के निर्माण की ओर अग्रसर किया, जो कर्म, पुनर्जन्म, और मोक्ष पर जोर देते हैं।
- उपनिषदों ने भौतिकवादी धर्म से दर्शन की ओर एक बदलाव को चिह्नित किया, जिसने आत्मा की अपरिवर्तनीयता और जनपदों और महाजनपदों के उदय के दौरान स्थिरता और एकीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया।
- पूरे वैदिक काल में, मंदिरों और मूर्तिपूजा का अभ्यास नहीं किया गया, जो बाद में विकसित हुआ।
वैदिक धर्म को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण
ऋग्वेद में प्राकृतिक बहुदेववाद
- ऋग्वेद एक प्रकार के प्राकृतिक बहुदेववाद को प्रदर्शित करता है, जहाँ कई देवता विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- उदाहरणस्वरूप, अग्नि (Fire), सूर्य (the Sun), और उषस (Dawn) जैसे देवताओं का सीधा संबंध प्राकृतिक तत्वों से है।
- देवताओं को मानव-सदृश के रूप में चित्रित किया गया है, जिनमें मानव जैसे शारीरिक गुण जैसे कि सिर, चेहरे, मुँह, बाल, हाथ, पैर, कपड़े, और हथियार शामिल हैं, हालाँकि विवरण की मात्रा भिन्न होती है।
हेनोटेइज़्म या कथेनेोटेइज़्म
- ऋग्वेद किसी कठोर देवताओं की पदानुक्रम या निश्चित पंथ का पालन नहीं करता। इसके बजाय, देवताओं की प्रमुखता भिन्न हो सकती है।
- जब किसी विशेष देवता को एक स्तोत्र में पुकारा जाता है, तो उस संदर्भ में उस देवता को सर्वोच्च देवता माना जाता है।
- मैक्स म्यूलर ने इस सिद्धांत को हेनोटेइज़्म या कथेनेोटेइज़्म के रूप में नामित किया, जहाँ प्रत्येक देवता को बारी-बारी से सर्वोच्च माना जाता है।
- कथेनेोटेइज़्म एक समय में एक देवता की पूजा को संदर्भित करता है, जबकि हेनोटेइज़्म कई देवताओं को स्वीकार करता है बिना उनके अस्तित्व को अस्वीकार किए।
एकत्ववाद और एकेश्वरवाद
- वेद और उपनिषद एकेश्वरवाद और एकत्ववाद को बढ़ावा देते हैं, यह सुझाव देते हुए कि जबकि कई देवता हैं, वे सभी एक ही अंतिम वास्तविकता के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- एकत्ववाद ब्रह्मन को अंतिम वास्तविकता के रूप में केंद्रित करता है, जबकि एकेश्वरवाद ब्रह्मन के व्यक्तिगत रूप को प्रमुखता देता है।
- विभिन्न वैदिक अंशों में, अंतिम वास्तविकता को अव्यक्त और अव्यय दोनों के रूप में चित्रित किया गया है।
- तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मन को सभी प्राणियों का स्रोत, उनकी जीविका, और मृत्यु के बाद का अंतिम गंतव्य बताता है।
- ब्रह्मन को ब्रह्मांड के भीतर शाश्वत और अमर वास्तविकता के रूप में चित्रित किया गया है।
- कुछ व्याख्याएँ सुझाव देती हैं कि वेदों में एकत्ववाद के तत्वों के साथ-साथ पंथीवाद के पहलू भी शामिल हैं।
वैदिक धर्म एक बलिदान पूजा के रूप में
- पुरुष-सुक्त में विश्व के निर्माण को एक प्राचीन बलिदान के परिणाम के रूप में वर्णित किया गया है।
- विष्कर्मा देवता के लिए स्तोत्र में सृष्टिकर्ता देवता को पहले बलिदानकर्ता और बलिदान के रूप में कल्पित किया गया है।
- ब्राह्मण ग्रंथों में संकेत मिलता है कि बलिदान समय के साथ अधिक लंबे, विस्तृत, और महंगे हो गए हैं।
- बलिदान को एक मौलिक कार्य के रूप में चित्रित किया गया है जिसने विश्व का निर्माण किया, और इसका सही प्रदर्शन जीवन और संसार को विनियमित करने के लिए आवश्यक माना गया।
- देवता प्रजापति, जो बलिदान से निकटता से जुड़े हुए हैं, ब्राह्मणों में से एक महत्वपूर्ण देवता हैं।
- जटिल बलिदान अनुष्ठानों जैसे वाजपेया, अश्वमेघ, और राजसूय को राजत्व से जोड़ा गया, जबकि अग्निहोत्र एक सरल घरेलू बलिदान था।
अज्ञेयवाद और नास्तिकता
- ऋग्वेद देवताओं के प्रति विश्वास पर प्रश्न उठाता है, जिसमें इंद्र जैसे कुछ देवताओं की महानता भी शामिल है।
- उदाहरण के लिए, एक ऋग्वैदिक स्तोत्र पूछता है, “जिसने इंद्र को देखा है। यदि वह नहीं देखा गया है, तो उसकी अस्तित्व पर विश्वास क्यों किया जाए?”
- ऋग्वेद संहिता में एक अन्य स्तोत्र प्राइमल प्राणी के जन्म और पदार्थ और आत्मा की प्रकृति के बारे में प्रश्न उठाता है।
- स्वसन्वाद उपनिषद में विचार, जो संख्य सूत्र में संक्षेपित हैं, अवतार, देवता, स्वर्ग, और नरक जैसे अवधारणाओं को अस्वीकार करते हैं।
- यह तर्क करता है कि पारंपरिक धार्मिक ग्रंथ गर्वित व्यक्तियों के उत्पाद हैं, जहाँ प्रकृति निर्माता और समय विनाशक है, जो मानव सुख या दुख को निर्धारित करने में धर्म या अधर्म की अनदेखी करता है।
वेदिक भारत में बलिदान एक अनुष्ठान और सामाजिक विनिमय के रूप में
वेदिक भारत में, बलिदान एक अनुष्ठान और सामाजिक विनिमय का एक रूप था। देवताओं की पूजा प्रार्थना और बलिदान अनुष्ठानों के माध्यम से की जाती थी, जिन्हें यज्ञ कहा जाता था। ये बलिदान साधारण, दैनिक गतिविधियों से पवित्र क्षेत्र में संक्रमण का प्रतीक थे। देवताओं को शक्तिशाली और ज्यादातर दयालु प्राणी के रूप में चित्रित किया गया था, जिन्हें बलिदान के प्रदर्शन के माध्यम से मानव जगत में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया जा सकता था।
इन बलिदानों के उद्देश्यों में धन, मवेशी, अच्छे फसल, संघर्ष में सफलता, अच्छे स्वास्थ्य, पुत्र और बलिदान करने वालों के लिए दीर्घकालिक जीवन की मांग शामिल थी। यह विश्वास किया जाता था कि ये अनुष्ठान कुल और सामाजिक व्यवस्था की भलाई में योगदान करते थे।
वेदिक भारत में बलिदान के रूप में अनुष्ठान का विश्लेषण
- बलिदान या तो बलिदानकर्ता के घर पर या पास में विशेष रूप से तैयार की गई भूमि पर आयोजित किए जाते थे।
- अनुष्ठान में मुख्यतः दूध, घी (स्पष्ट मक्खन) और अनाज की आहूतियाँ अग्नि में डाली जाती थीं, साथ ही कुछ विशेष बलिदान सूत्रों का पाठ किया जाता था।
- कुछ यज्ञों में जानवरों का बलिदान भी शामिल होता था।
- देवताओं को यह विश्वास था कि वे आहूतियों का सेवन करते हैं जैसे कि वे अग्नि द्वारा उपभोग की जाती हैं, जबकि आहूतियों का एक हिस्सा officiating पुरोहितों द्वारा उपभोग किया जाता था।
- कुछ बलिदान सरल, घरेलू मामलों के रूप में घर वालों द्वारा किए जाते थे, जबकि अन्य के लिए अनुष्ठान विशेषज्ञों की भागीदारी आवश्यक थी।
- ऋग्वेद में सात प्रकार के बलिदान पुरोहितों का उल्लेख है, प्रत्येक के पास विशेष कार्य होते हैं।
- अग्निहोत्र एक बुनियादी घरेलू बलिदान था जिसे प्रत्येक दिन दवी परिवार के प्रमुख द्वारा सुबह और शाम किया जाना था। इसमें भगवान अग्नि को समर्पित अग्नि में दूध की आहूतियाँ डालना शामिल था।
- नए चंद्रमा और पूर्णिमा के दौरान, साथ ही तीन ऋतुओं की शुरुआत में भी आवधिक बलिदान आयोजित किए जाते थे। ऋग्वेद में उल्लिखित सोमा नामक अनुष्ठानिक पेय का उपयोग इन बलिदान अनुष्ठानों के दौरान किया जाता था।
बाद के वेदिक काल में, बलिदान अधिक लंबे, जटिल और महंगे हो गए। बलिदान के कार्य को दुनिया का निर्माता माना गया, और इसका वर्तमान प्रदर्शन जीवन और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक समझा गया।
राजशाही से जुड़ी जटिल बलिदान परंपराएँ:
- वाजपेय बलिदान का संबंध सत्ता और समृद्धि की प्राप्ति से था, जिसमें विभिन्न उपज संबंधी अनुष्ठान शामिल थे।
- अश्वमेध का संबंध राजनीतिक सर्वोच्चता के दावों से था और इसमें घोड़े का बलिदान और उर्वरता के अनुष्ठान शामिल थे।
- राजसूय शाही अभिषेक समारोह था।
इन अनुष्ठानों में कृषि उर्वरता अनुष्ठान, एक अनुष्ठानिक पशु लूट, और एक ताश का खेल शामिल था, जिसमें राजा विजयी हो रहा था। प्रतीकात्मक रूप से, राजसूय ने राजा को सृष्टि के चक्रीय पुनर्जनन की प्रक्रियाओं का केंद्रीय पात्र प्रस्तुत किया।
वेदिक भारत में सामाजिक आदान-प्रदान के रूप में बलिदान
- पुरोहितों को अनुष्ठानों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए दक्षिणा (शुल्क) प्राप्त होती थी।
- जैसे-जैसे बलिदान लम्बे और जटिल होते गए, पुरोहित की भूमिका और उन्हें दी गई दक्षिणा बढ़ने लगी।
- छोटे बलिदान घरेलू बलिदानों तक सीमित थे, लेकिन कभी-कभी बड़े बलिदान आयोजित किए जाते थे, जिसमें कबीले से महत्वपूर्ण योगदान की आवश्यकता होती थी।
- सार्वजनिक बलिदान गंभीर अवसर होते थे, लेकिन इसके बाद होने वाले उत्सवों के माध्यम से ऊर्जा भी मुक्त होती थी।
- राजा द्वारा स्वैच्छिक श्रद्धांजलि और विष (लोगों) से एकत्र की गई धनराशि अनुष्ठान में खर्च होती थी और अंत में अन्य राजाओं और पुरोहितों को उपहार के रूप में वितरित की जाती थी।
- उपहार देने के कार्य को यह विश्वास दिलाने वाला माना जाता था कि उपहारों की वापसी और भी अधिक मात्रा में होगी।
- बलिदान के अनुष्ठान पुरोहित की शक्ति को बढ़ाते थे, जिनके बिना बलिदान नहीं हो सकता था, और राजा की भी, जिसके पास आवश्यक धन था।
- इस धन को एकत्र करना विष को उनके उत्पाद को छोड़ने के लिए दबाव डालना था।
- बलिदान ने क्षत्रिय (योद्धा वर्ग) को विष और शूद्र (श्रमिक वर्ग) पर अधिक शक्ति स्थापित करने में मदद की।
- सार्वजनिक बलिदान राजा की धन प्रदर्शित करने और एकत्रित करने के अवसर होते थे। यह धन खर्च होता था, और जो भी बचता था उसे उपहार में दिया जाता था, कुछ जानबूझकर अनुष्ठानों के माध्यम से नष्ट किया जाता था।
- बलिदान के संरक्षक, आमतौर पर राजा, अपने समकक्षों के साथ अवसर की भव्यता और उपहारों की उदारता में प्रतिस्पर्धा करते थे।
- धन प्रदर्शित करने में इस प्रकार की प्रतिस्पर्धाएँ याजमान की स्थिति और शक्ति को स्थापित करती थीं, यह विश्वास बढ़ाती थीं कि और भी अधिक धन उनके पास आएगा।
- राजा के उपहारों ने पुरोहितों को समृद्ध और सशक्त बनाया।
- बलिदान ने राजा को इस हद तक धन संचय करने से रोका कि उसकी स्थिति आर्थिक शक्ति पर आधारित हो जाए, न कि अनुष्ठानिक स्वीकृति पर।
- हालांकि, आर्थिक शक्ति उस प्रकार की राजशाही के निर्माण के लिए आवश्यक थी जो राज्य से जुड़ी थी, जहाँ राजा धन के संचय और वितरण को नियंत्रित करता था।
- इन बलिदानों के लिए आवश्यक धन को इकट्ठा करने के लिए, राजा को विष से उपहार और प्रस्तुतियों के रूप में अधिक मांग करनी होती थी और समर्थन के लिए एक बुनियादी प्रशासन स्थापित करना होता था।
धन के संग्रहण और विभिन्न अधिकारों के सहायक तत्वों पर खर्च करने के बिंदु पर, राजशाही ने अनुष्ठानिक अधिकार पर राजनीतिक अधिकार पर निर्भर होना शुरू किया।
समय के साथ, राजा बनने के लिए बलिदान की रस्म स्थायी विशेषता नहीं रह सकी। एक बार जब राजतंत्र स्थापित हो गए, तो उन राज्यों का समर्थन करने वाले धन पर अन्य मांगें थीं।
एक स्तर पर, इस रस्म की केंद्रीयता पर सवाल उठाने को मानव और दिव्य के बीच संबंध की नई धारणाओं ने प्रोत्साहित किया। दूसरी ओर, मध्य गंगा मैदान में शहरीकरण से पहले धन का बढ़ता उत्पादन, जिसका अधिकांश भाग रस्मों में उपभोग नहीं किया जा सका, ने राजाओं को धन संचय करने की अनुमति दी, जिससे सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं में बदलाव आया।
वेदिक देवताओं का वैचारिक आधार
- ऋग्वेद में कई देवताओं में विश्वास का चित्रण किया गया है जो प्राकृतिक घटनाओं का व्यक्ति रूप हैं, जिसे प्राकृतिक बहुदेववाद (naturalistic polytheism) कहा जाता है। कुछ देवताओं, जैसे अग्नि (Fire), सूर्य (the Sun), और उषा (Dawn), के नाम सीधे उनके प्राकृतिक तत्वों से जुड़ाव को दिखाते हैं।
इंद्र और मारुत
- इंद्र, जो ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित देवता हैं, एक शक्तिशाली और मजबूत योद्धा के रूप में चित्रित किए गए हैं, जो एक वज्र का उपयोग करते हैं। वह आर्याओं को युद्ध में जीत दिलाते हैं, विशेष रूप से स्थानीय जनजातियों के खिलाफ, और उन्हें एक मौसम देवता के रूप में भी पुकारा जाता है जो वर्षा लाते हैं। मारुत इंद्र के साथी हैं जो युद्ध में उनकी सहायता करते हैं।
- अग्नि अग्नि के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें शवदाह की आग, जंगलों को engulf करने वाली आग, दुश्मनों को जलाने वाली आग, और तप (संन्यास) और यौन इच्छा द्वारा उत्पन्न गर्मी शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण, बलिदान की आग के रूप में, अग्नि देवताओं और मनुष्यों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है, जो एक दिव्य पुजारी के रूप में कार्य करती है।
सोमा सोमा पौधे का व्यक्ति रूप है और इसे एक बुद्धिमान देवता के रूप में वर्णित किया गया है जो कवियों को स्तोत्र रचना के लिए प्रेरित करता है। इसे बाद के स्तोत्रों में चंद्रमा के साथ भी जोड़ा गया है।
वरुण का संबंध क्षत्र (धर्मनिरपेक्ष शक्ति), सौम्यत और राजत्व से है। वह ब्रह्मांडीय व्यवस्था ऋत का रक्षक है और गलत काम करने वालों को अपनी आज्ञा से बंधनों या बेड़ियों से दंडित करता है।
सूर्य, आश्विन, वायु, रुद्र
- सूर्य, जो कि सूर्य देवता और द्यौस के पुत्र हैं, अपने रथ में आकाश में सवारी करके अंधकार को दूर करते हैं।
- वायु वायु देवता हैं।
- आश्विन दो जुड़वाँ देवता हैं जो युद्ध और प्रजनन से जुड़े हैं।
- रुद्र एक ऐसे देवता हैं जिनका महान विनाशकारी потенциал है और जो भय उत्पन्न करते हैं।
- उषा, जो सुबह की देवी हैं, ऋग्वेद में 300 बार उल्लेखित हैं, जिनमें से 20 स्तोत्र उनके लिए समर्पित हैं। वह प्रकाश की अंधकार पर विजय का प्रतीक हैं और धन की आकांक्षा रखने वालों द्वारा उन्हें पुकारा जाता है।
- अदिति, जिसका अर्थ स्वतंत्रता है, का आवाहन बीमारियों, हानि और बुराई से मुक्ति के लिए किया जाता है।
|
28 videos|739 docs|84 tests
|















