संस्कृतिक संक्रमण: ग्रंथों और पुरातत्व से चित्र, लगभग 2000–600 ईसा पूर्व - 4 | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download
विभिन्न कालों की मिट्टी के बर्तन, मास्की
हल्लूर, जो धारवाड़ क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, विभिन्न कालों के अद्वितीय मिट्टी के बर्तन शैलियों का प्रदर्शन करता है। काल I, जिसे निओलिथिक के रूप में पहचाना गया है, को पूर्व और बाद के चरणों में विभाजित किया गया है।
- पूर्व चरण: गोल वट और मिट्टी के झोपड़ियों के फर्श पत्थर के चिप्स और नदी की बालू से बने थे।
- मिट्टी के बर्तन मुख्य रूप से हस्तनिर्मित साधारण और चमकदार भूरे रंग के थे, साथ ही कुछ लाल-भूरे रंग के बर्तन जिनमें बैंगनी चित्रण था।
- बाद का चरण: इस चरण में चित्रित काले और लाल बर्तनों का परिचय हुआ। इस काल के पत्थर के उपकरणों में ग्राउंड और पॉलिश किए गए उपकरण, साथ ही माइक्रोलिथ्स शामिल थे। अन्य प्राप्त वस्तुओं में तांबे की मछलीhooks, दोहरे कुल्हाड़ी, और स्टीटाइट, क्वार्ट्ज, हड्डी, और शेल से बने मनके शामिल थे। एक उल्लेखनीय खोज एक डबल urn दफन था। इस काल के पशु हड्डियों में गाय, भेड़, और बकरी की हड्डियाँ शामिल थीं, जबकि घोड़े की हड्डियाँ बाद के चरण में दिखाई दीं। हल्लूर काल I के लिए कैलिब्रेटेड तिथियाँ लगभग 2000 से 1400 BCE के बीच हैं।
- दक्षिणी निओलिथिक–चाल्कोलिथिक समुदायों की जीविका का आधार कृषि, पशु पालतन, और शिकार था। टेक्कालकोटा और हल्लूर जैसे स्थलों से मिली जानकारी ने घोड़े की दाल और रागी की उपस्थिति को उजागर किया, जबकि पैयमपल्ली ने घोड़े की दाल और हरी दाल का उत्पादन किया। ये फसलें आज भी क्षेत्र में मुख्य खाद्य हैं।
- यह माना जाता है कि निओलिथिक–चाल्कोलिथिक किसान खेती के लिए पहाड़ियों पर टेरासिंग का उपयोग करते थे। विभिन्न स्थलों पर गाय की हड्डियों की प्रचुरता, जिनमें कई कट मार्क्स थीं, ने पशुपालन के महत्व को रेखांकित किया। ऊँट की आकृतियाँ प्रचुर मात्रा में हैं, और इन जानवरों को मास्की जैसे स्थलों पर चट्टान चित्रों में भी चित्रित किया गया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बुदगवी के चट्टान आश्रयों में ऊँट के बैल की विशेष शैली में चित्रित मेसोलिथिक और निओलिथिक चट्टान चित्रों की हाल की खोजें की गई हैं।
- कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के सात निओलिथिक स्थलों से पौधों और पशुओं के अवशेषों की हाल की पुनः जांच ने दक्षिणी निओलिथिक समुदायों में जीविका के पैटर्न पर प्रकाश डाला है। जिन स्थलों का अध्ययन किया गया उनमें हल्लूर, सांगानकल्लू, टेक्कालकोटा,Hiregudda, कुरुगोडू, हत्तिबेलागल्लू, और वेलपुमडुगु शामिल हैं।
- पालित पशु: गाय सबसे महत्वपूर्ण पालतू जानवर थे, जबकि बकरी और भेड़ कम महत्वपूर्ण थीं। मुर्गियों के पालतन का प्रमाण भी है। जल भैंस की हड्डियाँ मिलीं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वे पालतू थीं या नहीं।
- जंगली जानवर: जंगली जानवर जैसे एंटेलोप, हिरण, और सुअर का शिकार भोजन के लिए किया गया। ताजे पानी के संसाधनों जैसे मछली और मोलस्क का उपयोग कभी-कभी किया गया, यहां तक कि उन स्थलों पर जो नदियों से दूर थे।
- गाय का आकार: गाय की हड्डियों के माप से पता चलता है कि दक्षिणी निओलिथिक लोगों द्वारा पाले गए गायों का आकार मध्यम से मध्यम-भारी था।
- फसल पैटर्न: ध्यान मुख्य रूप से खड़ी (गर्मी) फसलों पर था, जिसमें छोटे बाजरे, दालें (जैसे मूंग), और घोड़े की दाल शामिल थीं। अन्य फसलों में गेहूँ, जौ, पिगन पी, मोती बाजरा, और हयासिन्थ बीन्स selectively उगाई गईं, जिसमें गेहूँ और जौ सर्दी की फसलें होने की संभावना है। सूखे मौसम में फलों और कंदों को इकट्ठा किया गया।
- साल भर का निवास: विभिन्न मौसमों में उगाए गए पौधों के साक्ष्य इन स्थलों पर निवास के जमा की मोटाई के साथ मेल खाते हैं, जो साल भर के निवास का सुझाव देते हैं।
तांबे से लोहे तक: उपमहाद्वीप की प्रारंभिक आयरन युग संस्कृतियाँ
तांबा-पीतल युग से लोहे के युग में संक्रमण ने विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव को चिह्नित किया। यह बदलाव कई दिलचस्प प्रश्न उठाता है:
क्या लोहे का गलाना तांबे के गलाने का एक आकस्मिक उप-उत्पाद था? क्या लोहे का गलाना और कार्य करना एक विशाल तकनीकी छलांग की आवश्यकता थी, या क्या यह तांबाकारी के कौशल में था? कुछ समुदायों ने, जो सदियों से तांबा और कांस्य जैसे धातुओं का उपयोग कर रहे थे, अचानक लोहे के उपकरण बनाना और उपयोग करना क्यों शुरू किया?
- क्या लोहे का गलाना तांबे के गलाने का एक आकस्मिक उप-उत्पाद था?
- क्या लोहे का गलाना और कार्य करना एक विशाल तकनीकी छलांग की आवश्यकता थी, या क्या यह तांबाकारी के कौशल में था?
- कुछ समुदायों ने, जो सदियों से तांबा और कांस्य जैसे धातुओं का उपयोग कर रहे थे, अचानक लोहे के उपकरण बनाना और उपयोग करना क्यों शुरू किया?
इन प्रश्नों को समझने के लिए, हमें कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं पर विचार करना होगा:
- गलन बिंदु: तांबा 1083°C पर गलता है, जबकि लोहे का गलन बिंदु 1534°C है। इसका मतलब यह है कि लोहे का गलाना बहुत उच्च तापमान बनाए रखने वाली भट्ठियों की आवश्यकता होती है।
- Impurities और परिस्थितियाँ: लोहे के अयस्क में तांबे के अयस्क की तुलना में अधिक अशुद्धियाँ होती हैं और सफल गलाने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। भट्ठी में 1250°C का तापमान बनाए रखना आवश्यक है ताकि अवांछित गैंज सामग्री को गलाए गए सामग्री से अलग किया जा सके।
- हवा और ईंधन: लोहे के गलाने के लिए एक अच्छी हवा का प्रवाह और ईंधन की निरंतर आपूर्ति आवश्यक है।
- फ्लक्स: फ्लक्स, जो गलाने में सहायक होते हैं, गलाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें द्रव्यमान अयस्क में मिलाया जाता है ताकि यह अशुद्धियों के साथ मिलकर स्लैग का निर्माण कर सके, जिसे निकाला जा सके।
- कार्बुराइजेशन: कार्बुराइजेशन की तकनीक, जिसमें लोहे को कार्बन के साथ गर्म करके स्टील बनाया जाता है, एक और महत्वपूर्ण कदम था जिसे लोहे के व्यापक उपयोग से पहले समझना आवश्यक था।
- लौथल, मोहनजोदड़ो, पिराक, अल्लाहदीनो, आहर, और गुफकराल जैसे स्थलों से सबूत बताते हैं कि कुछ चाल्कोलिथिक समुदाय लोहे से परिचित थे और अयस्कों से इसे गलाने में सक्षम थे। यह दर्शाता है कि इन समुदायों को लोहे के गलाने और कार्य करने का कुछ ज्ञान था, हालांकि यह छोटे पैमाने पर था।
प्रारंभिक लोहे का निष्कर्षण आकस्मिक रूप से तांबे के गलाने वाली भट्ठियों में हो सकता है जब उच्च तापमान प्राप्त किए गए, या तो लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण तांबे के अयस्क में या हेमाटाइट फ्लक्स के उपयोग के कारण। हालाँकि, यह एक प्रयोगात्मक चरण का प्रतिनिधित्व करता था, और लोहे का बड़े पैमाने पर उपयोग और लोहे के कार्य में तकनीकी दक्षता धीरे-धीरे विकसित हुई।
- तांबे के अयस्क लोहे के अयस्कों की तुलना में कम व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। व्यापार नेटवर्क में कमी ने समुदायों को तांबे के स्थान पर लोहे का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया हो सकता है, खासकर जब उन्होंने लोहे के गलाने के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और तांबे और कांस्य की तुलना में लोहे की बेहतर कठोरता और दीर्घकालिकता को पहचाना।
लोहे की प्रौद्योगिकी की शुरुआत बनाम लोहे का युग
लोहे की तकनीक की शुरुआत आयरन एज की शुरुआत से भिन्न है। हमें यह समझना आवश्यक है कि किसी स्थल पर कुछ लोहे के वस्तुओं की खोज और लोहे के महत्वपूर्ण उपयोग में अंतर है। लेकिन हम यह कैसे निर्धारित करें कि 'महत्वपूर्ण उपयोग' का क्या अर्थ है?
महत्वपूर्ण उपयोग का मूल्यांकन
- कुल मात्रा: हमें लोहे की कलाकृतियों की समग्र मात्रा का अध्ययन करना होगा और इसे अन्य धातुओं और सामग्रियों के साथ तुलना करनी होगी।
- प्रकृति और उद्देश्य: लोहे की वस्तुओं के प्रकार और उनके Intended उपयोग महत्वपूर्ण कारक हैं।
- दैनिक गतिविधियाँ: यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि लोग कब से उत्पादन में दैनिक कार्यों के लिए लोहे का उपयोग करने लगे।
कृषि में लोहे का उपयोग
- कृषि समाजों के लिए, हमें यह निर्धारित करना होगा कि कब लोहे के औजार जैसे हल, फावड़े और हंसिया कृषि कार्यों में उपयोग होने लगे।
महत्व
- यह आयरन एज की असली शुरुआत को दर्शाता है।
- आवश्यक औजारों और उपकरणों के लिए लोहे का उपयोग करना इन समाजों में एक महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नति का प्रतिनिधित्व करता है।
उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग के प्रारंभिक प्रमाण

लोहे की अयस्क की उपलब्धता
- उपमहाद्वीप में लोहे के अयस्क प्री-इंडस्ट्रियल धातु धारण के लिए उपयुक्त हैं, इसके अलावा सभीuvial नदी घाटियों के।
- बाद के वैदिक ग्रंथों में लोहे की जानकारी और इसके कृषि में उपयोग का उल्लेख है, विशेषकर इंदो-गंगा विभाजन और ऊपरी गंगा घाटी में, लगभग 1000–500 ईसा पूर्व।
पुरातात्विक प्रमाण
- पुरातात्विक खोजों से उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में लोहे की प्रौद्योगिकी और लौह युग की शुरुआत का विस्तृत प्रमाण मिलता है।
- प्रारंभिक लोहे का उपयोग करने वाले केंद्र बलूचिस्तान, इंदो-गंगा विभाजन, राजस्थान, पूर्वी भारत, मालवा, मध्य भारत, विदर्भ, दक्कन, और दक्षिण भारत में पहचाने गए हैं।
प्री-इंडस्ट्रियल धातु धारण
- सभी पहचाने गए प्रारंभिक लोहे के उपयोग केंद्र लोहे के अयस्क संसाधनों के निकट या उनके भीतर स्थित हैं और प्री-इंडस्ट्रियल धातु धारण के प्रमाण हैं।
- यह एक गलत धारणा है कि लोहे की प्रौद्योगिकी उपमहाद्वीप में इंदो-आर्यनों द्वारा लाई गई थी।
लोहे की प्रौद्योगिकी की उत्पत्ति
- चक्रवर्ती के विश्लेषण से पता चलता है कि लोहे की प्रौद्योगिकी पश्चिम एशिया या अन्य स्थानों से भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं फैली।
- केंद्र और दक्षिण भारत में लोहे का उपयोग संभवतः उत्तर-पश्चिम या गंगा घाटी की तुलना में पहले शुरू हुआ, और उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में यह लगभग 800 ईसा पूर्व में उत्पादक प्रणाली में प्रवेश कर गया।
- हालांकि, उत्तर प्रदेश के कुछ स्थलों से हाल की खोजों ने इस समझ को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है।
क्षेत्रीय अवलोकन
- अगली अनुभाग में उपमहाद्वीप में प्रारंभिक लौह युग के क्षेत्रों के प्रमाण का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है।
- कुछ क्षेत्रों का उल्लेख नहीं किया गया है या तो अन्वेषण की कमी के कारण या क्योंकि वहां लोहे का उपयोग बाद में शुरू हुआ।
- उदाहरण के लिए, असम, ओडिशा, और गुजरात में ऐतिहासिक अवधि से पहले लोहे का कोई प्रमाण नहीं है।
- पंजाब के मैदानों और सिंध की स्थिति अभी भी अस्पष्ट है।
भारत में मेगालिथ्स: एक नजदीकी नज़र
- मेगालिथ बड़े पत्थर के स्मारक हैं, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पाए गए हैं, जिसमें यूरोप, एशिया, अफ्रीका, और अमेरिका शामिल हैं।
- शब्द "मेगालिथ" ग्रीक शब्दों "मेगास" (महान या बड़ा) और "लिथोस" (पत्थर) से आया है।
- भारत में, मेगालिथ दूर दक्षिण, दक्कन प्लेटौ, विंध्य और अरावली पर्वत श्रृंखलाओं, और उत्तर-पश्चिम में पाए जाते हैं।
- भारत में कुछ जनजातीय समुदाय, जैसे असम के खासी और छोटानागपुर के मुंडा, आज भी मेगालिथ बनाने की परंपरा का पालन करते हैं।
- शब्द "मेगालिथिक संस्कृति" उन सांस्कृतिक अवशेषों को संदर्भित करता है जो मेगालिथ्स के चारों ओर पाए जाते हैं।
- हालांकि, अब यह समझा गया है कि विभिन्न मेगालिथ्स से जुड़े सांस्कृतिक अवशेषों में महत्वपूर्ण भिन्नताएँ हैं, इसलिए "मेगालिथिक संस्कृतियाँ" शब्द अधिक उपयुक्त है।
- मेगालिथ्स विभिन्न दफन शैलियों को दर्शाते हैं जो विभिन्न समयों और स्थानों पर उभरीं, जिनमें से कुछ का पता नवपाषाण-ताम्रपाषाण काल तक लगाया जा सकता है।
- उदाहरण के लिए, दक्षिण भारतीय नवपाषाण-ताम्रपाषाण स्थलों में गड्ढे और कलश दफनाए गए थे, और वाटगाल में पत्थर से चिह्नित दफनाएं पाई गईं।
- चेंबर टॉम्ब्स, एक प्रकार की मेगालिथिक संरचना, दफन प्रथाओं में एक नया विकास का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- मेगालिथ्स के तीन मूल प्रकार हैं: (क) चेंबर टॉम्ब्स, (ख) बिना चेंबर के टॉम्ब्स, और (ग) दफनों से जुड़े मेगालिथ्स नहीं।
- चेंबर टॉम्ब्स एक चेंबर से बने होते हैं जो पत्थर की लंबवत स्लैब से बने होते हैं, जो एक क्षैतिज कैपस्टोन से ढके होते हैं।
- यदि चेंबर भूमिगत है, तो इसे सिस्ट कहा जाता है; यदि यह आंशिक रूप से भूमिगत है, तो इसे डोलमेनॉइड सिस्ट कहा जाता है; और यदि यह पूरी तरह से ऊपर है, तो इसे डोलमेन कहा जाता है।
- चेंबर टॉम्ब्स में एक पत्थर की लंबवत स्लैब में एक छिद्र हो सकता है जिसे "पोर्टहोल" कहा जाता है और इसमें ऐसे फीचर्स भी शामिल हो सकते हैं जैसे मार्ग और ट्रांसपेट जो चेंबर को अनुभागों में विभाजित करते हैं।
- चेंबर टॉम्ब्स के उदाहरणों में केरल और कर्नाटक में पाए जाने वाले टॉपिकल और कुदैकल शामिल हैं।
- टॉपिकल्स में, दफन कलश को एक भूमिगत गड्ढे में रखा जाता है और इसे एक निम्न, उत्तल कैपस्टोन से ढक दिया जाता है, जबकि कुदैकल में, कलश को एक चेंबर में रखा जाता है जिसे एक बड़े अर्धगोलाकार कैपस्टोन से ढका जाता है।
दफन प्रथाएं
- Unchambered शवदाह के तीन प्रकार हैं: पिट शवदाह, अर्न शवदाह, और सार्कोफैगस शवदाह.
- पिट शवदाह में शव को एक गड्ढे में रखा जाता है और इसे कई तरीकों से चिह्नित किया जा सकता है:
- पिट वृत्त: बड़े पत्थरों का एक वृत्त शवदाह को चिह्नित करता है.
- केर्न: बड़े पत्थरों का एक ढेर ऊपर रखा जाता है.
- केर्न पत्थर वृत्त: यहाँ दोनों, पत्थर का वृत्त और जमा किए गए पत्थर होते हैं.
- मेंहिर: एक अकेला बड़ा खड़ा पत्थर शवदाह को चिह्नित करता है.
- अर्न शवदाह में शव को एक बड़े बर्तन या अर्न में रखा जाता है, जिसे कभी-कभी एक पत्थर की स्लैब से ढक दिया जाता है.
- सार्कोफैगस शवदाह एक टेराकोटा ट्रफ होता है, जो अक्सर पैरों और ढक्कन के साथ होता है, जिसमें शव रखा होता है.
- अर्न और सार्कोफैगस शवदाह अक्सर मेगालिथिक शवदाह के अंतर्गत आते हैं, भले ही उन्हें पत्थरों से चिह्नित न किया गया हो.
विश्वास और सामाजिक संगठन
- मेगालिथ्स को उनके आकार और आकार के संदर्भ में वर्णित करना आसान है, लेकिन वे जो विश्वास दर्शाते हैं, उन्हें समझना कठिन है.
- ये संरचनाएँ संभवतः उन लोगों के जीवन और विश्वास प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं जिन्होंने इन्हें बनाया.
- नवपाषाण-ताम्रपाषाण शवदाह के विपरीत, जो अक्सर निवास क्षेत्रों के भीतर होते हैं, मेगालिथिक शवदाह अलग से स्थित होते हैं.
- जीवित और मृत के बीच का यह पृथक्करण सामाजिक संगठन में बदलाव का संकेत देता है.
- मेगालिथ्स विभिन्न शवदाह प्रथाओं को दर्शाते हैं, जिसमें विस्तारित, अंशीय, पोस्ट-एक्सकार्नेट, और पोस्ट-क्रेमेशन शवदाह शामिल हैं.
- कुछ कब्रों में एक से अधिक व्यक्तियों के अवशेष होते हैं, जो परिवार के ताबूत या एक साथ मृत्यु का संकेत देते हैं.
- कब्र सामान की उपस्थिति, जैसे कि हथियार, मिट्टी के बर्तन, और आभूषण, पुनर्जन्म में विश्वास को दर्शाती है.
- कुछ मेगालिथ स्पष्ट रूप से शवदाह स्थल हैं, जबकि अन्य मृतकों के लिए स्मारक के रूप में कार्य कर सकते हैं.
मेगालिथ्स और उनके संदर्भ
विंध्य के मेगालिथ्स- विंध्य में मेगालिथ्स प्राचीन ताम्रपाषाण काल से संबंधित हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में मेगालिथ्स को आमतौर पर लौह युग से जोड़ा जाता है।
- मेगालिथिक स्थलों की आयु भिन्न है, कुछ लगभग 1300 ईसा पूर्व के आस-पास की हैं और अन्य प्रारंभिक शताब्दियों तक जारी हैं।
- आदिचनल्लूर से एक C-14 दिनांक यह सुझाव देता है कि कुछ मेगालिथ्स 12वीं शताब्दी ईस्वी तक के हो सकते हैं।
- इनकी व्यापक वितरण और विभिन्न तिथियों और संदर्भों के कारण, मेगालिथ्स कोई एक समान संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
उत्तरी-पश्चिम
- बलूचिस्तान में, कैरन दफन स्थलों में बर्तन, भाला के सिर, तलवार के ब्लेड, तीर के सिर, भालों के सिर, एक घोड़े की नाल, और एक मछलीhook जैसी लौह वस्तुएं पाई गई हैं।
- हालांकि, इन दफनों की तिथि निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण है। कुछ विद्वान इसे लगभग 1100 से 500 ईसा पूर्व के बीच की तिथि मानते हैं, लेकिन ये दफन बाद की अवधि के भी हो सकते हैं।
- बलूचिस्तान के काची मैदान में पीरक में, स्तर VI में लौह वस्तुएं कम थीं लेकिन स्तर IV और III में बढ़ गईं, जिसमें तीर के सिर प्रमुख प्रकार थे।
- एक लोहार की भट्टी स्थानीय लौह उत्पादन को दर्शाती है।
- मिट्टी के बर्तन और पत्थर के ब्लेड ताम्रपाषाण से प्रारंभिक लौह स्तरों तक निरंतरता दिखाते हैं, लेकिन एक नया ग्रे या काला बर्तन उभरा।
- स्तर IV में खुदाई से एक enclosing दीवार के भीतर कमरे, लकड़ी के दरवाजे, ओवन, चूल्हे, और संग्रहण बर्तन मिले।
- स्तर III में घरों का पुनर्निर्माण हुआ जिसमें बढ़ती शिल्प गतिविधि देखी गई, जिसमें अधिक चूल्हे, ओवन, और वस्तुएं जैसे कि टेरेकोटा मुहरें और मनके शामिल थे।
- हड्डी के बिंदु, ज्यादातर सींग से बने और उकेरे गए वृत्तों से सजाए गए थे, भी पाए गए।
- पीरक में सबसे प्रारंभिक लौह साक्ष्य लगभग 1000 से 800 ईसा पूर्व के बीच की तारीख दी गई है।
- पाकिस्तान के उत्तरी-पश्चिमी सीमांत प्रांत में गंधार कब्र संस्कृति में लौह वस्तुएं काल VII में प्रकट होती हैं, जो 1st सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत की तारीख है।
- लौह वस्तुएं जैसे कि भाला के सिर, तीर के सिर, पिन, चम्मच, अंगूठी, कांटे, और एक कुल्हाड़ी पहले के ताम्रपाषाण चरण से निरंतरता को दर्शाते हैं।
- लौह वस्तुएं काल III में: साराikhoला: लौह काल III के कब्रों के दूसरे चरण में प्रकट होता है, जिसमें दो अंगूठी, एक रॉड, और एक लौह क्लैप शामिल है, जो संभवतः 1st सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के पहले भाग की तारीख में हैं।
- गुफ्कराल, कश्मीर: लगभग 1000 ईसा पूर्व की तारीख वाली एक लौह वस्तु मेगालिथिक स्तरों में पाई गई, जिसमें काल III में लौह उद्योग का महत्वपूर्ण विकास हुआ।
- कुमाऊं–गढ़वाल क्षेत्र: ऊपरी रामगंगा बेसिन में उलेनी स्थल में स्लैग और लौह वस्तुओं के ढेर मिले, जो यह दर्शाते हैं कि यह एक लौह स्मेल्टिंग और कार्य स्थल था, जिसमें 1022–826 ईसा पूर्व की कैलिब्रेटेड तारीखें हैं।
इंडो-गंगा विभाजन और ऊपरी गंगा घाटी: पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति
PGW स्थलों: घग्गर-हाकरा क्षेत्र: भगवांपुरा जैसे स्थलों और बीकानेर क्षेत्र में लोहे के कलाकृतियों के सबूत नहीं मिले।
- PGW की पहचान और वितरण: अहिच्छत्र: PGW की पहचान यहां 1940 के दशक में हुई, और इसकी महत्वपूर्णता B. B. लाल के हस्तिनापुर में उत्खनन के बाद समझी गई।
- भौगोलिक विस्तार: PGW का विस्तार हिमालय की तलहटी से मलवा पठार तक और पाकिस्तान के बहावलपुर से इलाहाबाद के निकट कौशांबी तक हुआ।
पर्वतीय क्षेत्र: कुमाऊं और गढ़वाल में काशीपुर, थापली, और पुरोला जैसे स्थलों पर पाया गया, जबकि बिहार में वैशाली और मध्य प्रदेश में उज्जैन जैसी जगहों पर भी sporadic खोजें हुईं।
कालक्रम और क्षेत्रीय भिन्नताएं:
- तारीख की सीमा: PGW संस्कृति लगभग 1100 से 500/400 BCE तक की मानी जाती है, जिसमें उत्तर-पश्चिम में पहले के स्थल गंगा घाटी की तुलना में हैं।
- क्षेत्रीय भिन्नताएं: विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी के बर्तन और संबंधित अवशेषों में भिन्नता।
उत्तर काली चमकीली वस्तु (NBPW) की ओर संक्रमण:
- पुरातात्विक अनुक्रम: PGW चरण के बाद NBPW चरण आता है, जो लगभग 700 BCE में श्रिंगवेरपुर में शुरू होता है।
- प्रोटो-शहरी साक्ष्य: विभिन्न PGW स्थलों से पता चलता है कि NBPW से पूर्व एक प्रोटो-शहरी चरण था।
चित्रित ग्रे बर्तन के कुछ स्थल

- चित्रित ग्रे बर्तन (PGW) की भौतिक संस्कृति के साक्ष्य उत्तरी भारत के विभिन्न खुदाई किए गए स्थलों पर पाए गए हैं।
PGW साक्ष्य वाले स्थल
- उत्तर प्रदेश: हस्तिनापुर, अहिच्छत्र, मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, नोह, जोधपुर, अत्रंजिकेरा
- पंजाब: रुपड़, संगोल, दादेरी, कटपालों, नगर
- हरियाणा: दौलतपुर, भगवानपुर
- राजस्थान: जोधपुर
PGW के स्तरीकरणीय संदर्भ
PGW चार अलग-अलग स्तरीकरणीय संदर्भों में पाया जाता है:
- लेट हारप्पन द्वारा पूर्ववत: स्थलों जैसे रुपड़, संगोल, दौलतपुर, आलमगीरपुर, और हुलास में PGW एक लेट हारप्पन स्तर के बाद आता है जिसमें आवास में अंतराल है।
- लेट हारप्पन के साथ ओवरलैप: स्थलों जैसे दादेरी, कटपालों, नगर, और भगवानपुर में PGW लेट हारप्पन चरण के साथ ओवरलैप करता है।
- OCP द्वारा पूर्ववत: स्थलों जैसे हस्तिनापुर और अहिच्छत्र में PGW OCP संस्कृति के बाद आता है जिसमें बीच में एक अंतराल है।
- BRW द्वारा पूर्ववत: स्थलों जैसे अत्रंजिकेरा, नोह, और जोधपुर में PGW BRW चरण के बाद आता है जिसमें बीच में एक अंतराल है।
PGW स्तरों पर संरचनात्मक अवशेष
- झोंपड़ियों के प्रकार: संरचनात्मक अवशेष मुख्य रूप से कंडा और गारा तथा मिट्टी की झोंपड़ियों से बने होते हैं।
- ईंटें: हस्तिनापुर में कच्ची ईंटें और एक पकाई गई ईंट मिली। जखेरा में संभवतः धार्मिक उद्देश्यों के लिए बड़ी पकाई गई ईंटें मिलीं।
- घर के अवशेष: भगवानपुर में पकाई गई ईंटों से बने एक बड़े, 13-कमरे वाले घर के अवशेष मिले, हालाँकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह घर PGW का है या पूर्व की लेट हारप्पन चरण का।
पाई गई कलाकृतियाँ
- पत्थर, हड्डी, और टेराकोटा से बने कलाकृतियाँ PGW स्थलों पर खोजी गई हैं।
- हस्तिनापुर में चर्ट और जैस्पर के वजन मिले, जो विशेष हस्तशिल्प गतिविधियों का संकेत देते हैं।
हस्तिनापुर और अहिच्छत्र के पेंटेड ग्रे वेयर के टुकड़े
पेंटेड ग्रे वेयर (PGW) एक प्रकार की मिट्टी की बर्तन हैं, जो अपनी बारीक, चिकनी, और समान रंग की सतह के लिए जानी जाती हैं, जो आमतौर पर चांदी-gray से युद्धपोत के ग्रे रंगों में होती हैं। इस मिट्टी के बर्तन पर काले रंग में सरल ज्यामितीय पैटर्न चित्रित होते हैं। रंग और बनावट की समानता उन्नत आग लगाने की तकनीकों का सुझाव देती है, जिसमें उच्च तापमान या मिट्टी में काले लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति शामिल हो सकती है। PGW बर्तन तेज गति वाले चाक पर बनाए जाते हैं, जिनकी मोटाई अंडे की खोल जैसी होती है, और इन्हें दूसरी बार घुमाने और चिकना करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
जखेरा: एक अवलोकन
- प्रोटो-शहरी चरण: जखेरा पेंटेड ग्रे वेयर (PGW) संस्कृति के विकसित चरण का प्रदर्शन करता है, जो प्रारंभिक शहरी या अर्ध-शहरी विशेषताओं को दर्शाता है।
- जल प्रबंधन: स्थल पर एक महत्वपूर्ण जल प्रबंधन प्रणाली है, जिसमें 60 मीटर लंबा जल चैनल और एक बांध शामिल है, जो उन्नत जल प्रबंधन रणनीतियों को उजागर करता है।
- घरों और सड़कों के अवशेष: घरों के प्रमाण, जिनमें कई चूल्हे हैं, और बर्तनों के टुकड़ों से पक्की सड़कें और गली-नुक्कड़, संगठित रहने की जगहों और मार्गों का संकेत देते हैं।
- अग्नि वेदी: एक असमान मिट्टी-ईंट का मंच, जो एक अग्नि वेदी से संबंधित है, अनुष्ठानिक या सामुदायिक प्रथाओं का संकेत देता है।
- दिलचस्प खोजें: एक अग्नि गड्ढे के साथ टेराकोटा की ढकी हुई सांप, एक कच्ची हस्तनिर्मित आकृति, और एक कटोरा जैसे कलाकृतियाँ निवासियों के दैनिक जीवन और प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं।
- भंडारण बिन: वर्ग और गोल भंडारण बिन की उपस्थिति खाद्य उत्पादन के अधिशेष को दर्शाती है, जो एक स्थिर और उत्पादक समुदाय का संकेत देती है।
- कलाकृतियों की विविधता: स्थल ने सोने और तांबे की आभूषण, अर्ध-कीमती पत्थर की मणियाँ, तांबे और ज्यामितीय पत्थर के टुकड़े, और हाथी दांत की वस्तुओं सहित कलाकृतियों की समृद्ध विविधता प्रदान की, जो शिल्प कौशल और व्यापार का संकेत देती है।
- लोहे की वस्तुएँ: कृषि उपकरणों जैसे फावड़े और दरांती के रूप में लोहे की वस्तुओं की बड़ी संख्या उस समय की तकनीकी और कृषि प्रथाओं को दर्शाती है।
पेंटेड ग्रे वेयर (PGW) की विशेषताएँ
- PGW के चित्रित ग्रेवेयर की मिट्टी के बर्तन की गुणवत्ता और उपस्थिति: PGW की मिट्टी के बर्तन की गुणवत्ता, चिकनी और समान रंग की होती है, जिसमें रंग सिल्वर ग्रे से battleship grey के बीच में होता है। ये बर्तन उच्च गुणवत्ता की मिट्टी से बने होते हैं, जो एक पतली बनावट प्रदान करते हैं।
- फायरिंग तकनीकें: बर्तनों का समान रंग और बनावट उन्नत फायरिंग तकनीकों का संकेत देती है, जिसमें संभवतः उच्च तापमान या मिट्टी में काले लौह ऑक्साइड की उपस्थिति शामिल है। बर्तन तेज़ गति वाली पहिए पर बनाए गए थे और उन्हें स्क्रेपर्स से चिकना किया गया, जिससे अंडे के छिलके जैसी मोटाई प्राप्त हुई।
- डिज़ाइन पैटर्न: डिज़ाइन, मुख्य रूप से सरल ज्यामितीय पैटर्न, काले या गहरे चॉकलेट ब्राउन रंग में पेंट किए गए थे। सामान्य आकृतियों में रेखाएँ, बिंदु, डैश, वृत्त और स्वस्तिक शामिल हैं, जबकि प्राकृतिक डिज़ाइन जैसे फूलों के पैटर्न कम बार दिखाई देते हैं।
- बर्तन के आकार: PGW की मिट्टी के बर्तनों में खुली मुँह वाली कटोरे और थालियाँ शामिल हैं, जबकि लोटा और लघु बर्तन कम सामान्य हैं।
- उपयोग: PGW की मिट्टी के बर्तन संपन्न व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाते थे, क्योंकि ये कुल मिट्टी के बर्तनों के समूह का 3-10 प्रतिशत ही बनाते हैं। इन्हें अक्सर अन्य मिट्टी के बर्तनों जैसे कि सादा ग्रेवेयर और काले स्लिप्ड वेयर के साथ पाया जाता है, जो शायद दैनिक खाना पकाने और भंडारण के लिए उपयोग किए जाते थे।
चित्रित ग्रेवेयर मिट्टी के बर्तन
- चित्रित ग्रेवेयर (PGW) से जुड़े स्थलों से पता चलता है कि इस अवधि के लोग चावल, गेहूँ, और जौ की खेती में संलग्न थे, जो साल में दो फसलें उगाने की क्षमता का संकेत देता है। हालांकि, सिंचाई विधियों का सीधे प्रमाण नहीं है, लेकिन आगरा के अत्रांजिखेड़ा में आवास क्षेत्र के बाहर गहरे गोल गड्ढों की उपस्थिति कच्चे कुओं के अस्तित्व का संकेत देती है, जो आज भी सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं।
- पशुपालन भी प्रचलित था, जैसा कि मवेशियों, भेड़ों, और सूअरों की हड्डियों की खोज से स्पष्ट होता है, जिनमें से कई जली हुई और कटने के निशान दिखाती हैं। इसके अतिरिक्त, इन स्थलों पर मछली की हड्डियाँ और मछली पकड़ने के हुक भी मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि मछली पकड़ना उनके जीवनयापन के कार्यों का हिस्सा था।
- हस्तिनापुर में घोड़े की हड्डियाँ भी खोजी गई हैं, जो इस क्षेत्र में घोड़ों की उपस्थिति का संकेत देती हैं।
- PGW स्तरों से प्राप्त अधिकांश कलाकृतियाँ युद्ध या शिकार से संबंधित प्रतीत होती हैं, जिनमें तीर के सिर, भाला के सिर, ब्लेड, खंजर, और भाले जैसी वस्तुएँ शामिल हैं।
- हालांकि, वहाँ ऐसे उपकरण भी हैं जैसे कि क्लैंप, सॉकेट, रॉड्स, रिंग्स, पिन्स, चाकू, कुल्हाड़ी, आड़्ज़ और स्क्रेपर्स, जिनमें से कुछ लकड़हारे के काम में उपयोगी होते।
- जखेरा में PGW चरण का परिपक्व स्तर कृषि में उपयोग किए जाने वाले लोहे के औजारों के महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करता है, जैसे कि हार्वेस्टर, हल, और फावड़ा।
- अत्रांजिखेड़ा में PGW स्तरों से पाए गए लोहे के वस्तुओं की विविधता और जखेरा में खोजे गए कृषि उपकरण यह संकेत करते हैं कि इस क्षेत्र में इस अवधि के दौरान लौह उद्योग अच्छी तरह से स्थापित था।
- अत्रांजिखेड़ा में PGW स्तरों से लोहे की कलाकृतियों के रासायनिक विश्लेषण यह बताते हैं कि ये वस्तुएँ व्रॉट आइरन से बनी थीं और फिर संभवतः उच्च तापमान पर चारकोल के बिस्तर पर लंबे समय तक गर्म करके कार्बराइज्ड की गईं।
- इन वस्तुओं की संरचना के साथ-साथ साइट पर पाए गए लोहे के स्लैग के टुकड़े आगरा और ग्वालियर के बीच स्थित लोहे से समृद्ध चट्टानों से मेल खाती है, जो दर्शाता है कि यह क्षेत्र लोहे के अयस्क का स्रोत था।
- PGW चरण के दौरान बस्तियों के पैटर्न के विस्तृत अध्ययन स्थलों के आकार और वितरण में भिन्नताएँ प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए, मक्कन लाल के अध्ययन ने कानपुर जिला में 46 PGW स्थलों की पहचान की, जिनमें से बड़े स्थल आमतौर पर नदी के किनारे स्थित होते हैं।
- इसी तरह, एर्डोसी के शोध ने इलाहाबाद जिला में बस्तियों की दो-स्तरीय पदानुक्रम की पहचान की, जिनमें स्थलों के आकार 0.42 से 10 हेक्टेयर के बीच थे।
- उत्तर हरियाणा में, PGW स्थल भी दो-स्तरीय पदानुक्रम प्रदर्शित करते हैं, जबकि बहावलपुर क्षेत्र में अध्ययन ने स्थलों के आकार की विविधता प्रदर्शित की, जिनमें से अधिकांश 5 हेक्टेयर से कम थे।
राजस्थान से साक्ष्य
भरतपुर के निकट नोह
- अवधि I: पुराना सिरेमिक काल (OCP)
- अवधि II: काले और लाल बर्तन (BRW) कुछ लोहे की वस्तुओं के साथ
- अवधि III: चित्रित ग्रे बर्तन (PGW) लोहे के उपकरणों जैसे कि भाला की धार, तीर की धार, और कुल्हाड़ी के साथ
पूर्वी राजस्थान:
- जोधपुरा: PGW स्तरों से एक क्रूसिबल-आकृति भट्टी का पता चला है, जिसका उपयोग सीधे अयस्क में कमी के लिए किया गया, जो उन्नत धातु विज्ञान प्रथाओं को दर्शाता है।
आहर, दक्षिण-पूर्व राजस्थान में:
- तीन चाँकुलिथिक चरणों की पहचान की गई, जिनमें लोहे की वस्तुएँ चरण Ib और Ic में पाई गईं।
- चरण Ib: तीर की धार, अंगूठियाँ, और स्लैग
- चरण Ic: तीर की धार, छेनी, कीलें, पेग, और सॉकेट
- लोहे की सामग्री वाले स्तरों के लिए कैलिब्रेटेड तिथियाँ 2nd सहस्त्राब्दी BCE में प्रारंभिक लोहे के उपयोग का सुझाव देती हैं, जो संभवतः उपमहाद्वीप में सबसे प्रारंभिक है।
मध्य और निम्न गंगा घाटी
- प्रारंभिक साक्ष्य: लोहे की प्रौद्योगिकी संभवतः मध्य गंगा घाटी में 2nd सहस्त्राब्दी BCE के प्रारंभ से मध्य तक शुरू हुई।
- डडुपुर: BRW स्तरों से कैलिब्रेटेड रेडियोकार्बन तिथियाँ लगभग 1700 BCE के आसपास लोहे के परिचय का सुझाव देती हैं।
- मल्हार: लोहे की सामग्री वाला अवधि II प्रारंभिक 2nd सहस्त्राब्दी BCE का है।
- राजा नल का टीला: लोहे की धातुकर्म और कार्य का साक्ष्य लगभग 1300 BCE का है।
- झूसी: लोहे की वस्तुएँ लगभग 1300 BCE की हैं।
- गंवेरिया: काले-स्लिप वाले बर्तन के साथ लोहे का पता चला।
- कोल्डीहवा: चाँकुलिथिक स्तरों के बाद लोहे के स्तर, जहाँ कुल्हाड़ियों, तीर की धार, क्रूसिबल, और स्लैग का प्रमाण है।
- पंचोह: विभिन्न बर्तन और सूक्ष्म पत्थरों के साथ लोहे की गांठें मिलीं।
- नरहन: अवधि I में पहली बार लोहे की वस्तुएँ प्रकट हुईं और अवधि II में विविधता और मात्रा में वृद्धि हुई, साथ ही अन्य प्रकार की वस्तुओं और कृषि निरंतरता का प्रमाण।
1. पूर्वी भारत
(i) बिहार और बंगाल
बिहार और बंगाल में सबसे प्राचीन लोहे के कलाकृतियाँ BRW संदर्भ (काले और लाल बर्तन) में दिखाई देती हैं, जैसे कि चिरंद, सोनपुर, तरादिह, बहिरी, महिस्दल, और भारतपुर में, जो 1st सहस्त्राब्दी BCE के पहले चौथाई की तिथि में आती हैं। कई स्थलों में चाकोलिथिक BRW चरण से प्रारंभिक लोहे के BRW चरण तक सांस्कृतिक निरंतरता दिखाई देती है। महिस्दल में, प्रारंभिक लोहे के कलाकृतियों को माइक्रोलिथ्स के साथ पाया गया, जबकि बारुदीह में, लोहे को नवपाषाण सामग्री के साथ जोड़ा गया।
(ii) पांडु राजा धिबी और अजय घाटी स्थलों
- पांडु राजा धिबी, अजय घाटी, पश्चिम बंगाल में, चाकोलिथिक स्तरों पर लोहे के कलाकृतियों की रिपोर्ट की गई।
- बहिरी और मंगालकोट स्थलों में भी, अजय घाटी में, समान निष्कर्ष सामने आए।
(iii) बहिरी स्थल
- बहिरी में अवधि I (1112–803 BCE से आगे की तिथि) में निम्नलिखित का प्रमाण मिला:
- वाटल-एंड-डाब घरों के रेमेड फ़्लोर।
- हड्डी के उपकरण, BRW और संबंधित बर्तन, माइक्रोलिथ्स।
- लोहे का अयस्क और स्लाग जमा।
- एक तांबे की तार का टुकड़ा जिसमें लगभग 10% टिन का मिश्रण था।
(iv) मंगालकोट स्थल
- मंगालकोट में अवधि I (बहिरी के समान तिथि सीमा) में निम्नलिखित अवशेष शामिल थे:
- गाय के गोबर से प्लास्टर की गई मिट्टी की फ़्लोर वाले वाटल-एंड-डाब घर, बर्तन के टुकड़े, और ग्रेन्युलर ग्रैवल्स।
- कलाकृतियाँ जैसे कि टेरेकोटा की मूर्तियाँ, वस्तुएँ (गहने, कंगन, स्लिंग बॉल्स, नेट सिंकर), अर्ध-कीमती पत्थर की माणिक, हड्डी के उपकरण, तांबे के कंगन और मछली पकड़ने के हुक।
- लोहे के कलाकृतियाँ जैसे कि बिंदु, भाला के सिर, और चाकू; लोहे का स्लाग और ब्लूम भी पाया गया।
2. मध्य भारत
- लोहे के कलाकृतियाँ BRW स्तरों पर नागदा (चंबल नदी) और एरान (बिना नदी) जैसे स्थलों पर पाई गई हैं, जो चाकोलिथिक और प्रारंभिक लौह युग स्तरों के बीच सांस्कृतिक निरंतरता को दर्शाती हैं।
- नागदा:
अवधि I: मालवा संस्कृति।
अवधि II: BRW द्वारा चिह्नित, जिसमें लोहे की वस्तुएँ जैसे कि डैगर, कुल्हाड़ी, चम्मच, और हल शामिल हैं।
मिट्टी के बर्तन में लाल या क्रीम रंग के बर्तन शामिल थे जिन पर काले रंग में ज्यामितीय डिज़ाइन बनाए गए थे। - एरान:
अवधि I: मालवा संस्कृति।
अवधि IIA: BRW और लोहे के कलाकृतियाँ।
3. उज्जैन स्थल
- BRW स्तरों पर पाए गए लोहे के कलाकृतियों में भाले के सिर, तीर के सिर, चाकू, crowbars, और फावड़े शामिल थे।
इन स्थलों पर लोहे से युक्त BRW स्तर, मालवा संस्कृति स्तरों के बाद, लगभग 1300 ईसा पूर्व की तिथि में हैं, जिसे एरण के चाँदलीथिक स्तरों से प्राप्त कॅलिब्रेटेड C-14 तिथियों द्वारा समर्थित किया गया है।
लोहे का युग एक ऐतिहासिक अवधि को संदर्भित करता है जो लोहे के उपकरणों और हथियारों के व्यापक उपयोग द्वारा विशेषता है, जो प्रौद्योगिकी और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देता है।
मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश में, कई मेगालिथिक स्थलों का पता चला है जिनमें लोहे के कलाकृतियाँ पाई गई हैं। कुछ प्रमुख स्थल हैं:
- Dhanora
- Sonabhir
- Karhibhandari
- Chirachori
- Majagahan
- Kabrahata
- Sorara
- Sankanpalli
- Timmelwada
- Handaguda
- Nelakanker
डेक्कन: डेक्कन क्षेत्र में, सबसे पुराने लोहे के कलाकृतियाँ काले और लाल बर्तन (BRW) स्तरों में पाई जाती हैं, जो अक्सर मेगालिथिक संरचनाओं से जुड़ी होती हैं।
- इन स्तरों और पहले के चाँदलीथिक जोरवे संस्कृति के बीच संबंध स्पष्ट नहीं है।
- कुछ जोरवे स्थलों को कई शताब्दियों के लिए छोड़ दिया गया प्रतीत होता है, फिर 6ठी या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आस-पास फिर से बसने के संकेत मिलते हैं, जबकि अन्य जोरवे चरण और उसके बाद के लोहे के युग के बीच निरंतरता दिखाते हैं।
- प्रकाश जैसे स्थलों पर, नागदा के समान सांस्कृतिक परतों का एक अनुक्रम देखा जाता है, जिसमें मालवा संस्कृति स्तर, निवास का एक अंतराल, लोहे के कलाकृतियों के साथ BRW जमा, और प्रारंभिक ऐतिहासिक उत्तरी काले चमकदार बर्तन (NBPW) स्तर शामिल हैं।
प्रकाश में BRW स्तरों से प्राप्त लोहे के कलाकृतियों में विभिन्न उपकरण और हथियार शामिल थे, जैसे:
तंग किए गए तीर के सिर
- कुल्हाड़ी के सिर
- चाकू के ब्लेड
- सिक्ल
- चिसेल
- तंग वस्तुएं
- क्लैंप
- भाला या भाले के सिर
- फेरुल
- नाखून
महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में कई मेगालिथिक कब्रें और निवास स्थानों ने लोहे की वस्तुएं खोजी हैं, जो उन्नत कृषि बस्तियों का संकेत देती हैं। प्रमुख स्थलों में शामिल हैं:
- तकलघाट-खापा
- नाइकुंड
- महुरझरी
- भागिमोहारी
- बोर्गांव
- रणजला
- पिंपलसुटी
- जुनापानी
नाइकुंड में, कैलिब्रेटेड तिथियां 800–420 ईसा पूर्व और 785–410 ईसा पूर्व के बीच हैं। खुदाई में विभिन्न तांबे और लोहे के कलाकृतियाँ मिलीं, जिनमें शामिल हैं:
- लड्डल
- नाखून
- डैगर के ब्लेड
- तीर के सिर
- चाकू
- चिसेल
- स्पाइक
- कुल्हाड़ी
- दोहरी धार वाली आड्ज़
- ब्लेड और बार/रॉड
- मछलीhooks
- घोड़े के बिट्स
- चूड़ियाँ
- त्रिशूल
- भाले
- तलवारें
- कौर्ड्रन
लोहे की खुरपें और स्थानीय लोहे के पिघलाने के सबूत मिले, जिसमें एक कार्यशाला थी जिसमें भट्ठी और नजदीकी से प्राप्त लोहे का अयस्क था।
महुरझरी: यह स्थल मोती निर्माण के लिए जाना जाता था, और कब्रों में दफनाए गए सामान की समृद्धि इस गतिविधि से जुड़ी हो सकती है। मोती उत्पादन मेगालिथिक काल से लेकर प्रारंभिक ऐतिहासिक चरण तक जारी रहा।
कब्रें और योद्धा परंपरा: महुरझरी और नाइकुंड में, पत्थर के वृत्तों में लोहे के बिट्स और तांबे के आभूषण के साथ घोड़े के अवशेष पाए गए। उल्लेखनीय कब्रों में शामिल हैं:
- एक घोड़े की कब्र जो बलिदान के संकेत दिखाती है
- एक वयस्क पुरुष की कब्र जिसमें तीर का घाव है
- एक वयस्क पुरुष के सीने पर डैगर के साथ एक कब्र
ये कब्रें क्षेत्र में एक योद्धा परंपरा का सुझाव देती हैं।
दक्षिण भारत में, सबसे प्राचीन लोहे की वस्तुएं नियोलीथिक और मेगालिथिक काल के बीच के संक्रमण में पाई जाती हैं। मेगालिथ्स दक्षिण भारत में व्यापक रूप से फैले हुए हैं, जिसमें विभिन्न राज्यों में उल्लेखनीय स्थल हैं:
- तमिलनाडु: महत्वपूर्ण स्थल जैसे अदिचनल्लूर, अमृतमंगलम, कुनटटूर, सनूर, वासुदेवनल्लूर, तेनकासी, कोर्काई, कयाल, कालुगुमलाई, पेरुमलमलाई, पुडुकोटाई, तिरुक्कंपुलियाईर, और ओडुगट-तुर।
- केरल: महत्वपूर्ण स्थलों में पुलिमट्टू, तेंगक्कल, सेंकोट्टा, मुथुकार, पेरिया कणाल, माचाद, pazhayannur, और मंगाडू शामिल हैं। माचाद और pazhayannur को 2वीं सदी BCE और 2वीं सदी CE के बीच का माना जाता है, जबकि मंगाडू में मेगालिथ्स लगभग 1000 से 100 BCE के बीच की तारीख के हैं।
- कर्नाटका: प्रमुख स्थलों में ब्रह्मगिरी, मास्की, हनामसागर, तेरडाल-हलिंगाली, टी. नरसिपुर, और हाल्लूर शामिल हैं, जिनमें हाल्लूर लगभग 1000 BCE का है और कुमर्नाहल्ली का समय 1300–1200 BCE से भी पहले का है।
- आंध्र प्रदेश: स्थलों में कदंबापुर, नागार्जुनकोंडा, येल्लेस्वरम, गल्लापल्ली, तडापत्री, मिरापुरम, और अमरावती शामिल हैं।
- श्रीलंका: काले और लाल बर्तन (BRW) से जुड़े मेगालिथ्स भी पाए गए हैं।
मेगालिथिक प्रकार और क्षेत्रीय संघ: कुछ मेगालिथिक प्रकार विशिष्ट क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जैसे:
- कोडाइकल्स और टोपिकल्स: केरल और कर्नाटका से जुड़े हुए।
- मेंहिर: केरल, आंध्र प्रदेश, और कर्नाटका में पाए जाते हैं।
मेगालिथिक स्थल और प्रारंभिक लौह युग के समुदाय
शुरुआत में, मेगालिथिक स्थलों को घुमंतू पशुपालकों के बस्तियों के रूप में समझा जाता था। हालांकि, सबूत बताते हैं कि दक्षिण भारत के प्रारंभिक लौह युग के समुदाय कृषि, शिकार, मछली पकड़ने, और पशुपालन में संलग्न थे। यहाँ उन्नत कारीगरी परंपराओं के प्रमाण भी हैं, जो स्थायी जीवनशैली का संकेत देते हैं।
कृषि और फसलें: लोग अनाज, बाजरा, और दालें उगाते थे, जिनमें विशिष्ट खोजें शामिल हैं:
पैयम्पल्ली: जौ की जली हुई अनाज, हरे चने, और संभवतः रागी।
- कोडग और खापा (कर्नाटका): चावल की भूसी।
- हलूर: रागी के जले हुए अनाज।
- कुन्नातूर (तमिलनाडु): कब्रों में पाए जाने वाले चावल के दाने।
उपकरण और पीसने के पत्थर: विभिन्न मेगालिथिक स्थलों पर कूटने और पीसने के उपकरण जैसे कूटने वाले और पीसने के पत्थर पाए गए, जो कृषि गतिविधियों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, केरल में मचाड में एक ग्रेनाइट पीसने का पत्थर एक चेस्ट में मिला।
मेगालिथिक स्थलों का स्थान: 2003 में K. राजन द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि तमिलनाडु के पुडुकोट्टाई क्षेत्र में मेगालिथिक स्थलों की निकटता सिंचाई टैंकों (अधिकतर वर्षा आधारित, कुछ धाराओं से भरे) के साथ महत्वपूर्ण थी, जो मेगालिथिक समुदायों और जल संसाधनों के बीच के संबंध को दर्शाती है।
- कुछ संकेत पुराने चित्रों और मूर्तियों से मिलते हैं कि लोग अतीत में कैसे रहते थे। उदाहरण के लिए, केरल के मरयूर और अट्टाला जैसे स्थानों पर शिकार के चित्र दिखाए गए हैं।
- कर्नाटका के हिरे बेंकल में विभिन्न जानवरों जैसे मोरनी, मोर, हरिण और नीलगाय का शिकार करते हुए लोगों के चित्र हैं।
- जंगली और पालतू प्रजातियों की पशु हड्डियों की खोज से पता चलता है कि लोग शिकार और पालतूपन में संलग्न थे।
- गाय, भेड़, कुत्ते और घोड़ों जैसे जानवरों को पालतू बनाया गया, जिसमें गाय सबसे महत्वपूर्ण थीं।
- यह पहले के समय से आजीविका के तरीकों के निरंतरता को दर्शाता है।
- तमिलनाडु के कुछ मेगालिथिक कब्रों में मछली पकड़ने की गतिविधियों को दर्शाते हुए मछलीhooks पाए गए हैं।
विशेषीकृत शिल्प और बर्तन बनाने के प्रमाण
- दक्षिण भारत के मेगालिथिक स्थलों पर विशेष शिल्प के उन्नत परंपराओं के प्रमाण मिले हैं।
- विभिन्न प्रकार के बर्तन पाए गए हैं, जिनमें काले और लाल बर्तन (BRW) शामिल हैं।
- कुछ बर्तन जिनके ढक्कन पर पक्षियों या जानवरों के समान सजावटी फिनियल्स हैं, वे अनुष्ठानिक प्रकृति के प्रतीत होते हैं।
- गहनों के निर्माण की गतिविधियों के संकेत मिलते हैं, जिसमें उकेरे हुए कार्नेलियन गहने और विभिन्न सामग्रियों से बने गहने शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, बर्तन, कटोरे और कंगनों जैसे तांबे और कांस्य के कलाकृतियाँ भी मिली हैं, साथ ही कुछ चांदी और सोने के आभूषण भी।
मेगालिथिक मानवाकृतियों का रहस्य
- कई साल पहले, तमिलनाडु के मोतुर में एक बड़ा मानवाकृति आकृति मिली थी। यह आकृति तीन समवृत्त वृत्तों वाले पत्थर के एक सेट का हिस्सा थी, जिसमें सबसे अंदर का वृत्त आकृति का दक्षिण की ओर मुंह था।
- यह मानवाकृति 3.25 मीटर चौड़ी और ऊंची थी, जिसके मुड़े हुए हाथ और कंधे के ऊपर एक अर्धवृत्ताकार उभार था, जो गर्दन और सिर का प्रतिनिधित्व करता था।
- पैरों के बजाय, इसका आधार था, जिससे यह एक बैठी हुई आकृति का आभास देती थी।
- एक और समान आकृति पहले उदयर्नट्टम में विल्लुपुरम तालुक में मिली थी, जो एक पत्थर के वृत्त का हिस्सा थी, जो एक चेस्ट दफन को चिह्नित करती थी। यह आकृति लगभग 3 मीटर लंबी थी, जिसमें कंधे के ऊपर एक छोटा त्रिकोणीय उभार था जो गर्दन जैसा दिखता है।
- स्थानीय परंपरा इन सिरहीन आकृतियों के लिए एक रोचक व्याख्या प्रस्तुत करती है। यह एक वालियार नामक लघु मानवों के समूह की कहानी सुनाती है, जिन्होंने ‘बारिश की आग’ की आशंका में दक्षिण की ओर भागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने देवता से उनके साथ चलने का अनुरोध किया, लेकिन जब उसने मना कर दिया, तो उन्होंने उसका सिर काट दिया और इसे अपने साथ ले गए, सिरहीन आकृति को पीछे छोड़ दिया।
मानवाकृतियाँ
मानवाकृतियाँ 15 मेगालिथिक स्थलों पर पाई गई हैं, जो मध्य गोदावरी घाटी से लेकर तमिलनाडु की पहाड़ियों तक फैली हुई हैं। महत्वपूर्ण स्थानों में शामिल हैं:
कपरलागुरु गोदावरी पर, अम्बाला वायल केरल में, मिडिमल्ला चित्तूर के निकट, कुमती बेल्लारी जिले में स्थित हैं।
चित्तूर जिले में एगुवाकंताला चेरीवु में तीन मानवाकृत आकृतियाँ निकटता में पाई गईं। पूर्व की आकृति में एक विशेष गोल पोरथोल था। उत्तरी आंध्र प्रदेश में, विशेष रूप से गोदावरी के दक्षिण किनारे पर टोट्टिगुंटा और डोंगाटोगु जैसे स्थलों पर, ऐसी मानवाकृत आकृतियाँ पाई गईं जिनके सिर थे लेकिन हाथ नहीं थे।
इन विशाल मानवाकृत आकृतियों का सटीक महत्व स्पष्ट नहीं है। ये आमतौर पर चेंबर टॉम्ब्स और डोलमेंस के साथ पाई जाती हैं, जो संभावित रूप से पूर्वज पूजा से संबंधित हो सकती हैं।
- मिगालिथिक स्थलों पर लौह वस्तुएँ अन्य धातुओं की तुलना में अधिक सामान्य हैं।
- लौह कलाकृतियों की विस्तृत श्रृंखला पाई गई है—जैसे बर्तन, हथियार (जैसे तीर के सिर, भाले के सिर, तलवारें, और चाकू), लकड़हारे के औजार (जिनमें कुल्हाड़ी, चश्मा, और आरी शामिल हैं), और कृषि उपकरण (जैसे दरांती, फावड़े, और कुल्टर्स)—जो दर्शाता है कि लौह का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता था। कुछ अधिक जटिल धातु की वस्तुएँ जो दफनों में पाई गईं, संभवतः धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई थीं।
धातु की कलाकृतियाँ बनाने के लिए विभिन्न धातुकर्म तकनीकों का उपयोग किया गया था। कुछ तांबे और कांस्य की वस्तुएँ स्पष्ट रूप से मोल्ड में ढाली गई थीं, जबकि अन्य को हथौड़े से आकार दिया गया था।
- कुछ समुदायों के पास धातु मिश्र धातुओं को बनाने का ज्ञान था। उदाहरण के लिए, पझायन्नूर और मचाद से पाए गए लौह कलाकृतियाँ अपेक्षाकृत शुद्ध थीं, जिनमें केवल अन्य तत्वों के ट्रेस मात्रा थे।
- इन स्थलों से अधिकांश धातु की वस्तुएँ पतली धातु की पट्टियों को ठोककर बनाने और उन्हें जोड़ने से तैयार की गई थीं। एक वस्तु, एक हुक, को मोल्डिंग करके बनाया गया था।
कर्नाटका के पैयम्पल्ली जैसे स्थानों पर स्थानीय लौह स्मेल्टिंग के प्रमाण हैं।
कुछ मेगालिथिक स्थल संभवतः व्यापार नेटवर्क से जुड़े शिल्प उत्पादन के केंद्र थे, जैसा कि उनके प्रारंभिक ऐतिहासिक व्यापार मार्गों पर स्थितियों द्वारा संकेत मिलता है। कीमती धातुओं और अर्ध-कीमती पत्थरों से बने गैर-स्थानीय वस्तुओं की उपस्थिति भी अंतर-क्षेत्रीय व्यापार का सुझाव देती है।
मेगालिथिक सिस्ट, ब्रह्मगिरी
- हाल की पुरातात्त्विक कार्यवाही कुदातिनी में बेल्लारी जिले में एक अद्भुत रूप से संरक्षित उत्तर-नवपाषाण काल से प्रारंभिक लौह युग के शवगृह की खोज की गई। इस विशेष दफन में एक द्वितीयक दफन शामिल था। शवगृह और साथ में रखे गए बर्तनों के अंदर एक बच्चे के अवशेष थे, जिसकी उम्र 6 या 7 वर्ष के आस-पास होने का अनुमान है।
- कोडुमनाल के मेगालिथिक स्थल की खुदाई, जो 3वीं शताब्दी BCE से 1वीं शताब्दी CE के बीच है, ने कई दिलचस्प विशेषताओं का खुलासा किया। एक सिस्ट में एक बकरी के अवशेष एक बर्तन में दफनाए गए थे, साथ ही खुदी हुई कार्नेलियन मनके, एक तलवार, और कुल्हाड़ी भी थीं। ऐसा लगता है कि सिस्ट दफनों में, गलियारे का उपयोग अनुष्ठानों के लिए पर्याप्त स्थान बनाने के लिए किया गया।
- कोडुमनाल में कब्रों पर प्राचीन तमिल-ब्रह्मी में ग्रैफिटी चिन्हों की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण खोज थी। कुछ मेगालिथिक कब्रें कई सदियों तक एक ही दफन क्षेत्र के निरंतर उपयोग को दर्शाती हैं। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि ये कब्रें एक पीढ़ी में एक या दो बार से अधिक उपयोग में नहीं आईं, जो संभवतः एक रैंक वाली समाज में एक छोटी कुलीन समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- पूर्व के नवपाषाण-चालकोलिथिक दफनों की तुलना में, बच्चों और युवा वयस्कों के दफनों के साथ मेगालिथिक कब्रों की संख्या कम है, जबकि वयस्क पुरुष दफनों का अनुपात काफी अधिक है।
- मेगालिथिक स्थलों पर पाए गए चट्टान चित्र लड़ाई, मवेशियों की लूट और शिकार के दृश्य दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, तिरुप्पट्टुर तालुक, तमिल नाडु के मेगालिथिक आवास स्थल मल्लापाड़ी में, चट्टान आश्रय में सफेद काओलिन से बने चित्र थे। एक दृश्य में दो घुड़सवारों को लड़ाई करते हुए दिखाया गया है, जबकि दूसरे में एक मानव आकृति को ऊपर उठाए हुए दर्शाया गया है, संभवतः एक डंडा या हथियार पकड़े हुए।
- पैयम्पल्ली में, चित्रों में लड़ाई के दृश्य, नृत्य करने वाली आकृतियाँ, घुड़सवार, वनस्पति, पक्षी, और सूर्य के प्रतीक शामिल थे। ये चित्र मेगालिथिक समुदायों के जीवन और अनुभवों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।
- मेगालिथों के निर्माण में संभवतः समुदाय के सामूहिक प्रयास शामिल थे। ये स्मारक संभवतः उन अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण स्थान के रूप में कार्य करते थे जो लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में अभिन्न थे। समकालीन मेगालिथिक समुदायों के एथनोग्राफिक अध्ययन से पता चलता है कि ऐसे स्मारकों का निर्माण संभवतः भोज, उपहारों के आदान-प्रदान, और गठबंधनों की स्थापना से जुड़ा हो सकता है।
विभिन्न स्थलों से मेगालिथ्स के चित्र
लौह प्रौद्योगिकी का प्रभाव
- लौह प्रौद्योगिकी ने अपने प्रारंभिक चरण से लेकर व्यापक प्रभाव तक एक क्रमिक विकास का अनुभव किया। प्रारंभ में, 2वीं सहस्त्राब्दी BCE के प्रारंभ में कुछ स्थलों पर लौह की छोटी मात्रा पाई गई। हालांकि, लौह का उपयोग लगभग 1000-800 BCE के आस-पास अधिक सामान्य हो गया।
- 800-500 BCE तक, भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में लौह का उपयोग सामान्य था, जो अधिकांश क्षेत्रों में लौह युग की शुरुआत का संकेत देता है, जिसमें गंगा घाटी भी शामिल है। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन बहुत बाद में हुआ।
लौह प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर बहस
- प्राचीन भारत में लोहे की तकनीक का प्रभाव दशकों से बहस का विषय रहा है। यह बहस इतिहास में तकनीक की भूमिका को समझने और विभिन्न क्षेत्रों और समयावधियों में लोहे के उपयोग के प्रमाणों का मूल्यांकन करने से संबंधित है। ध्यान विशेष रूप से 1st सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान गंगा घाटी पर केंद्रित रहा है।
अस्वीकृत परिकल्पनाएँ
- D. D. कोसंबी ने प्रस्तावित किया कि इंडो-आर्यन पूर्व की ओर लोहे के अयस्कों तक पहुँचने के लिए चले गए, जिसने प्रारंभिक ऐतिहासिक समय में मगध राज्य की राजनीतिक प्रभुत्व में योगदान दिया। यह विचार अब अमान्य माना जाता है क्योंकि लोहे के अयस्क पूरे उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से वितरित हैं। हाल की विश्लेषणों से पता चलता है कि प्रारंभिक लोहे के कलाकृतियों के अयस्क संभवतः आगरा और ग्वालियर के बीच की पहाड़ियों से आए, न कि बिहार से।
आर. एस. शर्मा की परिकल्पना
- आर. एस. शर्मा ने गंगा घाटी में लोहे की कुल्हाड़ी और हल की महत्वता पर जोर दिया। उन्होंने तर्क किया कि ये उपकरण जंगलों को साफ करने और कृषि के विस्तार में सहायक थे, जिससे कृषि अधिशेष और शहरीकरण के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। शर्मा ने यह भी सुझाव दिया कि बौद्ध धर्म जैसी धर्मों का उदय लोहे की तकनीक द्वारा लाए गए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों का उत्तर था।
शर्मा की परिकल्पना की आलोचना
- आलोचकों जैसे A. Ghosh और निहारंजन राय ने शर्मा के विचारों पर सवाल उठाया, यह सुझाव देते हुए कि जंगलों को साफ करने के लिए जलने की प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता था, न कि लोहे की कुल्हाड़ियों का। उन्होंने तर्क किया कि पुरातात्त्विक प्रमाण शर्मा के दावों का समर्थन नहीं करते और लोहे की तकनीक का प्रभाव क्रमिक था, जो कि मध्य NBPW चरण के दौरान स्पष्ट हुआ, जब शहरीकरण पहले से ही प्रगति पर था। उन्होंने 1st सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी के ऐतिहासिक परिवर्तनों में सामाजिक-राजनीतिक कारकों के महत्व को भी उजागर किया।
मक्खन लाल का दृष्टिकोण
- मक्खन लाल ने बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई के विचार और यह धारणा कि कृषि अधिशेष और शहरीकरण के लिए लोहे के हल आवश्यक हैं, को चुनौती दी। उन्होंने यह तर्क किया कि पीजीडब्ल्यू से एनबीपीडब्ल्यू स्तरों तक लोहे के उपयोग में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई और कि लोहे की तकनीक कृषि अधिशेष या शहरी विकास के लिए आवश्यक नहीं थी। उन्होंने यह भी इंगित किया कि इस अवधि के दौरान बिहार में लोहे के अयस्कों का दोहन नहीं किया गया।
गंगा घाटी में वन और कृषि
- गंगा के मैदान वास्तव में 16वीं और 17वीं शताब्दी CE तक घने जंगलों से ढके हुए थे, जो पहले सोचा गया था उससे बहुत बाद। जबकि लोहे की जैसी तकनीक ने इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह एकमात्र कारक नहीं था। पुरातात्विक साक्ष्य दिखाते हैं कि गंगा घाटी के कुछ भागों में लोहे की तकनीक का आरंभ 2,000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, जिसमें सबसे प्राचीन लोहे की वस्तुएं BRW या PGW संदर्भों में पाई गईं। समय के साथ, लोहे का उपयोग बढ़ा, विशेष रूप से एनबीपीडब्ल्यू चरण के दौरान।
- कृषि का विस्तार हुआ और इसमें कुछ भूमि की सफाई शामिल थी, लेकिन बड़े क्षेत्र लंबे समय तक वनस्पतिपूर्ण बने रहे। उपनिवेशी काल में, रेलवे के विस्तार, बढ़ती जनसंख्या और कृषि के व्यावसायीकरण के साथ, गंगा घाटी और उपमहाद्वीप में व्यापक वनों की कटाई हुई।
- भिन्न क्षेत्रों के पुरातात्विक डेटा के विस्तृत अध्ययन यह दिखाते हैं कि तकनीकी परिवर्तन और इतिहास के बीच संबंध जटिल है। उदाहरण के लिए, दक्षिण के दूरदराज के क्षेत्रों में, लोहे के प्रारंभिक उपयोग ने तत्काल सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को जन्म नहीं दिया। लोहे के हल मुख्य रूप से जलवृष्टि वाले क्षेत्रों में उपयोग किए गए, और युद्ध और लूट की सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों ने तमिलकम में कृषि वृद्धि में बाधा डाली।
- प्रारंभिक विश्वास कि तकनीक ने अकेले ही इन परिवर्तनों को प्रेरित किया है, को संशोधित किया गया है।
साहित्यिक और पुरातात्त्विक साक्ष्यों के संबंध में चुनौतियाँ
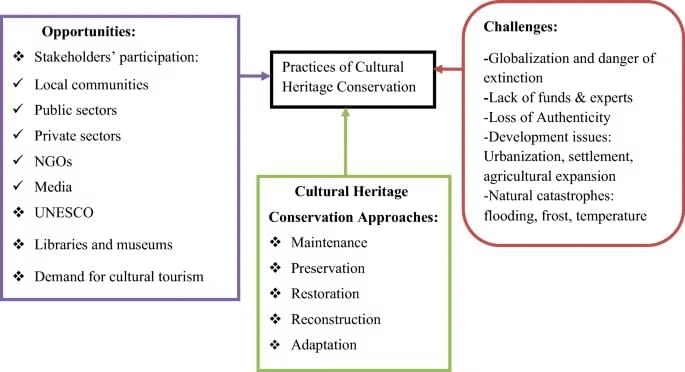
- साहित्य और पुरातत्त्व के बीच संबंध को 2000 से 500 BCE के बीच के समय में मुख्य रूप से आर्यन मुद्दे और वैदिक तथा हरप्पन संस्कृतियों के बीच के संबंध पर केंद्रित किया गया है।
- इसके विपरीत, संगम साहित्य और दक्षिण भारत की मेगालिथिक संस्कृति के बाद के चरणों के बीच संभावित संबंध कम विवादास्पद हैं और इन्हें एक आगामी अध्याय में जांचा जाएगा।
- वैदिक साहित्य को हरप्पन और उत्तर भारत की पोस्ट-हरप्पन पुरातात्त्विक संस्कृतियों से जोड़ने के लिए कई प्रयास किए गए हैं।
- हालांकि, इंडो-आर्यनों और हरप्पन सभ्यता के बीच संबंध विवादास्पद बना हुआ है।
- शोधकर्ताओं के बीच इस बात पर भिन्न दृष्टिकोण हैं कि क्या हरप्पन सभ्यता को वैदिक आर्यनों ने नष्ट किया, क्या हरप्पन के परिपक्व/लेट चरण और इंडो-आर्यन आप्रवासन के बीच ओवरलैप था, या हरप्पन सभ्यता वैदिक आर्यनों की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है।
- साहित्यिक और पुरातात्त्विक साक्ष्यों के बीच संबंध स्थापित करने में चुनौतियाँ उनके मौलिक रूप से अलग स्वभाव, अस्पष्टता और तिथि निर्धारण की समस्याओं से उत्पन्न होती हैं।
- हरप्पन भाषा अज्ञात है, और बिना व्याख्यायित लिखित साक्ष्य के, हरप्पन स्थलों को पाठों से भाषाई, जातीय या सांस्कृतिक समूहों से जोड़ना कठिन है।
- केनेथ कैनेडी का कंकाली रिकॉर्ड का विश्लेषण दिखाता है कि उत्तर-पश्चिम में शारीरिक प्रकारों में असंगतताएँ 6000 से 4500 BCE के बीच हुईं, दूसरी चरण 800 BCE के बाद आई।
- हरप्पन सभ्यता के पतन के दौरान या उसके बाद उत्तर-पश्चिम में जनसांख्यिकीय व्यवधान का कोई प्रमाण नहीं है, जिससे यह संकेत मिलता है कि उस अवधि में कोई आक्रमण या बड़े पैमाने पर प्रवास नहीं हुआ।
- हालांकि, छोटे पैमाने पर प्रवाह की संभावना बनी रहती है।
- इंडो-आर्यनों की पहचान के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं। कुछ पुरातत्वविदों ने Cemetery-H संस्कृति को इंडो-आर्यनों से जोड़ा है, जबकि अन्य ने चनहुदरो में पोस्ट-शहरी चरण में विदेशी तत्वों की पहचान की है।
- गंधार कब्र संस्कृति स्थलों पर अंत्येष्टि प्रथाओं, अग्नि पूजा और घोड़े के उपयोग में परिवर्तनों को भी इंडो-आर्यनों से जोड़ा गया है।
- ताम्र खजाने को प्रारंभिक इंडो-आर्यनों, हरप्पन शरणार्थियों, या दोआब के पूर्व-आर्यन निवासियों के साथ जोड़ा गया है।
- PGW संस्कृति को कालानुक्रमिक और भौगोलिक ओवरलैप के आधार पर बाद के वैदिक आर्यनों से संबंधित करने का सुझाव दिया गया है।
- PGW संस्कृति को महाभारत में घटनाओं से भी जोड़ा गया है।
- राजस्थान, मध्य भारत और दक्कन में ताम्र-पाषाण काल की संस्कृतियों को पूर्व-आर्यनों, आर्यनों, या गैर-वैदिक आप्रवासी के रूप में विभिन्न रूप से पहचाना गया है।
- इन संबंधों में, कई शोधकर्ता बाद की वैदिक संस्कृति और PGW के बीच संबंध को स्वीकार करते हैं।
निष्कर्ष
2000 से 500 ईसा पूर्व के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक परिदृश्य देखा गया, जैसा कि साहित्य और पुरातत्व द्वारा प्रकट होता है। इस युग में कई क्षेत्रों ने ताम्र-पाषाण (chalcolithic) चरण से लौह युग (iron age) में संक्रमण किया। इतिहासकारों ने ऐतिहासिक परिवर्तन के व्यापक पैटर्न की पहचान करने के लिए वेदिक ग्रंथों का उपयोग किया, विशेष रूप से उत्तर-पश्चिम और ऊपरी गंगा घाटी में, जबकि पुरातत्व ने उपमहाद्वीप में लोगों के दैनिक जीवन और बस्तियों के पैटर्न पर अंतर्दृष्टि प्रदान की।
- इस अवधि से मिले साक्ष्य बताते हैं कि कई बस्तियों की उपस्थिति थी, जिनमें से कई एक स्थिर कृषि आधार पर आधारित थीं, जो वर्ष में दो फसलों का समर्थन करने में सक्षम थीं।
- इन्हें पशु पालन और शिकार की प्रथाओं के साथ जोड़ा गया था।
- कुछ क्षेत्रों में एक श्रेणीबद्ध बस्ती संरचना देखी गई, जिसमें कुछ बड़े, कभी-कभी किलेबंद बस्तियाँ महत्वपूर्ण जनसंख्या का समर्थन करती थीं।
- विशेषीकृत हस्तशिल्प और लौह धातु विज्ञान अधिकांश क्षेत्रों में प्रमुख हो गए, और कच्चे माल और तैयार वस्तुओं के बीच क्षेत्रीय और लंबी दूरी के व्यापार के सबूत मौजूद हैं, जो बढ़ती सामाजिक-आर्थिक जटिलता का सुझाव देते हैं।
- दक्कन में इनामगाँव जैसी स्थलों से पुरातात्विक निष्कर्षों से पता चलता है कि समाज का एक प्रमुख स्तर था, जबकि बाद के वेदिक ग्रंथ गंगा घाटी में जनजातीय से क्षेत्रीय राज्य संगठन के संक्रमण को दर्शाते हैं।
- इस अवधि के अंत तक, उत्तरी भारत शहरीकरण के कगार पर था, जो भविष्य के विकास के लिए मंच तैयार कर रहा था।
|
198 videos|620 docs|193 tests
|















