स्पेक्ट्रम सारांश: 1857 से पहले ब्रिटिश के खिलाफ लोगों का प्रतिरोध | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download
1857 के विद्रोह से पहले, भारत में लोग पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष के संकेत दिखा रहे थे। विभिन्न घटनाओं ने यह संकेत दिया कि हर कोई खुश नहीं था, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिरोध का माहौल बना। 1857 का विद्रोह एक बड़ा विस्फोट था, लेकिन यह विदेशी शासन के खिलाफ असंतोष की पहली अभिव्यक्ति नहीं थी।
लोगों का प्रतिरोध: अर्थ
- समाज के विविध वर्ग: ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों का प्रतिरोध भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में फैला हुआ था, जिसमें किसान, कारीगर, जनजातीय लोग, शासक वर्ग (सक्रिय और वंचित दोनों), ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत सैन्य कर्मी, पूर्व शासकों के गैर-कार्यरत सैनिक और हिंदू एवं मुस्लिम समुदायों के धार्मिक नेता शामिल थे।
- संयुक्त और अलग आंदोलन: विभिन्न समूह कभी-कभी अपने प्रतिरोध में एकजुट हो जाते थे। उदाहरणों में 1810 में वाराणसी में घर कर के खिलाफ आंदोलन, 1814 में सूरत में नमक कर के खिलाफ दंगे और 1816 में बरेली में पुलिस और नगरपालिका कर के खिलाफ विद्रोह शामिल हैं। इन आंदोलनों में विभिन्न सामाजिक स्तरों के लोग शामिल थे, जैसे कारीगर, छोटे दुकानदार, शहरी गरीब और समृद्ध शहरी वर्ग।
- विभिन्न grievances: जबकि प्रत्येक वर्ग की अपनी विशिष्ट grievances थीं, उनका सामान्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। इन प्रतिरोधों के हित भिन्न थे, लेकिन वे स्वतंत्रता के साझा लक्ष्य पर संगठित हुए।
प्रतिरोध के रूप: इतिहासकार बिपिन चंद्र के अनुसार, लोगों का प्रतिरोध तीन व्यापक रूपों में प्रकट हुआ:
- नागरिक विद्रोह: शहरी क्षेत्रों में विशिष्ट औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ उठने वाले विद्रोह, जैसे कि वाराणसी, सूरत, और बरेली के उदाहरण।
- जनजातीय विद्रोह: ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनजातीय समुदायों के प्रतिरोध आंदोलन।
- किसान आंदोलन: ग्रामीण समुदायों, मुख्यतः किसानों द्वारा ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन और विद्रोह।
सैन्य विद्रोह: सैन्य विद्रोहों को भी लोगों के प्रतिरोध के एक रूप के रूप में देखा गया। इसमें कंपनी की सेनाओं में कार्यरत भारतीय शामिल थे जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। यह समावेश इस अवधि के दौरान लोगों के प्रतिरोध को एक व्यापक समझ प्रदान करने के लिए था।
लोगों के प्रतिरोध की उत्पत्ति
- पूर्व-औपनिवेशिक विरोध: पूर्व-औपनिवेशिक भारत में, लोग आमतौर पर शासकों और अधिकारियों के खिलाफ उच्च भूमि राजस्व मांगों, भ्रष्टाचार और अधिकारियों के कठोर व्यवहार के कारण विरोध करते थे।
- औपनिवेशिक शासन का प्रभाव: औपनिवेशिक शासन की स्थापना का भारतीयों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। औपनिवेशिक नीतियाँ विनाशकारी थीं, और ब्रिटिश मुख्य रूप से राजस्व निकालने पर केंद्रित थे बिना लोगों की चिंताओं को संबोधित किए।
- grievances पर ध्यान की कमी: औपनिवेशिक शासन के तहत, भारतीय जनसंख्या की समस्याओं पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। कंपनी का मुख्य हित राजस्व संग्रहण में था।
- पार्टी प्रतिरोध: अन्य विकल्पों की कमी के चलते, लोगों ने औपनिवेशिक शासकों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ खुद को बचाने के लिए हथियार उठाने का निर्णय लिया।
- जनजातीय लोगों की दुर्दशा: जनजातीय लोगों की स्थिति मुख्य भूमि की तरह ही थी, लेकिन उनके स्वतंत्र जनजातीय राजनीति में बाहरी लोगों के हस्तक्षेप ने उन्हें अधिक आक्रोशित और हिंसा के प्रति प्रवृत्त बना दिया।
लोगों के विद्रोहों के कारण: कंपनी शासन के खिलाफ लोगों के असंतोष और विद्रोह के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:
- औपनिवेशिक भूमि राजस्व निपटान, नए करों का भारी बोझ, किसानों को उनकी भूमि से बेदखल करना, और जनजातीय भूमि पर अतिक्रमण।
- ग्रामीण समाज में शोषण और मध्यस्थ राजस्व संग्रहकर्ताओं, किरायेदारों और साहूकारों की वृद्धि।
- जनजातीय भूमि पर राजस्व प्रशासन का विस्तार जनजातीय लोगों की कृषि और वन भूमि पर नियंत्रण का हनन।
- ब्रिटिश निर्मित सामानों को बढ़ावा देना, और भारतीय उद्योगों पर भारी शुल्क, विशेषकर निर्यात शुल्क, ने भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योगों को नष्ट कर दिया।
- देशी उद्योगों के विनाश के कारण श्रमिकों का कृषि की ओर पलायन हुआ, जिससे भूमि/कृषि पर दबाव बढ़ा।
नागरिक विद्रोह: इस संदर्भ में 'नागरिक' शब्द में वे विद्रोह शामिल हैं जो सैन्य से संबंधित नहीं थे। ये विद्रोह आमतौर पर निर्वासित स्वदेशी शासकों, उनके वंशजों, पूर्व जमींदारों, और दक्षिण भारतीय पोलिगारों द्वारा नेतृत्व किए गए। पोलिगार वे लोग थे जो शासकों द्वारा सैन्य सेवा और कर के बदले में भूमि का अधिकार रखते थे।
ये विद्रोह पूर्व-नियुक्त रिटेनर्स, पराजित राज्यों के अधिकारियों, और कभी-कभी धार्मिक नेताओं द्वारा शामिल थे। मुख्य समर्थन रैक-रेंटेड किसानों, बेरोजगार कारीगरों, और गैर-कार्यरत सैनिकों से आया। हालाँकि, इन आंदोलनों के मूल में वे once-powerful वर्ग थे जिन्होंने अपनी सत्ता खो दी थी और अब प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहे थे।
महत्वपूर्ण नागरिक विद्रोह:
- संस्यासी विद्रोह (1763-1800): 1770 में हुई भयंकर famine और कठिन ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण पूर्वी भारत में unrest फैला। संस्यासी, जो मूल रूप से किसानों थे जिन्हें उनकी भूमि से बेदखल किया गया था, ने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया।
- मिदनापुर और डालभूम में विद्रोह (1766-74): अंग्रेजों ने 1760 में मिदनापुर पर नियंत्रण प्राप्त किया, जहाँ लगभग 3,000 जमींदारों और तालुकदारों के अपने रैयतों (किसान किरायेदारों) के साथ मित्रवत संबंध थे।
- मोमारिया विद्रोह (1769-99): 1769 में मोमारिया विद्रोह ने असम में अहोम राजाओं के अधिकार को चुनौती दी।
- गोरखपुर, बस्ती, और बहेराइच में नागरिक विद्रोह (1781): वॉरेन हेस्टिंग्स ने मराठों और मैसूर के खिलाफ युद्ध खर्चों के लिए धन जुटाने का प्रयास किया।
- विजयनगरम के राजा का विद्रोह (1794): अंग्रेजों ने एक वैधता के बिना विजयनगरम के राजा से तीन लाख रुपये की ट्रिब्यूट की मांग की, जिससे राजा ने विद्रोह किया।
- बेदनूर में धुंडिया का विद्रोह (1799-1800): मैसूर के विजय के बाद, अंग्रेजों ने स्थानीय नेताओं से प्रतिरोध का सामना किया।
- केरला वर्मा पझास्सी राजा का प्रतिरोध (1797; 1800-05): पझास्सी राजा ने ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध किया।
- अवध में नागरिक विद्रोह (1799): वजीर अली खान, अवध के चौथे नवाब, ने ब्रिटिशों के साथ संघर्ष किया।
- गंजाम और गुम्सुर में विद्रोह (1800, 1835-37): गंजाम में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ।
- पलामऊ में विद्रोह (1800-02): 1800 में, भुखन सिंह, एक चेरो प्रमुख, ने विद्रोह किया।
- पोलिगारों का विद्रोह (1795-1805): दक्षिण भारत में पोलिगारों ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया।
- भिवानी में विद्रोह (1809): 1809 में, हरियाणा के जाटों ने विद्रोह किया।
- दीवान वेलू थम्पी का विद्रोह (1808-1809): ट्रावंकोर में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह हुआ।
- Bundelkhand में disturbances (1808-12): बंडेलखंड को ब्रिटिशों ने जीत लिया और वहां विद्रोह हुआ।
- पार्लाकिमेडी विद्रोह (1813-34): कंपनी के अधिग्रहण के बाद, ब्रिटिशों ने एक सेना भेजी।
- कच्छ विद्रोह (1816-1832): कच्छ के महाराजा ने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया।
- बरेली में विद्रोह (1816): पुलिस कर के प्रस्ताव ने नागरिकों में आक्रोश पैदा किया।
- हाथरस में उथल-पुथल (1817): बढ़ते राजस्व के कारण विद्रोह हुआ।
- पैका विद्रोह (1817): ओडिशा में पैका विद्रोह हुआ।
- वाघेरा विद्रोह (1818-1820): वाघेरा प्रमुखों ने बाहरी शासन के खिलाफ विद्रोह किया।
- आहोम विद्रोह (1828): ब्रिटिशों ने आहोम क्षेत्र में विद्रोह को जन्म दिया।
- सूरत नमक आंदोलन (1840 के दशक): सूरत की स्थानीय जनसंख्या ने नमक शुल्क में वृद्धि के खिलाफ विद्रोह किया।
- कोल्हापुर और सावंतवाड़ी विद्रोह: गडकरी वर्ग ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया।
- वहाबी आंदोलन: वहाबी आंदोलन एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था।
- कुका आंदोलन: कुका आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था।
किसान आंदोलन धार्मिक रंग में: किसान विद्रोह भूमि से बेदखली, किरायों में वृद्धि और साहूकारों की लालची नीतियों के खिलाफ थे।
- नर्केलबरिया विद्रोह: तितु मीर ने पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया।
- पागल पंथी: पागल पंथी, मुख्य रूप से हाजोंग और गारो जनजातियों का एक अर्ध-धार्मिक समूह था।
- फराज़ी विद्रोह: फराज़ी एक मुस्लिम पंथ के अनुयायी थे।
- मोप्पला विद्रोह: राजस्व मांग में वृद्धि और क्षेत्र में अधिकारियों के अत्याचार से विद्रोह हुआ।
- 1857 के विद्रोह में किसानों की भूमिका: किसानों ने कई स्थानों पर स्थानीय सामंती नेताओं के साथ मिलकर विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
जनजातीय विद्रोह: ब्रिटिश शासन के तहत जनजातीय आंदोलन सबसे अधिक आवर्ती, मिलिटेंट, और हिंसक थे।
- पहाड़िया विद्रोह: ब्रिटिशों के क्षेत्र में विस्तार ने पहाड़ी जनजातियों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया।
- चुआर विद्रोह: भूमि राजस्व मांगों और आर्थिक संकट ने चुआर जनजातियों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया।
- कोल विद्रोह (1831): कोल जनजातियों ने भूमि हस्तांतरण के खिलाफ विद्रोह किया।
- हो और मुंडा विद्रोह (1820-1837): हो जनजातियों ने सिंहभूम के अधिग्रहण के खिलाफ विद्रोह किया।
- सांथाल विद्रोह (1855-56): सांथालों ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया।
- खोंड विद्रोह (1837-1856): खोंड जनजातियों ने कंपनी शासन के खिलाफ विद्रोह किया।
- कोया विद्रोह: कोया जनजातियों ने कई बार विद्रोह किया।
- भील विद्रोह: भील जनजातियों ने कंपनी शासन के खिलाफ विद्रोह किया।
- कोली विद्रोह: कोली जनजातियों ने कंपनी शासन के खिलाफ विद्रोह किया।
- रामोसी विद्रोह: रामोसी जनजातियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया।
उत्तर-पूर्व के जनजातीय आंदोलन: उत्तर-पूर्वी सीमा क्षेत्र के कुछ प्रसिद्ध जनजातीय आंदोलनों में शामिल हैं:
- खासी विद्रोह: खासी, गारो, खामpti और सिंगफो ने खुद को संगठित किया।
- सिंगफो विद्रोह: सिंगफो विद्रोह 1830 में हुआ।
- सेपॉय विद्रोह: 1857 के महान विद्रोह से पहले कई स्थानों पर सैन्य विद्रोह हुए।
लोगों के विद्रोहों की कमजोरियाँ: ये विद्रोह एक बड़ी संख्या में प्रतिभागियों को आकर्षित करते थे, लेकिन स्थानीयकृत थे और विभिन्न समयों पर अलग-अलग क्षेत्रों में होते थे।
- इनमें से अधिकांश स्थानीय grievances से उत्पन्न हुए।
- नेतृत्व आधे-फ्यूडल था, पारंपरिक दृष्टिकोण रखता था और उनका प्रतिरोध मौजूदा सामाजिक सेट-अप के लिए कोई विकल्प नहीं देता था।
- जो विद्रोह समान थे, वे सभी विदेशी शासन के खिलाफ थे।
- ये विद्रोह सदियों पुरानी रूप और वैचारिकी/संस्कृति की सामग्री में थे।
- जो लोग इतने असहयोगी या जिद्दी नहीं थे, उन्हें अधिकारियों द्वारा रियायतों के माध्यम से संतुष्ट किया गया।
- इन विद्रोहों में लड़ाकों द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियाँ और हथियार उनके विरोधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियारों और रणनीतियों की तुलना में लगभग पुरानी थीं।
जैसा कि आपने पहले स्वतंत्रता के पहले युद्ध की ओर ले जाने वाले छोटे-छोटे घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। अगली EduRev दस्तावेज़ में आप प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे और 1857 के युद्ध के बारे में, जिसे भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है और यह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ राजनैतिक संघ के पहले संकेतों का प्रतीक है।
1857 की विद्रोह से पहले, भारत में लोग पूर्वी भारत कंपनी के तहत ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष के संकेत दिखा रहे थे। विभिन्न घटनाओं ने यह संकेत दिया कि हर कोई खुश नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिरोध पैदा हुआ। 1857 का विद्रोह एक प्रमुख विस्फोट था, लेकिन यह विदेशी शासन के खिलाफ असंतोष की पहली अभिव्यक्ति नहीं थी।
- समाज के विविध वर्ग: ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों का प्रतिरोध भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में शामिल था, जिसमें किसान, कारीगर, आदिवासी, शासक वर्ग (सक्रिय और वंचित दोनों), पूर्वी भारत कंपनी के तहत सैन्य कर्मी, पूर्व शासकों के निरस्त्रीकरण किए गए सैनिक, और हिंदू तथा मुस्लिम समुदायों के धार्मिक नेता शामिल थे।
- संयुक्त और अलग आंदोलन: विभिन्न समूह कभी-कभी अपने प्रतिरोध में एकजुट होते थे। उदाहरणों में वाराणसी में 1810 का घर कर के खिलाफ आक्रोश, सूरत में 1814 का नमक कर के खिलाफ दंगें, और बरेली में 1816 का पुलिस और नगरपालिका कर के खिलाफ विद्रोह शामिल हैं। इन आंदोलनों में विभिन्न सामाजिक स्तरों के लोग शामिल थे, जैसे कारीगर, छोटे दुकानदार, शहरी गरीब, और समृद्ध शहरी उच्च वर्ग।
- विभिन्न शिकायतें: जबकि प्रत्येक वर्ग की अपनी अलग शिकायतें थीं, उनका सामान्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन का अंत करना था। इन प्रतिरोधों के हित भिन्न थे, लेकिन वे मुक्ति के साझा लक्ष्य पर केंद्रित थे।
- प्रतिरोध के रूप: इतिहासकार बिपिन चंद्र के अनुसार, लोगों का प्रतिरोध तीन व्यापक रूपों में सामने आया:
- नागरिक विद्रोह: शहरी क्षेत्रों में विशिष्ट उपनिवेशी नीतियों के खिलाफ उठ खड़े होने वाले आंदोलन, जैसे कि वाराणसी, सूरत और बरेली में उल्लेखित उदाहरण।
- आदिवासी विद्रोह: आदिवासी समुदायों का ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध आंदोलन।
- किसान आंदोलन: ग्रामीण समुदायों, मुख्य रूप से किसानों द्वारा, ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन और विद्रोह।
- सैन्य विद्रोह: सैन्य विद्रोह को भी लोगों के प्रतिरोध के एक रूप के रूप में माना गया। इसमें कंपनी की सेनाओं में कार्यरत भारतीय शामिल थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इस समावेश का उद्देश्य इस अवधि के दौरान लोगों के प्रतिरोध का अधिक व्यापक समझ प्रदान करना था।
लोगों के प्रतिरोध की उत्पत्ति
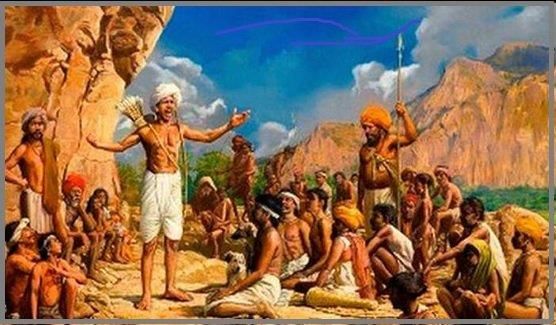
लोगों के प्रतिरोध का उद्भव
- पूर्व-औपनिवेशिक विरोध: पूर्व-औपनिवेशिक भारत में, लोग उच्च भूमि राजस्व मांगों, भ्रष्टाचार, और अधिकारियों के कठोर व्यवहार के कारण शासकों और अधिकारियों के खिलाफ सामान्यतः विरोध करते थे।
- औपनिवेशिक शासन का प्रभाव: औपनिवेशिक शासन की स्थापना ने भारतीयों पर गंभीर प्रभाव डाला। औपनिवेशिक नीतियाँ विनाशकारी थीं, और ब्रिटिश मुख्यतः राजस्व निकालने पर केंद्रित थे, जबकि लोगों की चिंताओं का समाधान नहीं किया गया।
- शिकायतों पर ध्यान की कमी: औपनिवेशिक शासन के तहत, भारतीय जनसंख्या की शिकायतों को सुनने या उनके समस्याओं पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। कंपनी का मुख्य ध्यान राजस्व एकत्रित करने में था।
- पक्षपाती कानूनी प्रणाली: औपनिवेशिक कानून और न्यायपालिका ने सरकार और इसके सहयोगियों, जैसे ज़मींदारों, व्यापारियों, और धन उधार देने वालों के हितों की रक्षा की। इस प्रणाली ने आम लोगों को न्याय नहीं दिया।
- सशस्त्र प्रतिरोध: अन्य विकल्पों के बिना, लोगों ने औपनिवेशिक शासकों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अपने बचाव के लिए हथियार उठाने का फैसला किया।
- आदिवासी लोगों की दुर्दशा: आदिवासी लोगों की स्थिति मुख्य भूमि के समान थी, लेकिन उनके स्वतंत्र आदिवासी शासन में बाहरी लोगों के हस्तक्षेप ने उन्हें और अधिक पीड़ित और हिंसा के प्रति प्रवृत्त किया। अतिक्रमण ने उनके अन्याय की भावना को बढ़ा दिया और अधिक आक्रामक प्रतिक्रिया का कारण बना।
- भूमि राजस्व की औपनिवेशिक समझौतें: नए करों का भारी बोझ, किसानों को उनकी भूमि से निकालना, और आदिवासी भूमि पर अतिक्रमण।
- ग्रामीण समाज में शोषण: मध्यस्थ राजस्व संग्रहकर्ताओं, किरायेदारों और धन उधार देने वालों की वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ।
- आदिवासी भूमि पर राजस्व प्रशासन का विस्तार: आदिवासी लोगों की कृषि और वन भूमि पर नियंत्रण का नुकसान।
- ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रचार: भारतीय उद्योगों पर भारी शुल्क, विशेष रूप से निर्यात शुल्क, ने भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योगों को नष्ट कर दिया।
- स्वदेशी उद्योग का विनाश: इससे श्रमिकों का उद्योग से कृषि में प्रवास हुआ, जिससे भूमि/कृषि पर दबाव बढ़ गया।
- इस संदर्भ में 'नागरिक' शब्द: यह उन विद्रोहों को शामिल करता है जो सैन्य से अप्रासंगिक हैं। ये विद्रोह आमतौर पर अपदस्थ स्वदेशी शासकों, उनके वंशजों, पूर्व ज़मींदारों, ज़मींदारों, और दक्षिण भारतीय पोलिगारों द्वारा नेतृत्व किए जाते थे।
- विद्रोह में शामिल: पूर्व रिटेनर्स, विजय प्राप्त राज्यों के अधिकारी, और कभी-कभी धार्मिक नेता। मुख्य समर्थन किरायेदार किसानों, बेरोजगार कारीगरों, और निरस्त्र सैनिकों से आता था।
- हालांकि, इन आंदोलनों के केंद्र में वे once-शक्ति शाली वर्ग थे जिन्होंने अपनी सत्ता खो दी थी और अब प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहे थे।
- 1770 की भयंकर अकाल: और कठिन ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने पूर्वी भारत में अशांति पैदा की।
- सांयासी विद्रोह: मूल रूप से भूमि से निकाले गए किसान, ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया।
- छोटे ज़मींदारों, विघटनकारी सैनिकों, और ग्रामीण गरीबों द्वारा सहयोग: सांयासी ने कंपनी के कारखानों और खजानों पर छापे मारे, कंपनी की सेनाओं के खिलाफ युद्ध में भाग लिया।
- महत्वपूर्ण नेता: मेजनूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, और देवी चौधुरानी शामिल थे।
- हिंदू और मुस्लिम समान रूप से इस विद्रोह में भाग लेते थे, जिसे फकीर विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
- वॉरेन हेस्टिंग्स ने लंबे संघर्ष के बाद सांयासी को दबा दिया।
- देवी चौधुरानी की भागीदारी ने ब्रिटिश के खिलाफ प्रारंभिक प्रतिरोधों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया।
- बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की उपन्यास \"आनंदमठ\" और \"देवी चौधुरानी\" ने सांयासी विद्रोह से प्रेरणा ली, जो महिलाओं के पारंपरिक भारतीय मूल्यों को बचाने में उनके महत्व को रेखांकित करती है।
- 1799 में मैसूर के विजय के बाद: अंग्रेजों ने स्वदेशी नेताओं से प्रतिरोध का सामना किया।
- धुंडिया वाघ: एक स्थानीय मराठा नेता जो टिपू सुलतान द्वारा इस्लाम में परिवर्तित हुआ, सिरींगपट्टम के पतन के बाद जेल से रिहा हुआ।
- धुंडिया ने एक विरोधी ब्रिटिश बल का गठन किया: और अपने लिए एक छोटा क्षेत्र स्थापित किया।
- अगस्त 1799 में अंग्रेजों द्वारा पराजित होकर, उसने मराठा क्षेत्र में शरण ली।
- धुंडिया ने निराश राजकुमारों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया और नेतृत्व किया।
- सितंबर 1800 में, वह ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए मारा गया।
- अपनी असफलता के बावजूद, धुंडिया जनता के बीच एक पूजनीय नेता बन गया।
- केरल वर्मा पझसी राजा: केरल सिम्हम या 'पिचे राजा' के नाम से जाने जाते हैं।
- मलाबार में कुट्टायम के प्रभावी प्रमुख।
- 1793 से 1805 तक हैदर अली, टिपू सुलतान, और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा।
- तीसरा ऐंग्लो-मैसूर युद्ध (1790-92): अंग्रेजों ने 1790 के समझौते का उल्लंघन किया, कुट्टायम पर सर्वोच्चता बढ़ाई।
- जनता का प्रतिरोध (1793): नए राजा ने कंपनी के राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसानों पर अत्यधिक कर लगाया।
- शांति संधि (1797): पझसी राजा ने गुरिल्ला युद्ध का उपयोग करते हुए बहादुरी से लड़ा, जिससे 1797 में शांति संधि हुई।
- विद्रोही युद्ध (1800): 1800 में वायनाड पर संघर्ष ने विद्रोही युद्ध को फिर से भड़काया।
- संगठित बल (1805): पझसी राजा ने नायरों, मप्पिलास, और पठानों (टिपू के निरस्त्र सैनिकों) का एक बड़ा बल संगठित किया।
- मृत्यु (नवंबर 1805): केरल सिम्हम मविला तोडु के पास एक गोलीबारी में मारा गया।
- वजीर अली खान: अवध के चौथे नवाब, प्रारंभ में ब्रिटिश समर्थन प्राप्त करते थे लेकिन बाद में उनके साथ संघर्ष किया।
- 1799 में बनारस का नरसंहार: जब वजीर अली ने एक ब्रिटिश निवासी को मार डाला, तो संघर्ष उत्पन्न हुआ।
- जनरल अर्स्किन द्वारा पराजित होने के बाद, वजीर अली बुटवाल भाग गया और जयपुर में शरण मांगी।
- आर्थर वेल्सले ने वजीर अली को कुछ शर्तों के तहत जयपुर से प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया।
- वजीर अली ने दिसंबर 1799 में आत्मसमर्पण किया और कलकत्ता के फोर्ट विलियम में कैद कर दिया गया।
9. गंजाम और गुम्सुर में विद्रोह (1800, 1835-37)



उत्तर भारत के सर्कारों में विद्रोह, जिसमें गंजाम शामिल है, ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध किया। गुमसुर के जमींदार स्ट्रिकार भंज ने 1797 में राजस्व न चुकाने के कारण इस विद्रोह का नेतृत्व किया। 1800 में खुला विद्रोह हुआ; दमनकारी कलेक्टर स्नोडग्रास को विद्रोह को दबाने के लिए बदला गया।
- 1800 में खुला विद्रोह; दमनकारी कलेक्टर स्नोडग्रास को विद्रोह दबाने के लिए बदला गया।
- 1819 और 1830 के बीच स्ट्रिकार को फिर से जमींदार के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन वे बकाया राशि के कारण सेवानिवृत्त हो गए।
- 1835 में गुमसुर और कोलैडा के ब्रिटिश अधिग्रहण के खिलाफ धनंजय की दूसरी विद्रोह।
- 1835 में धनंजय की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा निरंतर प्रतिरोध।
1800 में, भूखान सिंह, एक चेरो प्रमुख, ने विद्रोह किया। कर्नल जोन्स ने विद्रोह को दबाने के लिए पलामऊ और सरगुजा में दो साल तक डेरा डाला।
- 1800 में भूखान सिंह, एक चेरो प्रमुख, ने विद्रोह किया।
- कर्नल जोन्स ने विद्रोह को दबाने के लिए पलामऊ और सरगुजा में दो साल तक डेरा डाला।
1795 और 1805 के बीच, दक्षिण भारत के पोलिगार (स्थानीय शासक) ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया, जिसमें तिननेवेली, रामानाथापुरम, शिवगंगा, शिवागिरी, मदुरै और उत्तर आर्कोट में मुख्य विद्रोह हुए। संघर्ष 1781 में शुरू हुआ जब आर्कोट के नवाब ने तिननेवेली और कर्णाटक प्रांतों का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, जिससे पोलिगारों में नफरत बढ़ी।
- 1795 में पहला विद्रोह, जिसका नेतृत्व कट्टाबोम्मन नायकन ने किया, कराधान और अंग्रेजों के व्यवहार के चारों ओर केंद्रित था।
- प्रारंभिक सफलता के बाद, कट्टाबोम्मन को धोखा दिया गया, पकड़ा गया और फांसी पर लटकाया गया।
- 1801 में दूसरे चरण में एक हिंसक विद्रोह हुआ, जिसमें ऊमतुराई और मारथु पांडियन का नेतृत्व था।
- उत्तर आर्कोट में 1803 से 1805 के बीच विद्रोह हुआ, जिसमें कावल शुल्क संग्रह अधिकारों का इनकार शामिल था।
- व्यापक विद्रोह ने विदेशी शासन के खिलाफ एक जन आंदोलन और स्वतंत्रता की खोज के विश्वास को दर्शाया।
1809 में, हरियाणा के जाटों ने विद्रोह किया।
- 1809 में, हरियाणा के जाटों ने विद्रोह किया।
ईस्ट इंडिया कंपनी और त्रावणकोर ने 1805 में एक साथ काम करने पर सहमति जताई, लेकिन कंपनी ने कड़े नियम लागू किए जिससे त्रावणकोर के लोग बहुत असंतुष्ट हो गए। त्रावणकोर पैसे का भुगतान नहीं कर सका और वहां के ब्रिटिश अधिकारी उनके मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। इन सभी समस्याओं के कारण त्रावणकोर के नेता वेलू थांपी ने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने का निर्णय लिया। उन्होंने जनता से ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया, जिसे अब कुंदरा घोषणापत्र कहा जाता है। इससे बहुत से लोग विद्रोह में शामिल हो गए, और ब्रिटिशों को इसे रोकने के लिए बड़ी सेना का उपयोग करना पड़ा। त्रावणकोर के महाराजा, स्थानीय नेता, ने विद्रोह का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया और ब्रिटिश पक्ष में शामिल हो गए। वेलू थांपी, ब्रिटिशों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए, आत्महत्या करने का निर्णय लिया। इसके बाद, विद्रोह धीरे-धीरे समाप्त हो गया और स्थिति सामान्य हो गई।
- ईस्ट इंडिया कंपनी और त्रावणकोर ने 1805 में एक साथ काम करने पर सहमति जताई, लेकिन कंपनी ने कड़े नियम लागू किए जिससे त्रावणकोर के लोग बहुत असंतुष्ट हो गए।
- त्रावणकोर पैसे का भुगतान नहीं कर सका और वहां के ब्रिटिश अधिकारी उनके मामलों में हस्तक्षेप करने लगे।
- इन सभी समस्याओं के कारण त्रावणकोर के नेता वेलू थांपी ने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने का निर्णय लिया।
- उन्होंने जनता से ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया, जिसे अब कुंदरा घोषणापत्र कहा जाता है।
- इससे बहुत से लोग विद्रोह में शामिल हो गए, और ब्रिटिशों को इसे रोकने के लिए बड़ी सेना का उपयोग करना पड़ा।
- त्रावणकोर के महाराजा ने विद्रोह का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया और ब्रिटिश पक्ष में शामिल हो गए। वेलू थांपी, ब्रिटिशों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए, आत्महत्या करने का निर्णय लिया।
- इसके बाद, विद्रोह धीरे-धीरे समाप्त हो गया और स्थिति सामान्य हो गई।
बुंदेलखंड प्रांत को ब्रिटिशों ने द्वितीय एंग्लो-माराठा युद्ध (1803-05) के दौरान जीत लिया और इसे बंगाल की प्रेसीडेंसी में रखा। बुंदेला chiefs ने नए ब्रिटिश शासन का विरोध किया, लगभग 150 किलों से लड़ाई की। लक्ष्मण दवा, अजयरगढ़ के किले के कमांडर ने पहले प्रमुख प्रतिरोध का प्रदर्शन किया। उन्हें 1808 तक किला बनाए रखने की अनुमति दी गई लेकिन उन्होंने फरवरी 1809 में आत्मसमर्पण कर दिया।
- बुंदेलखंड प्रांत को ब्रिटिशों ने द्वितीय एंग्लो-माराठा युद्ध (1803-05) के दौरान जीत लिया और इसे बंगाल की प्रेसीडेंसी में रखा।
- बुंदेला chiefs ने नए ब्रिटिश शासन का विरोध किया, लगभग 150 किलों से लड़ाई की।
- कालनजर के किलेदार, दरिया सिंह, ने जनवरी 1812 में प्रतिरोध किया, लेकिन विद्रोह को दबा दिया गया।
- गोपाल सिंह, एक सैन्य साहसी, जिसने अपने चाचा के खिलाफ विवाद में ब्रिटिशों का समर्थन प्राप्त किया, ने गंभीर खतरा पेश किया।
- उन्होंने चार साल तक ब्रिटिश बलों से बचने में सफलता पाई।
जब कंपनी ने गंजाम का अधिग्रहण किया, नारायण देव पार्लाकिमेडी के राजा थे जिनकी प्रतिरोध ने ब्रिटिशों को कर्नल पीच के तहत एक सेना भेजने के लिए मजबूर किया।
- जब कंपनी ने गंजाम का अधिग्रहण किया, नारायण देव पार्लाकिमेडी के राजा थे जिनकी प्रतिरोध ने ब्रिटिशों को कर्नल पीच के तहत एक सेना भेजने के लिए मजबूर किया।
1816 में ब्रिटिशों और कच्छ के महाराजा भारामल II के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत शक्ति सिंहासन में निहित थी। ब्रिटिशों ने कच्छ के आंतरिक झगड़ों में हस्तक्षेप किया और 1819 में राजा भारामल II ने ब्रिटिशों को अपने क्षेत्र से हटाने के दृढ़ इरादे से अरब और अफ्रीकियों की सेना जुटाई।
- 1816 में ब्रिटिशों और कच्छ के महाराजा भारामल II के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत शक्ति सिंहासन में निहित थी।
- ब्रिटिशों ने कच्छ के आंतरिक झगड़ों में हस्तक्षेप किया और 1819 में राजा भारामल II ने ब्रिटिशों को अपने क्षेत्र से हटाने के दृढ़ इरादे से अरब और अफ्रीकियों की सेना जुटाई।
उत्थान का तात्कालिक कारण पुलिस कर को लागू करना था, जिससे नागरिकों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। कई सशस्त्र मुसलमानों ने पिलिभीत, शाहजहांपुर और रामपुर से धर्म और मुफ्ती की रक्षा के लिए विद्रोह किया।
- उत्थान का तात्कालिक कारण पुलिस कर को लागू करना था, जिससे नागरिकों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ।
- कई सशस्त्र मुसलमानों ने पिलिभीत, शाहजहांपुर और रामपुर से धर्म और मुफ्ती की रक्षा के लिए विद्रोह किया।
राजस्व में लगातार वृद्धि के कारण, दयराम लगातार बकाया चुकाने में असफल रहा और यहां तक कि सरकारी भगोड़ों को आश्रय देकर कई शत्रुतापूर्ण कृत्यों का निर्माण किया। इसलिए, कंपनी ने फरवरी 1817 में हाथरस पर बड़े पैमाने पर हमला किया।
- राजस्व में लगातार वृद्धि के कारण, दयराम लगातार बकाया चुकाने में असफल रहा और यहां तक कि सरकारी भगोड़ों को आश्रय देकर कई शत्रुतापूर्ण कृत्यों का निर्माण किया।
- इसलिए, कंपनी ने फरवरी 1817 में हाथरस पर बड़े पैमाने पर हमला किया।
विदेशी शासन के खिलाफ असंतोष और ब्रिटिश सरकार द्वारा समर्थित गायकवाड़ के व्यक्तिगत करों ने ओखा मंडल के वाघेरा chiefs को सशस्त्र संघर्ष करने के लिए मजबूर किया। वाघेरों ने 1818-19 के दौरान ब्रिटिश क्षेत्र में दखल दिया। नवंबर 1820 में एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए।
- विदेशी शासन के खिलाफ असंतोष और ब्रिटिश सरकार द्वारा समर्थित गायकवाड़ के व्यक्तिगत करों ने ओखा मंडल के वाघेरा chiefs को सशस्त्र संघर्ष करने के लिए मजबूर किया।
- वाघेरों ने 1818-19 के दौरान ब्रिटिश क्षेत्र में दखल दिया। नवंबर 1820 में एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए।
प्रथम बर्मा युद्ध (1824-26) के बाद, ब्रिटिशों ने अहेम के क्षेत्रों को कंपनी के डोमिनियन में शामिल करने के प्रयास किए। यह 1828 में गोंधर कोंवर, एक अहोम राजकुमार, और उनके साथियों के नेतृत्व में विद्रोह का कारण बना। अंततः, कंपनी ने समर्पण की नीति अपनाई और ऊपरी असम को सौंप दिया।
- यह 1828 में गोंधर कोंवर, एक अहोम राजकुमार, और उनके साथियों के नेतृत्व में विद्रोह का कारण बना।
- अंततः, कंपनी ने समर्पण की नीति अपनाई और ऊपरी असम को सौंप दिया।
गड़करी, एक पारंपरिक सैन्य वर्ग, मराठा किलों में तैनात थे। 1844 के बाद कोल्हापुर राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन ने गड़करी गार्द को भंग कर दिया। इससे गड़करियों में बेरोजगारी हुई। बेरोजगारी का सामना करते हुए गड़करियों ने विद्रोह किया। उन्होंने सामंगढ़ और भूदरगढ़ किलों पर कब्जा कर लिया। सावंतवाड़ी क्षेत्रों में असंतोष पनप रहा था। ब्रिटिश अधिकारियों ने असंतोष के जवाब में क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू किए।
- 1844 के बाद कोल्हापुर राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन ने गड़करी गार्द को भंग कर दिया।
- इससे गड़करियों में बेरोजगारी हुई।
- बेरोजगारी का सामना करते हुए गड़करियों ने विद्रोह किया।
- उन्होंने सामंगढ़ और भूदरगढ़ किलों पर कब्जा कर लिया।
- सावंतवाड़ी क्षेत्रों में असंतोष पनप रहा था।
- ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1830, 1836 और 1838 में पिछले विद्रोह हुए।
वहाबी आंदोलन मूल रूप से एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसकी स्थापना सैयद अहमद ने राय बरेली में की थी, जो सऊदी अरब के अब्दुल वहाब (1703-87) और दिल्ली के शाह वलीउल्लाह की शिक्षाओं से प्रेरित था। सिख शासक की पराजय और 1849 में पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी के डोमिनियन में शामिल करने के बाद, भारत में अंग्रेजी शासन वहाबी हमलों का एकमात्र लक्ष्य बन गया। वहाबियों ने ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1860 के दशक में ब्रिटिशों द्वारा वहाबी आधार पर कई सैन्य अभियान और विभिन्न राजद्रोह के मामलों ने वहाबी प्रतिरोध को कमजोर कर दिया।
- वहाबी आंदोलन मूल रूप से एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसकी स्थापना सैयद अहमद ने राय बरेली में की थी, जो सऊदी अरब के अब्दुल वहाब (1703-87) और दिल्ली के शाह वलीउल्लाह की शिक्षाओं से प्रेरित था।
- सिख शासक की पराजय और 1849 में पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी के डोमिनियन में शामिल करने के बाद, भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजी शासन वहाबी हमलों का एकमात्र लक्ष्य बन गया।
- वहाबियों ने ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1860 के दशक में ब्रिटिशों द्वारा वहाबी आधार पर कई सैन्य अभियान और विभिन्न राजद्रोह के मामलों ने वहाबी प्रतिरोध को कमजोर कर दिया।
कुका आंदोलन की स्थापना 1840 में भगत जवाहर माई (जिन्हें सियान साहब भी कहा जाता है) ने पश्चिमी पंजाब में की। इसके मूल सिद्धांत जाति और सिखों के बीच समान भेदभाव के उन्मूलन, मांस, शराब और नशीली दवाओं के सेवन को हतोत्साहित करने, अंतरजातीय विवाह की अनुमति, विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं को अलगाव से बाहर आने के लिए प्रोत्साहित करना थे। राजनीतिक दृष्टिकोण से, कुका ब्रिटिशों को हटाना और पंजाब में सिख शासन को बहाल करना चाहते थे; उन्होंने हाथ से बुने हुए कपड़े पहनने और अंग्रेजी कानूनों और शिक्षा तथा उत्पादों का बहिष्कार करने की वकालत की। इस प्रकार, कुका द्वारा स्वदेशी और असहयोग के विचारों का प्रचार किया गया।
- इसके मूल सिद्धांत जाति और सिखों के बीच समान भेदभाव के उन्मूलन, मांस, शराब और नशीली दवाओं के सेवन को हतोत्साहित करने, अंतरजातीय विवाह की अनुमति, विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं को अलगाव से बाहर आने के लिए प्रोत्साहित करना थे।
- राजनीतिक दृष्टिकोण से, कुका ब्रिटिशों को हटाना और पंजाब में सिख शासन को बहाल करना चाहते थे; उन्होंने हाथ से बुने हुए कपड़े पहनने और अंग्रेजी कानूनों और शिक्षा तथा उत्पादों का बहिष्कार करने की वकालत की।
किसान विद्रोह, भूमि से बेदखली, भूमि के किराए में वृद्धि, और साहूकारों की लालची नीतियों के खिलाफ विरोध थे, और उनका लक्ष्य किसान के लिए कब्जे के अधिकार सहित अन्य चीजें थीं। ये विद्रोह और किसान स्वयं के विद्रोह थे, हालांकि कई मामलों में स्थानीय नेताओं द्वारा नेतृत्व किया गया।
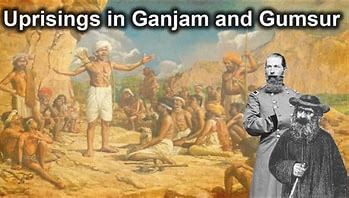



- मीर निठार अली (1782-1831) या तितु मीर ने पश्चिम बंगाल के मुस्लिम किसानों को जागृत किया कि वे मुख्यतः हिंदू जमींदारों के खिलाफ उठ खड़े हों, जिन्होंने फ़राज़ियों पर दाढ़ी कर लगाने का कर लगाया और ब्रिटिश नील उत्पादकों के खिलाफ भी।
- इन्हें अक्सर ब्रिटिश के खिलाफ पहले सशस्त्र किसान विद्रोह के रूप में माना जाता है, जो बाद में वहाबी आंदोलन में विलीन हो गया।
- पागल पंथी, जो मुख्यतः मymensingh जिले (पूर्व में बंगाल) के हाजोंग और गारो जनजातियों से मिलकर बना एक अर्ध-धार्मिक समूह है, की स्थापना कराम शाह ने की।
- जनजातीय किसान जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ संगठित हुए। 1825 से 1835 के बीच, पागल पंथियों ने एक निश्चित सीमा से अधिक किराया देने से इनकार कर दिया।
- फराज़ी एक मुस्लिम संप्रदाय के अनुयायी थे, जिसकी स्थापना हाजी शरीयत-अल्लाह ने पूर्वी बंगाल के फरीदपुर में की थी। वे धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलावों का समर्थन करते थे।
- शरीयत-अल्लाह ने अपने अनुयायियों को संगठित किया ताकि वे बंगाल से अंग्रेज़ों को निकाल सकें। इस संप्रदाय ने जमींदारों के खिलाफ किसानों के कारण का भी समर्थन किया।
- राजस्व मांग में वृद्धि और खेत के आकार में कमी, साथ ही अधिकारियों के अत्याचार ने मोपलाहों के बीच व्यापक किसान असंतोष पैदा किया। 1836 से 1854 के बीच बाईस विद्रोह हुए।
- किसान कई स्थानों पर स्थानीय सामंती नेताओं के साथ मिलकर विदेशी शासन के खिलाफ लड़े। विद्रोह के बाद, किसानों की स्थिति बिगड़ गई क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जमींदार वर्ग का समर्थन प्राप्त करने का निर्णय लिया, जबकि किसानों को नजरअंदाज किया।
- भूमि या जंगलों द्वारा उत्पन्न मुख्य जनजातीय विद्रोह। ब्रिटिश भूमि समझौतों ने संयुक्त स्वामित्व परंपरा को प्रभावित किया।
- कंपनी सरकार द्वारा कृषि को व्यवस्थित रूप में विस्तारित करने के कारण जनजातियों ने अपनी भूमि खो दी, और जंगलों में स्थानांतरित कृषि पर अंकुश लगा, जिससे जनजातियों की समस्याएं बढ़ गईं।
- पुलिस, व्यापारियों और पैसे lenders द्वारा शोषण; कुछ सामान्य कानूनों को भी उनकी intrusive प्रकृति के कारण नफरत की गई।
- जनजातीय पहचान या जातीय संबंध इन समूहों द्वारा दिखाई गई एकता के पीछे थे। “विदेशी सरकार” द्वारा कानूनों के लागू करने के खिलाफ असंतोष था, जो जनजातियों के पारंपरिक सामाजिक-आर्थिक ढांचे को नष्ट करने का प्रयास माना जाता था।
- कई विद्रोह ऐसे मसीहा जैसे व्यक्तियों द्वारा नेतृत्व किए गए जिन्होंने अपने लोगों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। जनजातीय विद्रोहों की शुरुआत से ही पराजय निश्चित थी, क्योंकि उनके पास पुराने हथियार थे।
- ब्रिटिश विस्तार ने राजमहल पहाड़ियों के मार्शल पहाड़ियों द्वारा विद्रोह को जन्म दिया। ब्रिटिशों को अपने क्षेत्र को डमनीकोल क्षेत्र घोषित करके शांति लाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- महामारी से बढ़ी भूमि राजस्व मांग और आर्थिक संकट ने चुआर आदिवासी लोगों को जंगल महल के मिदनापुर जिले और बांकुड़ा जिले (बंगाल) में हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया।
- विद्रोह 1766 से 1772 तक चला और फिर, 1795 से 1816 के बीच फिर से उभरा। चुआर प्रमुख रूप से मानभूम और बराबहुम में, विशेषकर बाराबहुम और घाटशिला के बीच की पहाड़ियों में सक्रिय थे।
- कोल अन्य जनजातियों के साथ छोटा नागपुर के निवासी हैं। इसमें रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पालामऊ, और मानभूम के पश्चिमी भाग शामिल हैं।
- 1831 में कोल प्रमुखों से भूमि के बड़े पैमाने पर हस्तांतरण के साथ समस्याएं शुरू हुईं। ब्रिटिश न्यायिक और राजस्व नीतियों ने कोल की पारंपरिक सामाजिक स्थितियों को बुरी तरह प्रभावित किया।
- पराशात के राजा ने अपने हो जनजातियों को सिंहभूम (अब झारखंड में) के कब्जे के खिलाफ विद्रोह करने के लिए संगठित किया। विद्रोह 1827 तक जारी रहा जब हो जनजातियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया।
- 1831 में, उन्होंने एक विद्रोह का आयोजन किया, जिसमें छोटा नागपुर के मुंडा भी शामिल हुए, नए कृषि राजस्व नीति और उनके क्षेत्र में बंगालियों की एंट्री के खिलाफ विरोध किया।
- किसानों पर लगातार दबाव, जो कृषि करते थे, जो राजमहल पहाड़ियों (बिहार) के मैदानों में बस गए थे, ने जमींदारों के खिलाफ संथाल विद्रोह को जन्म दिया।
- यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक आंदोलन में बदल गया। सिद्धू और कान्हू, दो भाइयों के तहत, संथालों ने कंपनी शासन के अंत की घोषणा की और भागलपुर और राजमहल के बीच के क्षेत्र को स्वायत्त घोषित किया।
- भिल जो पश्चिमी घाट में रहते थे, उत्तर और डेक्कन के बीच के पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करते थे। उन्होंने 1817-19 में कंपनी शासन के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि उन्हें अकाल, आर्थिक संकट और गलत शासन का सामना करना पड़ा।
- रामोसी, पश्चिमी घाट की पहाड़ी जनजातियाँ, ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश प्रशासन के पैटर्न से समझौता नहीं कर पाईं। उन्होंने 1822 में चित्तूर सिंह के तहत विद्रोह किया और सतारा के चारों ओर लूटपाट की।
- खासी, गारो, खाम्पती, और सिंगफोस ने ब्रह्मपुत्र घाटी से अजनबियों को बाहर निकालने के लिए तिरथ सिंह के तहत संगठित किया। यह विद्रोह क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक लोकप्रिय विद्रोह में विकसित हुआ।
- असम में सिंगफो का विद्रोह 1830 की शुरुआत में तुरंत दबा दिया गया। मुखिया निरंग फिदु ने 1843 में विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें ब्रिटिश गार्द के खिलाफ हमले और कई सैनिकों की मौत हुई।
- कुछ छोटे आंदोलन थे जैसे कि मिशमी (1836 में), खाम्पती विद्रोह असम में 1839 और 1842 के बीच, और लुशाई का विद्रोह 1842 और 1844 में।
- भुगतान और पदोन्नति में भेदभाव।
- ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सिपाहियों के प्रति दुर्व्यवहार।
- दूरदराज के क्षेत्रों में लड़ाई के दौरान विदेशी सेवा भत्ते का भुगतान करने से सरकार की इनकार।
- उच्च जाति के हिंदू सिपाहियों के लॉर्ड कैनिंग के सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम (1856) के प्रति धार्मिक आपत्तियाँ।
- 1806 में, पगड़ी को चमड़े की कोकाड से बदलने के कारण वेल्लोर में एक विद्रोह हुआ।
- 1844 में, बंगाल सेना के सिपाहियों के विद्रोह का प्रकोप हुआ क्योंकि उन्हें दूर के सिंध में भेजा गया था।
- 1824 में, बैरकपुर के सिपाही विद्रोह कर उठे जब उनसे बर्मा जाने के लिए कहा गया, क्योंकि समुद्र पार करना जाति खोने का मतलब था।
- 1764 में बंगाल में सिपाहियों का विद्रोह। वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था जब सिपाहियों ने अपनी सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप के खिलाफ विरोध किया और मैसूर के शासक का ध्वज फहराया।
- 1824 में 47वीं नटिव इन्फैंट्री यूनिट के सिपाहियों का विद्रोह।
- 1825 में असम में ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह।
- 1838 में शोलापुर में एक भारतीय रेजिमेंट का विद्रोह।
- 1844, 1849, 1850, और 1852 में क्रमशः 34वीं नटिव इन्फैंट्री (N.I), 22वीं N.I., 66वीं N.I., और 37वीं N.I. के विद्रोह।
- ये विद्रोह एक बड़ी संख्या में प्रतिभागियों को आकर्षित करते थे, स्थानीयकृत होते थे और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समय पर होते थे।
- ये विद्रोह स्थानीय शिकायतों से उत्पन्न होते थे।
- नेतृत्व अर्ध-फ्यूडल चरित्र का था, पीछे की ओर देखने वाला, पारंपरिक दृष्टिकोण का था और उनकी प्रतिरोध ने मौजूदा सामाजिक व्यवस्था के लिए वैकल्पिक समाधान नहीं प्रस्तुत किए।
- यदि इनमें से कई विद्रोह एक-दूसरे के समान लगते थे, तो यह इसलिए था क्योंकि वे विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा रखते थे, क्योंकि वे उन परिस्थितियों के खिलाफ विरोध कर रहे थे जो उनके लिए सामान्य थीं।
- ये विद्रोह सदियों पुरानी रूप और वैचारिक/संस्कृतिक सामग्री के थे।
- जो लोग इतने असहयोगी या जिद्दी नहीं थे, उन्हें अधिकारियों द्वारा रियायतों के माध्यम से शांत किया गया।
- इन विद्रोहों में लड़ाकों द्वारा इस्तेमाल की गई विधियाँ और हथियार उनके विरोधियों द्वारा उपयोग की गई रणनीतियों, धोखे और चालाकी की तुलना में प्रायः पुरानी थीं।
जैसा कि आप स्वतंत्रता की पहली लड़ाई की ओर ले जाने वाले छोटे घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। अगले EduRev दस्तावेज़ में आप प्रमुख घटनाओं और 1857 के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जिसे भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है और जो राजसी राज्यों की एकता के पहले संकेतों में से एक है, जिसका सामान्य दुश्मन अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी है।
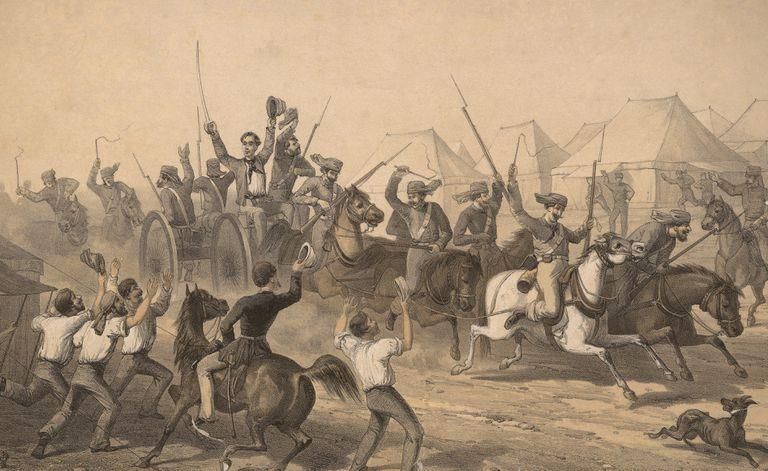

|
198 videos|620 docs|193 tests
|





















