स्पेक्ट्रम सारांश: साइमोन आयोग और नेहरू रिपोर्ट | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download
भारतीय वैधानिक आयोग की नियुक्ति
साइमन आयोग, जिसे औपचारिक रूप से भारतीय वैधानिक आयोग के नाम से जाना जाता है, को 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में शासन की प्रगति का आकलन करने के लिए स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष, सर जॉन साइमन के नाम पर रखे गए इस सात-सदस्यीय आयोग ने इस तथ्य के लिए ध्यान आकर्षित किया कि यह पूरी तरह से श्वेत व्यक्तियों से बना था।

- भारत सरकार अधिनियम, 1919 का पृष्ठभूमि: 1919 में भारत सरकार अधिनियम में एक प्रावधान शामिल किया गया था जो दस वर्षों बाद आयोग की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता था। यह आयोग पिछले दशक के दौरान भारत में शासन की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए स्थापित किया गया था। इस प्रावधान को शामिल करके, अधिनियम का उद्देश्य शासन संरचना की प्रभावशीलता की आवधिक और प्रणालीबद्ध समीक्षा सुनिश्चित करना था, ताकि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर समायोजन और सुधार किए जा सकें।
- साइमन आयोग की स्थापना: 1927 में एक पूरी तरह से श्वेत, सात-सदस्यीय आयोग जिसे भारतीय वैधानिक आयोग कहा गया, का गठन किया गया। इसे इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम से लोकप्रियता मिली। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या भारत अतिरिक्त संवैधानिक सुधारों के लिए तैयार है और यदि हां, तो इन सुधारों के लिए विशेष दिशा-निर्देश प्रदान करना।
- प्रारंभिक आयोग नियुक्ति (1927): इस समय, ब्रिटिश राजनीतिक परिदृश्य में कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी, और वे लेबर पार्टी के अगले चुनाव में जीतने की संभावना से चिंतित थे। "कीमती उपनिवेश" की परिभाषा भारत के लिए थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान हिस्सा था। डर था कि यदि लेबर पार्टी सत्ता में आई, तो वे भारत के संवैधानिक भविष्य के निर्णय लेने को "अविवेकपूर्ण" तरीके से संभाल सकते हैं। इसलिए, कंजर्वेटिवों ने यह सुनिश्चित करने के लिए साइमन आयोग के गठन को तेजी से आगे बढ़ाया कि यह महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामला उनके शासन के अधीन निपटाया जाए।
- मध्य-1920 के संसदीय रिपोर्ट और जांच: ली आयोग ने यह देखने की कोशिश की कि भारत में ब्रिटिश अधिकारियों की संख्या क्यों कम है। ब्रिटिश अधिकारी विभिन्न शासन के पहलुओं के प्रभारी थे, और इस कमी के बारे में चिंता थी। वे यह जानना चाहते थे कि यह क्यों हो रहा है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। मडिमन आयोग ने द्वैध प्रणाली में एक समस्या को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। द्वैध का अर्थ है दो प्राधिकरण या शक्ति केंद्र होना। भारत में, यह भारतीय अधिकारियों और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच शक्तियों के विभाजन के बारे में था। आयोग का उद्देश्य यह पता लगाना था कि इस प्रणाली में निर्णय लेने में क्यों गतिरोध या ऐसी स्थिति थी जहां निर्णय आसानी से नहीं लिए जा सकते थे।
- साइमन आयोग की नियुक्ति के कारण: 1919 का अधिनियम, जिसे भारत को संचालन के लिए बनाया गया था, स्थिरता के मुद्दों का सामना कर रहा था, जिससे ब्रिटिश सरकार को करीब से देखने की आवश्यकता महसूस हुई। लॉर्ड बिर्केनहेड, जो भारत के लिए कंजर्वेटिव सचिव थे, ने भारतीयों की क्षमता पर सवाल उठाया कि वे व्यापक राजनीतिक समर्थन के साथ सुधार के लिए एक प्रभावी योजना तैयार कर सकें। मौजूदा नियमों की कमियों को देखते हुए और अस्थिरता के डर से, ब्रिटिश सरकार ने 1919 के अधिनियम के कार्यों की पूरी तरह से जांच करने की आवश्यकता महसूस की। यह मूल्यांकन कमियों को संबोधित करने और भारत में शासन की अधिक प्रभावीता के लिए सुधार करने की इच्छा से प्रेरित था।
- लॉर्ड बिर्केनहेड की भूमिका: साइमन आयोग की नियुक्ति का जिम्मा लॉर्ड बिर्केनहेड के पास था, जो भारत के लिए कंजर्वेटिव सचिव थे। लॉर्ड बिर्केनहेड का यह मानना था कि भारतीय एक मजबूत और व्यापक योजना तैयार करने में सक्षम नहीं थे जो संवैधानिक सुधारों के लिए व्यापक समर्थन प्राप्त करे। उनके अनुसार, भारतीय लोग देश के शासन के मौलिक नियमों को बदलने के लिए एक ठोस और व्यापक रूप से स्वीकृत प्रस्ताव नहीं बना सकते थे। इस विश्वास के कारण, लॉर्ड बिर्केनहेड ने स्वयं साइमन आयोग की नियुक्ति की।
भारतीय प्रतिक्रिया
भारतीय लोग साइमोन आयोग के प्रति बहुत परेशान थे, और उनकी प्रतिक्रिया त्वरित और एकजुट थी। उनके गुस्से का मुख्य कारण यह था कि आयोग में कोई भारतीय शामिल नहीं था और यह धारणा कि विदेशी लोग यह तय करेंगे कि क्या भारत अपने आप को शासन करने के लिए तैयार है। इससे भारतीयों को ऐसा महसूस हुआ कि उनके भविष्य का निर्णय लेने का अधिकार, जिसे स्वायत्तता कहा जाता है, को नजरअंदाज किया जा रहा है।
(क) कांग्रेस की प्रतिक्रिया:
M.A. अंसारी
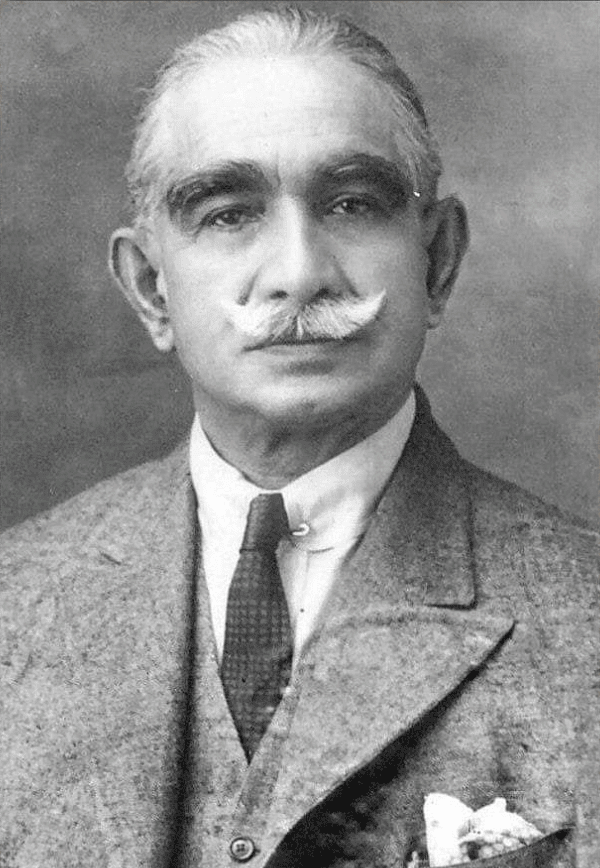
- दिसंबर 1927 में, M.A. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में एक कांग्रेस बैठक के दौरान, साइमोन आयोग के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उपस्थित लोगों, जिनमें जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता शामिल थे, ने साइमोन आयोग का पूरी तरह से बहिष्कार करने का निर्णय लिया, हर कदम पर और हर संभव तरीके से।
- इसका मतलब था कि वे आयोग के साथ किसी भी रूप में सहयोग या संलग्न होने से इनकार करेंगे। इसके अलावा, नेहरू ने इस सत्र के दौरान एक प्रस्ताव पेश करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रस्ताव में यह घोषित किया गया कि कांग्रेस का अंतिम या अंतिम लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है।
(ख) अन्य समूह:
- साइमोन आयोग के बहिष्कार में कांग्रेस का समर्थन करने वालों में हिन्दू महासभा के उदार सदस्य और जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का बड़ा धड़ा शामिल था। 1927 में, मुस्लिम लीग ने साइमोन आयोग पर अपने रुख पर चर्चा करने के लिए दो अलग-अलग सत्र आयोजित किए।
- जिन्ना के नेतृत्व में कोलकाता में, आयोग का विरोध करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, लाहौर में मोहम्मद शफी के तहत एक और सत्र में सरकार का समर्थन किया गया। दूसरी ओर, कुछ समूहों ने बहिष्कार में शामिल न होने का निर्णय लिया। पंजाब में यूनियनिस्ट और भारत के दक्षिणी भाग में न्याय पार्टी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने साइमोन आयोग का बहिष्कार करने का विकल्प नहीं चुना।
(ग) सार्वजनिक प्रतिक्रिया:
जब साइमोन कमीशन 3 फरवरी, 1928 को मुंबई आया, तो भारत में जन प्रतिक्रिया मजबूत और व्यापक थी। उस दिन, एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल (hartal) आयोजित की गई, जिसमें बड़े पैमाने पर रैलियाँ शामिल थीं।
- जहाँ भी कमीशन गया, वहाँ काले झंडों के साथ प्रदर्शन, हड़तालें और 'साइमोन गो बैक' के नारे लगाए गए। यह आंदोलन एक नई पीढ़ी के युवाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए उल्लेखनीय था, जो राजनीतिक गतिविधियों में उनकी पहली संलग्नता को दर्शाता है।
- नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस युवा और छात्र सक्रियता की लहर के दौरान प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में उभरे।
- उन्होंने व्यापक रूप से यात्रा की, बड़े सम्मेलनों को संबोधित किया, और बैठकों की अध्यक्षता की, जिससे वे साइमोन कमीशन के खिलाफ विरोध में प्रभावशाली आवाज बन गए।
- युवाओं की भागीदारी में वृद्धि ने नए कट्टरपंथी विचारों के लिए एक मंच भी तैयार किया। इससे पंजाब नौजवान भारत सभा, श्रमिकों और किसानों की पार्टियों, और कर्नाटका में हिंदुस्तानी सेवा दल जैसी समूहों का गठन हुआ, जो बदलते और विकसित होते राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाते हैं।
(d) पुलिस दमन:

- पुलिस ने विरोध कर रहे लोगों के प्रति बहुत कठोरता दिखाई। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं बख्शा और बलात लाठियाँ (batons) चलाईं।
- लखनऊ में, जवाहरलाल नेहरू और जी. बी. पंत पर शारीरिक हमला किया गया। अक्टूबर 1928 में, लाला लाजपत राय को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान छाती में गंभीर चोटें आईं, जो इतनी गंभीर थीं कि वे 17 नवंबर 1928 को चल बसे।
- इन प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई बहुत हिंसक थी और इसके गंभीर परिणाम हुए, जिसमें प्रमुख नेताओं को चोटें आईं और यहाँ तक कि कुछ की मृत्यु भी हुई।
साइमन आयोग की नियुक्ति का राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव
साइमन आयोग की नियुक्ति का राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव
(i) साइमन आयोग की घोषणा ने महत्वपूर्ण परिवर्तनों की मांग को जन्म दिया, न केवल पूर्ण स्वतंत्रता की खोज में, बल्कि समाजवादी विचारों से प्रेरित प्रमुख सामाजिक और आर्थिक सुधारों की भी मांग की गई। कांग्रेस के लिए, जिसके पास उस समय कोई विशिष्ट योजना नहीं थी, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया जिसने लोगों को सामूहिक कार्रवाई के लिए एकजुट किया।
(ii) जब लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीय राजनीतिज्ञों को एक एकीकृत संविधान तैयार करने की चुनौती दी, तो विभिन्न राजनीतिक समूहों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। इसने उस समय भारतीयों के बीच एकता की उम्मीद जगाई। सरल शब्दों में, यह भारतीय नेताओं के लिए एक अवसर था कि वे एक ऐसा संविधान बनाने के लिए मिलकर काम करें जिस पर सभी सहमत हो सकें।
साइमन आयोग की सिफारिशें
- साइमन आयोग की सिफारिशें (1930): डायरकी समाप्त करने और प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार स्थापित करने का प्रस्ताव। प्रांतों के लिए स्वायत्तता की सिफारिश की, जिसमें प्रांतीय विधायी परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई। सुझाव दिया गया कि गवर्नर को आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक मामलों के लिए विवेकाधीन शक्तियाँ होनी चाहिए, ताकि समुदायों की रक्षा की जा सके। केंद्र में संसदीय जिम्मेदारी को अस्वीकार किया गया, और गवर्नर-जनरल को कैबिनेट के सदस्यों को नियुक्त करने की पूरी शक्ति दी गई। भारत सरकार की उच्च न्यायालय पर पूरी नियंत्रण की सिफारिश की गई।
- चुनाव और मतदाता सिफारिशें: तनाव कम होने तक अलग-अलग सामुदायिक मतदाता सूची (हिंदुओं और मुसलमानों के लिए) बनाए रखने की सिफारिश की। सार्वभौमिक मताधिकार के विचार को अस्वीकार किया गया; यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि सभी को मतदान का अधिकार हो।
- संघवाद और परामर्श परिषद: संघवाद के विचार को स्वीकार किया लेकिन इसे भविष्य के लिए सुझाया। ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक महान भारत की परामर्श परिषद के निर्माण का प्रस्ताव दिया।
- प्रांतीय प्रतिनिधित्व और पृथक्करण: उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान के लिए स्थानीय विधायिकाएँ सुझाई गईं, जिसमें केंद्र में प्रतिनिधित्व हो। प्राकृतिक विछेदन के कारण सिंध को बंबई और बर्मा को भारत से अलग करने की सिफारिश की गई।
- भारतीय सेना और सिफारिशों की प्रासंगिकता: भारतीय सेना का भारतीयकरण करने का प्रस्ताव दिया गया, जबकि भारत को पूर्ण रूप से सुसज्जित होने तक ब्रिटिश बलों को बनाए रखने की बात कही गई। जब रिपोर्ट जारी हुई, तब घटनाएँ इसकी महत्वता को पार कर गई थीं, जिससे इसकी सिफारिशें कम प्रासंगिक हो गईं।
नेहरू रिपोर्ट
चुनौती और प्रतिक्रिया: लॉर्ड बिर्केनहेड ने भारतीय राजनीतिज्ञों को एक संविधान बनाने की चुनौती दी, जिससे फरवरी 1928 में सभी दलों की सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- उपसमिति का गठन: सभी दलों की सम्मेलन ने एक उपसमिति का नियुक्त किया, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने संविधान का मसौदा तैयार करने के प्रयास का नेतृत्व किया। यह भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि यह भारतीयों द्वारा देश के लिए संविधानात्मक ढांचे को बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था।
- समिति के सदस्य: समिति में तेज बहादुर सप्रू, सुभाष बोस, एम.एस. अने, मंगल सिंह, अली इमाम, शुआब कुरैशी, और जी.आर. प्रधान जैसे प्रभावशाली सदस्य शामिल थे। ये व्यक्तियों विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे, जो विचारों की विविधता में योगदान देते थे।
- समयरेखा और अंतिमकरण: समिति ने संविधान के मसौदे पर मेहनत की और अगस्त 1928 तक रिपोर्ट को सफलतापूर्वक अंतिम रूप दिया। यह त्वरित समयरेखा भारतीय नेताओं की संविधान संबंधी मुद्दों को हल करने की तत्परता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- सिफारिशें: नेहरू समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशें अधिकांशतः सर्वसम्मत थीं, जो प्रस्तावित संविधानात्मक ढांचे पर सामान्य सहमति को इंगित करती हैं। हालांकि, एक महत्वपूर्ण असहमति \"डोमिनियन स्थिति\" और \"पूर्ण स्वतंत्रता\" के बीच चुनाव के आसपास केंद्रित थी।
- बहुमत का दृष्टिकोण: संविधान के आधार पर विचारों में भिन्नता के बावजूद, समिति के बहुमत ने \"डोमिनियन स्थिति\" का समर्थन किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुमत ने \"पूर्ण स्वतंत्रता\" की वकालत करने वाले अल्पसंख्यक को अपनी पसंद का लक्ष्य प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी, जो समिति के भीतर समायोजन की भावना को दर्शाता है।
मुख्य सिफारिशें:
- डोमिनियन स्थिति: नेहरू रिपोर्ट ने भारत को आत्म-शासित डोमिनियनों के समान स्थिति देने की सिफारिश की, जिसमें राजघरानों के साथ भविष्य के संघीय संबंध की कल्पना की गई। हालांकि, इस प्रस्ताव ने असहमतियों को जन्म दिया, विशेषकर युवा और अधिक उग्र वर्ग के बीच, जिसमें नेहरू जैसे व्यक्तियों ने असंतोष व्यक्त किया।
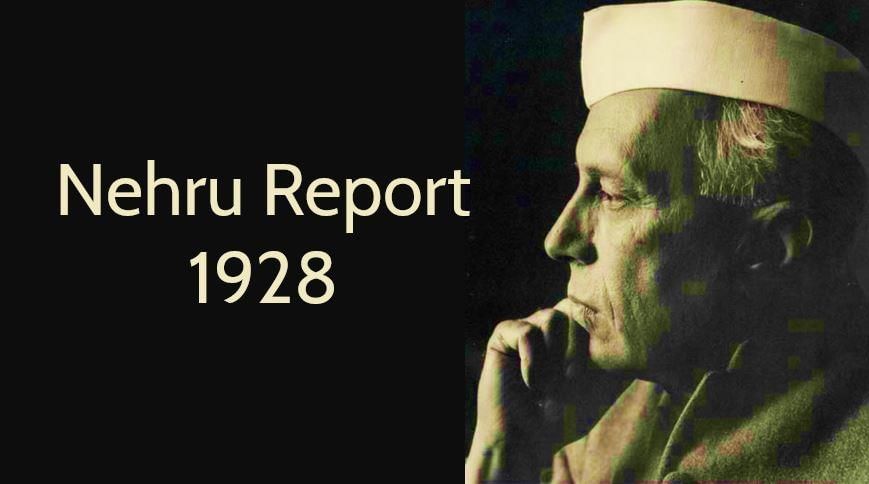
2. पृथक निर्वाचन का अस्वीकृति: मौजूदा संवैधानिक सुधारों से एक मौलिक प्रस्थान करते हुए, रिपोर्ट ने पृथक निर्वाचन को अस्वीकृत करने का प्रस्ताव रखा। इसके बजाय, इसने संयुक्त निर्वाचन का समर्थन किया जिसमें मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें होंगी, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ वे अल्पसंख्यक हैं, ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर जहाँ वे बहुसंख्यक हैं, जैसे कि पंजाब और बंगाल।
3. भाषाई प्रांत: नेहरू रिपोर्ट ने प्रशासनिक विभाजन के लिए भाषाई आधार पर प्रांतों के निर्माण का सुझाव दिया।
4. मौलिक अधिकार: उन्नीस मौलिक अधिकारों को रेखांकित करते हुए, रिपोर्ट ने महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियनों का गठन करने का अधिकार, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जैसे पहलुओं को शामिल किया।
5. जिम्मेदार सरकार: रिपोर्ट ने केंद्र और प्रांतों दोनों में जिम्मेदार सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया। इसने एक संरचित भारतीय संसद का प्रस्ताव रखा जिसमें 500 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा और 200 सदस्यीय सेनट होगी, प्रत्येक विभिन्न तरीकों से निर्वाचित और विभिन्न कार्यकालों की सेवा करेगी। केंद्र सरकार, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एक गवर्नर-जनरल के नेतृत्व में होगी लेकिन भारतीय राजस्व से भुगतान की जाएगी, संसद के प्रति जिम्मेदार केंद्रीय कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करेगी। प्रांतीय परिषदें, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, एक गवर्नर के नेतृत्व में होंगी जो प्रांतीय कार्यकारी परिषद की सलाह का पालन करेगी।
6. मुसलमानों के हितों की सुरक्षा: नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों की सांस्कृतिक और धार्मिक हितों की पूर्ण सुरक्षा पर जोर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए।
7. राज्य और धर्म का पृथक्करण: एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को उजागर करते हुए, रिपोर्ट ने धर्म से राज्य के पूर्ण पृथक्करण की मांग की, जो एक धर्मनिरपेक्ष सरकार की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
मुस्लिम और हिंदू साम्प्रदायिक प्रतिक्रियाएँ
मुस्लिम और हिंदू साम्प्रदायिक प्रतिक्रियाएँ
1. संविधान निर्माण में साम्प्रदायिक भिन्नताएँ: जब राजनीतिक नेताओं ने उत्साहपूर्वक भारत के लिए एक संविधान ढाँचा तैयार करना शुरू किया, तब साम्प्रदायिक भिन्नताएँ उभरकर सामने आईं, विशेष रूप से नेहरू रिपोर्ट में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के संबंध में।
2. मुस्लिम लीग के दिल्ली प्रस्ताव: दिसंबर 1927 में, मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम लीग सत्र के दौरान दिल्ली में एकत्र होकर चार प्रस्ताव तैयार किए, जिन्हें 'दिल्ली प्रस्ताव' के नाम से जाना जाता है। ये थे: (i) मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों के साथ पृथक निर्वाचनों की जगह संयुक्त निर्वाचनों का प्रावधान; (ii) केंद्रीय विधायी सभा में मुसलमानों के लिए एक-तिहाई प्रतिनिधित्व; (iii) पंजाब और बंगाल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुसार; (iv) तीन नए मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन—सिन्ध, बलूचिस्तान, और उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत।
3. हिंदू महासभा की मांगें: हिंदू महासभा ने नए मुस्लिम बहुल प्रांतों के निर्माण और विधायिकाओं में मुसलमानों के लिए आरक्षण का कड़ा विरोध किया। उन्होंने एक सख्त एकात्मक संरचना पर जोर दिया, जिससे स्थिति और जटिल हो गई।
4. समझौते: सभी दलों के सम्मेलन में चर्चा के दौरान, मुस्लिम लीग ने केंद्रीय विधायिका और मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों की मांग को बनाए रखा। यह नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाले नेताओं जैसे मोतीलाल नेहरू के लिए एक दुविधा पैदा कर रहा था। चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ रियायतें दी गईं, जिनमें शामिल हैं: (i) हर जगह संयुक्त निर्वाचनों का प्रस्ताव, लेकिन आरक्षण केवल वहाँ जहां मुसलमान अल्पसंख्यक थे; (ii) सिन्ध को बंबई से तभी अलग किया जाएगा जब डोमिनियन स्थिति प्रदान की जाएगी और सिन्ध में हिंदू अल्पसंख्यक को दिए गए भार के अनुसार; (iii) राजनीतिक ढाँचा मुख्यतः एकात्मक प्रस्तावित किया गया, क्योंकि शेष शक्तियाँ केंद्र के पास थीं।
ये समझौते हिंदू और मुस्लिम समुदायों के हितों के बीच संतुलन बनाने के लिए किए गए थे।
जिन्ना द्वारा प्रस्तावित संशोधन
- दिसंबर 1928 में कोलकाता में आयोजित ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में, जिन्ना ने मुस्लिम लीग की ओर से नेहरू रिपोर्ट में तीन संशोधनों का प्रस्ताव रखा: (i) केंद्रीय विधायिका में मुसलमानों के लिए एक-तिहाई प्रतिनिधित्व; (ii) बंगाल और पंजाब की विधायिकाओं में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें उनकी जनसंख्या के आधार पर जब तक कि सभी को मतदान का अधिकार न हो।
दुर्भाग्यवश, ये सुझाव स्वीकार नहीं किए गए।
जिन्ना के चौदह बिंदु
बाद में, मार्च 1929 में, जिन्ना ने मुस्लिम लीग की भविष्य की गतिविधियों के लिए चौदह बिंदुओं का प्रस्ताव रखा।
- एक संघीय संविधान जिसमें कुछ शक्तियाँ प्रांतों को दी जाएँ।
- निर्णय लेने में प्रांतों की स्वतंत्रता।
- भारतीय संघ का गठन करने वाले सभी राज्यों की सहमति के बिना संविधान में कोई परिवर्तन नहीं।
- प्रत्येक प्रांत में विधायिकाओं में मुसलमानों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
- सरकारी सेवाओं और स्व-शासनिक संस्थाओं में मुसलमानों के लिए उचित प्रतिनिधित्व।
- केंद्रीय विधायिका में मुसलमानों के लिए एक-तिहाई प्रतिनिधित्व।
- केंद्रीय या प्रांतीय मंत्रिमंडल में मुसलमानों के लिए एक-तिहाई प्रतिनिधित्व।
- अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए रखना।
- यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय के तीन-चौथाई सदस्य असहमत हों, तो कोई कानून या निर्णय पारित न किया जाए।
- किसी भी क्षेत्रीय परिवर्तन के दौरान पंजाब, बंगाल और NWFP में मुस्लिम बहुमत की सुरक्षा करना।
- सिंध को मुंबई से अलग करना।
- NWFP और बलूचिस्तान में संवैधानिक परिवर्तन।
- सभी समुदायों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता।
- धर्म, संस्कृति, शिक्षा, और भाषा में मुस्लिम अधिकारों की सुरक्षा।
नेहरू रिपोर्ट असंतोषजनक पाई गई
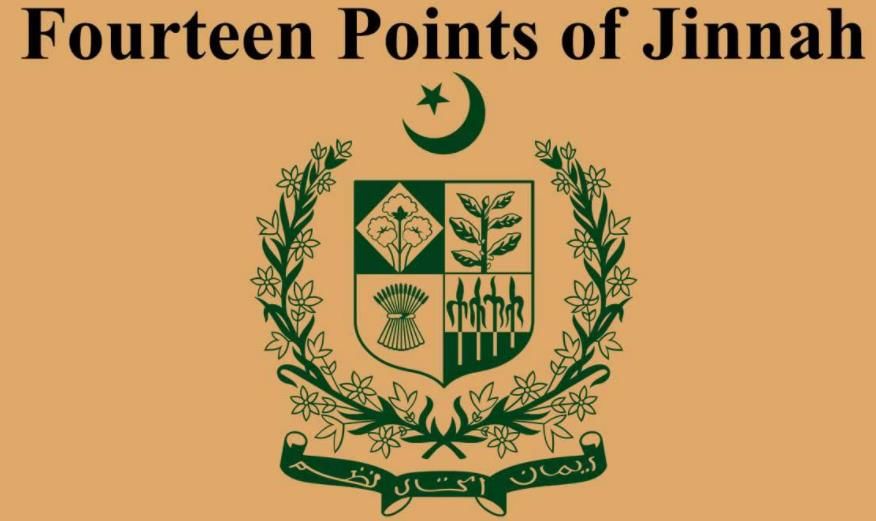
कई समूह नेहरू रिपोर्ट से असंतुष्ट थे, न केवल मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख साम्प्रदायिकताएँ, बल्कि कांग्रेस के युवा सदस्य भी, जिनका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस कर रहे थे। युवा वर्ग ने रिपोर्ट में स्वायत्तता की स्थिति के प्रस्ताव को पीछे की ओर एक कदम के रूप में देखा। सभी दलों का सम्मेलन इस विचार के प्रति उनकी आलोचना को और बढ़ा दिया। इसके जवाब में, नेहरू और सुभाष बोस ने कांग्रेस के संशोधित लक्ष्य को अस्वीकार कर दिया और मिलकर भारत के लिए स्वतंत्रता लीग का गठन किया।
|
198 videos|620 docs|193 tests
|















